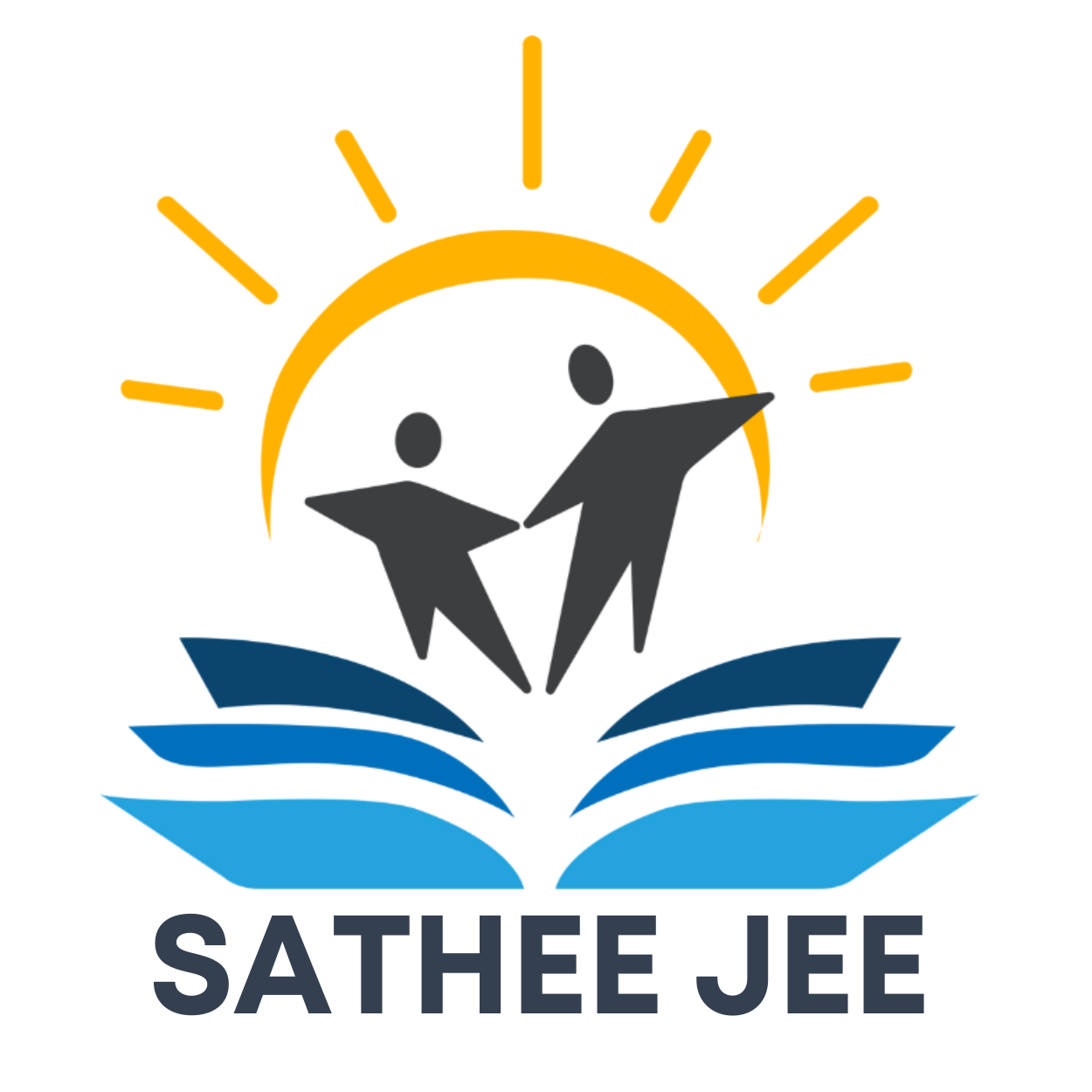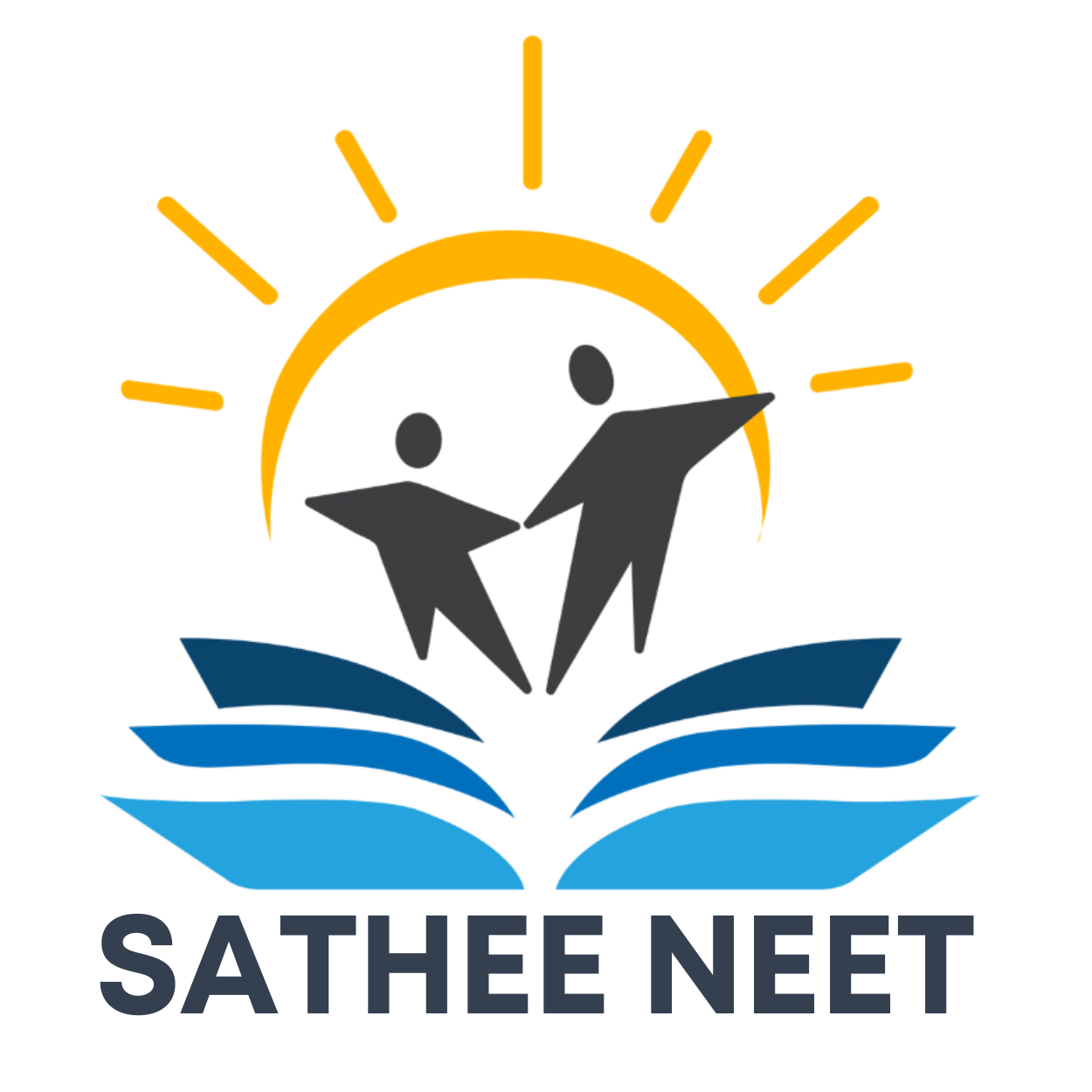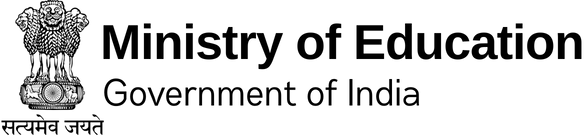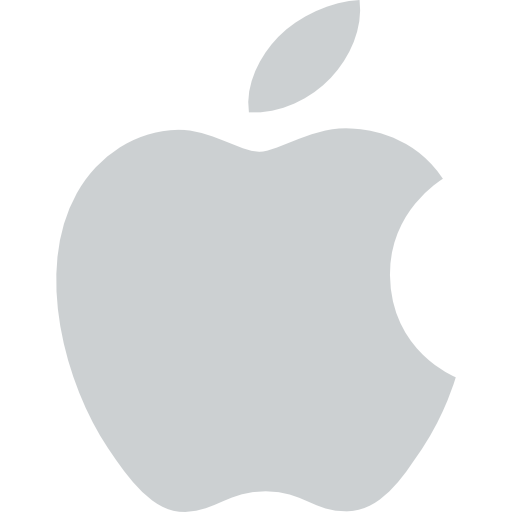अध्याय 11 ऊष्मागतिकी
11.1 भूमिका
पिछले अध्याय में हमने द्रव्यों के तापीय गुणों का अध्ययन किया। इस अध्याय में हम उन नियमों का अध्ययन करेंगे जो ऊष्मीय ऊर्जा को निर्धारित करते हैं। हम उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनमें कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होता है, तथा विलोमतः ऊष्मा भी कार्य में परिवर्तित होती है । शीत ऋतु में जब हम हथेलियों को परस्पर रगड़ते हैं तो हमें गरमी की अनुभूति होती है क्योंकि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य ऊष्मा उत्पन्न करता है । इसके विपरीत, भाप इंजन में वाष्प की ऊष्मा का उपयोग लाभप्रद कार्य को संपन्न करने में अर्थात् पिस्टन को गति देने में होता है जिसके परिणामस्वरूप रेलगाड़ी के पहिए घूतते हैं।
भौतिकी में ऊष्मा, ताप, कार्य आदि की अवधारणाओं को अधिक सावधानीपूर्वक परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ती है । ऐतिहासिक रूप से ऊष्मा की सटीक अवधारणा तक पहुँचने के लिए पर्याप्त समय लगा। आधुनिक अवधारणा के पूर्व ऊष्मा को ऐसे सूक्ष्म अदृश्य तरल के रूप में समझा गया जो किसी पदार्थ के रंध्रों में भरा रहता है । गरम व ठंडे पिंडों के पारस्परिक संपर्क में आने पर यह तरल (जिसे कैलॉरिक कहते थे) ठंडे पिंड से अपेक्षाकृत गरम पिंड में बहने लगता है ! यह बिलकुल वैसा ही है जैसा उस समय होता है जब भिन्न-भिन्न ऊँचाइयों तक पानी से भरी दो टंकियों को एक क्षैतिज नल से जोड़ दिया जाता है। जल का बहाव उस समय तक निरंतर बना रहता है जब तक दोनों टंकियों में जल के तल समान न हो जाएँ। इसी के समान ऊष्मा की ‘कैलॉरिक’ धारणा में ऊष्मा उस समय तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि ‘कैलॉरिक तल’ (अर्थात् ताप) समान नहीं हो जाते ।
इसी बीच, ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में कल्पित करने की आधुनिक अवधारणा के कारण इसके (ऊष्मा के) तरल स्वरूप को नकार दिया गया। इस संबंध में 1798 में बेंजामिन थॉमसन (जिन्हें काउन्ट रम्फोर्ड भी कहते हैं) ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग भी किया। इन्होंने पाया कि पीतल की तोप में छेद करते समय इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उससे पानी उबल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह प्राप्त हुआ कि प्रयोग में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस कार्य पर निर्भर करता था जो घोड़े ड्रिल को घुमाने में करते थे न कि ड्रिल के पैनेपन पर। कैलॉरिक स्वरूप के अनुसार अधिक पैनी ड्रिल को रंध्रों से अधिक ऊष्मा तरल बाहर निकालना चाहिए, किंतु प्रयोग में यह सही नहीं पाया गया। प्रेक्षणों की सबसे अधिक स्वाभाविक व्याख्या यह थी कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है तथा प्रयोग से भी यह प्रमाणित हो गया कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में अर्थात् कार्य से ऊष्मा में रूपांतारित हो जाती है ।
ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा तथा ताप की अवधारणा एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में अंतरारूपान्तरण का विवेचन करती है। ऊष्मागतिकी एक स्थूल विज्ञान है, क्योंकि यह किसी निकाय की स्थूल प्रकृति पर विचार करती है न कि द्रव्य की आण्विक संरचना पर । वास्तव में, इससे संबंधित अवधारणाओं तथा नियमों का प्रतिपादन 19 वीं शताब्दी में उस समय हुआ था जब द्रव्य के आण्विक स्वरूप को दृढ़तापूर्वक प्रमाणित नहीं किया गया था। ऊष्मागतिकी के वर्णन में निकाय के अपेक्षाकृत कुछ ही स्थूल चर समाहित होते हैं जो सामान्य अनुभव पर आधारित हैं तथा जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है । उदाहरणार्थ, किसी गैस के सूक्ष्म वर्णन में उसकी रचना करने वाले अगणित अणुओं के निर्देशांकों एवं वेगों का निर्धारण आवश्यक होता है। हालांकि गैसों के अणुगति सिद्धांत का विवरण बहुत विस्तृत नहीं है फिर भी इसमें अणुओं के वेर्गों का विवरण समाहित है। इसके विपरीत किसी गैस के ऊष्मागतिकीय विवरण में आण्विक वर्णन पूर्ण रूप से नकार दिया जाता है। ऊष्मागतिकी में किसी गैस को अवस्था दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान तथा संगठन जैसे ऐसे स्थूल चरों द्वारा निर्धारित होती है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं और माप सकते हैं।
यांत्रिकी एवं ऊष्मागतिकी के बीच भेद आपके मस्तिष्क में भलीभांति आ जाना चाहिए । यांत्रिकी में हमारी रुचि बलों तथा बल आघूर्णों के प्रभाव में गति कर रहे कणों एवं पिण्डों में होती है । ऊष्मागतिकी में संपूर्ण निकाय की गति पर विचार नहीं किया जाता। इसकी रुचि पिण्ड की आंतिरक स्थूल अवस्था में होती है। जब बंदूक से गोली दागते हैं तब जो परिवर्तन होता है वह गोली की यांत्रिक अवस्था (विशेषकर गतिज ऊर्जा) में परिवर्तन होता है, उसके ताप में नहीं। जब गोली लकड़ी में धँसकर रुक जाती है तो गोली की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है जिससे गोली तथा उसके चारों ओर की लकड़ी की सतहों का ताप परिवर्तित हो जाता है। ताप गोली की आंतरिक गति (जो अव्यवस्थित है) की ऊर्जा से संबंधित होता है न कि गोली की संपूर्ण गति से ।
11.2 तापीय साम्य
यांत्रिकी में साम्यावस्था से तात्पर्य है कि निकाय पर नेट बाह्य बल व बल आघूर्ण शून्य हैं। ऊष्मागतिकी में साम्यावस्था का अर्थ भिन्न संदर्भ में दृष्टिगोचर होता है : निकाय की अवस्था को हम उस समय साम्यावस्था में कहते हैं जब निकाय को अभिलक्षणित करने वाले स्थूल चर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते । उदाहरणार्थ, किसी पर्यावरण से पूर्णतः ऊष्मारोधी बंद दृढ़ पात्र में भरी कोई गैस ऊष्मागतिक रूप से तब साम्यावस्था में होगी जब उसके दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान के परिमाण तथा संगठन समय के साथ परिवर्तित न हों।

(a)

(b)
चित्र 11.1 (a) (दो गैसों के) निकाय
कोई निकाय साम्यावस्था में है कि नहीं व्यापक रूप में यह चारों ओर के परिवेश तथा उस दीवार की प्रकृति पर निर्भर करता है जो निकाय को परिवेश से पृथक् करती है। कल्पना कीजिए कि दो गैसें
भी संभावित युग्म का मान
दो निकायों के मध्य की साम्यावस्था की स्थिति को क्या अभिलक्षित करती है ? आप अपने अनुभव से उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं । तापीय साम्य में, दो निकायों के ताप समान होते हैं। हम जानेंगे कि ऊष्मागतिकी में ताप की अवधारणा तक कैसे पहुँचते हैं ? ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम इसकी ओर संकेत करता है ।
11.3 ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम
कल्पना कीजिए कि दो निकाय
शून्य कोटि नियम के माध्यम से हमने विधिवत ताप की अवधारणा विकसित की है । हमारे सामने पुनः एक प्रश्न उत्पन्न होता है : भिन्न-भिन्न पिंडों के ताप के लिए हम अंकिक मानों का निर्धारण कैसे करें? दूसरे शब्दों में, हम ताप मापक्रम कैसे बनाएँ? तापमिति इस मौलिक प्रश्न से संबंध रखती है जिसके विषय में हम अगले अनुभाग में अध्ययन करेंगे।

(a)

(b)
चित्र
11.4 ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य
ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियम से ताप की अवधारणा की उत्पत्ति हुई जो हमारे सामान्य ज्ञान के अनुकूल है। ताप किसी पिण्ड की उष्णता का द्योतक है। जब दो पिण्ड ऊष्मीय संपर्क में लाए जाते हैं तो इससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है। ऊष्मा उच्च ताप वाले पिण्ड से निम्न ताप वाले पिण्ड की ओर प्रवाहित होती है। जब ताप समान हो जाते हैं तो प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों पिण्ड तापीय साम्य में होते हैं। हम यह विस्तार से पढ़ चुके हैं कि भांति-भांति के पिण्डों के ताप के निर्धरण के लिए ताप मापक्रम कैसे बनाए जाते हैं। अब हम ऊष्मा तथा तत्संबंधित राशियों; जैसे-आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य की अवधारणाओं का वर्णन करेंगे ।
किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को समझना कठिन नहीं है। हम जानते हैं कि प्रत्येक स्थूल निकाय असंख्य अणुओं से निर्मित है। आंतरिक ऊर्जा इन अणुओं की स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं का योग है । हमने यह टिप्पणी की है कि ऊष्मागतिकी में निकाय की समग्र रूप से गतिज ऊर्जा प्रासंगिक नहीं होती । इस प्रकार, निर्देश फ्रेम में आंतरिक ऊर्जा अणु की गतिज व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है जिसके सापेक्ष निकाय का द्रव्यमान-केंद्र विरामावस्था में होता है । इस प्रकार, इसमें केवल निकाय के अणुओं की यादृच्छिक गति से संबंधित (अव्यवस्थित) ऊर्जा ही समाहित होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा को
यद्यपि हमने आंतरिक ऊर्जा के अर्थ को समझने के लिए आण्विक चित्र प्रस्तुत किया है तथापि जहाँ तक ऊष्मागतिकी का संबंध है,

(a)

(b)
चित्र 11.3 (a) जब बॉक्स विरामावस्था में है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा
(b)

चित्र 11.4 ऊष्मा व कार्य किसी निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण की दो विभिन्न विधियाँ हैं जिनसे उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। (a) निकाय तथा परिवेश के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा को ऊर्जा के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित करते हैं। (b) कार्य उन साधनों (उदाहरणार्थ, पिस्टन से जुड़े भारों को ऊपर नीचे करके पिस्टन को गति देना) द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का स्थानांतरण है जिनमें तापांतर समाहित नहीं होता।
किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में किन उपायों से परिवर्तन किए जा सकते हैं ? सुविधा की दृष्टि से पुनः कल्पना कीजिए कि चित्र 11.4 के अनुसार निकाय किसी दिए गए द्रव्यमान की एक गैस है जो एक सिलिंडर में भरी है जिसमें गतिशील पिस्टन लगा है। अनुभव यह बताता है कि गैस की अवस्था (तथा इस प्रकार उसकी आंतरिक ऊर्जा) परिवर्तित करने के दो उपाय होते हैं। एक उपाय है कि सिलिंडर को उस पिण्ड के संपर्क में रखें जो गैस की अपेक्षा उच्च ताप पर है। तापांतर के कारण ऊर्जा (ऊष्मा) गरम पिण्ड से गैस में प्रवाहित होगी। इससे गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय है कि पिस्टन को नीचे की ओर दबाया जाए (अर्थात् निकाय पर कार्य किया जाए)। इसमें भी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है । निःसंदेह ये दोनों बातें विपरीत दिशा में भी संभव होती हैं। यदि चारों ओर के परिवेश का ताप कम है तो ऊष्मा गैस से परिवेश में प्रवाहित होगी। इसी प्रकार, गैस पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का दे सकती है और परिवेश पर कार्य कर सकती है। संक्षेप में, ऊष्मा और कार्य दो भिन्न-भिन्न विधियाँ हैं जिनसे ऊष्मीय निकाय की स्थिति परिवर्तित होती है तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है।
ऊष्मा एवं आंतरिक ऊर्जा की धारणाओं में अंतर को सावधानीपूर्वक समझना आवश्यक है । ऊष्मा निश्चित रूप से ऊर्जा है परंतु यह ऊर्जा पारगमन में है । यह मात्र शब्दों का खेल नहीं है । दोनों में अंतर मूल महत्त्व का है । किसी ऊष्मागतिकी निकाय की स्थिति उसकी आंतरिक ऊर्जा से अभिलक्षित होती है न कि ऊष्मा से । इस प्रकार का प्रकथन कि ‘किसी दी हुई अवस्था में गैस में ऊष्मा की कुछ मात्रा होती है’ उतना ही निरर्थक है जितना कि यह प्रकथन कि ‘किसी दी हुई स्थिति में गैस में कुछ कार्य निहित होता है।’ इसके विपरीत, ‘किसी दी हुई अवस्था में गैस में आंतरिक ऊर्जा की कुछ मात्रा होती है’ पूरी तरह से एक सार्थक प्रकथन है । इसी प्रकार से, ऐसे प्रकथन जैसे ‘निकाय को एक निश्चित मात्रा की ऊष्मा दी गई है’ या ‘निकाय द्वारा एक निश्चित मात्रा का कार्य किया गया’ पूर्णतः अर्थपूर्ण सार्थक प्रकथन हैं।
संक्षेप में, ऊष्मा व कार्य ऊष्मागतिकी में स्थिति चर नहीं होते । ये किसी निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण की विधियाँ होती हैं जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। जो, जैसा कि पहले वर्णन कर चुके हैं, एक अवस्था चर होता है।
साधारण भाषा में हमें प्रायः ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा में भ्रम बना रहता है। कुछ प्राथमिक भौतिकी की पुस्तकों में कभी-कभी इस भेद की उपेक्षा कर दी जाती है । तथापि ऊष्मागतिकी को भलीभांति समझने के लिए यह विभेद आवश्यक है ।
11.5 ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम
हम यह देख चुके हैं कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा
ऊर्जा संरक्षण के सामान्य नियम में यह अंतर्निहित है कि
इसका तात्पर्य यह है कि जो ऊर्जा
मान लीजिए कि हम समीकरण (11.1) को वैकल्पिक रूप में प्रस्तुत करते हैं,
अब मान लीजिए कि निकाय किसी आरंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में कई प्रकार से आता है। उदाहरणार्थ, गैस की अवस्था
अर्थात् निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य करने में पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाती है ।
यदि निकाय सिलिंडर में भरी गैस है तथा सिलिंडर में गतिशील पिस्टन लगा है तो पिस्टन को गति देने में गैस को कार्य करना पड़ता है । चूंकि बल को दाब
यहाँ
समीकरण (11.3) के अनुप्रयोग के रूप में हमें
समीकरण (11.3) से हमें आंतरिक ऊर्जा का मान प्राप्त होता है,
इस प्रकार, हम देखते हैं कि ऊष्मा का अधिकांश भाग जल की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होता है। इस प्रक्रिया में जल द्रव से वाष्प प्रावस्था में परिवर्तित होता है ।
11.6 विशिष्ट ऊष्मा धारिता
कल्पना कीजिए कि किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा
हम आशा करते हैं कि
यदि पदार्थ के परिमाण का निर्धारण
सारणी 11.1 में कमरे के ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर कुछ ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता तथा मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता दी गई हैं।
हम अध्याय 12 में पढ़ंगे कि गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं के संबंध में की गई भविष्यवाणियाँ सामान्यतया प्रयोग से मेल खाती हैं। हम उसी ऊर्जा सम विभाजन नियम का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने वहाँ ठोसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा की भविष्यवाणी में किया है (खंड 12.5 और 12.6 देखें)।
अब स्थिर दाब पर,
सारणी 11.1 कमरे के ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर कुछ ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता तथा मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता
| पदार्थ | विशिष्ट ऊष्मा धारिता |
मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता |
|---|---|---|
| ऐलुमिनियम | 900.0 | 24.4 |
| कार्बन | 506.5 | 6.1 |
| ताँबा | 386.4 | 24.5 |
| सीसा | 127.7 | 26.5 |
| चाँदी | 236.1 | 25.5 |
| टंगस्टन | 134.4 | 24.9 |
जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि भविष्यवाणियाँ सामान्यतया साधारण तापों पर प्रायोगिक मानों से मेल खाती हैं (कार्बन एक अपवाद है)। यह ज्ञात है कि यह मेल निम्न तापों पर भंग हो जाता है ।
जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता
ऊष्मा का पुराना मात्रक कैलोरी था। 1 कैलोरी को ऊष्मा के उस परिमाण के रूप में परिभाषित करते थे जो

चित्र 11.5 ताप के साथ जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता में परिवर्तन
इसलिए कैलोरी की यथार्थ परिभाषा के लिए यह आवश्यक समझा गया कि एकांक ताप अंतराल को निर्धारित किया जाए। ऊष्मा का वह परिमाण जो
जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता, प्रक्रिया या उन परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनके अंतर्गत ऊष्मा का स्थानांतरण होता है । उदाहरणार्थ, गैसों के लिए हम दो विशिष्ट ऊष्माओं को परिभाषित करते हैं : स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता तथा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। किसी आदर्श गैस के लिए हमारे पास एक सरल संबंध होता है जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं :
यहाँ
यदि
यहाँ अधोलिखित

अधोलिखित
जो निम्नलिखित परिणाम देता है :
समीकरणों (11.9) से (11.11) तक के उपयोग से हमें वांछित संबंध ( 11.8 ) प्राप्त होता है ।
11.7 ऊष्मागतिकीय अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण
किसी भी ऊष्मागतिकीय निकाय की प्रत्येक साम्य अवस्था को कुछ स्थूल चरों के विशिष्ट मानों के उपयोग द्वारा पूरी तरह से वर्णित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, किसी गैस की साम्य अवस्था उसके दाब, आयतन, ताप व द्रव्यमान (तथा संगठन यदि गैसों का सम्मिश्रण है) के मानों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। कोई ऊष्मागतिक निकाय सदैव साम्य स्थिति में नहीं होता। उदाहरणार्थ, किसी गैस को निर्वात के विरुद्ध यदि फैलने दिया जाता है तो यह साम्य अवस्था नहीं होती [चित्र 11.6(a)]। द्रुत्र प्रसरण की अवधि में गैस का दाब संभव है कि सभी स्थानों पर एकसमान न हो। इसी प्रकार, गैसों का वह सम्मिश्रण जिसमें विस्फोटक रासायनिक अभिक्रिया होती है (उदाहरणार्थ, पेट्रोल की वाष्प तथा वायु का मिश्रण जिसे एक चिंगारी से प्रज्ज्वलित किया जाता है) एक साम्य अवस्था नहीं है; इसके अतिरिक्त इसके ताप व दाब एकसमान नहीं हैं [चित्र 11.6(b)]। अंततः, गैस का ताप व दाब एकसमान हो जाता है तथा वह परिवेश के साथ तापीय व यांत्रिक साम्य में आ जाती है ।
(a)

(b)
चित्र 11.6 (a) बॉक्स के विभाजक को अचानक हटा दिया गया है जिससे गैस का मुक्त प्रसरण होता है।
संक्षेप में, ऊष्मागतिकीय अवस्था चर निकायों की साम्यावस्था का विवरण देते हैं । यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न अवस्था चर स्वतंत्र हों । अवस्था चरों के पारस्परिक संबंध को अवस्था का समीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ, किसी आदर्श गैस के लिए अवस्था का समीकरण आदर्श गैस संबंध होता है,
गैस की निश्चित मात्रा के लिए अर्थात् दिए गए
ऊष्मागतिकीय अवस्था चर दो प्रकार के होते हैं : विस्तीर्ण तथा गहन। विस्तीर्ण चर निकाय के आकार का संकेत देते हैं जबकि गहन चर जैसे दाब तथा ताप से ऐसा नहीं करते । यह निर्णय लेने के लिए कि कौन-सा चर विस्तीर्ण है तथा कौन-सा गहन है, किसी प्रासंगिक निकाय पर विचार कीजिए तथा कल्पना कीजिए कि उसे दो समान भागों में बाँट दिया गया है। वे चर जो हर भाग में अपरिवर्तित रहते हैं गहन चर कहलाते हैं किंतु जिन चरों का मान हर भाग में आधा हो जाता है, उन्हें विस्तीर्ण चर कहते हैं। उदाहरणार्थ, यह आसानी से देखा जा सकता है कि आंतरिक ऊर्जा
में दोनों ओर की राशियाँ विस्तीर्ण है* (किसी गहन चर जैसे
11.8 ऊष्मागतिकीय प्रक्रम
11.8.1 स्थैतिककल्प प्रक्रम
ऐसी गैस पर विचार कीजिए जो अपने परिवेश से तापीय तथा यांत्रिक रूप से साम्य में हो । ऐसी स्थिति में गैस का दाब बाह्य दाब के बराबर होगा तथा इसका ताप वही होगा जो परिवेश का है । कल्पना कीजिए कि बाह्य दाब को यकायक कम कर देते हैं (मान लीजिए कि बर्तन में लगे गतिशील पिस्टन से भार हटा लेते हैं)। पिस्टन बाहर की ओर त्वरित होगा। प्रक्रम की अवधि में गैस उन अवस्थाओं से गुजरती है जो साम्यावस्थाएँ नहीं हैं । असाम्य अवस्थाओं का सुनिश्चित दाब व ताप नहीं होता । इसी प्रकार, यदि गैस व उसके परिवेश के मध्य सीमित तापांतर है, तो ऊष्मा का विनिमय द्रुत गति से होता है। इस प्रक्रम में गैस असाम्यावस्था से गुजरती है । यथासमय, गैस संतुलन की अवस्था में पहुँच जाएगी जिसमें सुनिश्चित ताप व दाब परिवेश के ताप व दाब के बराबर हो जाएगा । निर्वात में गैस का स्वतंत्र प्रसार[^8]
तथा विस्फोटक रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाली गैसों का सम्मिश्रण (जिसका खंड (11.7) में वर्णन किया गया है) भी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें निकाय असाम्यावस्था से गुजरता है।
किसी निकाय की असाम्यावस्था से व्यवहार करना कठिन होता है । इसलिए एक आदर्शीकृत प्रक्रम की कल्पना करना सरल होता है जिसके हर चरण में निकाय एक साम्यावस्था में है । ऐसा प्रक्रम सिद्धांतः अनंत रूप से धीमा होता है । इस कारण इस प्रक्रम को स्थैतिककल्प (लगभग स्थिर) प्रक्रम कहते हैं। यह निकाय अपने चरों
स्पष्ट रूप से, स्थैतिककल्प प्रक्रम काल्पनिक रचना है। व्यवहार रूप से उन प्रक्रमों को, जो बहुत ही धीमे हैं, जिनके पिस्टन में त्वरित गति नहीं होती तथा जिनमें अधिक ताप प्रवणता नहीं होती, इन्हें आदर्श स्थैतिककल्प प्रक्रम मानना तर्कसंगत है। यदि अन्य बात का वर्णन न किया जाए तो हम अब स्थैतिककल्प प्रक्रमों के विषय में ही अध्ययन करेंगे।

चित्र 11.7 स्थैतिककल्प प्रक्रम में परिवेश के पात्र का ताप तथा बाह्य दाब एवं निकाय के ताप व दाब का अंतर अत्यल्प है । वह प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि में निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है । स्थिर ताप के किसी विशाल ऊष्मा भंडार में रखे धात्विक सिलिंडर में प्रसरित हो रही गैस समतापीय प्रक्रम का एक उदाहरण है । (ऊष्मा भंडार से निकाय में ऊष्मा के स्थानांतरण से ऊष्माशय का ताप यथार्थ रूप से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी ऊष्माधारिता अत्यधिक होती है)। समदाबीय प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है जबकि समआयतनिक प्रक्रम में आयतन स्थिर रहता है। अंततः, यदि निकाय को परिवेश से ऊष्मारुद्ध कर दिया जाए तथा निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा प्रवाहित न हो, तो प्रक्रम रुद्धोष्म होता है । इन विशेष प्रक्रमों की परिभाषाओं का सार सारणी 11.2 में प्रस्तुत किया गया है ।
सारणी 11.2 कुछ विशिष्ट ऊष्मागतिकीय प्रक्रम
| प्रक्रमों का प्रकार | विशेषता |
|---|---|
| समतापीय | स्थिर ताप |
| समदाबीय | स्थिर दाब |
| समआयतनिक | स्थिर आयतन |
| रुद्धोष्म | निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा प्रवाह |
| नहीं |
करेंगे।
अब हम इन प्रक्रमों के विषय में विस्तार से अध्ययन
11.8.2 समतापीय प्रक्रम
किसी समतापीय प्रक्रम में (जिसमें
अर्थात् किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है । यह और कुछ नहीं वरन् बॉयल का नियम है ।
कल्पना कीजिए कि कोई आदर्श गैस समतापीय (ताप
दूसरे चरण में हमने आदर्श गैस समीकरण
11.8.3 रुद्धोष्म प्रक्रम
रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय को परिवेश से ऊष्मारुद्ध कर देते हैं फलस्वरूप अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है । समीकरण (11.1) से पता चलता है कि गैस द्वारा संपादित कार्य के फलस्वरूप आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है (और इस प्रकार आदर्श गैस के लिए उसका ताप)। यहाँ हम बिना उपपत्ति के इस तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं (जिसका आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे) कि आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में
जहाँ
अतः यदि कोई आदर्श गैस रुद्धोष्म ढंग से
चित्र 11.8 में आदर्श गैस के लिए

चित्र 11.8 आदर्श गैस के समतापीय व रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए
समीकरण (11.14), से नियतांक
जैसा अपेक्षित है, यदि रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य गैस द्वारा संपन्न होता है
11.8.4 समआयतनिक प्रक्रम
किसी समआयतनिक प्रक्रम में
11.8.5 समदाबीय प्रक्रम
समदाबीय प्रक्रम में दाब
चूंकि ताप परिवर्तित होता है, अतः आंतरिक ऊर्जा भी परिवर्तित होती है । अवशोषित ऊष्मा आंशिक रूप से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में तथा आंशिक रूप से कार्य करने में व्यय होती है । किसी नियत ऊष्मा की मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा निर्धारित किया जाता है ।
11.8.6 चक्रीय प्रक्रम
चक्रीय प्रक्रम में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है । चूंकि आंतरिक ऊर्जा अवस्था चर है, चक्रीय प्रक्रम के लिए
11.9 ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम है। सामान्य अनुभव यह बतलाता है कि ऐसे बहुत से मनोगम्य प्रक्रम हैं जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से पूर्णतया अनुमत हैं तथापि कभी भी होते हुए दिखाई नहीं देते । उदाहरणार्थ, ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा कि मेज पर पड़ी कोई पुस्तक स्वतः उछलकर किसी ऊँचाई पर पहुँच जाए। किंतु ऐसी बात तभी संभव हो सकती है यदि केवल ऊर्जा संरक्षण नियम का ही नियंत्रण हो । मेज स्वतः ठंडी होकर अपनी आंतरिक ऊर्जा का कुछ अंश पुस्तक की समान मात्रा की यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने में करे और इस यांत्रिक ऊर्जा के कारण पुस्तक उस ऊँचाई तक उछले जिसकी स्थितिज ऊर्जा पुस्तक द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो। परंतु ऐसा कदापि नहीं होता। स्पष्ट है कि प्रकृति के किसी आंतरिक मूल नियम के कारण यह निषेध है। यद्यपि यह ऊर्जा संरक्षण नियम का अनुपालन करता है। वह नियम जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संगत अनेक परिघटनाओं को स्वीकृति नहीं देता, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाता है।
ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता तथा किसी प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की मूल सीमा निर्धरित करता है। सरल भाषा में, यह नियम बताता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कदापि 1 नहीं हो सकती। ठंडे ऊष्मा भंडार की मुक्त ऊष्मा को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। प्रशीतक के लिए द्वितीय नियम यह बताता है कि निष्पादन गुणांक कदापि अनंत नहीं हो सकता। प्रशीतक पर बाह्य कार्य
केल्विन-प्लैंक का प्रकथन
ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा उस ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में रूपांतरित करना हो।
क्लासियस का प्रकथन
ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ठंडे पिंड से किसी गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरण हो। उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में आप इसकी उपपत्ति पढ़ेंगे कि दोनों प्रकथन पूर्णतया समतुल्य हैं ।
11.10 उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम
किसी ऐसे प्रक्रम की कल्पना कीजिए जिसमें कोई ऊष्मागतिकीय निकाय आरंभिक अवस्था
कोई ऊष्मागतिकीय प्रक्रम (अवस्था
उत्क्रमणीयता ऊष्मागतिकी की ऐसी मूल धारणा क्यों है ? जैसा कि हम देख चुके है, ऊष्मागतिकी के महत्त्वों में से एक महत्त्व दक्षता का है जिससे ऊष्मा कार्य में रूपांतरित की जा सकती है । ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम
11.11 कार्नो इंजन
कल्पना कीजिए कि हमारे पास ताप
हम यह आशा करते हैं कि दो तापों के बीच कार्य करने वाला आदर्श इंजन उत्क्रमणीय इंजन है । जैसा कि पहले अनुभागों में बताया जा चुका है, अनुत्क्रमणीयता से दक्षता को कम करने वाले क्षयकारी प्रभाव संबद्ध होते हैं। कोई प्रक्रम तभी उत्क्रमणीय होता है यदि वह स्थैतिककल्प तथा ऊर्जा-संरक्षी हो। हम यह देख चुके हैं कि वह प्रक्रम स्थैतिककल्प नहीं होता है जिसमें निकाय व ऊष्मा भंडार के बीच तापांतर पर्याप्त हो। इसका तात्पर्य यह है कि दो तापों के मध्य कार्य कर रहे किसी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन में ऊष्मा का अवशोषण (गरम ऊष्मा भंडार से) समतापीय विधि द्वारा होना चाहिए तथा (अपेक्षाकृत

चित्र 11.9 किसी ऊष्मा इंजन के लिए कार्नो चक्र जिसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस का उपयोग होता है।
ठंडे ऊष्मा भंडार को) समतापीय विधि द्वारा ऊष्मा मुक्त होनी चाहिए। इस प्रकार, हमने उत्क्रमणीय इंजन के दो चरणों की पहचान की : ताप
दो तापों के मध्य कार्य करने वाला कोई उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन कार्नो इंजन कहलाता है । हमने अभी विवेचना की है कि इस इंजन में चरणों का क्रम निम्नलिखित होना चाहिए, जो चित्र 11.11 में दर्शाए अनुसार एक चक्र का निर्माण करते हैं, जिसे
कार्नो चक्र कहते हैं। हमने कार्नो इंजन का कार्यकारी पदार्थ एक आदर्श गैस लिया है ।
(a) चरण
ताप
(b) चरण
(c) चरण
ताप
(d) चरण
समीकरणों (11.18) से (11.21) के उपयोग से एक पूरे चक्र में गैस द्वारा संपादित कुल कार्य की मात्रा,
कार्नो इंजन की दक्षता
अब चूंकि चरण
अथवा
इसी प्रकार, चूंकि चरण
समीकरणों (11.24) तथा (11.25) से,
समीकरण (11.26) के उपयोग से समीकरण (11.23) से
हम जानते हैं कि कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन है। वास्तव में यही एकमात्र ऐसा इंजन संभव है जो भिन्न तापों के दो ऊष्मा भंडारों के मध्य कार्य करता है। चित्र 11.9 में दर्शाए कार्नो चक्र का हर चरण उत्क्रमित किया जा सकता है। यह उस प्रक्रम के समान होता है, जिसमें
अब हम महत्वपूर्ण परिणाम सिद्ध करेंगे (जिसे कभी-कभी कार्नो प्रमेय कहते हैं) (a) दिए हुए गरम तथा ठंडे ऊष्माशयों के क्रमशः दो तापों
परिणाम (a) को सिद्ध करने के लिए हम कल्पना करते हैं कि एक उत्क्रमणीय (कार्नो) इंजन
कि

चित्र 11.10 उत्क्रमणीय प्रशीतक
यह अंतिम टिप्पणी दर्शाती है कि कार्नो इंजन के लिए,
एक व्यापक संबंध है जो निकाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। यहाँ
सारांश
1. ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम यह अभिव्यक्त करता है कि “दो निकाय जो किसी तीसरे निकाय के साथ स्वतंत्र रूप से तापीय साम्य में हैं, वे एक-दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होते हैं”। शून्यवाँ नियम ताप की अवधारणा का सूत्रपात करता है ।
2. निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसके आण्विक घटकों की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है । इसमें निकाय की संपूर्ण गतिज ऊर्जा सम्मिलित नहीं होती । ऊष्मा और कार्य किसी निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण के दो रूप हैं। निकाय व उसके परिवेश के बीच तापांतर के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा के रूप में होता है । कार्य अन्य साधनों (जैसे गैस भरे सिलिंडर के पिस्टन जिससे कुछ भार संबद्ध है, को ऊपर नीचे करने में) द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का स्थानांतरण है । इसमें तापांतर समाहित नहीं होता है ।
3. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम है, जो उस निकाय में लागू होता है जिसमें परिवेश को या परिवेश से (ऊष्मा व कार्य द्वारा) ऊर्जा स्थानांतरण हो । यह बताता है कि
यहाँ
4. पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता को हम निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिभाषित करते हैं
यहाँ
जो सामान्यतया साधारण तापों पर किए जाने वाले प्रयोगों से प्राप्त परिणामों से मेल खाता है ।
कैलोरी ऊष्मा का पुराना मात्रक है । 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो
5. किसी आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर मोलीय विशिष्ट ऊष्मा धारिताएँ निम्नलिखित संबंध का पालन करती हैं
यहाँ
6. किसी ऊष्मागतिकीय निकाय की साम्यावस्था का विवरण अवस्था चरों द्वारा होता है। किसी अवस्था चर का मान केवल उसकी किसी विशेष अवस्था पर निर्भर करता है न कि उस पथ पर जिससे यह अवस्था प्राप्त होती है। अवस्था चरों के उदाहरण हैं : दाब
7. कोई स्थैतिककल्प प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से संपन्न होने वाला प्रक्रम है जिसमें निकाय परिवेश के साथ पूरे समय तापीय व यांत्रिक साम्य में रहता हैं। स्थैतिककल्प प्रक्रम में परिवेश के दाब व ताप तथा निकाय के दाब व ताप में अनंत सूक्ष्म अंतर हो सकता है।
8. किसी आदर्श गैस के ताप
9. किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में
किसी आदर्श गैस द्वारा अवस्था
10. ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कुछ उन प्रक्रमों की स्वीकृति नहीं देता जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुकूल हैं। इसके दो प्रकथन इस प्रकार हैं :
केल्विन-प्लैंक का प्रकथन
ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका मात्र परिणाम केवल किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करके उसे पूर्णतया कार्य में रूपांतरित करना हो।
क्लॉसियस का प्रकथन
ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका मात्र परिणाम ऊष्मा का किसी ठंडे पिंड से अपेक्षाकृत गरम पिंड में स्थानांतरण हो। इसे सरल ढंग से कहा जाए तो द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता
11. कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है यदि उसे इस प्रकार उत्क्रमित किया जाए कि निकाय व परिवेश दोनों अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वापस पहुँच जाएँ और परिवेश में कहीं भी कोई परिवर्तन न हो। प्रकृति के नैसर्गिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। आदर्शीकृत उत्क्रमणीय प्रक्रम स्थैतिककल्प प्रक्रम होता है जिसमें कोई भी क्षयकारी घटक; जैसे - घर्षण, श्यानता आदि विद्यमान नहीं रहते।
12. किन्हीं दो तापों
किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती।
13. यदि
| राशि | प्रतीक | विमाएँ | मात्रक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. आयतन प्रसार गुणांक | ||||
| 2. किसी निकाय को प्रदत ऊष्मा | J | चर नहीं है । |
||
| 3. विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||||
| ऊष्मा इंजन की दक्षता | विमाहीन | - | ||
| प्रशीतक का निष्पादन गुणांक | विमाहीन | - | ||
| 4. तापीय चालकता |
विचारणीय विषय
1. किसी पिंड का ताप उसकी माध्य आंतरिक ऊर्जा से संबंधित है न कि उसके द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा से बंदूक से दागी गई किसी गोली का उच्च ताप उसकी अधिक चाल के कारण नहीं होता ।
2. ऊष्मागतिकी में साम्य उस परिस्थिति की ओर निर्देश करता है जब निकाय की ऊष्मागतिकीय अवस्था का वर्णन करने वाले स्थूल चर, समय पर निर्भर नहीं करते । यांत्रिकी में किसी निकाय की साम्यावस्था से अभिप्राय है कि निकाय पर कार्य करने वाले नेट बल तथा बल आघूर्ण दोनों शून्य होते हैं ।
3. ऊष्मागतिकीय साम्य में निकाय के सूक्ष्म संघटक साम्यावस्था में नहीं होते (यांत्रिकी के प्रसंग में)।
4. ऊष्माधारिता, व्यापक रूप में उस प्रक्रम पर निर्भर करती है जिससे निकाय तब गुजरता है जब वह ऊष्मा ग्रहण करता है ।
5. समतापीय स्थैतिककल्प प्रक्रमों में, निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित या निर्गत होती है यद्यपि हर चरण में गैस का ताप वही होता है जो परिवेशीय ऊष्मा भंडार होता है । निकाय तथा ऊष्मा भंडार के मध्य अत्यंत सूक्ष्म तापांतर के कारण ऐसा संभव हो पाता है ।
अभ्यास
11.1 कोई गीज़र 3.0 लीटर प्रति मिनट की दर से बहते हुए जल को
11.2 स्थिर दाब पर
11.3 व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों होता है :
(a) भिन्न-भिन्न तापों
(b) रासायनिक या नाभिकीय संयत्रों में शीतलक (अर्थात् द्रव जो संयत्र के भिन्न-भिन्न भागों को अधिक गर्म होने से रोकता है) की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होनी चाहिए।
(c) कार को चलाते-चलाते उसके टायरों में वायुदाब बढ़ जाता है।
(d) किसी बंदरगाह के समीप के शहर की जलवायु, समान अक्षांश के किसी रेगिस्तानी शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है।
11.4 गतिशील पिस्टन लगे किसी सिलिंडर में मानक ताप व दाब पर 3 मोल हाइड्रोजन भरी है । सिलिंडर की दीवारें ऊष्मारोधी पदार्थ की बनी हैं तथा पिस्टन को उस पर बालू की परत लगाकर ऊष्मारोधी बनाया गया है । यदि गैस को उसके आरंभिक आयतन के आधे आयतन तक संपीडित किया जाए तो गैस का दाब कितना बढ़ेगा ?
11.5 रुद्धोष्म विधि द्वारा किसी गैस की अवस्था परिवर्तन करते समय उसकी एक साम्यावस्था
11.6 समान धारिता वाले दो सिलिंडर
(a) सिलिंडर
(b) गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा ?
(c) गैस के ताप में क्या परिवर्तन होगा ?
(d) क्या निकाय की माध्यमिक अवस्थाएँ (अंतिम साम्यावस्था प्राप्त करने के पूर्व) इसके
11.7 एक हीटर किसी निकाय को
11.8 किसी ऊष्मागतिकीय निकाय को मूल अवस्था से मध्यवर्ती अवस्था तक चित्र (11.11) में दर्शाये अनुसार एक रेखीय प्रक्रम द्वारा ले जाया गया है।

चित्र 11.11
एक समदाबी प्रक्रम द्वारा इसके आयतन को