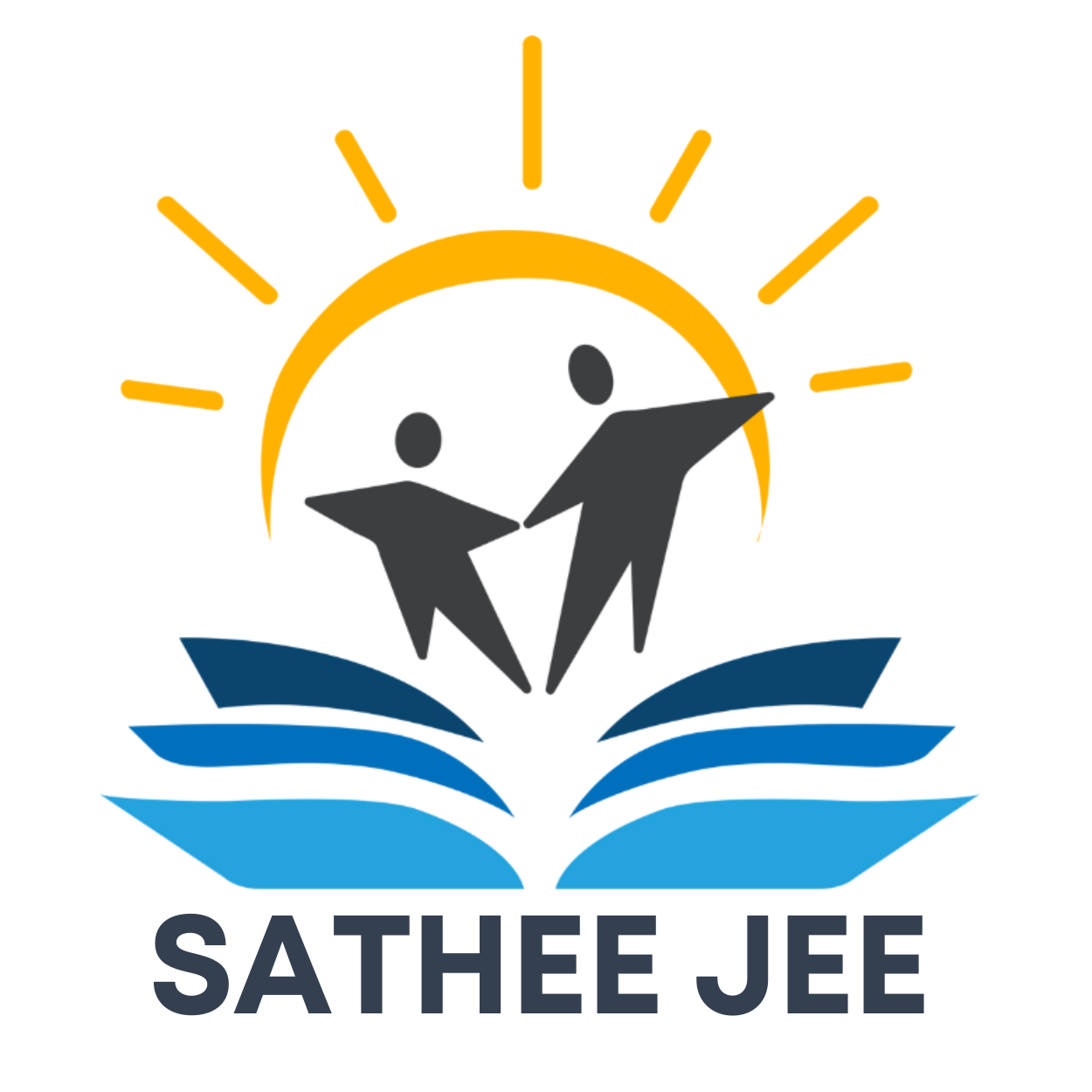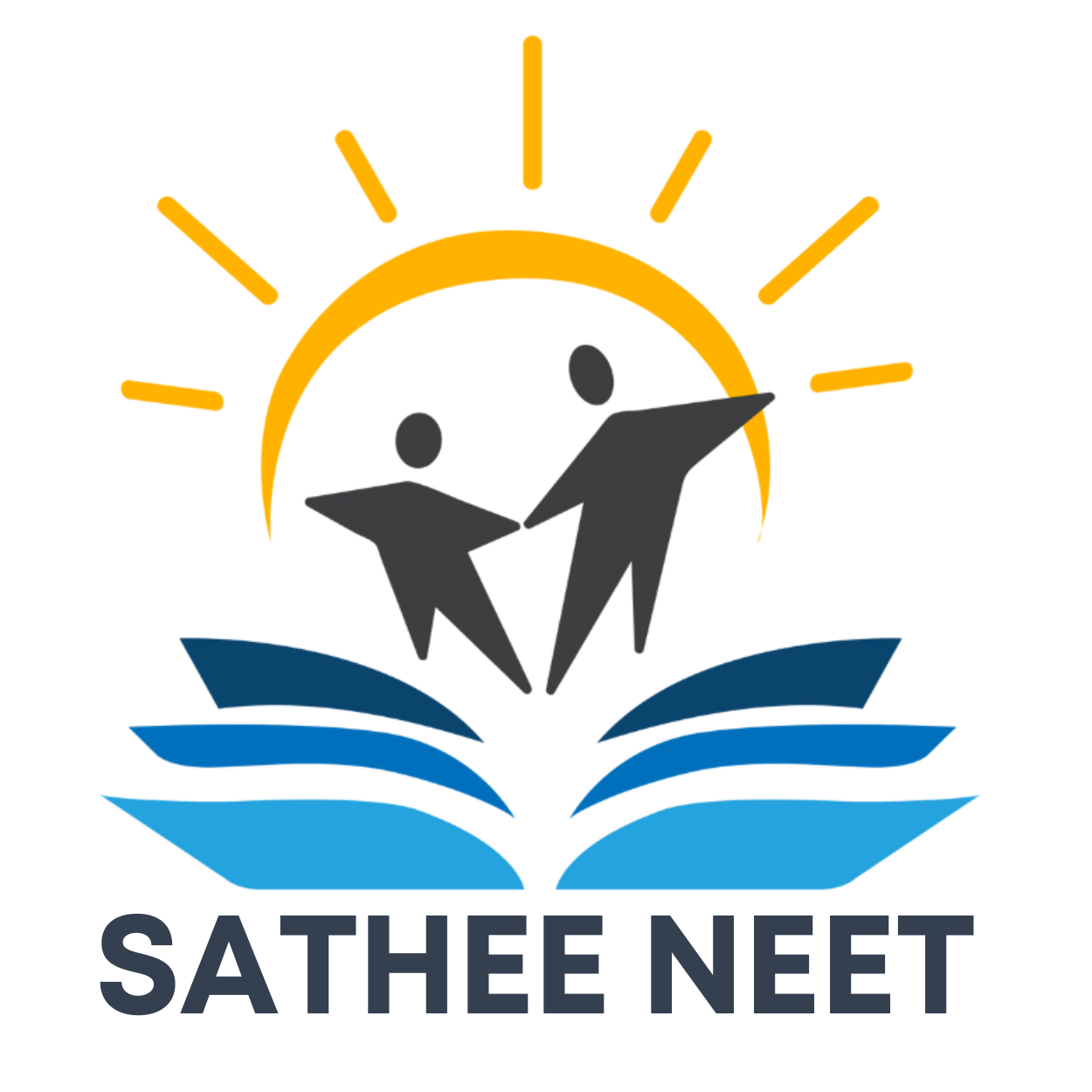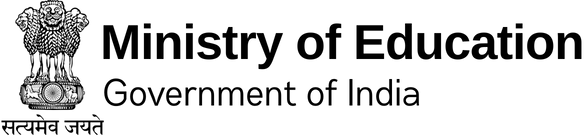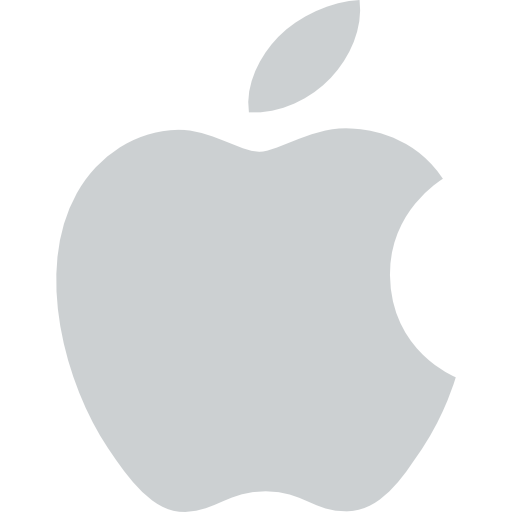यह शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं की सुव्यवस्थित एवं समक्रमिक और समकालिक प्रगति है जो जीवन को प्रेरित करती है।
एक जैव-तंत्र स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। जैव-तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनता है। जीवित तंत्र में रसायनतः क्या होता है? इसके ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैव-तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अन्योन्यक्रिया करते हैं तथा जैव-प्रणाली का आण्विक आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य-प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचनाएं एवं कार्य प्रणालियों की विवेचना इस एकक में की गई है।
10.1 कर्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट मुख्यतया पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का वृहत समूह बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सामान्य उदाहरण इक्षु-शर्करा, ग्लूकोस तथा स्टार्च (मंड) आदि हैं। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र
10.1.1 कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण
कार्बोहाइड्रेटों को जलअपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
(i) मोनोसैकैराइड- वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलिहाइड्राक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकैराइड कहलाते हैं। लगभग 20 मोनोसैकैराइड प्रकृति में ज्ञात हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण ग्लूकोस, फ्रक्टोज़, राइबोस आदि हैं।
(ii) ओलिगोसैकैराइड- वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलअपघटन से मोनोसैकैराइड की दो से दस तक इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, ओलिगोसैकैराइड कहलाते हैं। जलअपघटन से प्राप्त मोनोसैकैराइडों की संख्या के आधार पर इन्हें पुन: डाइसैकैराइड, ट्राइसैकैराइड, टेट्रासैकैराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से डाइसैकैराइड प्रमुख हैं। डाइसैकैराइड के जलअपघटन से प्राप्त दो मोनोसैकैराइड इकाइयाँ समान अथवा भिन्न हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, सूक्रोस का एक अणु जल अपघटन द्वारा ग्लूकोस व फ्रक्टोज़ की एक-एक इकाई देता है, जबकि माल्टोस से प्राप्त दोनों इकाइयाँ केवल ग्लूकोस की होती हैं।
(iii) पॉलिसैकैराइड- वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकैराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, पॉलिसैकैराइड कहलाते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन तथा गोंद आदि हैं। पॉलिसैकैराइड स्वाद में मीठे नहीं होते अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं।
कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनपचायी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उन सभी कार्बोहाइड्रेटों को जो फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहा जाता है। सभी मोनोसैकैराइड चाहे वे ऐल्डोस हों अथवा कीटोस, अपचायी शर्करा होती है।
10.1.2 मोनोसैकैराइड
कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकैराइड को पुन: वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मोनोसैकैराइड में ऐल्डिहाइड समूह है तो उसे ऐल्डोस और यदि उसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोस कहते हैं। मोनोसैकैराइड में निहित कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है जो कि सारणी 10.1 में दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है-
सारणी 10.1- विभिन्न प्रकार के मोनोसैकैराइड
| कार्बन परमाणु | सामान्य पद | ऐल्डिहाइड | कीटोन |
|---|---|---|---|
| 3 | ट्रायोस | ऐल्डोट्रायोस | कीटोट्रायोस |
| 4 | टेट्रोस | ऐल्डोटेट्रोस | कीटोटेट्रोस |
| 5 | पेन्टोस | ऐल्डोपेन्टोस | कीटोपेन्टोस |
| 6 | हैक्सोज | ऐल्डोहैक्सोज | कीटो हैक्सोस |
| 7 | हेप्टोस | ऐल्डोहैप्टोस | कीटोहैप्टोस |
10.1.2.1 ग्लूकोस
ग्लूकोस प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होता है। पके हुए अंगूर में भी बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोस होता है। इसे निम्नानुसार बनाया जा सकता है।
ग्लूकोस को बनाने की विधियाँ
1. सूक्रोस (इक्षु-शर्करा) से- सूक्रोस को तनु
2. स्टार्च से- औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोस को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को तनु
ग्लूकोस की संरचना
ग्लूकोस एक ऐल्डोहैक्सोस है तथा इसे डेक्सट्रोस कहते हैं। यह अनेक कार्बोहाइड्रेटों यथा स्टार्च, सेलुलोस आदि का एकलक होता है। यह संभवतः पृथ्वी पर बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर यह संरचना दिए गए चित्र के अनुसार प्रदर्शित की जा सकती है-
1. इसका आण्विक सूत्र
2.

3. ग्लूकोस, हाइड्रॉक्सिल ऐमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सिम देता है तथा हाइड्रोजन सायनाइड के एक अणु से संयोग कर सायनोहाइड्रिन देता है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोस में कार्बोनिल समूह

4. ग्लूकोस ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से छः कार्बन परमाणुयुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल (ग्लूकोनिक अम्ल) देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोस का कार्बोनिल समूह ऐल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है।

5. ग्लूकोस के ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड द्वारा ऐसीटिलन से ग्लूकोस पेन्टाऐसीटेट बनाता है जो ग्लूकोस में पाँच
6. ग्लूकोस तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, सैकैरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोस में प्राथमिक ऐल्कोहॉलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है।

बहुत से अन्य अनेक गुणों के अध्ययन के उपरांत फिशर ने विभिन्न -
I
II
III
ग्लूकोस को सही रूप में
किसी यौगिक के नाम से पहले लिखे अक्षर

D- (+) - ग्लिसरैल्डिहाइड
ग्लिसरैलिडहाइड के
ग्लूकोस कहलाते हैं। आप संरचना में देख सकते हैं कि
ग्लूकोस की चक्रीय संरचना
संरचना I ग्लूकोस के अधिकांश गुणों को स्पष्ट करती है परंतु निम्नलिखित अभिक्रियाएं एवं तथ्य इस संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं होते।
1. ऐल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोस शिफ-परीक्षण नहीं देता एवं यह
2. ग्लूकोस का पेन्टाऐसीटेट, हाइड्रॉक्सिलऐमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता जो मुक्त
3. ग्लूकोस दो भिन्न क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है जिन्हें


ग्लूकोस के दोनों चक्रीय हैमीऐसीटैल रूपों में भिन्नता केवल

पाइरैन


10.1.2.2 फ्रक्टोज़ ( फल शर्करा )
फ्रक्टोज़ एक महत्वपूर्ण कीटोहैक्सोस है। यह डाइसैकैराइड, सूक्रोस के जलअपघटन पर ग्लूकोस के साथ प्राप्त होता है। फ्रक्टोज़ एक प्राकृतिक मोनोसैकैराइड है जो कि फलों एवं सब्ज़ियों में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में प्रयोग होता है।
फ्रक्टोज़ की संरचना
फ्रक्टोज़ का अणुसूत्र भी
यह भी दो चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है जो

फ्यूरान


फ्रक्टोज़ के दोनों ऐनोमर की चक्रीय संरचना को हावर्थ संरचनाओं द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है-

10.1.3 डाइसैकैराइड
हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाइसैकैराइडों का तनु अम्ल अथवा एन्जाइम की उपस्थिति में जलअपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकैराइडों के दो अणु देते हैं। दोनों मोनोसैकैराइड इकाइयाँ, जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। परमाणु के द्वारा दो मोनोसैकैराइड इकाइयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं।
यदि डाइसैकैराइड में मोनोसैकैराइडों के अपचायी समूह जैसे ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हों तो वह अनअपचायी शर्करा होती है। उदाहरणार्थ सूक्रोस। दूसरी ओर यदि शर्करा में ये प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हों तो यह अपचायी शर्करा कहलाती है। उदाहरणार्थ- माल्टोस तथा लेक्टोस।
I. सूक्रोस- सूक्रोस एक सामान्य डाइसैकैराइड है जो जलअपघटन पर सममोलर (equimolar) मात्रा में
ये दोनों मोनोसैकैराइड इकाइयाँ

सूक्रोस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है। लेकिन जल अपघटन के उपरांत दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ग्लूकोस तथा वामु घ्रुवण घूर्णक फ्रक्टोज़ देता है। चूंकि फ्रक्टोज़ के वामु ध्रुवण घूर्णन का मान
II माल्टोस- एक अन्य डाइसैकैराइड माल्टोस

(I)
माल्टोस
III लैक्टोस- लैक्टोस दुग्ध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। यह
लैक्टोस
10.1.4 पॉलिसैकैराइड
पॉलिसैकैराइड में असंख्य मोनोसैकैराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा संयुक्त रहती हैं। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं।
I. स्टार्च- स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलिसैकैराइड है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्ज़ियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह
ऐमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होती है तथा यह स्टार्च का

ऐमिलोस

II. सेलुलोस- सेलुलोस विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है तथा यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का प्रधान अवयव है। सेलुलोस,

III. ग्लाइकोजन- प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। चूँकि इसकी संरचना ऐमिलोपेक्टिन के समान होती है, अतः इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है एवं यह ऐमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोस की आवश्यकता होती है, एन्जाइम, ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में तोड़ देते हैं। ग्लाइकोजन यीस्ट तथा कवक में भी मिलता है।
10.1.5 कार्बोहाइड्रेटों का महत्व
कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग होते हैं। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा में तात्कालिक स्रोत के रूप में वैद्यों द्वारा शहद का उपयोग किया जाता रहा है। कार्बोहाइड्रेट अणु वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में एवं
जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोस की बनी होती है। लकड़ी के रूप में प्राप्त सेलुलोस से हम फ़र्नीचर आदि बनाते हैं तथा सूती रेशों के रूप में प्राप्त सेलुलोस से हमारे वस्त्र बनते हैं। अनेक प्रमुख उद्योगों जैसे वस्त्र, कागज़, प्रलाक्ष (लैकर), निसवन (मद्यनिर्माण) उद्योग इत्यादि के लिए इनसे कच्चा माल उपलब्ध होता है।
न्युक्लीक अम्ल में दो ऐल्डोपेन्टोस यथा
10.2 प्रोटीन
(
10.2.1 ऐमीनो अम्ल
ऐमीनो अम्ल में ऐमीनो
सभी ऐमीनो अम्लों के रूढ़ नाम हैं जो इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं। ग्लाइसीन को उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस (glykos) का अर्थ मीठा होता है तथा टाइरोसीन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था (ग्रीक भाषा में टाइरोस (tyros) का अर्थ पनीर है)। प्रत्येक ऐमीनो अम्ल को साधारणतः एक तीन अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी-कभी एक अक्षर प्रतीक का उपयोग भी किया जाता है। सामान्यतः उपलब्ध-ऐमीनो अम्लों की संरचनाएं एवं उनके 3 -अक्षर व 1 -अक्षर प्रतीक सारणी 10.2 में दिए गए हैं।
10.2.2 ऐमीनो अम्लों का वर्गीकरण
ऐमीनो अम्लों को उनके अणुओं में उपस्थित ऐमीनो तथा कार्बोक्सिल समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऐमीनो तथा कार्बोक्सिल समूहों की समान संख्या ऐमीनो अम्ल की प्रकृति को उदासीन बनाती है। कार्बोक्सिल समूहों की अपेक्षा ऐमीनो समूहों को संख्या अधिक होने पर यह क्षारकीय तथा कार्बोक्सिल समूहों की संख्या ऐमीनो समूहों की संख्या से अधिक होने पर यह अम्लीय होते हैं जो ऐमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें अनावश्यक ऐमीनो अम्ल कहते हैं जबकि वे ऐमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते तथा जिनको भोजन में लेना आवश्यक है, आवश्यक ऐमीनो अम्ल कहलाते हैं (सारणी 10.2 में तारक द्वारा चिह्नित)।

ऐमीनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिसलीय ठोस होते हैं। ये जल-विलेय तथा उच्च गलनांकी ठोस होते हैं जो सामान्य ऐमीनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भाँति व्यवहार नहीं करते, अपितु लवणों की भाँति गुण दर्शाते हैं। इसका कारण एक ही अणु में अम्लीय (कार्बोक्सिल समूह) तथा क्षारकीय (ऐमीनो समूह) समूहों की उपस्थिति
है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है जबकि ऐमीनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसे ज़्विटर आयन अथवा उभयाविष्ट आयन कहते हैं। यह उदासीन होता है परंतु इसमें धनावेश तथा ॠणावेश दोनों ही उपस्थित हैं।
उभयाविष्ट आयनिक रूप में ऐमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं। तथा वे अम्लों एवं क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं।
ग्लाइसीन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध ऐमीनो अम्ल ध्रुवण घूर्णक होते हैं क्योंकि इनमें
10.2.3 प्रोटीनों की संरचना
आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन

यदि तीसरा ऐमीनो अम्ल, डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद ट्राइपेप्टाइड कहलाता है। एक ट्राइपेप्टाइड में तीन ऐमीनो अम्ल होते हैं जो दो पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार से जब चार, पाँच, अथवा छः एमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो परिणामी उत्पादों को ग्लाइसिलएलनीन (Gly-Ala) टेट्रापेप्टाइड, पेन्टापेप्टाइड अथवा हैक्सापेप्टाइड कहते हैं। जब ऐमीनो अम्लों की संख्या दस से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलिपेप्टाइड कहलाते हैं। एक पॉलिपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक ऐमीनो अम्ल अवशेष होते हैं तथा जिनका आण्विक द्रव्यमान
( अ) रेशेदार प्रोटीन
जब पॉलिपेप्टाइड शृंखलाएं समानांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती हैं तो रेशासम (रेशे जैसी) संरचना बनती है। इस प्रकार के प्रोटीन सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण किरेटिन (बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित) तथा मायोसिन (मांसपेशियों में उपस्थित) आदि हैं।
(ब) गोलिकाकार प्रोटीन
जब पॉलिपेप्टाइड की शृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती हैं ये सामान्यतः जल में विलेय होती है। इन्सुलिन तथा ऐल्बूमिन इनके सामान्य उदाहरण हैं।
प्रोटीनों की संरचना एवं आकृति का अध्ययन चार भिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचनाएं तथा प्रत्येक स्तर पूर्व की तुलना में जटिल होती हैं।
(i) प्रोटीन की प्राथमिक संरचना- प्रोटीनों में एक अथवा अनेक पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलिपेप्टाइड में ऐमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। ऐमीनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात् ऐमीनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं।

चित्र 10.1 - प्रोटीन की

चित्र 10.2 - प्रोटीन की
(ii) प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना- किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलिपेप्टाइड भृंखला विद्यमान होती है। यह दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती हैं-
तथा
(iii) प्रोटीन की तृतीयक संरचना- प्रोटीन की तृतीयक संरचना पॉलिपेप्टाइड शृंखलाओं के समग्र वलन, अर्थात् द्वितीयक संरचना के और अधिक वलन ( लिपटना) को प्रदर्शित करती है। इससे दो प्रमुख आण्विक आकृतियाँ बनती हैंरेशेदार तथा गोलिकाकार। प्रमुख बल जो प्रोटीन की
(iv) प्रोटीन की चतुष्क संरचना- कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलिपेटाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं जिन्हें उप-इकाई कहते हैं। इन उप-इकाइयों की परस्पर दिक्-स्थान व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। इन चारो संरचनाओं का चित्रात्मक निरूपण चित्र 10.3 में दिया गया है जिसमें प्रत्येक रंगीन गेंद, एक ऐमीनो अम्ल को निरूपित करती है।
10.2.4 प्रोटीन का विकृतीकरण
जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविमा संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन, प्राकृत प्रोटीन कहलाता है। जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे- ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन करते हैं जैसे, 
(a) प्राथमिक संरचना
(b) द्वितीयक संरचना (c) तृतीयक संरचना
(d) चतुष्क संरचना O C ON
चित्र 10.3 - प्रोटीन की संरचनाओं का चित्रात्मक निरूपण (चतुष्क संरचना में दो प्रकार की दो उप इकाइयाँ)
चित्र 10.4 - हीमोग्लोबिन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचनाएं
10.3 डन्जाइम
जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव है। इसका एक उदाहरणार्थ है भोजन का पाचन, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अंततः ऊर्जा का उत्पादन। इस प्रक्रम में अभिक्रियाएं एक अनुक्रम होती हैं तथा ये सभी अभिक्रियाएं शरीर में मध्यम परिस्थितियों में सम्पन्न होती हैं। यह कुछ जैव उत्प्रेरकों की सहायता से होता है जिन्हें एन्जाइम कहते हैं। लगभग सभी एन्जाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। एन्जाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। इनका नामकरण सामान्यतया उस यौगिक अथवा यौगिकों के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, उस एन्जाइम का नाम माल्टेस है जो माल्टोस के ग्लूकोस में जलअपघटन को उत्प्रेरित करता है।

कभी-कभी एन्जाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिसमें इनका उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, जो एन्जाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार का अपचयन उन्हें आक्सिडोरिडक्टेस नाम दिया जाता है। एन्जाइम के नाम के अंत में ऐस (-ase) आता है।
10.3.1 एन्जाइम क्रिया की क्रियाविधि
किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एन्जाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान कहा जाता है कि एन्जाइम, संक्रियण ऊर्जा के परिमाण को कम कर देते हैं। उदाहरणार्थ, सूक्रोस के अम्लीय जलअपघटन के लिए संक्रियण ऊर्जा
10.4 विटामिन
ऐसा देखा गया है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता लेकिन पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, अतः इन्हें आवश्यक आहार कारक माना गया है। यद्यपि आहारनली के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिनों को उत्पन्न कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे आहार में सभी विटामिन उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न विटामिन भिन्न श्रेणियों से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें संरचना के आधार पर परिभाषित करना कठिन है। इन्हें सामान्यतः इस प्रकार विचारित किया जाता है कि ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। विटामिनों को
विटामिन (vitamine) दो शब्दों- विटल (vital) + ऐमीन (amine) से जुड़कर बना है; क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में ऐमीनो समूह था। लेकिन बाद के कार्यों से प्रदर्शित हुआ कि इनमें से अधिकांश में ऐमीनो समूह नहीं होता, अतः अंग्रेज़ी में लिखे शब्द का अंतिम अक्षर ’
10.4.1 विटामिनों का वर्गीकरण
जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है
(i) वसा विलेय विटामिन- इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय। ये विटामिन
(ii) जल में विलेय विटामिन-
कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत तथा उनकी कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को सारणी 10.3 में दर्शाया गया है।
सारणी 10.3- कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत तथा उनकी कमी से जनित रोग

10.5 न्यूक्लीक अम्ल
प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के सदृश्य होती है। ये विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी तक किस प्रकार संचरित होते हैं? यह पाया गया है कि जीवित कोशिका का नाभिक इन जन्मजात गुणों, के लिए उत्तरदायी हैं, जिसे आनुवांशिकता भी कहते हैं। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लीक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लीक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लीक अम्ल (DNA) तथा राइबोसन्यूक्लीक अम्ल (RNA)। चूँकि न्यूक्लीक अम्ल न्यूक्लिओटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं अतः इन्हें पॉलिन्यूक्लिओटाइड भी कहते हैं।
10.5.1 न्यूक्लीक अम्लों का रासायनिक संघटन
DNA (अथवा RNA) के पूर्ण जलअपघटन से एक पेन्टोस शर्करा, फ़ास्फ़ोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषमचक्रीय यौगिक (जिन्हें क्षारक कहते हैं) प्राप्त होते हैं। DNA अणु में शर्करा अर्धांश इकाई


जेम्स डेवे वाटसन

डॉ. वाटसन का जन्म शिकागो के इलिनॉयस में वर्ष 1928 में हुआ था। इन्होंने 1950 में प्राणिविज्ञान में इंडियाना विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। उनकी सर्वाधिक ख्याति DNA की संरचना निर्धारित करने के कारण हुई जिसके लिए उन्हें 1962 में शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषध क्षेत्र में फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्किस के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि DNA अणु द्विकुंडलित आकृति ग्रहण करता है जो वास्तव में एक परिष्कृत एवं सरल संरचना है। इसकी तुलना थोड़ी सी मरोड़ी गई सीढ़ी से की जा सकती है जिसकी पार्श्व छड़ें (रेलिंग) एकांतर क्रम में बंधित फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा की इकाइयों द्वारा निर्मित होती हैं जबकि उनके बीच के डंडे प्यूरीन/ पिरिमिडीन क्षारक युगलों द्वारा बनते हैं। इस शोध कार्य ने वास्तव में अणुजैविकी के विकास की नींव रखी। न्यूक्लिओटाइड क्षारकों के पूरक युगलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार जनक DNA की समरूप प्रतिलिपियाँ दो संतति कोशिकाओं में पहुँचती हैं। इस शोध ने जीवविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी जिसके फलस्वरूप आधुनिक पुनर्योगज DNA तकनीक का विकास हो सका।
DNA में चार क्षारक यथा ऐडेनीन (A), ग्वानीन
ऐडेनीन (A)
ग्वानीन (G)
साइटोसीन (C)
थायमीन (
यूरेसिल (U)
10.5.2 न्यूक्लीक अम्ल की संरचना
किसी क्षारक के शर्करा की

(क)

(ख) चित्र 10.5- (क) एक न्यूक्लिओसाइड तथा (ख) एक न्यूक्लिओटाइड की संरचना
न्यूक्लिओटाइड आपस में फ़ॉस्फ़ोडाइएस्टर बंधन द्वारा संयुक्त होते हैं जो पेन्टोस शर्करा के

श्रृंखला का 3’ सिरा चित्र 10.6 - डाइन्यूक्लिओटाइड का बनना
न्यूक्लिक अम्ल की एक शृंखला का सरलतम विवरण नीचे दर्शाया गया है-

न्यूक्लीक अम्ल की एक शृंखला के अनुक्रम से संबंधित सूचना को इसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं। न्यूक्लीक अम्लों की द्वितीयक संरचना भी होती है। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने DNA की द्विकुंडलनी संरचना दी (चित्र 10.7)। न्यूक्लीक अम्ल की दो श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रहती हैं तथा क्षारक युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। दोनों रज्जुक एक-दूसरे की पूरक होती हैं क्योंकि क्षारकों के विशिष्ट युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। ऐडेनीन, थायेमीन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है जबकि साइटोसीन, ग्वानीन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है।
RNA की द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जुक की बनी होती है जो कभी-कभी RNA में उपस्थित एक रज्जुक के स्वयं को मोड़ने से बनती है। RNA अणु तीन प्रकार के होते हैं तथा ये भिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं। इनके नाम संदेशवाहक RNA ( m-RNA) राइबोसोमल RNA (
10.5.3 न्यूक्लीक अम्ल के जैविक कार्य

चित्र 10.7 - डी.एन.ए. की द्विकुंडलनी संरचना रसायन विज्ञान
डी.एन.ए. आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक की तरह जाना जाता है। डी.एन.ए. लाखों वर्षो से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है। कोशिका विभाजन के समय एक DNA अणु स्वप्रतिकरण (Self Replication) में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान DNA रज्जुक का अंतरण होता है।
न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न RNA अणुओं द्वारा होता है। परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश DNA में उपस्थित होता है।
हरगोबिंद खुराना
डॉ. हरगोबिंद खुराना का जन्म 1922 में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर से एम.एससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने प्रोफ़ेसर व्लादिमिर प्रेलॉग के साथ कार्य किया जिन्होंने खुराना के विचारों तथा दर्शन को विज्ञान कर्म तथा प्रयत्न की ओर आमुख किया। 1949 में भारत में कुछ समय ठहरने के पश्चात खुराना वापस इंग्लैंड चले गए तथा वहाँ उन्होंने प्रोफ़ेसर जी.डब्ल्यू. केनर तथा ए.आर. टॉड के साथ कार्य किया। कैंब्रिज, इंग्लैंड में कार्य करते समय उनकी रुचि प्रोटीनों तथा न्यूक्लीक अम्लों में हुई। 1968 में डॉ. खुराना को आनुवांशिक कोड ज्ञात करने के लिए मार्शल निरेनवर्ग तथा रॉबर्ट हॉली के साथ संयुक्त रूप से औषध तथा भौतिक चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
डीडनड अंगुलि छापन (DNA Fingerprinting)
यह ज्ञात है कि प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुलि छाप होते हैं। ये अंगुलि के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता रहा, लेकिन इन्हें शल्य चिकित्सा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में DNA के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना DNA अंगुली छाप कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। DNA अंगुली छाप का उपयोग आजकल-
(i) विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में होता है।
(ii) किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में होता है।
(iii) किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों अथवा जनक के DNA की तुलना करके किया जाता है, तथा
(iv) जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान में होता है।
10.6 हर्मोन
हॉर्मोन वह अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं। यह शरीर में अंतः-स्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जो इन्हें कार्य स्थल तक पहुँचा देती है।
रासायनिक प्रकृति के अनुसार इनमें से कुछ स्टेरॉयड होते हैं, उदाहरणार्थ, एस्ट्रोजन और ऐन्ड्रोजन; इन्सुलिन और एन्डोर्फिन जैसे कुछ हॉर्मोन पॉलिपेप्टाइड होते हैं तथा कुछ अन्य ऐमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, उदाहरणार्थ एपिनेफरिन एवं नॉरएपिनेफरिन।
शरीर में हॉर्मोनों के अनेक कार्य हैं। यह शरीर में जैविक क्रियाकलाप में संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। रक्त में ग्लूकोस की मात्रा को सीमित रखने में इन्सुलिन की भूमिका इसका उदाहरण है। रक्त में ग्लूकोस की मात्रा तेजी से बढ़ने पर इन्सुलिन निकलने लगती है। दूसरी ओर हार्मोन ग्लूकागॉन की प्रवृत्ति रक्त में ग्लूकोस की मात्रा बढ़ाने की होती है। एक साथ ये दोनों हॉर्मोन रक्त में ग्लूकोस की मात्रा नियंत्रित करते हैं। एपिनेफरिन और नॉरएपिनेफरिन बाहय उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं। वृद्धि-हॉर्मोन और जनन-हॉर्मोन वृद्धि तथा विकास में भूमिका निभाते हैं। थायराइड ग्रंथी में बनने वाली थायरॉक्सिन, ऐमीनो अम्ल टायरोसिन का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होती है। थायरॉक्सिन की मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर अवअवटुता (हाइपोथायराइडिज्म) हो जाती है जो अकर्मण्यता और मोटापे से अभिलक्षणित होती है। थायरॉक्सिन की बढ़ी हुर्ह मात्रा से अतिअवटुता (हाइपरथयरॉयडिज़्म) हो जाती है। आहार में आयोडीन की कमी अवअवटुता और थायराइड ग्रन्थि के बढ़ने का कारण बन सकती है। अधिकतर इस स्थिति को खाने वाले नमक में सोडियम आयोडाइड मिलाकर (आयोडाइज्ड सॉल्ट) नियंत्रित किया जाता है।
स्टेरॉयड हॉर्मोन ऐड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनैड ग्रन्थियों (पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में डिम्बग्रन्थि) में बनते हैं। ऐड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन शरीरिक कार्यकलापों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरणार्थ ग्लूकोकॉर्टिकायड कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करते हैं, जलन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को घटाते हैं एवं तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में भी सम्मिलित होते हैं। मिनरैलोकॉर्टिकॉयड गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यदि ऐड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य न करें तो इसके परिणामस्वरूप ऐडीसन्सडिज़ीज हो सकती है जिसके अभिलक्षण हैं हाइपोग्लाइसीमिया, दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता की संभावना बढ़ना। यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉयड और मिनरैलोकॉर्टिकायड से इलाज न हो तो यह रोग घातक हो सकता है। गोनैडों से निकलने वाले
हॉर्मोन गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। टेस्टोस्टीरॉन पुरुषों के लक्षण जैसे-आवाज़ में भारीपन, चेहरे पर बाल और सामान्य शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होता है। एस्ट्राडाइऑल महिलाओं का प्रमुख हॉर्मोन है। यह महिलाओं में गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है और रजोधर्म के नियंत्रण में भागीदार होता है। प्रोजेस्टीरॉन, निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है।
सारांश
कार्बोडाइड्रेट, ध्रुवण घूर्णक पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन, अथवा वे अणु होते हैं, जिनके जल अपघटन पर इस प्रकार की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है- मोनोसैकैराइड, डाइसैकैराइड, पॉलिसैकैराइड। ग्लूकोस जो कि स्तनधारियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, स्टार्च के पाचन से प्राप्त होता है। मोनोसैकेराइड, ग्लाकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर डाइसैकेराइड तथा पॉलिसैकेराइड बनाते हैं।
प्रोटीन लगभग बीस विभिन्न
विटामिन आहार में आवश्यक सहायक भोज्य कारक हैं। इन्हें वसा विलेय (A, D, E तथा
न्यूक्लीक अम्ल, न्यूक्लिओटाइडों के बहुलक हैं जो एक क्षारक, एक पेन्टोस शर्करा तथा एक फ़ास्फेट अर्धांश से मिलकर बनता है। न्यूक्लीक अम्ल जनक से संतति में गुणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं- DNA तथा RNA। इनमें से DNA में पाँच कार्बन परमाणु वाला शर्करा अणु होता है जिसे 2 -डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, जबकि RNA में राइबोस शर्करा होती है। DNA तथा RNA दोनों में ऐडेनीन, ग्वानीन तथा साइटोसीन क्षारक होते हैं। चतुर्थ क्षारक DNA में थायमीन तथा RNA में यूरेसिल होता है। DNA की संरचना द्विरज्जुक द्विकुंडलनी है जबकि RNA की संरचना एक रज्जुक कुंडलनी होती है। DNA आनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है। तथा इनमें किसी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कोडित संदेश होता है RNA तीन प्रकार के होते हैं। - mRNA, r-RNA तथा t-RNA, जो कि वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं।