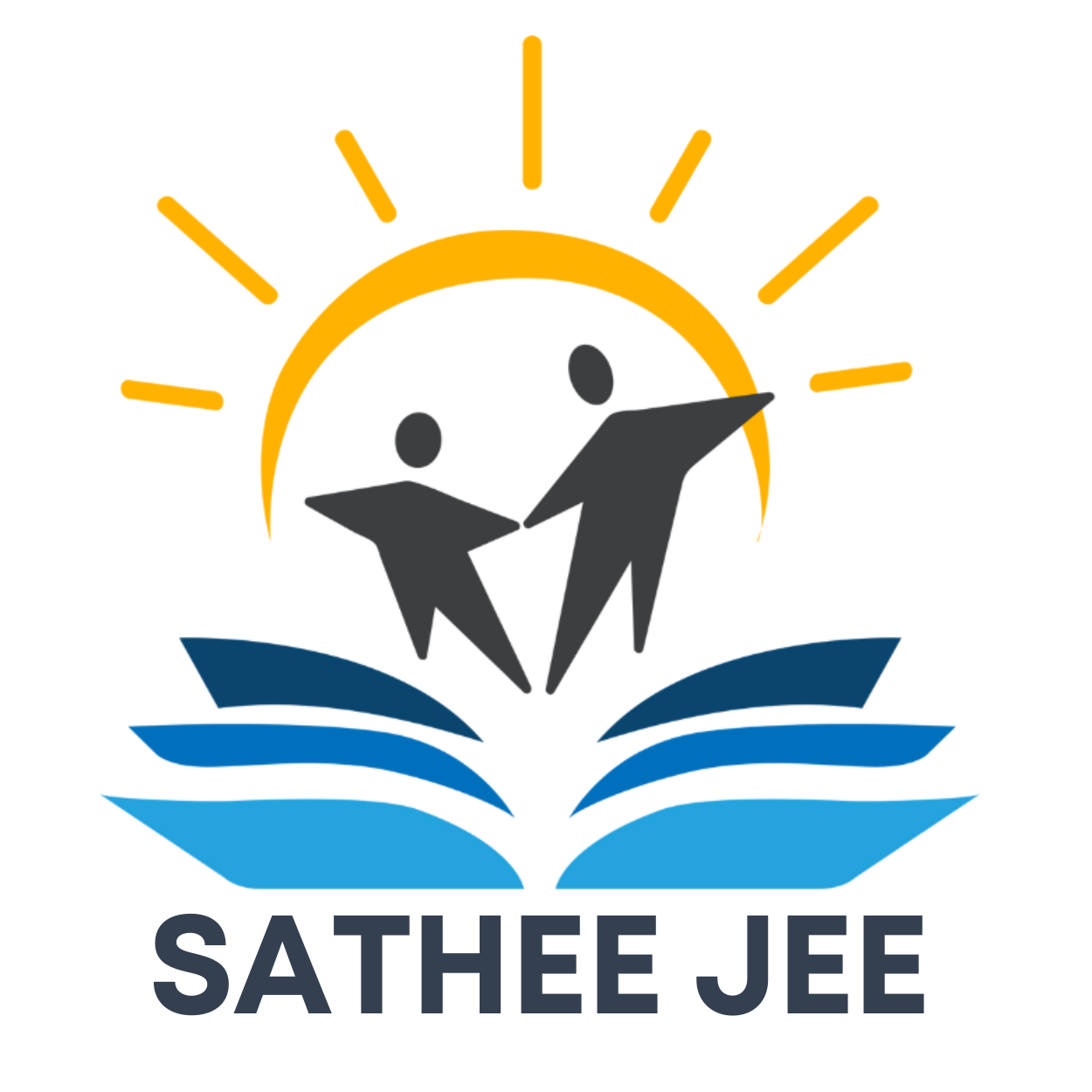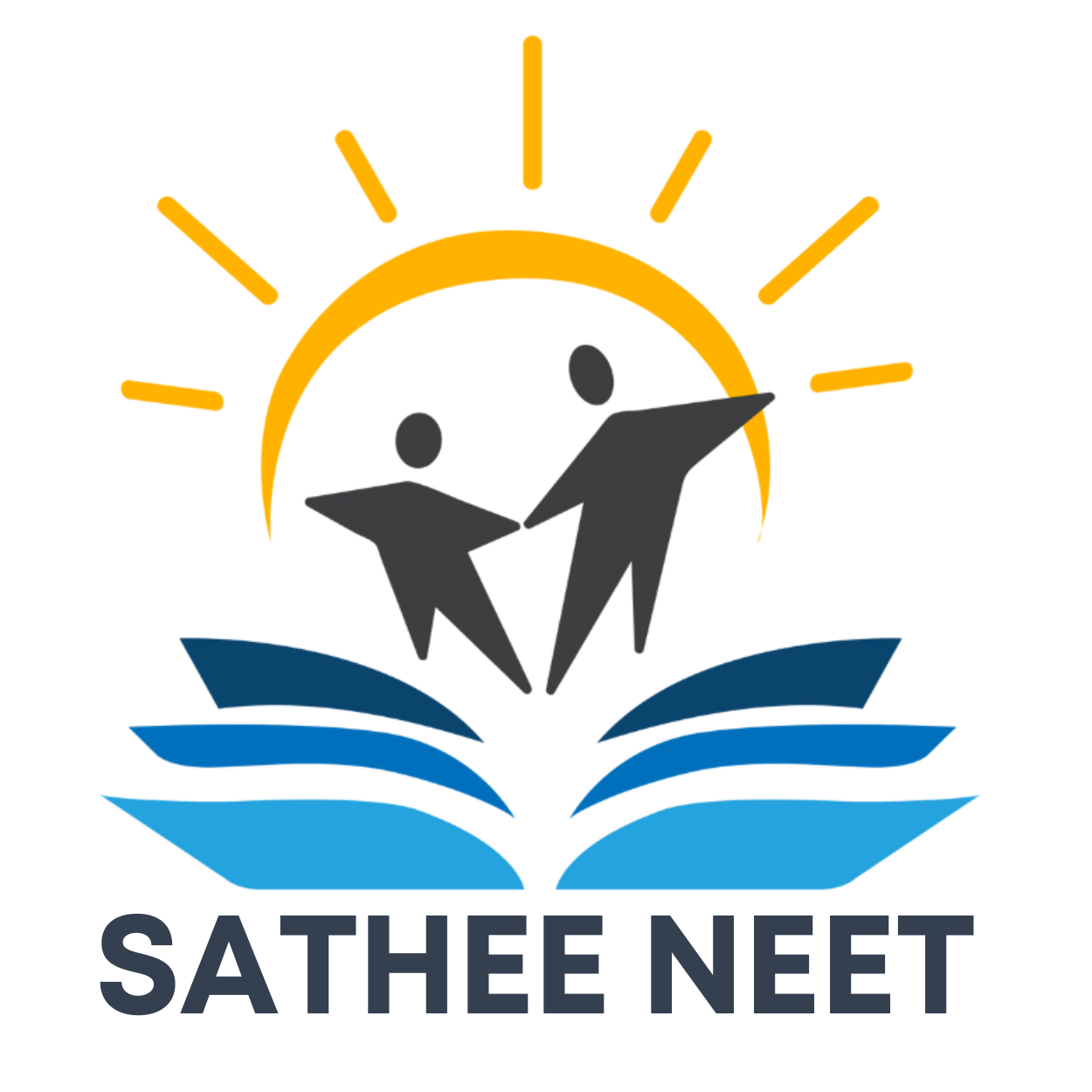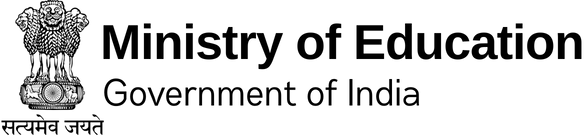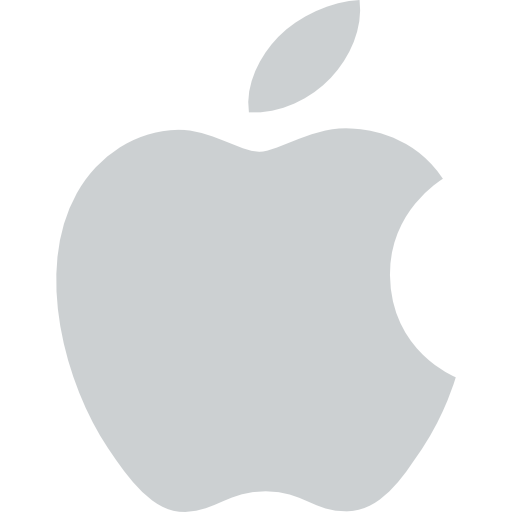श्वसन और गैसों का विनिमय
जैसाकि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे- ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन
14.1 श्वसन के अंग
प्राणियों के विभिन्न वर्गो के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सीलंटेरेटा चपटेकृमि आदि
में विभिन्न स्थान पर पहुँचती है; ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान-प्रदान कर सकें। जलीय आर्थोपोडा तथा मौलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम (गिल) द्वारा होता है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली फुप्फुस/फेफड़े द्वारा होता है। कशेरुकों में मछलियाँ क्लोम (गिल) द्वारा श्वसन करती हैं जबकि एम्फबिया (उभयचर), सरीसृप,पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा (नम त्वचा) द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है।
14.1.1 मानव श्वसन तंत्र
हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं, जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुँचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वासनली में खुलती है। कंठ एक उपास्थिमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है इसीलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाँटी एक पतली लोचदार उपास्थिल पल्ले/फ्लैप कंठच्छद (epiglottis) से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वासनली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5 वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाई और बाई दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनी, श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती हैं। श्वासनली, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थिल वलयों से आलंबित होती हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायित थैली जैसी संरचना कूपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कूपिका कहते हैं। श्वसनी, श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों (lungs) की रचना करते हैं (चित्र 14.1)। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुप्फुसावरण (pleura) से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुसावरणी द्रव भरा होता है। यह फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुप्फुसावरणी झिल्ली वक्षीय पर्त के निकट संपर्क में रहती है; जबकि आंतरिक फुप्फुसावरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है।
बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग; जबकि कूपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग (आदान-प्रदान इकाई) रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच
फेफड़े वक्ष-गुहा में स्थित होते हैं जो शारीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष-गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थि, पार्श्व में पसलियों और नीचे से गुंबदाकर डायाफ्राम (diaphragm) द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े (फुप्फुसी) की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है।

चित्र 14.1 मानव श्वसन तंत्र का आरेखीय दृश्य (साथ ही बाएं फेफड़े का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है)
श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं:
(i) श्वसन या फुप्फुसी संवातन जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और
(ii) कूपिका झिल्ली के आर-पार गैसों
(iii) रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन (अभिगमन)
(iv) रुधिर और ऊतकों के बीच
(v) अपचयी क्रियायों के लिए कोशिकाओं द्वारा
14.2 श्वासन की क्रियाविधि
श्वासन में दो चरण सम्मिलित हैं: अंतः श्वसन जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खीचा जाता है और नि:श्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है।
अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब (आंतर फुप्फुसी दाब) कम हो अर्थात् फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह नि:श्वसन तब होता है, जब आंतर फुप्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से

(अ)

(ब)
14.2.1 श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं
ज्वारीय आयतन (Tidal Volume/ TV): सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतः श्वासित या नि:श्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिली. होता है अर्थात् स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिली. वायु प्रति मिनट की दर से अंतः श्वासित/निःश्वासित कर सकता है।
अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन ( Inspiratory Reserve Volume IRV ): वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वासित कर सकता है। यह औसतन 2500 मिली. से 3000 मिली. होता है।
नि:श्वसन सुरक्षित आयतन ( Expiratory reserve volume, ERV ): वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक नि:श्वासित कर सकता है। औसतन यह 1000 मिली. से 1100 मिली. होती है।
अवशिष्ट आयतन (Residual Volume RV): वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका औसत 1100 मिली. से 1200 मिली. होता है।
ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुप्फुसी क्षमताएं (फुप्फुसी धारिताएं) निकाली जा सकती हैं जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है।
अंतःश्वसन क्षमता (Inspiratory Capacity, IC ): सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा (आयतन)जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है (TV+IRV)।
नि:श्वसन क्षमता (Expiratory Capacity, EC ): सामान्य अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा (आयतन) जिसे एक व्यक्ति नि:श्वासित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन और नि:श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं (TV+ERV)।
क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता (Functional Residual Capacity, FRC ): सामान्य नि:श्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा (आयतन)जो फेफड़ों में शेष रह जाती है। इसमें नि:श्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं
जैव क्षमता (Vital Capacity, VC): बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा (आयतन)जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है। इसमें
फेफड़ों की कुल क्षमता ( Total Lung Capacity, TLC ): बलपूर्वक नि:श्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित (उपस्थित) वायु की कुल मात्रा । इसमें RV,ERV,TV और
14.3 गैसों का विनिमय
कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर

चित्र 14.3 वायु कूपिका एवं शरीर ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय जो ऑक्सीजन तथा कार्बन-डाइऑक्साइड का रक्त के साथ वहन का आरेखीय चित्र
गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बनडाइऑक्साइड के लिए क्रमशः
तालिका 14.1 वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों पर ऑक्सीजन एवं कार्बनडाइऑक्साइड का आंशिक दबाव (
| श्वसन | वातावरणीय वायु | वायु कूपिका | अनॉक्सीकृत रक्त | ऑक्सीकृत रक्त | ऊतक |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 104 | 40 | 95 | 40 | |
| 0.3 | 40 | 45 | 40 | 45 |
घुलनशीलता से
14.4 गैसों का परिवहन (Transport of Gases )
14.4.1 ऑक्सीजन का परिवहन (Transport of Oxygen)
हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौहयुक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय (Rerersible) ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी-हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम चार

चित्र 14.5 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र
निम्न तापक्रम होता है, वहाँ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं जबकि ऊतकों में निम्न
14.4.2 कार्बनडाइऑक्साइड का परिवहन
कार्बनडाइऑक्साइड
ऊतकों में अपचय के कारण
14.5 श्वसन का नियमन (Regulation of Respiration)
मानव में अपने शरीर के ऊतकों की माँग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेड्यूला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लयकेंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोंस क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वासप्रभावी (श्वास अनुचन) (Pneumotaxic) केंद्र कहते हैं जो श्वसन लयकेंद्र के कार्यों को संयत (सुधार) कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर (Respiratory rate) को परिवर्तित कर सकते हैं। लयकेंद्र के पास एक रसोसंवेदी (Chemosensitive) केंद्र लयकेंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो
हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थो की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें। महाधमनी चाप (Aortic arch) और ग्रीवा धमनी (Carotid artery) से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी
14.6 श्वसन के विकार (Respiratory disorders)
दमा (Asthma) में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वासन के समय घरघरहाट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है।
श्वसनी शोथ (Bronchitis) : यह श्वसनी की शोथ है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना है जिससे लगातार खाँसी होती है।
वातस्फीति या एम्फाइसिमा(Emphysema) : एक चिरकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक है।
व्यावसायिक श्वसन रोग (Occupational Respiratory Disease) : कुछ उद्योगों में विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई - पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है जिनसे रेशामयता (रेशीय ऊतकों की प्रचुरता) होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए।
सारांश
कोशिकाएं अपापचयी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा ऊर्जा के साथ कार्बनडाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न करती हैं। प्राणियों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं वहाँ से कार्बनडाइऑक्साइड को भी बाहर करने के लिए कई तरह की क्रियाविधि विकसित हैं और जिनमें हमारे पास इस क्रिया के लिए एक पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र है जिसके अंतर्गत दो फेफड़े और इनसे जुड़े वायु मार्ग है।
श्वसन का पहला चरण श्वासन है जिसमें वायुमंडलीय वायु कूपिकाओं में ली जाती है (अंतःश्वसन)और कूपिकाओं से वायु को बाहर निकाला जाता है (नि:श्वसन)। ऑक्सीजनित रहित रक्त और कूपिका के बीच
ऑक्सीजन का मुख्य रूप से ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है कूपिका में जहाँ
श्वसन लय मस्तिष्क के मेड्यूला क्षेत्र स्थित श्वसन केंद्र द्वारा बनाए रखी जाती है। मस्तिष्क के पोंस क्षेत्र स्थित श्वास अनुचन श्वास प्रभावी (न्यूमोटैक्सिक) केंद्र तथा एक रसो संवेदी क्षेत्र श्वसन क्रियाविधि को परिवर्तित कर सकते हैं।