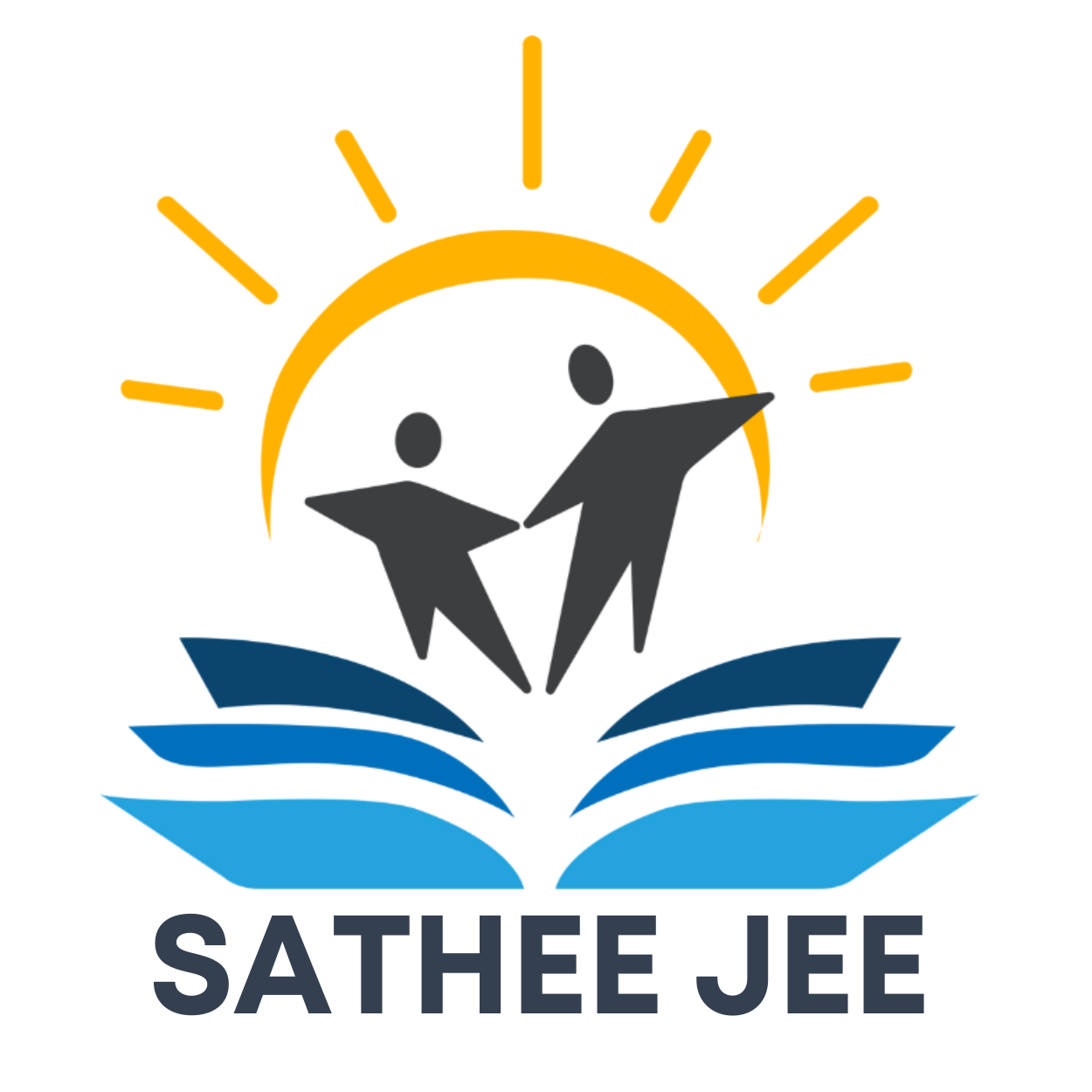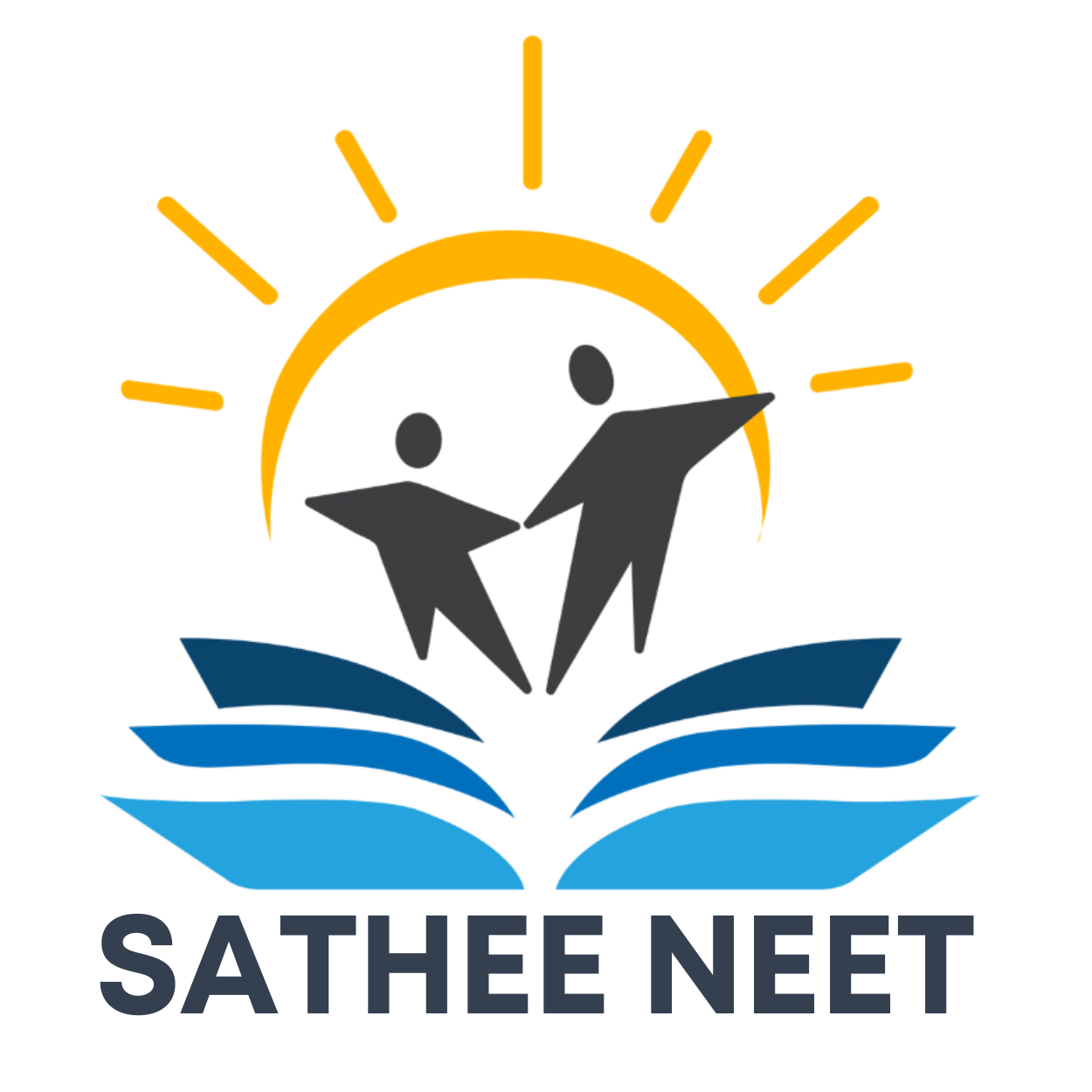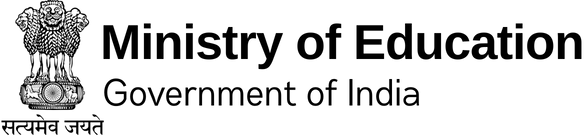अध्याय 06 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
जैसाकि आपने अध्याय 3 व 4 में पढ़ा है परिवार से लेकर बाज़ार तक की विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएँ लोगों को परस्पर संपर्क में ला सकती हैं, उनमें प्रबल सामूहिक पहचान स्थापित कर सकती हैं और सामाजिक संसक्ति या जुड़ाव को मज़ूूत बना सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर, जैसाकि अध्याय 4 व 5 में बताया गया है, यह समान संस्थाएँ असमानता और अपवर्जन या बहिष्कार की स्रोत भी हो सकती हैं। प्रस्तुत अध्याय में आप इस सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कुछ तनावों एवं कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। ‘सांस्कृतिक विविधता’ का सही-सही अर्थ क्या है और इसे चुनौती के रूप में क्यों देखा जाता है?
‘विविधता’ शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। यह समुदाय सांस्कृतिक चिह्नों जैसे, भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जब यह विविध समुदाय भी किसी बड़े सत्व जैसे एक राष्ट्र का भाग होते हैं तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
इसी कारण से सांस्कृतिक विविधता कठोर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं। कठिनाइयाँ इस तथ्य से भी उत्पन्न होती हैं कि सांस्कृतिक पहचानें बहुत प्रबल होती हैं, वे तीव्र भावावेशों को भड़का सकती हैं और अक्सर बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर देती हैं। कभी-कभी सांस्कृतिक अंतरों के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ भी जुड़ जाती हैं और तब स्थिति और भी जटिल हो जाती है। एक समुदाय द्वारा भुगती जा रही असमानताओं या अन्यायों को दूर करने के लिए किए गए उपाय दूसरे समुदायों में उनके प्रति विरोध को भड़का सकते हैं। स्थिति उस समय और भी बिगड़ जाती है जब नदी जल, रोजगार के अवसर या सरकारी धनराशियों जैसे दुर्लभ संसाधनों के बँटवारें का सवाल खड़ा होता है।
सामुदायिक पहचान का महत्त्व
इस संसार में अपना अस्तित्व सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एक स्थायी पहचान की जरूरत होती है। मैं कौन हूँ? मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? अन्य लोग मुझे कैसे जानते एवं समझते हैं? मेरी आकांक्षाएँ या लक्ष्य क्या होने चाहिए? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे जीवन में बचपन से लेकर आगे तक लगातार उपस्थित होते रहते हैं। हमारा समाजीकरण जिस तरीके से हुआ है या विभिन्न अर्थों में हमें हमारे निकटवर्ती परिवारों अथवा हमारे समुदाय द्वारा समाज में किस प्रकार रहना सिखाया गया है इसकी वजह से हम इनमें से अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होते हैं। (अपनी ग्यारहवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में समाजीकरण विषय पर की गई चर्चा को याद करें)। समाजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी विस्तृत एवं लंबी होती है जिसमें कुछ विशेष लोगों के साथ (जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं) लगातार संवाद, वार्तालाप और कभी-कभी संघर्ष भी होता रहता है जैसे कि हमारे माता-पिता, परिवार, नातेदार समूह एवं हमारा समुदाय। हमारा समुदाय हमें भाषा (मातृभाषा) और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है जिनके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं। यह हमारी स्वयं की पहचान को भी सहारा देता है।
सामुदायिक पहचान, जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, न कि किसी अर्जित योग्यता या ‘उपलब्धि’ के आधार पर। यह ‘हम क्या हैं’ इस भाव की द्योतक है न कि ‘हम क्या बन गए हैं। किसी समुदाय में जन्म लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। सच तो यह है कि किसी परिवार या समुदाय अथवा देश में जन्म लेने पर हमारा कोई वश नहीं है। इस प्रकार की पहचानें ‘प्रदत्त’ कही जाती हैं अर्थात्
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
ये जन्म से निर्धारित होती हैं और संबंधित व्यक्तियों की पसंद या नापसंद इसमें शामिल नहीं होती। सामाजिक जीवन का यह एक अजीब तथ्य है कि लोग उन समुदायों से संबंधित होकर अत्यंत सुरक्षित एवं संतुष्ट महसूस करते हैं जिनमें उनकी सदस्यता पूरी तरह जन्म पर आधारित होती है। हम अक्सर ऐसे समुदाय के साथ अपनी पहचान मज़बूती से स्थापित कर लेते हैं जिसकी सदस्यता के योग्य होने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, कोई परीक्षा पास नहीं की, कोई कुशलता या योग्यता प्रदर्शित नहीं की….। डॉक्टरों या वास्तुकारों को परीक्षाएँ पास करनी होती हैं और अपनी योग्यता का परिचय देना होता है, यहाँ तक कि खेलकूद में भी, एक दल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित स्तर का कौशल प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। लेकिन हमारे परिवारों या धार्मिक अथवा क्षेत्रीय समुदायों की सदस्यता के लिए ऐसा नहीं होता, फिर भी हमारी सदस्यता संपूर्ण होती है। वास्तव में, अधिकांश प्रदत्त पहचानें इतनी पक्की होती हैं कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता; भले ही हम उन्हें अस्वीकार करने की कोशिश करें तब भी दूसरे लोग शायद उन्हीं चिह्नों से जोड़कर हमारी पहचान करते रहेंगे।
संभवतः इस आकस्मिक, शर्त रहित अथवा लगभग अनिवारणीय तरीके से संबंधित होने के कारण ही हम अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान से भावनात्मक रूप से इतना गहरे जुड़े होते हैं। सामुदायिक संबंधों (परिवार, नातेदारी, जाति, नृजातीयता, भाषा, क्षेत्र या धर्म) के बढ़ते हुए और परस्परव्यापी दायरे ही हमारी दुनिया को सार्थकता प्रदान करते हैं और हमें एक पहचान प्रदान करते हैं कि हम कौन हैं। इसीलिए लोग अक्सर उस समय भावुक होकर अथवा कभी हिंसापूर्वक भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं जब उन्हें अपनी सामुदायिक पहचान को कोई खतरा दिखाई देता है।
प्रदत्त पहचानों और सामुदायिक भावना की एक दूसरी विशेषता यह होती है कि वे सर्वव्यापी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की एक मातृभूमि होती है, एक मातृभाषा होती है, उसका एक परिवार होता है और निष्ठा भी होती है…। हो सकता है कि यह बात प्रत्येक व्यक्ति पर पूरी तरह लागू न होती हो पर आमतौर पर ऐसा होता है और हम सब अपनी-अपनी पहचानों के प्रति समानरूप से प्रतिबद्ध एवं वफादार होते हैं। एक बार फिर यह संभव है कि शायद हमें ऐसे लोग भी मिलें जो अपनी पहचान के किसी एक या अन्य पक्ष के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध न हों। लेकिन इस प्रतिबद्धता की संभावना लगभग अधिकांश लोगों में पाई जाती है। इसी कारण, हमारे समुदायों (चाहें राष्ट्र, भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र विषयक) के बीच पैदा होने वाले लड़ाई-झगड़ों या विवादों को निपटाना बहुत कठिन होता है। विवाद का प्रत्येक पक्ष सामने वाले पक्ष को शत्रु मानते हुए घृणा की दृष्टि से देखता है और उसमें अपने पक्ष के गुणों को और विरोधी पक्ष के दुर्गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए जब दो राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो प्रत्येक राष्ट्र के देशभक्त लोग विरोधी राष्ट्र को आक्रमणकारी शत्रु मानते हैं। प्रत्येक पक्ष यह विश्वास करता है कि हम सच्चे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। गरमागरमी के क्षण में दोनों ही पक्षों के लोगों के लिए यह देखना बहुत कठिन होता है कि जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे भी तो हमारे बारे में वैसा ही सोच रहे हैं।
समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र-राज्य
सरल शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्र एक तरह का बड़े स्तर का समुदाय ही होता है, यह समुदायों से
मिलकर बना एक समुदाय है। राष्ट्र के सदस्य एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छारखते हैं। राजनीतिक एकता की यह इच्छा स्वयं को एक राज्य बनाने की आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त होती है। अपने सर्वाधिक सामान्य भाव में राज्य शब्द का अर्थ एक ऐसा अमूर्त सत्व होता है जिसमें राजनीतिक-विधिक संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं और वह एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर और उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियंत्रण रखता है। मैक्स वेबर की सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार, राज्य “एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधिसम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है” (वेबर 1970:78)।
राष्ट्र एक अनूटे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना कठिन है। हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे - धर्म, भाषा, नृजातीयता, इतिहास अथवा क्षेत्रीय संस्कृति जैसी साझी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। लेकिन किसी ऐसे पारिभाषिक लक्षणों को निर्धारित करना अथवा उन विशेषताओं का पता लगाना कठिन है जो एक राष्ट्र में होनी ही चाहिए। प्रत्येक संभव कसौटी के लिए अनेक अपवाद और विरोधी उदाहरण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या सामान्य भाषा, धर्म, नृजातीयता आदि नहीं हैं। दूसरी ओर ऐसी अनेक भाषाएँ, धर्म या नृजातियाँ हैं जो कई राष्ट्रों में पाई जाती हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं उदाहरण के लिए, सभी अंग्रेज़ी भाषी लोग या सभी बौद्धधर्मावलंबी।
तब हम एक राष्ट्र और अन्य प्रकार के समुदायों जैसे, एक नृजातीय समूह (जो सामान्य भाषा या संस्कृति के अलावा एक ही वंशपरंपरा पर आधारित हों), धार्मिक समुदाय अथवा क्षेत्रीय आधार पर परिभाषित समुदाय आदि के बीच कैसे भेद कर सकते हैं? संकल्पना की दृष्टि से तो कोई पक्का भेद दिखाई नहीं देता, अन्य प्रकार का कोई भी समुदाय किसी दिन एक राष्ट्र बन सकता है। विलोमतः किसी भी विशेष प्रकार के समुदाय के लिए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह राष्ट्र का रूप ग्रहण कर लेगा।
राष्ट्र का अंतर या भेद दर्शाने वाली सबसे नजदीकी कसौटी राज्य है। पहले बताए गए अन्य प्रकार के समुदायों के विपरीत, राष्ट्र ऐसे समुदाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है। इसीलिए ये दोनों राष्ट्र-राज्य शब्द के रूप में योजक-चिह्न से जुड़े होते हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हाल के समय में राष्ट्र और राज्य के बीच ‘एकैक’ (एक-एक का) संबंध है। (एक राष्ट्र, एक राज्य; एक राज्य, एक राष्ट्र)। लेकिन यह एक नया विकास है। पहले यह बात सच नहीं थी कि एक अकेला राज्य केवल एक ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकता था यानी एक ही राष्ट्र का द्योतक था या प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राज्य होना जरूरी था। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ ने अपने अस्तित्व काल में यह स्पष्ट रूप से मान रखा था कि जिन लोगों पर उसका शासन था वे विभिन्न ‘राष्ट्रों’ के थे और उसने एक सौ से भी अधिक आंतरिक राष्ट्रीयताओं को मान्यता दे रखी थी। इसी प्रकार, एक राष्ट्र को अस्तित्व प्रदान करने वाले लोग हो सकता है विभिन्न राज्यों के नागरिक या निवासी हों। उदाहरण के लिए, संपूर्ण जमैकाइयों (जमैकावासियों) में से जमैका से बाहर रहने वालों की संख्या, जमैका के भीतर रहने वाले जमैकाइयों से अधिक है यानी ‘अनिवासी’ जमैकाइयों की संख्या ‘निवासी’ जमैकाइयों की जनसंख्या से अधिक है। ‘दोहरी नागरिकता’ संबंधी कानून एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये कानून किसी राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक दूसरे राज्य का नागरिक बनने की इजाजजत देते हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यहूदी जाति के अमेरिकी लोग एक साथ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के नागरिक
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
हो सकते हैं; यहाँ तक कि वे इन दोनों में से किसी भी एक देश की सशस्त्र सेनाओं में दूसरे देश की नागरिकता खोए बगरर सेवा कर सकते हैं।
संक्षेप में, आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना बहुत कठिन है और इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसके विपरीत रूप भी अधिकाधिक सच हो गए हैं। जिस प्रकार आज भावी अथवा आकांक्षी राष्ट्रीयताएँ अपना राज्य बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील हैं, वैसे ही मौजूदा राज्य यह दावा करना ज़्यादा-से-ज़्यादा

ज़रूरी मान रहे हैं कि वे एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक युग (आपकी कक्षा ग्यारहवीं की पाठ्यपुस्तक समाज का बोध के अध्याय 4 में आधुनिकता पर की गई चर्चा को याद करें) का एक विशिष्ट लक्षण है राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की स्थापना। इसका अर्थ यह है कि आज एक राज्य के लिए ‘राष्ट्र’ एक सर्वाधिक स्वीकृत अथवा औचित्यपूर्ण आवश्यकता है, जबकि ‘लोग’ राष्ट्र की वैधता के चरम स्रोत हैं। दूसरे शब्दों में, राज्यों को राष्ट्र की उतनी ही या उससे भी अधिक ‘आवश्यकता’ होती है जितनी कि राष्ट्रों को राज्यों की।
लेकिन, जैसाकि हमने पूर्ववर्ती पैराग्राफ़ों में देखा है एक राज्य-राष्ट्र और समुदाय के उन विविध रूपों के बीच, जिन पर राज्य-राष्ट्र आधारित हो सकता है ऐतिहासिक दृष्टि से कोई निश्चित और तार्किक आवश्यक संबंध नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न का कोई पूर्व-निर्धारित उत्तर नहीं है: राष्ट्र-राज्य के ‘राज्य’ भाग को उन विभिन्न प्रकारों के समुदायों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए जो ‘राष्ट्र’ भाग को बनाते हैं? जैसाकि बॉक्स 6.2 में दिखाया गया है (जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संस्कृति एवं लोकतंत्र विषय पर 2004 की एक रिपोर्ट पर आधारित है), अधिकांश राज्य आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के प्रति शंकालु रहे हैं और उन्होंने उसे कम करने या मिटाने की कोशिशें की हैं। तथापि अनेक सफल उदाहरण हैं, जिनमें भारत भी एक है जो यह दर्शाते हैं कि विभिन्न प्रकार की सामुदायिक पहचानों को एक मानक प्रकार में ‘समरूप’ किए बिना भी एक मज़बूत राष्ट्र-राज्य बनना पूरी तरह संभव है।
बॉक्स 6.1 में ‘आत्मसात्करणवादी’ और ‘एकीकरणवादी’ नीतियों का उल्लेख किया गया है। आत्मसात्करण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का उद्देश्य सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को अपनाने के लिए राजी, प्रोत्साहित या मजबूर करना है। यह मूल्य तथा मानक आमतौर पर संपूर्ण रूप से या अधिकांशतः प्रभावशाली सामाजिक समूह के होते हैं। समाज में अन्य अप्रभावशाली अथवा अधीनस्थ बनाए गए समूहों से यह आशा अथवा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ दें और निर्धारित मूल्यों को अपना लें। एकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ शैली 107 की दृष्टि से तो अलग होती हैं पर उनका सर्वोपरि उद्देश्य भिन्न नहीं होता, वे इस बात पर बल देती हैं
सामुदायिक पहचानों के डर से राज्यों द्वारा सांस्कृतिक विविधता को मिटाने की कोशिश
ऐतिहासिक तौर पर राज्यों ने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने और उसे और ज़्यादा बढ़ाने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने आत्मसात्करण और एकीकरण की नीतियों के जरिए अपने नागरिकों की देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना खासतौर पर सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में आसान नहीं था क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में नागरिक अपने देश के साथ अपनत्व रखने के साथ-साथ संभवतः अपने नृजातीय, धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य किसी प्रकार के समुदाय के साथ भी गहरा तादात्म्य रखते हैं।
अधिकांश राज्यों को यह डर था कि इस अंतर को मान्यता प्रदान किए जाने से सामजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समरसतापूर्ण समाज के निर्माण में रुकावट आएगी। संक्षेप में, इस प्रकार की पहचान संबंधी राजनीति राज्य की एकता के लिए खतरा समझी गई। इसके अलावा, इस प्रकार के अंतरों का समायोजन करना राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए अनेक राज्यों ने इन विविध पहचानों को राजनीतिक स्तर पर दबाया या नज़रअंदाज़ किया।
आत्मसात्करण की नीतियाँ, जिनके अंतर्गत अक्सर नृजातीय, धार्मिक या भाषाई समूहों की पहचानों को एकदम दबा दिया जाता है, समूहों के बीच पायी जाने वाली सांस्कृतिक विभिन्नताओं को मिटाने की कोशिश करती हैं। एकीकरण की नीतियाँ केवल एक अकेली राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना चाहती हैं जिसके लिए वे सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्यक्षेत्रों से नृजातीय-राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दूर करने का प्रयत्न करती हैं लेकिन निजी क्षेत्रों में इन्हें बनाए रखने की इजाजत देती हैं। ये दोनों प्रकार की नीतियों के समुच्चय एक अकेली राष्ट्रीय पहचान को अपनाते हैं।
बॉक्स 6.1
आत्मसात्करणवादी और एकीकरणवादी रणनीतियाँ विभिन्न अंतः क्षेपी उपायों द्वारा एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती हैं जैसे:
संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंचों में केंद्रित करना जहाँ प्रभावशाली समूह बहुसंख्यक हों और स्थानीय या अल्पसंख्यक समूहों की स्वायत्तता को मिटाना;
प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एक एकीकृत कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना और अन्य समूहों द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देना;
प्रभावशाली समूह की भाषा को ही एकमात्र राजकीय ‘राष्ट्रभाषा’ के रूप में अपनाना और उसके प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य बना देना;
प्रभावशाली समूह की भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए, जिनमें राज्य नियंत्रित जनसंपर्क के माध्यम और शैक्षिक संस्थाएँ शामिल हैं, बढ़ावा देना;
प प्रभावशाली समूह के इतिहास, शूरवीरों और संस्कृति को सम्मान प्रदान करने वाले राज्य प्रतीकों को अपनाना, राष्ट्रीय पर्व, छुट्री या सड़कों आदि के नाम निर्धारित करते समय भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना;
अल्पसंख्यक समूहों और देशज लोगों से जमीनें, जंगल एवं मत्स्य क्षेत्र छीनकर, उन्हें ‘राष्ट्रीय संसाधन’ घोषित कर देन..
स्रोतः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2004, अध्याय 3 , फीचर 3.1 से यथोचित परिवर्तनों के साथ उद्धृत
कि सार्वजनिक संस्कृति को सामान्य राष्ट्रीय स्वरूप तक सीमित रखा जाए, जबकि सभी ‘गैर-राष्ट्रीय’ संस्कृतियों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाए। इस मामले में भी प्रभावशाली समूहों की संस्कृति को ‘राष्ट्रीय संस्कृति’ माने जाने का खतरा रहता है।
अब तक आप लोग संभवतः यह जान गए होंगे कि आखिर समस्या क्या है। समुदाय के किसी विशिष्ट रूप और राज्य के आधुनिक रूप के बीच कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। सामुदायिक पहचान के बहुत से आधारों (जैसे, भाषा, धर्म, नृजाति आदि) में से कोई एक आधार राष्ट्र को स्वरूप प्रदान कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन, चूँकि सामुदायिक पहचानें राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य कर सकती हैं इसलिए पहले से विद्यमान राज्य सभी प्रकार की सामुदायिक पहचानों को खतरनाक प्रतिद्वंद्री के रूप में देखते हैं। इसीलिए राज्य आमतौर पर किसी एक समरूप राष्ट्रीय पहचान का इसलिए पक्ष लेते हैं कि वे उसका नियंत्रण एवं प्रबंध कर सकेंगे। किंतु, सांस्कृतिक विविधता का दमन करना बहुत महँगा पड़ सकता है क्योंकि इससे उन अल्पसंख्यक अथवा अधीनस्थ समुदायों का अलगाव हो जाता है जिनकी संस्कृति को ‘गैर-राष्ट्रीय’ मान लिया जाता है। इसके अलावा कोई भी दमनकारी कार्य सामुदायिक पहचान को और गहरा बनाने का विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है इसलिए सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना अथवा कम-से-कम उसे बनाए रखना व्यावहारिक तथा सिद्धांताश्रित दोनों ही दृष्टिकोणों से अच्छी नीति है।
सांस्कृतिक विविधता और भारत राष्ट्र-राज्य के रूप में
भारतीय राष्ट्र-राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या सन् 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार 121.0 करोड़ है। जनसंख्या की
बॉक्स 6.2
राष्ट्रीय एकता के साथ सांस्कृतिक विविधताः एक लोकतांत्रिक ‘राज्य-राष्ट्र’ का निर्माण
तब, राष्ट्र-राज्य का एक विकल्प है: “राज्य-राष्ट्र” जहाँ नृजातीय, धार्मिक, भाषाई या
देशज पहचानों पर आधारित विभिन्न “राष्ट्र” एक अकेली राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शांति और सहयोगपूर्वक एक साथ रह सकते हैं।
वैयक्तिक अध्ययन और विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि बहुसांस्कृतिक राज्यव्यवस्थाओं में स्थायी, सहनशील लोकतंत्रों की स्थापना की जा सकती है। विविध समूहों के सांस्कृतिक अपवर्जन (बहिष्कार) को खत्म करने… और बहुविध तथा पूरक पहचानों का निर्माण करने के लिए स्पष्ट प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। ऐसी प्रतिसंवेदी नीतियाँ विविधता में एकता का निर्माण करने के लिए, ‘हम’ भाव जागृत करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। नागरिक अपने देश तथा अपनी अन्य सांस्कृतिक पहचानों के साथ तादात्म्य स्थापित करने, साझी संस्थाओं में अपना विश्वास बनाने और लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेने तथा उसे समर्थन देने के लिए संस्थाओं तथा राजनीति में अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी लोकतंत्रों को मज़ूत और गहरा बनाने तथा सहनशील ‘राज्य-राष्ट्रों’ का निर्माण करने के प्रमुख कारक हैं।
भारत के संविधान में इस अभिधारणा को स्थान दिया गया है। यद्यपि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है पर लंबेे समय से चल रहे लोकतंत्रों, जिनमें भारत भी एक है, का तुलनात्मक सर्वेक्षण 109 यह दर्शाता है कि अपनी विविधताओं के बावजूद यह एक अत्यंत सशक्त लोकतंत्र है। लेकिन आधुनिक
भारत संपूर्ण देश पर एक अकेली हिंदू पहचान को थोपने के लिए उत्सुक समूहों के उत्थान के साथ, बहुविध एवं पूरक पहचानों को दिए गए संवैधानिक वचनों के प्रति गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। आज भारत में यह खतरे समावेश के भाव को क्षति पहुँचाते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हाल में जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ हुई हैं उनसे भविष्य में सामाजिक मेल-मिलाप की भावनाओं के प्रति गहरी चिंताएँ खड़ी होती हैं और देश के द्वारा पहले प्राप्त की गई उपलब्धियों को ठेस पहुँचाने का खतरा पैदा होता है।
और ये उपलव्धियाँ थोड़ी नहीं काफ़ी अधिक हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के संवैधानिक स्वरूप में भिन्न-भिन्न समूहों के दावों को मान्यता देते हुए अनुकूल प्रतिक्रिया दिखलाई है और अनेक क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राज्य व्यवस्था को संगठित बनाए रखा है। जैसाकि तदात्मीकरण (पहचान), विश्वास और समर्थन के सूचकों के विषय में भारत के कार्य-निष्पादन से पता चलता है (चार्ट 1) इसके नागरिक देश के विविधतापूर्ण और अत्यंत स्तरबद्ध समाज के बावजूद, देश तथा लोकतंत्र के लिए गंभीरतापूर्वक प्रतिबद्ध हैं। जब भारतीय लोकतंत्र के कार्य-निष्पादन की तुलना अन्य लंबे समय से स्थापित एवं संचालित और अधिक संपन्न लोकतंत्रों से की जाती है तो भारत का कार्य-निष्पादन विशेष रूप से प्रभावोत्पादक नजर आता है।
भारत के सामने चुनौती इसलिए है कि उसने लोकतांत्रिक तरीकों से बहुलवाद, संस्थागत समायोजन और द्वंद्र समाधान की परिपाटियों में अपनी प्रतिबद्धता को उत्साहपूर्वक दोहराया है। एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के निर्माण के लिए राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक प्रयासों की कमजोरियों को स्वीकार करना और बहुविध तथा पूरक पहचानों के लोगों को मान्यता देना बहुत ज़ूरी है। पहचान, विश्वास और सर्मथन के माध्यम से समाज के सभी समूहों में समाज के प्रति निष्ठा की भावना जागॄत करने के प्रयत्न भी महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय संसक्ति यह अपेक्षा नहीं करती कि कोई एक अकेली पहचान सब पर थोप दी जाए और विविधता की निंदा की जाए। राज्य-राष्ट्रों के निर्माण की सफल रणनीतियाँ इस विविधता को रचनात्मक रीति से सांस्कृतिक मान्यता की प्रतिसंवेदी नीतियाँ बनाकर समायोजित कर सकती हैं और करती भी हैं। वे राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समरसता (मेल-मिलाप) के दीर्घकालीन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के प्रभावोत्पादक समाधान हैं।
स्रोतः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2004 , अध्याय 3 , फीचर 3.1 से यथोचित परिवर्तनों के साथ उद्धृत

दृष्टि से विश्वभर में इसका स्थान दूसरा है और जल्दी ही यह पहला स्थान प्राप्त करने वाला है। यहाँ के एक अरब (सौ करोड़) से ज़्यादा लोग कुल मिलाकर लगभग 1,632 भिन्न-भिन्न भाषाएँ और बोलियाँ बोलते हैं। इन भाषाओं में से बाईस भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देकर उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, इस प्रकार उन्हें विधिक प्रतिष्ठता की गारंटी दी गई है। जहाँ तक धर्म का सवाल है, यहाँ कि $80 %$ आबादी हिन्दुओं की है, जो स्वयं भी क्षेत्रीय रूप से तरह-तरह के विश्वासों और व्यवहारों तथा जातियों एवं भाषाओं की दृष्टि से बँटे हुए हैं। लगभग $13.4 %$ आबादी मुसलमानों की है जिसकी बदौलत भारत विश्व में इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुसलमान देश है। अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों में ईसाई लगभग $(2.3 %)$, सिख $(1.7 %)$, बौद्ध $(0.7 %)$ और जैन $(0.4 %)$ हैं। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण ये छोटे-छोटे प्रतिशतांश भी मिलकर बड़ी संख्याएँ बना सकते हैं।
सामुदायिक पहचानों के साथ राष्ट्र-राज्य के संबंधों की दृष्टि से भारत की स्थिति न तो आत्मसात्करणवादी और न ही एकीकरणवादी की है जिसके बारे में बॉक्स 6.1 में बताया गया है। अपने प्रारंभ से ही स्वतंत्र भारतीय राज्य में आत्मसात्करणवादी नीति को नहीं माना गया है। तथापि ऐसे प्रारूप के लिए प्रभावशाली बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से इसकी माँग की जाती रही है। हालाँकि, ‘राष्ट्रीय एकीकरण’ को राज्य की नीति में लगातार महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है, लेकिन भारत कभी उस रूप में एकीकरणवादी नहीं रहा जैसाकि बॉक्स 6.1 में बताया गया है। संविधान में यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य होगा पर धर्म, भाषा और अन्य ऐसे कारकों को सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह निष्कासित नहीं किया गया है। सच तो यह है कि राज्य द्वारा इन समुदायों को व्यक्त रूप से मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से मापा जाए तो अल्पसंख्यक धर्मों को अत्यंत प्रबल संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। आमतौर पर भारत में समस्या यह रही है कि यहाँ कानूनों या सिद्धांतों की तो कोई कमी नहीं रही बल्कि उनके पालन या व्यवहार में थोड़ी कसर रही है। लेकिन कुल मिलाकर भारत को ‘राज्य-राष्ट्र’ का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, यद्यपि यह राष्ट्र-राज्यों के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है।
6.1 भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद
भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। इसे विशेष क्षेत्रों में पहचान चिह्नकों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वंचन (deprivation) का भाव अग्नि में घी का काम करता है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने वाला एक साधन है (भट्टाचार्य 2005)।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, प्रारंभ में भारतीय राज्य ने ब्रिटिश-भारतीय व्यवस्था को ही अपनाए रखा जिसके अंतर्गत भारत बड़े-बड़े प्रांतों में, जिन्हें ‘प्रेसीडेंसी’ भी कहा जाता था, बँटा हुआ था। (मद्रास, बंबई और कलकत्ता तीन बड़ी प्रेसिडेंसियाँ थीं; प्रसंगवश हाल में इन तीनों शहरों के नाम जिनके नाम पर प्रेसिडेंसियों के नाम थे बदल दिए गए हैं)। यह बड़े-बड़े बहुनृजातीय और बहुभाषी प्रांतीय राज्य थे जो भारत संघ कहे जाने वाले अर्द्धसंघीय राज्य की बड़ी-बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में काम
भाषायी राज्यों ने भारतीय एकता को मज़बूत करने में सहायता दी
राज्य पुर्गाठन आयोग की रिपोर्ट, जो 1 नवंबर 1956 को कार्यांवित की गई थी, ने राष्ट्र के राजनीतिक और सांस्थानिक जीवन के रूपांतरण में सहायता दी।
राज्य पुर्गाठन आयोग की पृष्ठभूमि यहाँ दी जा रही है। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाषाई आधार पर पुनर्गठित की गई। अब इसकी प्रांतीय इकाइयों ने भाषाई आधार का अनुसरण किया, जैसे, एक मराठी बोलने वालों के लिए, दूसरी उड़िया बोलने वालों के लिए आदि-आदि। इसी समय, गाँधीजी तथा देश के अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों को वचन दिया कि जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तब नया राष्ट्र भाषाओं के अनुसार नए राज्यों के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा।
किंतु विडंबना यह रही कि जब भारत को 1947 में अंततः स्वतंत्र किया गया तो उसके साथ ही उसका विभाजन भी कर दिया गया। फिर जब भाषाई राज्यों के प्रस्तावकों ने नेताओं से अपने वचन पूरे करने के लिए कहा तो कांग्रेस ने हिचकिचाहट दिखलाई। देश का विभाजन अपने विश्वास के साथ गहरे लगाव का परिणाम था; इस प्रकार भाषा, गहरी निष्ठा न जाने कितने और बँटवारे करवा देगी? ऐसी विचारधारा उस समय के चोटी के कांग्रेसी नेताओं नेहरू, पटेल, और राजाजी आदि के मन में रही।
दूसरी ओर, सभी छोटे-बड़े कांग्रेसी नेता भाषाओं के आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार करने पर तुले हुए थे। मराठी और केन्न भाषाएँ बोलने वालों ने इसके लिए प्रबल आंदोलन छेड़ दिए; यह लोग उस समय की अनेक राजनीतिक रियासतों में फैले हुए थे। जैसे, तत्कालीन बंबई और मद्रास की प्रेसीडेंसियों और भूतपूर्व देसी राजाओं की रियासतें जैसे, मैसूर और हैदराबाद| लेकिन सबसे अधिक उत्रतापूर्ण विरोध बहुत बड़े तेलुगु भाषी समुदाय की ओर से किया गया जिनकी जनसंख्या बहुत बड़ी थी। दिसंबर 1952 में एक पूर्व गाँधीवादी नेता पोट्टि श्रीरामुलु इस मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए और सात सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोट्टि श्रीरामुलु के बलिदान ने हिंसात्मक विरोधों को भड़का दिया; परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करनी पड़ी। इसके अलावा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी। जिसने 1956 में भाषा आधारित सिद्धांत के अनुमोदन पर औपचारिक, अंतिम मोहर लगा दी।
1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत अनेक नेताओं को यह डर था कि भाषा आधारित राज्य कहीं भारत के उप-विभाजन की प्रक्रिया को और तेज़ न कर दें। लेकिन तथ्य तो यह है कि इसका उल्टा ही घटित हुआ। भाषा आधारित राज्यों ने भारतीय एकता को कोई ठेस नहीं पहुँचाई बल्कि उसे और भी मज़ूत करने में सहयोग दिया। क्नडिंग और भारतीय, बंगाली और भारतीय, तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय… दोनों साथ-साथ होना पूर्ण रूप से संगत साबित हुआ।
लेकिन यह भी सच है कि भाषा पर आधारित ये राज्य कभी-कभी आपस में लड़ते हैं। हालाँकि ये विवाद अच्छे नहीं होते पर यह और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। उसी 1956 के वर्ष में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार करने का समादेश दिया, सीलोन (जिसे अब श्रीलंका कहते हैं) की संसद ने उत्तर के तमिल भाषी नागरिकों के भारी विरोध के बावजूद सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया। एक वामपंथी सिंहली सांसद ने तो उग्रराष्ट्रवादियों को भविष्यवाणी के रूप में यह चेतावनी दे डाली: “एक भाषा, दो राष्ट्र” और “दो भाषाएँ, एक राष्ट्र"।
सन् 1983 से श्रीलंका में जो गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है वह कुछ हद तक बहुसंख्यक भाषाई समूह द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा किए जाने का ही परिणाम है। भारत के अन्य पड़ोसी राज्य पाकिस्तान का 1971 में विभाजन हो गया क्योंकि इसके पश्चिमी भाग के पंजाबी और उर्दू भाषी लोग पूर्वी भाग के बंगालियों की भावनाओं का आदर नहीं करना चाहते थे।
लेकिन भारत में भाषाई राज्यों के निर्माण के बदौलत ही भारत को ऐसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। यदि भारतीय भाषाई समुदायों की भावनाओं की उपेक्षा की जाती तो शायद हमारे यहाँ भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाती: “एक भाषा, चौदह या पंद्रह राष्ट्र"।
स्रोतः दिनांक 1 नवंबर 2006 के टाइम्स ऑफ़ इंडिया, दैनिक में प्रकाशित रामचंद्र गुहा के लेख से यथोचित परिवर्तनों के साथ उद्धृत
करते थे। उदाहरण के लिए, पुराना बंबई राज्य (जो बंबई प्रेसीडेंसी का ही दूसरा नाम था) मराठी, गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषी राज्य था। इसी प्रकार, मद्रास राज्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले लोगों से मिलकर बना था। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित प्रेसीडेंसियों और प्रांतों के अलावा संपूर्ण भारत में अनेक देशी राजाओं की रियासतें या रजवाड़े थे। इनमें मैसूर, कश्मीर और बड़ौदा के देशी राज्य अपेक्षाकृत बड़े थे। लेकिन संविधान को स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद औपनिवेशिक काल की इन सभी इकाइयों को तीव्र लोक आंदोलनों के कारण भारत संघ के भीतर नृजातीय-भाषाई राज्यों के रूप में पुनर्गठित करना पड़ा (बॉक्स 6.3 को देखिए)।
इस प्रकार, धर्म ने नहीं बल्कि भाषा ने क्षेत्रीय तथा जनजातीय पहचान के साथ मिलकर भारत में नृजातीय-राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक अत्यंत सशक्त साधन का काम किया है। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि सभी भाषाई समुदायों को राज्यत्व प्राप्त हो गया। उदाहरण के लिए, सन् 2000 में तीन नए राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के निर्माण में भाषा ने कोई प्रमुख भूमिका अदा
 113
113
1880 से 1930 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के दंपतीः सबसे ऊपर बाएँ कोने से: गुजरात; त्रिपुरा; सुंबई; अलीगढ़; दैदारादा; गोवा; कोलकाता। सोतः मालविका कारलेकर द्वारा संपा. विजुवलाइजिंग इंडियन वीमन 1875-1947, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली से
क्रियाकलाप 6.1
अपने राज्य के उद्भव के बारे में पता लगाएँ। यह कब बनाया गया था? इसे परिभाषित करने की मुख्य कसौटियाँ क्या थीं? क्या वह भाषा, नृजातीय/जनजातीय पहचान, क्षेत्रीय वंचन, पारिस्थितिक अंतर अथवा कोई अन्य कसौटी थी? भारतीय राष्ट्र-राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले अन्य राज्यों से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है?
भारत के सभी राज्यों का, उनके निर्माण की कसौटी के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास करें।
क्या आप वर्तमान में चल रहे किन्हीं सामाजिक आंदोलनों से परिचित हैं जो एक राज्य के निर्माण की माँग कर रहे हैं? इन आंदोलनों द्वारा प्रयोग की जा रही कसौटियों का पता लगाने की कोशिश करें।
[संकेतः विदर्भ आंदोलन और आप के अपने क्षेत्र में चल रहे किसी आंदोलन पर विचार करें…]
नहीं की, बल्कि जनजातीय पहचान, भाषा, क्षेत्रीय वंचन और पारिस्थितिकी पर आधारित नृजातीयता ने मिलकर तीव्र क्षेत्रीयता को आधार प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप नए राज्यों की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्र-राज्य में, इस समय 29 राज्य (संघीय इकाइयाँ) और 9 संघ राज्यक्षेत्र (केंद्रीय रूप से प्रशासित) हैं।
टिप्पणी: इस अध्याय में जहाँ ‘राज्य’ शब्द का प्रयोग मोटे अक्षरों में किया गया है वहाँ यह भारतीय राष्ट्र-राज्य के अंतर्गत आने वाली एक संघीय इकाई का द्योतक है; जहाँ सामान्य अक्षरों में इसे लिखा गया है वहाँ यह ऊपर वर्णित बृहत संकल्पना श्रेणी के तहत प्रयोग किया गया है।
क्षेत्रीय भावनाओं को आदर देना मात्र ही राज्य निर्माण के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक ऐसा संस्थागत ढाँचा होना भी जरूरी है जो यह
सुनिश्चित कर सके कि वह एक बड़े संघीय ढाँचे के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में चल सकता है। भारत में यह कार्य राज्यों तथा केंद्र की शक्तियों को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों द्वारा किया गया है। भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्यों की सूची होती है जिनकी जिम्मेदारी खासतौर पर राज्य या केंद्र की होती है, इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों की ‘समवर्ती सूची’ भी दी गई है जहाँ दोनों को ही कार्य संचालन की अनुमति है। जिनके बारे में राज्य और केंद्र दोनों ही कार्य कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा के गठन को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, कुछ आवधिक समितियाँ और आयोग हैं, जो केंद्र-राज्य संबंधों को निश्चित करते हैं। इसका एक उदाहरण वित्त आयोग है जिसे दस साल में, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बँटवारा करने के लिए स्थापित किया जाता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भी राज्यों की विस्तृत योजनाएँ शामिल होती हैं जो हर राज्य के राज्य योजना आयोगों द्वारा तैयार की जाती हैं।
6.2 धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचानें
सांस्कृतिक विविधता के सभी पक्षों में शायद धार्मिक समुदायों और धर्म-आधारित पहचानों के मुद्दे सबसे अधिक विवादास्पद हैं। इन मुद्दों को मोटे तौर पर दो संबंधित समूहों - धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक-के अंतर्गत बाँटा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के प्रश्न, राज्य के धर्म और उन राजनीतिक समूहों के साथ संबधों के बारे में होते हैं जो धर्म को अपनी प्राथमिक पहचान मानते हैं। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बारे में प्रश्न उन निर्णयों से संबंधित होते
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
हैं कि राज्य विभिन्न धार्मिक, नृजातीय या अन्य समुदायों के साथ, जो संख्या और/या शक्ति (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति सहित) की दृष्टि से असमान हैं, के साथ कैसा बर्ताव करता है।
अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र-निर्माण
भारतीय राष्ट्रवाद में प्रभावशाली प्रवृत्ति समावेशात्मक और लोकतंत्रात्मक दृष्टि द्वारा चिद्नित रही। इस दृष्टि को समावेशात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विविधता और बहुलता को मान्यता दी जाती रही है और लोकतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि यह भेदभाव और अपवर्जन को नकारती है और एक न्यायपूर्ण एवं साम्यिक (उचित) समाज की स्थापना करती है। ‘लोग’ शब्द को अपवर्जक दृष्टि से, धर्म, नृजातीय, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किसी विशेष समूह के प्रसंग से नहीं देखा गया है। मानवतावादी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रभावित किया और अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद के कुरूप पक्षों पर महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे अग्रणी महानुभावों द्वारा व्यापक रूप से टीका-टिप्पणी की गई।
बॉक्स 6.4
अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद की बुराइयों के बारे में रवींद्रनाथ टैगोर के विचार
…जहाँ पाश्चात्य राष्ट्रवाद की भावना का बोलबाला हो, तो सभी लोगों को बचपन से ही घृणा करना और महत्त्वाकांक्षाओं का पोषण करना तमाम तरीकों से सिखाया जाता है जैसे, इतिहास में अर्धसत्यों और असत्यों को गढ़कर, अन्य प्रजातियों के बारे में लगातार मिथ्यानिरूपण करके और उनके प्रति प्रतिकूल भावनाओं की संस्कृति बनाकर… कभी क्षणभर के लिए भी यह न सोंचे कि जो चोट आप दूसरी प्रजातियों को पहुँचाते हैं, वह आपको प्रभावित नहीं करेगी, अथवा जो वैमनस्य के बीज आप अपने घरों के चारों ओर बोते हैं, वे आने वाले संपूर्ण समय के लिए रक्षा की दीवार बनकर आपकी रक्षा करेंगे? संपूर्ण जनसमुदाय के मन में अपनी श्रेष्ठता का असामान्य दंभ भरना, अपनी नैतिक निर्दयता और गलत तरीकों से जमा की गई दौलत पर गर्व करना सिखाना, युद्ध के जरिए जीते गए विजयोपहारों के प्रदर्शन द्वारा विजित राष्ट्रों को सदैव अपमानित करना और बच्चों के मन में दूसरों के प्रति अवमानना के भाव भरने के लिए इन विद्यालयों का इस्तेमाल करना पश्चिम की नकल करना है जहाँ मानवता के घोवों से सड़ांध आ रही है…
स्रोतः ऑन नेशनल्जिम, खवांद्राथाथ टैगोर, 1917, पुनःमुर्रण, 1930, मैकमिलन, मद्रास
समावेशात्मक राष्ट्रवाद को प्रभावी बनाने के लिए, तत्संबंधी विचारधारा को संविधान में स्थान देना पड़ा। इसका कारण है, जैसाकि (अनुभाग 6.1 में) पहले ही चर्चा की जा चुकी है, प्रभावशाली समूह में यह मानकर चलने की अत्यंत प्रबल प्रवृत्ति होती है कि उनकी संस्कृति, भाषा अथवा धर्म राष्ट्र-राज्य की संस्कृति, भाषा या धर्म के समान है। किंतु एक मज़बूत और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए सभी समूहों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है। अल्पसंख्यकों की परिभाषा के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा हमें एक सबल, संयुक्त और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के महत्त्व को समझने में सक्षम बनाती है।
अल्पसंख्यक समूहों की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है एवं इसका सिर्फ़ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा और ज़्यादा महत्त्व है- इसमें आमतौर पर असुविधा या हानि का 115 कुछ भाव निहित है। अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यकों जैसे, अत्यंत धनवान लोगों को आमतौर पर

अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता; और यदि उल्लेख करना ही हो तो उनके साथ कोई विशेषक जोड़ दिया जाता है, जैसे ‘विशेषाधिकारप्राप्त अल्पसंख्यक’। जब अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग विशेषक के बिना किया जाता है तो सामान्यतः इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत छोटे लेकिन साथ ही सुविधावंचित समूह से होता है। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्रीय भाव यह भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, यानी उनमें अपने समूह के प्रति

एकात्मता, एकजुटता और उससे संबंधित होने का प्रबल भाव होता है। यह भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा है, क्योंकि पूर्वाग्रह और भेदभाव का शिकार होने का अनुभव आमतौर पर अपने ही समूह के प्रति निष्ठा और दिलचस्पी की भावनाओं को बढ़ावा देता है (गिडिंस 2001:248)। इसलिए, जो समूह सांख्यिकीय दृष्टि से अल्पसंख्यक हों जैसे, बाएँ हाथ से खेलने या लिखने वाले लोग या 29 फरवरी को जन्मे लोग, समाजशास्त्रीय अर्थ में अल्पसंख्यक नहीं होते, क्योंकि वे किसी सामूहिकता का निर्माण नहीं करते।
हालाँकि, कुछ ऐसे असामान्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं जहाँ कोई अल्पसंख्यक समूह किसी एक अर्थ में तो सुविधावंचित कहा जा सकता है लेकिन दूसरे अर्थ में नहीं। इसलिए, उदाहरण के लिए, पारसियों या सिक्खों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत संपन्न हो सकते हैं लेकिन वे फिर भी सांस्कृतिक अर्थ में सुविधावंचित हो सकते हैं क्योंकि हिंदुओं की विशाल जनसंख्या की तुलना में उनकी संख्या कम है। बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है।

बाएँ कोने पर कश्मीरी पोशाक में सजी बच्ची, दाएँ कोने में भारत के विभिन्न हिस्सों के व्यंजन, नीचे विभिन्न भारतीय राज्यों की पोशाकों में सजी गुड़ियाएँ
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
बॉक्स 6.5
धार्मिक अल्पसंख्यकों का तुलनात्मक आकार और वितरण
जैसाकि सर्वविदित है, भारत में हिंदुओं का बहुमत अत्यधिक हैः 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी लगभग 96.6 करोड़ है जो देश की संपूर्ण जनसंख्या का $80 %$ है। हिंदुओं की जनसंख्या सभी अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों की सम्मिलित जनसंख्या से लगभग चार गुना बड़ी है और सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों से लगभग छह गुना बड़ी है।
लेकिन यह तथ्य भ्रामक भी सिद्ध हो सकता है क्योंकि हिंदू लोग एक समजातीय समूह नहीं हैं बल्कि वे अनेक जातियों में बँटे हैं। वैसे अन्य सभी प्रमुख धर्मों में भी भिन्न-भिन्न सीमा तक जातियाँ होती हैं। अब तक मुसलमान समुदाय ही भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है, सन् 2011 में उनकी संख्या 13.8 करोड़ यानी संपूर्ण जनंसख्या का $14.2 %$ थी। वे देश में सर्वत्र फैले हुए हैं; जम्मू और कश्मीर में वे बहुसंख्यक हैं और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में उनके काफ़ी बड़े आंतर निवास हैं।
ईसाइयों की जनसंख्या 2.78 करोड़ यानी संपूर्ण जनंसख्या का $2.3 %$ है और वे सर्वत्र फैले हुए हैं, अलबत्ता पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में उनके आंतर निवास काफ़ी बड़े हैं। तीनों ईसाई बहुल राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं - नागालैंड $(88 %)$, मिजोरम $(87 %)$, मेघालय $(74.5 %)$ । गोवा $(25 %)$ और केरल $(18.4 %)$ में भी काफ़ी बड़ी संख्या में ईसाई लोग रहते हैं।
सिख धर्मावलंबियों की जनसंख्या $1.7 %$ (2.1 करोड़) है। वैसे तो वे देश के सभी भागों में फैले हुए हैं पर उनका विशेष जमाव पंजाब में है जहाँ वे बहुसंख्यक $(58 %)$ हैं।
इसके अलावा, और भी अन्य छोटे-छोटे धार्मिक समूह हैं-बौद्ध ( 80 लाख, $0.7 %$ ), जैन ( 45 लाख, $0.4 %$ ) और ‘अन्य धर्म एवं संप्रदाय’ ( 80 लाख, $0.7 %)$ । बौद्धों का सर्वाधिक अनुपात सिक्किम ( $27 %$ ) और अरुणाचल प्रदेश ( $12 %$ ) में है, जबकि बड़े राज्यों में से महाराष्ट्र में बौद्धों का अनुपात सर्वाधिक $6 %$ है। जैनों का सर्वाधिक अनुपात महाराष्ट्र $(1.3 %)$, दिल्ली और गुजरात $1 %$ में पाया जाता है।
कांग्रेस के अनेक विचार-विमर्श पूर्ण सत्रों में अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक अधिकारों पर अनेक चर्चाएँ हुई और अंततोगत्वा भारतीय संविधान में उन्हें अभिव्यक्ति मिली (ज़ैदी 1984)। भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक सुदृढ़ एवं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति तथा भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता होगी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डा. भीमराव अंबेडकर ने इस बिंदु को संविधान सभा में स्पष्ट किया, जैसाकि बॉक्स 6.6 में दर्शाया गया है।
बॉक्स 6.6
अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के विषय में डा. अंबेडकर के विचार
उन कट्टरपंथियों को, जिनके मन में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विरुद्ध एक तरह का दुराग्रह घर कर गया है, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक यह कि अल्पसंख्यक वर्ग एक ऐसी विस्फोटक शक्ति है जो यदि भड़क उठे तो राज्य की संपूर्ण रचना को तार-तार कर देगी। यूरोप का इतिहास इस तथ्य का ठोस एवं भयावह साक्ष्य प्रस्तुत करता है। दूसरी बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यक अपने अस्तित्व को बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपने के लिए सहमत हुए हैं। आयरलेंड के विभाजन को रोकने के लिए चली बातचीत के इतिहास में, रेडमंड ने कारसन से कहा, “आप प्रोटेस्टैंट अल्पसंख्यक के लिए चाहे जो सुरक्षा माँग लें, हमें आयरलैंड को संयुक्त, अविभाजित रखना है।” कारसन का उत्तर था: “लानत है तुम्हारी सुर्का पर, हम तुम्हारे द्वारा शासित होना ही नहीं चाहते|” भारत में अल्पसंख्यकों के किसी भी वर्ग ने यह रुख नहीं अपनाया।
(जॉन रेडमंड, बहुसंख्यक कैथोलिक के नेता, सर एडवर्ड कारसन, अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट के नेता)
सोतः संविधान सभा के वाद विवाद 1950:310-311, नारंग 2002:63 से उद्धृत
भीमराव रामजी अंबेडकर $(1891-1956)$
बौद्ध धर्म के पुनः प्रवर्तक, विधिवेत्ता, विद्वान एवं राजनीतिक नेता भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं। इनका जन्म एक गरीब अस्पृश्य समुदाय में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने में लगा दिया।

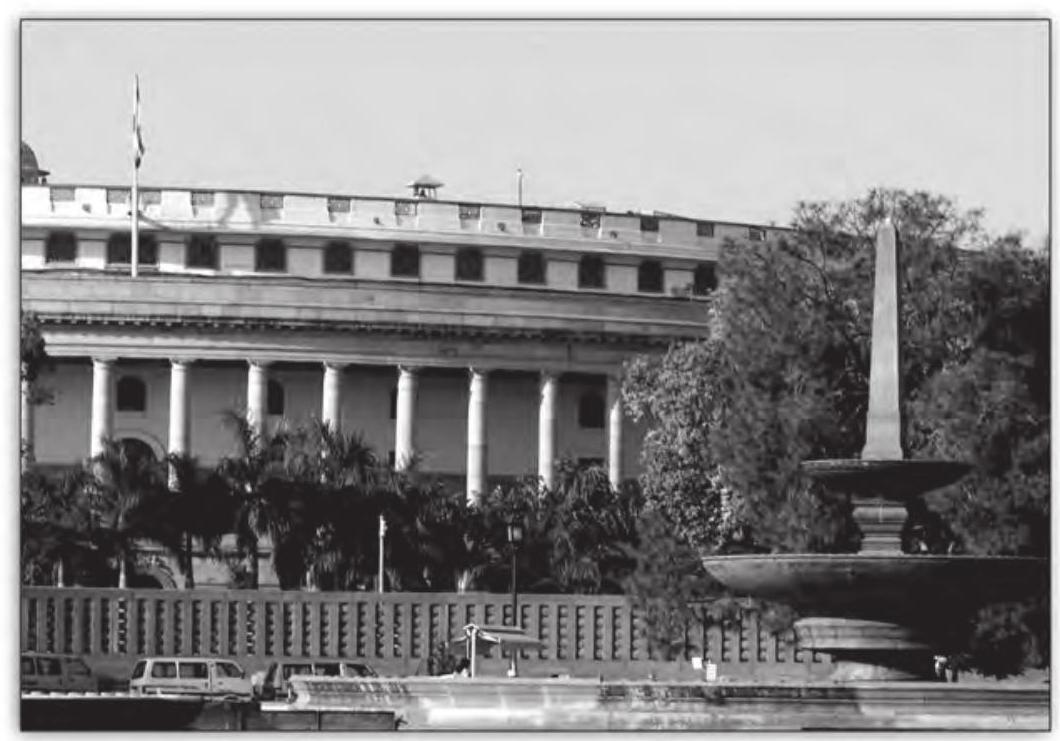
ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लंबे वर्षों में, भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत की विविधता को मान्यता और आदर देने की अनिवार्य आवश्यकता को समझा। वास्तव में, ‘विविधता में अनेकता’ का मुहावरा भारतीय समाज के बहुल एवं विविध स्वरूप को समझने का एक सूत्र बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक विचार-विमर्श पूर्ण सत्रों में अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक अधिकारों पर अनेक चर्चाएँ हुईं और अंततोगत्वा भारतीय संविधान में उन्हें अभिव्यक्ति मिली (जैदी 1984)।
भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक सुदृढ़ एवं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति तथा भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता होगी।
बॉक्स 6.7
अल्पसंख्यकों एवं सांस्कृतिक विविधता पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 29 :
(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 30 :
(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।
सांस्कृतिक विविधता की चुनततियाँ
भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डा. भीमराव अंबेडकर ने इस बिंदु को संविधान सभा में स्पष्ट किया, जैसाकि बॉक्स 6.6 में दर्शाया गया है।
पिछले तीन दशकों में हमने देखा है कि किसी देश में विभिन्न समूहों के लोगों के अधिकारों को मान्यता न दिए जाने से राष्ट्रीय एकता के लिए कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बांग्लादेश के निर्माण के अनेक मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा पाकिस्तानी राज्य की बांग्लादेश के लोगों के सांस्कृतिक तथा भाषाई अधिकारों को मान्यता देने की अनिच्छा था। श्रीलंका में नृजातीय संघर्ष के कारणभूत अनेक विवादास्पद मुद्दों में एक था, सिंहली भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपा जाना। इसी प्रकार, भारत में भी किसी भाषा या धर्म को किसी भी समूह पर जोर-जबरदस्ती से थोपा जाना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है जो विभिन्नताओं की मान्यता पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रवाद इसे मान्यता देता है और भारतीय संविधान इसकी परिपुष्टि करता है (बॉक्स 6.8 )।
अंत में, इस तथ्य को दृष्टिगत रखना उपयोगी है कि अल्पसंख्यक अकेले भारत में ही नहीं, सर्वत्र पाए जाते हैं। अधिकांश राज्य-राष्ट्रों में, एक प्रभावशाली सामाजिक समूह होता है चाहे वह सांस्कृतिक, नृजातीय, प्रजातीय अथवा धार्मिक हो। विश्व में कहीं भी ऐसा कोई राष्ट्र-राज्य नहीं है जो अन्य रूप में एक समरूप सांस्कृतिक समूह से बना हो। यहाँ तक कि जहाँ ऐसा काफ़ी हद तक सच था (जैसे, आइसलैंड, स्वीडन या दक्षिण कोरिया जैसे देशों में), वहाँ भी आधुनिक पूँजीवाद, उपनिवेशवाद और बड़े पैमाने पर हुए प्रवसन के कारण समूहों की बहुविधता पाई जाने लगी है। यहाँ तक की सबसे छोटे राज्य में भी अल्पसंख्यक पाए जाते हैं चाहे वह धार्मिक, नृजातीय, भाषाई अथवा प्रजातीय आधार पर हों।
सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र-राज्य
सांप्रदायिकता
रोज़मर्रा की भाषा में ‘सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद’ का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद, अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूहों को निम्न, अवैध अथवा विरोधी समझती है। इसी बात को और सरल शब्दों में कहें तो सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी होती है। यह एक अनूठा भारतीय अथवा शायद दक्षिण एशियाई अर्थ है जो साधारण अंग्रेज़ी शब्द के भाव से भिन्न है। अंग्रेज़ी भाषा में, ‘कम्युनल’ (communal) शब्द का अर्थ है व्यक्ति की बजाय समुदाय (यानी कम्युनिटी) या सामूहिकता से जुड़ा हुआ (व्यक्ति, भाव, विचार आदि)। अंग्रेज़ी अर्थ तटस्थ है जबकि दक्षिण एशियाई अर्थ प्रबल रूप से आवेशित है। इस आवेश को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है, यदि देखने वाला सांग्रदायिकता के प्रति सहानुभूति रखता हो अथवा नकारात्मक दृष्टि से भी, यदि देखने वाला इस का विरोधी हो।


बॉक्स 6.8
कबीरदास - समन्वयी परंपराओं का चिर, शाश्वत प्रतीक
हिंदू और मुसलमान भक्ति का समन्वित रूप प्रस्तुत करते कबीर के दोहे और पद बहुलवाद के चिरवांछित प्रतीक हैं:
मोको कहाँ ढ़ढ़े रे बंदे
मैं तो तेरे पास में
ना तीरथ में, न मूरत में
ना एकांत निवास में
ना मंदिर में, न मस्जिद में
ना काबे कैलास में
मैं तो तेरे पास में बंदे
मैं तो तरेर पास में …
इस बात पर बल देना ज़रूरी है कि सांग्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है धर्म से नहीं। यद्यपि संप्रदायवादी धर्म के साथ गहन रूप से जुड़े होते हैं, पर वास्तव में व्यक्तिगत विश्वास और संप्रदायवाद में आवश्यक रूप से कोई संबंध नहीं होता। एक संप्रदायवादी श्रद्धालु हो भी सकता है और नहीं भी एवं श्रद्धालु लोग संप्रदायवादी हो भी सकते हैं और नहीं भी। किंतु सभी संप्रदायवादी धर्म पर आधारित एक राजनीतिक पहचान में अवश्य विश्वास रखते हैं। मुख्य कारक है ऐसे लोगों के प्रति अभिवृत्ति जो अन्य प्रकार की पहचानों में, जिनमें अन्य धर्म आधारित पहचानें भी शामिल हैं, विश्वास रखते हैं। संप्रदायवादी आक्रामक राजनीतिक पहचान बनाते हैं और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की निंदा करने या उस पर आक्रमण करने को तैयार रहते हैं जो उनकी पहचान का साझेदार नहीं होता।
संप्रदायवाद की एक प्रमुख विशिष्टता उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होती है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, चाहे किसी का कोई भी व्यवसाय हो, जाति या राजनीतिक विश्वास हो, धर्म ही सब कुछ होता है, उसी के आधार पर उसकी पहचान है। सभी हिंदू एक समान होते हैं जैसे, सभी मुसलमान, सिख आदि। इसके प्रभावस्वरूप बड़े-बड़े और विविध समूह एक तथा समरूप हो जाते हैं।
भारत में संप्रदायवाद एक विशेष मुद्दा बन गया है क्योंकि यह तनाव और हिंसा का पुनरावर्त्तक स्रोत रहा है। भारत में स्वंतत्रता-प्राप्ति से पहले के समय में भी सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। ये दंगे अक्सर औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणामस्वरूप हुआ करते थे। लेकिन उपनिवेशवाद ने अंतर-सामुदायिक झगड़ों को जन्म नहीं दिया उपनिवेश काल से पहले भी ऐसे झगड़े होने का लंबा इतिहास रहा है और इसलिए स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के दंगों और मारकाट के लिए निश्चित रूप से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल, यदि हम धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय अथवा नृजातीय संघर्षों के उदाहरण खोजना चाहें तो वे हमारे इतिहास के लगभग प्रत्येक काल में मिल जाएँगे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ धार्मिक बहुलवाद की भी एक लंबी
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
परंपरा रही है जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से लेकर वास्तविक अंतरमिश्रण या समन्वयवाद शामिल है। यह समन्वयी विरासत भक्ति और सफफ़ी आंदोलनों के भक्ति गीतों और काव्यों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है (बॉक्स 6.8)। संक्षेप में, इतिहास हमारे समक्ष अच्छे और बुरे दोनों तरह के उदाहरण प्रस्तुत करता है इससे हम क्या सीखना चाहते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है।
धर्मनिरेक्षतावाद
धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। पाश्चात्य संदर्भ में, इन शब्दों का मुख्य भाव चर्च और राज्य की पृथकता का द्योतक है। धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के पृथक्करण ने पश्चिम के सामाजिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ ला दिया। यह पृथक्करण धर्मनिरपेक्षीकरण या जनजीवन से धर्म के उत्तरोत्तर पीछे हटते जाने की प्रक्रिया से संबंधित था, क्योंकि अब धर्म को एक अनिवार्य दायित्व की बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बदल दिया गया था। धर्मनिरपेक्षीकरण स्वयं आधुनिकता के आगमन और विश्व को समझने
क्रियाकलाप 6.2
अपने माता-पिता और परिवार के बुजुर्गों से बात करें और उनसे ऐसी कविताओं, गीतों, लघुकथाओं का संग्रह करें जिनमें धार्मिक बहुलवाद, समन्वयवाद अथवा सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। जब आप ऐसी संपूर्ण सामग्री इकही करके कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि धार्मिक बहुलवाद की हमारी परंपराओं का आधार कितना व्यापक है और विभिन्न भाषाई समूहों, क्षेत्रों और धर्मों के अनुयायी कितने व्यापक रूप से उन परंपराओं को आपस में बाँटते हैं। के धार्मिक तरीकों के विकल्प के रूप में विज्ञान तथा तर्कशक्ति के उदय से संबंधित था।
धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता के भारतीय अर्थों में उनके पश्चिमी भावार्थ तो शामिल हैं ही, पर उनमें कुछ और भाव भी जुड़े हैं। रोजमर्रा की भाषा में, धर्मनिरपेक्ष का सर्वाधिक सामान्य प्रयोग ‘सांप्रदायिक’ के बिल्कुल विपरीत यानी विलोम के रूप में किया जाता है। इस प्रकार, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। इस भाव में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है और इसमें धर्म के प्रति विद्येष का भाव होना जरूरी नहीं होता। राज्य और धर्म के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से, धर्मनिरपेक्षता का यह भाव सभी धर्मों के प्रति समान आदर का द्योतक होता है, न कि अलगाव या दूरी का। उदाहरण के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य सभी धर्मों के त्यौहारों के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करता है
भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध होने और साथ-साथ अल्पसंख्यकों के संरक्षण का वचन दिए जाने बीच तनाव के कारण भी कुछ जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उनका एक ऐसे संदर्भ में विशेष ध्यान रखा जाए जहाँ राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य काम-काज में उन्हें बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में हानि पहुँचती हो। लेकिन ऐसा संरक्षण दिए जाने से तुरंत ही अल्पसंख्यकों के पक्षपात या ‘तुष्टीकरण’ का आरोप लगता है। विरोधी यह तर्क देते हैं कि इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों के मत प्राप्त करने या उनसे अन्य प्रकार का समर्थन लेने के लिए उन्हें अपने पक्ष में लाने का एक बहाना मात्र है। समर्थक यह दलील देते हैं कि ऐसे विशेष संरक्षण के बिना तो धर्मनिरपेक्षतावाद अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक समुदाय के मूल्यों एवं प्रतिमानों को थोपने का एक बहाना बन सकता है।
6.3 राज्य और नागरिक समाज
आपने शायद यह ध्यान दिया होगा कि इस अध्याय के अधिकांश भाग में राज्य के बारे में ही विवेचना होती रही है। जब एक राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधता के प्रबंध की बात आती है तो राज्य वास्तव में, एक अत्यंत निर्णायक संस्था का रूप ले लेता है। हालाँकि यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, पर यह राष्ट्र और उसके लोगों से हटकर अपनी स्वतंत्र स्थिति भी बना सकता है। इस हद तक कि राज्य संरचना विधानमंडल, अधिकारीतंत्र (दफ़्तरशाही), न्यायपालिका, सशस्त्र सेनाएँ, पुलिस और राज्य के अन्य स्कंध, लोगों से पृथक हो जाते हैं, यह सत्तावादी बनने की संभाविता भी रखता है। एक सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है। एक सत्तावादी राज्य में लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती और जिनके पास शक्ति होती है वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। सत्तावादी राज्य अक्सर भाषण की
बॉक्स 6.9 लोगों के उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करना: सूचनाधिकार अधिनियम 2005
सूचनाधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम सं. $22 / 2005)$ भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक ऐसा कानून (विधि) है जिसके तहत भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुँचने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम की शर्तों के अधीन, कोई भी व्यक्ति किसी ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (सरकारी निकाय अथवा राज्य का करणत्व) से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है और उस प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वह शीघ्रता से यानी 30 दिन के भीतर उसे उत्तर देगा। यह अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण से यह अपेक्षा करता है कि वह व्यापक प्रसार के लिए अपने अभिलेखों को कंप्यूटरबद्ध करे और कतिपय श्रेणियों से संबंधित सूचना को स्वयं सक्रिय होकर प्रकाशित करे ताकि नागरिकों को सूचना के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करने की कम-से-कम आवश्यकता पड़े।
संसद द्वारा इस कानून को 15 जून 2005 को पारित किया गया था और यह 13 अक्तूबर 2005 से लागू हुआ। भारत में सूचना प्रकट करने का कार्य अब तक सरकारी गुप्त अधिनियम 1923 और अनेक अन्य विशेष कानूनों से प्रतिबंधित था, लेकिन नए सूचनाधिकार अधिनियम ने उन सबको रद्द कर दिया है। अधिनियम यह विनिर्दिष्ट करता है कि नागरिकों को:
किसी भी सूचना (यथापरिभाषित) के लिए अनुरोध करने,
द दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ लेने,
दस्तावेजों, कार्यों और अभिलेखों का निरीक्षण करने,
कार्य की सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार है।
नागरिक सूचना प्रिंटआउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से ले सकते हैं।
सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ
स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण का अधिकार, विधि (कानून) की अपेक्षित प्रक्रियाओं का अधिकार जैसी अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्सर सीमित या समाप्त कर देते हैं। सत्तावाद के अलावा, इस बात की संभावना भी रहती है कि राज्य की संस्थाएँ भ्रष्टाचार, अकुशलता अथवा संसाधनों की कमी के कारण, लोगों की ज़रूरतों के बारे में सुनवाई करने के लिए अक्षम अथवा अनिच्छुक हो जाएँ। संक्षेप में, ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से राज्य वैसा नहीं होगा जैसा उसे होना चाहिए। इस संदर्भ में गैर-राजकीय कर्ता अथवा संस्थाएँ महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे राज्य पर नज़र रख सकते हैं, उसके अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध कर सकते हैं अथवा उसके प्रयत्नों में सहयोग कर सकते हैं।
नागरिक समाज उस व्यापक कार्यक्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र
क्रियाकलाप 6.3
उन नागरिक समाज संगठनों अथवा गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाएँ जो आपके आस-पड़ोस में सक्रिय हैं। वे किस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं? उनमें किस प्रकार के लोग काम करते हैं? यह संगठन
(क) सरकारी संगठनों;
(ख) वाणिज्यिक संगठनों से कैसे और कितने भिन्न हैं।
से परे होता है, लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्र से बाहर होता है। नागरिक समाज सार्वजनिक अधिकार का गैर-राजकीय तथा गैर-बाजारी भाग होता है जिसमें अलग-अलग व्यक्ति संस्थाओं और संगठनों का निर्माण करने के लिए स्वेच्छा से परस्पर जुड़ जाते हैं। यह सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र है यहाँ व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, राज्य को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अथवा उसके समक्ष अपनी माँगे रखते हैं, अपने सामूहिक हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं या विभिन्न कार्यों के लिए समर्थन चाहते हैं। इस क्षेत्र में नागरिकों के समूहों द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक संघ, संगठन या संस्थाएँ शामिल होते हैं। इसमें राजनीतिक दल, जनसंचार की संस्थाएँ, मजदूर संघ, गैर-सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन और अन्य प्रकार के सामूहिक तत्त्व भी शामिल होते हैं। नागरिक समाज में शामिल होने की मुख्य कसौटियाँ यह हैं कि संगठन राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए और यह विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मुनाफ़ा कमाने वाले तत्त्व न हों।
आज नागरिक समाज के संगठनों के क्रियाकलाप और भी व्यापक रूप ले चुके हैं जिनमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ पक्ष समर्थन तथा प्रचार संबंधी गतिविधियाँ चलाने के साथ-साथ विभिन्न आंदोलनों में सक्रियतापूर्वक भाग लेना शामिल है। विविध प्रकार के मुद्दों को उठाया गया जिसमें भूमि संबंधी अधिकारों के लिए जनजातीय संघर्ष, नगरीय शासन का हस्तांतरण, स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध अभियान, बाँधों के निर्माण अथवा विकास की अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास, मशीनों की सहायता से मछली पकड़ने के विरुद्ध मछुआरों का संघर्ष, फेरी लगाकर सामान बेचने वालों या पटरी पर रहने वालों का पुनर्वास, गंदी बस्तियाँ हटाने के विरुद्ध और आवासीय अधिकारों के लिए अभियान, प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार, दलितों को भूमि का वितरण आदि शामिल हैं। नागरिक स्वतंत्रता संगठन राज्य के कामकाज पर नज़र रखने और उससे कानून का पालन करवाने की दिशा में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रहे हैं। जनसंचार माध्यमों ने भी, विशेष रूप से इसके उभरते हुए दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक खंडों ने उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सक्रिय भूमिका अदा की है।
हाल में उठाए गए उल्लेखनीय कदमों में सूचना के अधिकार के लिए चलाए गए अभियान को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत ग्रामीण राजस्थान में एक ऐसे आंदोलन के साथ 123 हुई थी जो वहाँ गाँवों के विकास पर खर्च की गई सरकारी निधियों के बारे में सूचना देने के लिए चलाया
गया था, आगे चलकर इस आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी अभियान का रूप धारण कर लिया। नौकरशाही के प्रतिरोध के बावजूद, सरकार को इस अभियान की सुनवाई करनी पड़ी और औपचारिक रूप से एक नया कानून बनाना पड़ा जिसके तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई (बॉक्स 6.9)। इस प्रकार के उदाहरण यह प्रकट करते हैं कि नागरिक समाज यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्तपूर्ण है कि राज्य, राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति जवाबदेह है।
प्रश्नावली
-
सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है?
-
सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है?
-
राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है? आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे संबंधित हैं?
-
राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं?
-
क्षेत्रवाद क्या होता है? आमतौर पर यह किन कारकों पर आधारित होता है?
-
आपकी राय में, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने भारत का हित या अहित किया है?
-
‘अल्पसंख्यक’ (वर्ग) क्या होता है? अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की क्यों जरूरत होती है?
-
सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है?
-
भारत में वह विभिन्न भाव (अर्थ) कौन से हैं जिनमें धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरेपेकतावाद को समझा जाता है?
-
आज नागरिक समाज संगठनों की क्या प्रासंगिकता है?