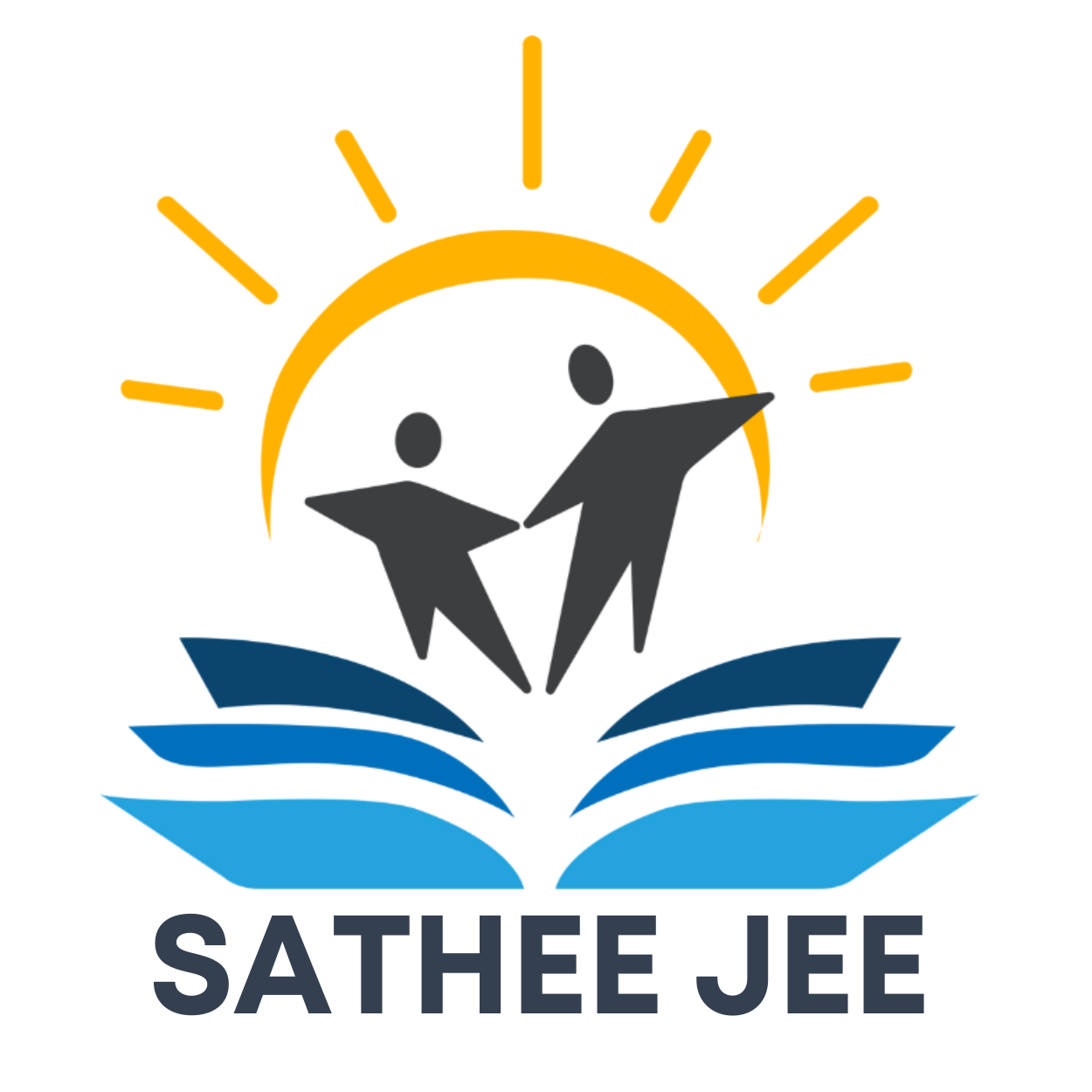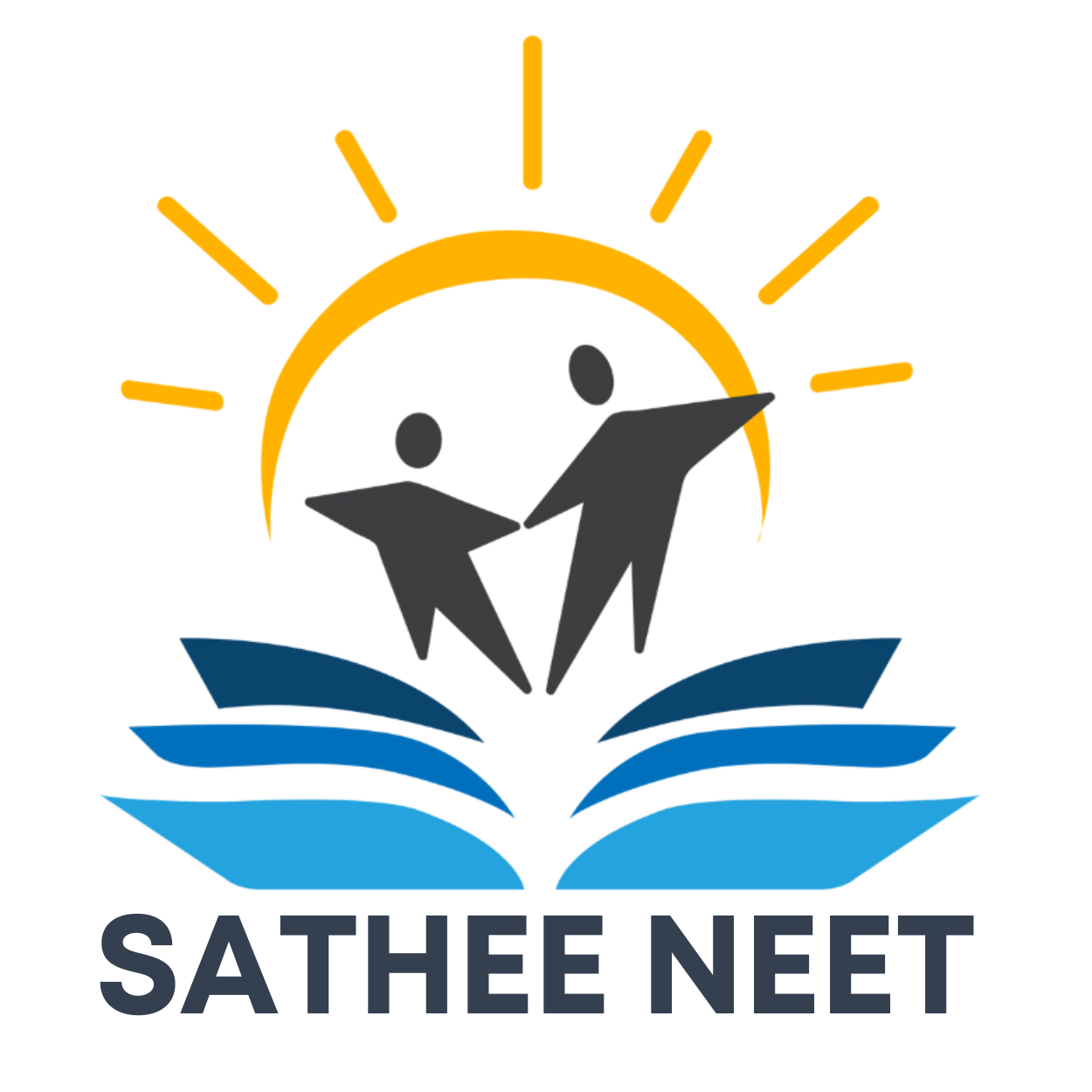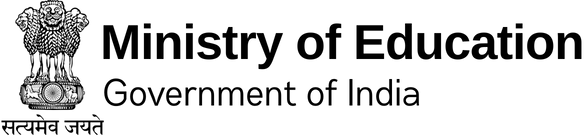अध्याय 07 क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
क्षेत्र और राष्ट्र
1980 के दशक को स्वायत्तता की माँग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की माँग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी माँग के पक्ष में हथियार उठाए; सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की माँग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक ज़ारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल, समझौते तक पहुँचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब-तब हिंसा के स्वर उभरे।
भारत सरकार का नज़ारिया
राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नजरों से बार-बार गुजरी है : भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषायी समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बँधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था, जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नज़ारिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया।
भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र-विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति-निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी।
ऐसी व्यवस्था में कभी-कभी तनाव या परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों
क्या इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रवाद सांप्रदायिकता के समान खतरनाक नहीं है? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद अपने आप में खतरनाक नहीं?

पर भारी पड़ें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की वृहत्तर आवश्यकताओं से आँखें मूँद लें। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहाँ क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है।
तनाव के दायरे
आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देसी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नगालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की माँग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठायी थी।
खतरे की बात हमेशा सीमांत के राज्यों के संदर्भ में ही क्यों उठाई जाती है? क्या इस सबके पीछे विदेशी हाथ ही होता है?

अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की माँग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों - खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ़ विरोध-आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध से पंजाबी-भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनकी माँग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया।
बहरहाल, इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नगालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियाँ इतनी विकट और जटिल थीं कि राष्ट्र-निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियाँ उभरीं। आइए, हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ-साथ राष्ट्र-निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ़ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान-बिंदु नहीं बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक ज़रूरी सबक है।
जम्मू एवं कश्मीर
आपने जैसा कि आपने गत वर्ष पढ़ा है, जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी और इसके आंतरिक तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और उग्रवादी शामिल थे। इसके अलावा, कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ।
केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख

जम्मू और कश्मीर तीन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियाँ और मैदानी भाग हैं। इसमें मुख्य रूप से हिन्दू रहते मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीरर घाटी है। यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिन्दू, सिख, बौद्ध तथा अन्य हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान हैं।
समस्या की जड़ें
1947 से पहले जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) एक राजसी रियासत थी। इसके शासक, महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का ‘हिस्सा’ है, क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान थी। परंतु उस रियासत के लोगों ने इसे इस तरह नहीं देखा - उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। राज्य में नेशनल कॉन्फेरेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहता था। साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था। नेशनल कॉन्फेरेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कॉग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। शेख अन्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे।

ई. वी. रामास्वामी नायकर
पेरियार के नाम से प्रसिद्ध; ऊनीश्वरवाद के प्रबल समर्थक जाति-विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक; राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में; आत्मसम्मान आंदोलन के जनक (1925); ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व; जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता और द्रविड़ कषगम की स्थापना; हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध; ‘उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आर्य हैं’ इस मत का प्रतिपादन किया।‘उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन-दिन घटता जाए’ द्रविड़ आंदोलन
यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतर है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रियतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालाँकि आंदोलन के नेतृवर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने को थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनायी। नेतृत्व ने अपनी माँग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया।
द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ई.वी. रामास्वामी नायकर ‘पेरियार’ के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन-‘द्रविड़ कषगम’ का सूत्रात हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और साँस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। प्रारंभ में, द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों से समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे-धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया।

बाद में द्रविड़ कषगम दो धड़ों में बंट गया और आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुनेत्र कषगम के पाले में केंद्रित हो गई। 1953-54 के दौरान डीएमके ने तीन-सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की तीन माँगें थी : पहली, कल्लाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम-डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह माँग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती थी।

दूसरी माँग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज़्यादा महत्त्व दिया जाए। संगठन की तीसरी माँग राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी। डीएमके हिंदी को राजभाषा का दर्ज़ा देने के भी खिलाफ़ थी। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया।
राजनीतिक आंदोलनों के एक लंबे सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनावों में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। डीएमके के संथापक सी. अन्नादुरै की मृत्यु के बाद दल में दोफाड़ हो गया। इसमें एक दल मूल नाम यानी डीएमके को लेकर आगे चला जबकि दूसरा दल खुद को आल इंडिया अन्ना द्रमुक कहने लगा। यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता था। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल चार दशकों से दबदबा बनाए हुए हैं। इनमें से एक न एक दल 1996 से केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा है। 1990 के दशक में एमडीएमके (मरुमलर्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम), पीएमके (पट्टाली मक्कल कच्ची), डीएमडी के (देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कषगम) जैसे कई अन्य दल अस्तित्व में आए। तमिलनाडु की राजनीति में इन सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा है। एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है।


शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ( 1905-1982 ) : जम्मू एवं कश्मीर के नेता; जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक; राजशाही के खिलाफ़ जन आंदोलन का नेतृत्व; धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध; नेशनल कांफ्रेंस के नेता; भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री (1947); भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास (1953-1964); पुनः कारावास (1965-1968); 1974 में इंदिरा गाँधी के साथ समझौता, राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़।
अक्टूबर 1947 में, पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया, परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।परंतु चूँकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसने दिनांक 21 अप्रैल, 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए एक तीन चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। पहला पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे, जो कश्मीर में घुस गए थे। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था। परंतु, इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति न हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थाई स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था।
बाहरी और आंतरिक झगड़े
तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्व-पूर्ण बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत दावा करता है कि इस क्षेत्र पर गैरकानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को ‘आजाद कश्मीर’ कहता है। 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वांद्र का प्रमुख मुद्धा बना रहा।
आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। आपने गत वर्ष भारत का संविधान : सिद्धान्त और व्यवहार में अनुच्छेदों 370 और 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा है। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू और कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता है। इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए।
दूसरे वर्ग, अधिकांश कश्मीरियों, का मानना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। उनकी कम से कम तीन मुख्य शिकायतें थीं। पहली यह कि कबायली हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इससे ‘जनमत-संग्रह’ की माँग उठी। दूसरे, यह अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है। इससे स्वायत्तता को बहाल करने या ‘अधिक राज्य स्वायत्ता"’ की माँग उठी। तीसरी, यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतन्त्र शेष भारत में है, वैसा जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया है।
आइए एक फिल्म देखें

दुख और साहस की कहानी चधान की गयी है। रोजा के पति का उग्रचारी अपहरण कर लेते हैं। वह खुफिया संदेशों को पढ़ने में माहिर है। उसे कश्मीर में तैनात किया गया है जहाँ उसका काम दुश्मन के खुफिया संदेशों को पड़ना है। पति-पानी में जैसे ही दाम्पत्य का प्रेम बढ़ने लगता है वैसे ही पति का अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ताओं की माँग है कि रोजा के पति ऋषि को तभी छोड़ा जाएगा जब जेल में बंद उनके सरगना को छोड़ दिया जाए।
रोजा का संसार कहने लगता है। वह अधिकारियों और राजनेताओं के दरवाजे खटखटाते हुए दर-दर भटकती है। यह फिल्म भारत-पाकिस्तान विवाद की पृष्ठभूमि में बनी थी इस वजह से लोगों में यह बड़ी लोकप्रिय हुई। इस फिल्म को हिंदी सहित अन्य भाषाओं में भी रूपांतरित किया गया।
वर्ष 1992
निर्देशक: मणिरानम्
पटकथा मणिरत्नम्
अभिनय (हिंदी): मधु, अरविन्द स्वामी पंकज कपूर, जनगराज।
1948 से राजनीति
प्रधानमंत्री बनने के बाद, शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियाँ शुरू की जिनसे सामान्य जन को लाभ पहुँचा। परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता गया। उन्हें 1953 में पद्च्चुत कर दिया गया और कई वर्षों तक कैद रखा गया। उनके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और वह राज्य में शासन नहीं चला पाए जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप थे।
1953 और 1974 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फेरेंस (शेख अन्दुल्ला रहित) का एक घडा़ कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा परंतु बाद में यह काँग्रेस में मिल गया। इस प्रकार काँग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और परिवर्तन किए गए। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुँचने के लिए कई प्रयास हुए। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। इसके अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने।

1974 में इंदिरा गाँधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फेरेंस को पुनर्जीवित किया जिसने 1977 के विधान सभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फेरेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, जो मुख्यमंत्री बने। परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया और नेशनल कॉन्फेरेंस से अलग हुआ एक गुट एक अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया।
केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई। इंदिरा गाँधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था, उसे धक्का लगा।यह भावना कि केन्द्र राज्य की राजनीति हस्तक्षेप कर रहा है, पुष्ट हुई जब 1986 में नेशनल कांफ्रेंस केंद्र में शासक दल काँग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हो गई।
सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद
यह वो वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए। सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फेरेंस-काँग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अन्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे। परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है, और सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। 1980 के दशक के प्रारम्भ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ कमजोर की जा रही हैं। इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद के उठने से गहरा गया।
1989 तक, राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला। कई वर्षों तक राज्य, राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशत्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। 1990 से पूरा समय, जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए जिसमें फारूक अन्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फेरेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्ता की माँग के साथ सत्ता में आई। अवधि के अंत में, 2002 में जम्मू और कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फेरेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके स्थान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और काँग्रेस की मिली-जुली सरकार आ गई।
2002 और इससे आगे
गठबंधन के समझौते के अनुसारए मुफ्ती मोहम्मद पहले तीन वर्ष सरकार के मुखिया रहे, जिनके बाद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के गुलामनबी आज़ाद मुखिया बने जो जुलाई, 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उससे अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ। एक और मिली-जुली सरकार (नेशनल कॉन्फ़रेंस और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस से बनी) 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई। परंतु, राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ़रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। 2014 में, राज्य में फिर चुनाव हुए, जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकार्ड किया गया। परिणाम स्वरूप पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिली-जुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल, 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएँ हुई। जून, 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर दो केंद्र शासित प्रदेश-जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए।
यह सारी बात तो सरकार, अधिकारियों, नेताओं और आतंकवादियों के बारे में है। जम्मू एवं कश्मीर जनता के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता? लोकतंत्र में तो जनता की इच्छा को महत्त्व दिया जाना चाहिए। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ न?


मास्टर तारा सिंह (1885-1967) : प्रमुख सिख धार्मिक एवं राजनीतिक नेता; शिरोमणि गुर्द्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के शुरुआती नेताओं में से एक; अकाली आंदोलन के नेता; स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के साथ समझौते की कांग्रेस नीति के विरोधी; स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक।
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते-जागते उदाहरण हैं। वहाँ न केवल सभी प्रकार (धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय) की विविधताएँ हैं बल्कि वहाँ विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएँ हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है।
पंजाब
1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालाँकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया गया था लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतज़ार करना पड़ा। इस साल पंजाबी-भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने ‘पंजाबी सूबा’ के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी-भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए।
राजनीतिक संदर्भ
पंज़ाब सूबे के पुरर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनायी। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावज़ूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावांडोल है। पहली बात तो यही कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बँटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच चाहे वे सिख हों या हिंदू— अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था।
इन्हीं परिस्थितियों के ममद्देनज़र 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की माँग उठायी। 1973 में, आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठायी गई थी। प्रस्ताव की माँगों में केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख ‘कौम’ (नेशन या समुदाय) की आकांक्षाओं पर ज़ोर देते हुए सिखों के ‘बोलबाला’ (प्रभुत्व या वर्चस्व) का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव भारत में संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है।
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन-समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बँटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठायी।

संत हरचंद सिंह लोंगोवाल
सिखों के धार्मिक एवं राजनीतिक नेता; छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली नेता के रूप में; 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष; अकालियों की प्रमुख माँगों को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गाँधी से समझौता; अज्ञात
हिंसा का चक्र
जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंधी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्त्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्णमंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्णमंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ चलाया। यह स्वर्णमंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य-अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफ़लतापूर्वक मार भगाया लेकिन सैन्य कर्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्णमंदिर को क्षति भी पहुँची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य-अभियान को अपने धर्म-विश्वास पर हमला माना। इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और बल मिला।

कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की 31 अक्तूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हों के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक-संतप्त था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई
हफ्तों तक जारी रही। दो हज़ार से ज्यादा की तादाद में सिख, दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख-परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुँचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सिख युवक द्वारा हत्या। बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही, हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख-विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी माँगी।

इंदिरा गांधी की हत्या के विषय पर बने एक दीवार-चित्र को यहाँ महिलाएँ देख रही हैं

इंदिरा गाँधी की हत्या के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने अखबार का एक विशेष अपराह्न संस्करण प्रकाशित किया।
शांति की ओर
1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगोंवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गाँधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा-विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब-हरियाणा-राजस्थान के बीच रावी-व्यास के पानी के बँटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही, पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई।
“सिख समुदाय से ही नहीं पूरे भारत राष्ट्र से माफी माँगने में मुझे कोई संकोच नहीं क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र की अवधारणा तथा संविधान के लिखे का नकार था। इसलिए, मैं यहाँ किसी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर नहों खड़ा हूँ। अपनी सरकार को तरफ़ से, इस देश की समूची जनता को तरफ़ से मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूँ कि ऐसा हादसा पेश आया। लेकिन, मान्यवर, राष्ट्र के जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं। अतीत हमारे साथ होता है। हम अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते। लेकिन, मनुष्य के रूप में हमारे पास वह इच्छाशक्ति और क्षमता है कि हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।”
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 अगस्त, 2005 को राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेते हुए।
बहरहाल, पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद। हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही, पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24 फीसदी मतदाता वोट डालने के लिए आए।
उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हों या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल (बादल) और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। हालाँकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है।
पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थीं। क्षेत्र में सात राज्य हैं और इन्हें ‘सात बहनें’ कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश की कुल 4 फीसदी आबादी निवास करती है। लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली-सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएँ चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश-द्वार है।
इस इलाके में 1947 के बाद से अनेक बदलाव आए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र, पहले अलग-अलग रियासत थे। आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। नगालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्ज़ा दिया गया। 1947 के भारत-विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग-थलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भागों से अलग-थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ-साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया।
नोट: यह नक्शा कोई पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए।
पूर्वोत्तर का अलग-थलग पड़ जाना, इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा की। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की माँगें उठीं। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी है लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार-व्यवस्था बड़ी लचर है। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर तीन मुद्दे हावी हैं: स्वायत्तता की माँग, अलगाव के आंदोलन और ‘बाहरी’ लोगों का विरोध। इसमें पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की माँग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी। इससे शेष दो मुद्रों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया।

स्वायत्तता की माँग
आजादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। गैर-असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की माँग उठी। पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ‘ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन’ का गठन किया जो 1960 में कहीं ज्यादा व्यापक ‘ऑल पार्टी हिल्स कांफ्रेंस’ में तब्दील हो गया। इन नेताओं की माँग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने। केंद्र सरकार ने अलग-थलग वक्त पर असम को बाँटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया।
1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था। लेकिन, स्वायत्तता की माँग खत्म न हुई। उदाहरण के लिए, असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की माँग की। अपनी माँग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास किए, जन आंदोलन चलाए और विद्रोही कार्रवाइयाँ भी कीं। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जतायी। छोटे-छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। इस वजह से संघीय राजव्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की माँग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। करबी और दिमसा समुदायों को जिला-परिषद् के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद् का दर्जा दिया गया है।
अलगाववादी आंदोलन
स्वायत्तता की माँगों से निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। लेकिन जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की माँग की और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस माँग से निपटना मुश्किल हो गया। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के दो राज्यों में अलगाववादी माँग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। इन दो मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है।
आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ‘ब्रिटिश इंडिया’ के अंग नहीं रहे इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जनसमर्थन मिलना शुरू हुआ। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया।
1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की माँग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच दो दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक दफ़े तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हुई।
दो दशकों तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इसी बात को भाँपकर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया।
दोस्त चोन कहती है कि दिल्ली के लोग यूरोप के नक्शे के बारे में ज्यादा जानते हैं और अपने देश के पूर्वोत्तर के हिस्से के बारे में कम। अपने सहपाठियों को देखकर तो यही लगता है कि उसकी बात एक हद तक सही है।


लालडेंगा (1937-1990) : मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता: 1959 के अकाल के बाद विद्रोही बन गए: भारत के खिलाफ़ दो दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व; 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के साथ सुलह और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए; नव-निर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री बने।

पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लालडेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गाँधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुँचाया। 1986 में राजीव गाँधी और लालडेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया। लालडेंगा मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है।

नगालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है लेकिन नगालैंड का अलगावादी आंदोलन ज्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हल नहीं निकल पाया है। अंगमी जापू फ़िजो के नेतृत्व में नगा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया था। फ़िजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नगा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नगालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है।
बाहरी लोगों के खिलाफ़ आंदोलन
पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवासी आए हैं। इससे एक खास समस्या पैदा हुई है। स्थानीय जनता इन्हें ‘बाहरी’ समझती है और ‘बाहरी’ लोगों के खिलाफ़ उसके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंद्धी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कभी-कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएँ भी होती हैं।
1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ़ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत-सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचानकर उन्हें अपने देश नहों भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
1979 में ऑल असम स्टूडेंटस् यूनियन (आसू-AASU) ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। ‘आसू’ एक छात्र-संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहों था। ‘आसू’ का आंदोलन अवैध आप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों आप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ़ था। आंदोलन की माँग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएँ भी हुईं। बहुत-से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन-संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेलशोधक कारखाने को तेल-आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई।
छह साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गाँधी के नेतृत्व वाली सरकार ने ‘आसू’ के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणामस्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश-युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद ‘आसू’ और असम गण संग्राम परिषद् ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम ‘असम गण परिषद्’ रखा गया। असम गण परिषद् 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक ‘स्वर्णिम असम’ का निर्माण किया जाएगा।
असम-समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला लेकिन ‘आप्रवास’ की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ‘बाहरी’ का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की,

अंगमी जापू फिजो
नगालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता; नगा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष; भारत सरकार के खिलाफ़ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की; ‘भूमिगत’ हुए; पाकिस्तान में शरण ली; जीवन के अंतिम तीन दशक ब्रिटेन में गुजारे।[^0]
मुझे यह ‘भीतरी’ और ‘बाहरी’ का मामला कभी समझ में नहीं आता। कोई आदमी कहीं पहले चला गया हो तो वही दूसरों को ‘बाहरी’ समझने लगता है।

राजनीति में एक जीवंत मसला है। यह समस्या त्रिपुरा में ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है।

खबर को खत्म करने के लिए, यहां चार क्षेत्रों में आतंकवादियों की गतिविधियों पर एक नजर है… पंजाब, दार्जिलिंग, दिल्ली, मिजोरम
सिक्किम का विलय
आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की ‘शरणागति’ प्राप्त थी। इसका मतलब यह कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथों में थी। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पायी क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। नेपाली मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेपचा-भूटिया के एक छोटे-से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। चोग्याल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद माँगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया।
सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के ‘सह-प्रान्त’ बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत-संग्रह कराया गया और जनमत-संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22 वाँ राज्य बन गया। चोग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल-प्रयोग करने का आरोप लगाया। बहरहाल, भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा न बन सका!

काजी लैंदुप दोरजी खांगसरपा ( 1904 ) : सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता; सिक्किम प्रजामंडल एवं सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक; 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना; चुनावों में विजय के उपरांत सिक्किम के भारत में विलय के समर्थक; एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय।
समाहार और राष्ट्रीय अखंडता
इन मामलों से पता चलता है कि आज़ादी के छह दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लगातार एक न एक रूप में उभरती रहीं। कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की माँग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा। कहीं-कहीं से अलगाववाद के स्वर उभरे। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबको की माँगों में पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं।
पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उभरी हैं। स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी माँग की। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नताएँ भी बड़े पैमाने पर हैं। अतः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी।

राजीव गाँधी ( 1944-1991 ) : 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री; इंदिरा गाँधी के पुत्र; 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय; पंजाब के आतंकवादियों, मिजो-विद्रोहियों तथा असम में छात्र संघ से समझौता; खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती; सिंहली-तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा; संदिग्ध एलटीटीई आत्मघाती द्वारा हत्या।
दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। जरा अस्सी के दशक की तरफ़ नज़र दौड़ाएँ-पंजाब में उग्रवाद का जोर था; पूर्वोत्तर में समस्याएँ बनी हुई थीं; असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल अशांत था। इन मसलों को सरकार ने कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया। इससे सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुआ। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है।
तीसरा सबक है सत्ता की साझेदारी के महत्त्व को समझना। सिर्फ लोकतांत्रिक ढाँचा खड़ा कर लेना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय राजव्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी नाकफ़ी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्तता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा।
चौथा सबक यह है कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियाँ अपनायी हैं उसी के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहें और बाकी तेजी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। साथ ही, अंतर्प्रान्तीय अथवा अंतर्षेत्रीय आप्रवास में भी बढ़ोत्तरी होगी।
सबसे आखिरी बात यह कि इन मामलों से हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता चलता है। वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य हैं। भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनायी है वह बहुत लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान हैं तो जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान को छठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार-व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए।
भारत का संवैधानिक ढाँचा ज्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। जिस तरह की चुनौतियाँ भारत में पेश आयों वैसी कुछ दूसरे देशों में भी आयी लेकिन भारत का संवैधानिक ढाँचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीयता, लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है।
गोवा की मुक्ति
हालाँकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। यह क्षेत्र सोलहवीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था। अपने लंबे शासनकाल में पुर्गगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था। उसने यहाँ के लोगों को नागरिकों अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म-परिवर्तन कराया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश की। गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। आखिरकार, दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। दो दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। गोवा, दमन और दीव संघशासित प्रदेश।
जल्दी ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने माँग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए क्योंकि यह मराठी-भाषी क्षेत्र है। बहरहाल, बहुत-से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोअन पार्टी (यूजीपी) ने किया। 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं। इस मसले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत-संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनायी थी। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघशासित प्रदेश बना रहा। अंततः 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना।

प्रश्नावली
1. निम्नलिखित में मेल करें:
अ
क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रकृति
(क) सामाजिक-धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण
(ख) भाषायी पहचान और केंद्र के साथ तनाव
(ग) क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण
(ख) आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी माँग
ब
राज्य
(i) नगालैंड/मिजोरम
(ii) झारखंड/छत्तीसगढ़
(iii) पंजाब
(iv) तमिलनाडु
2. पूर्वोत्तर के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है। बाहरी लोगों के खिलाफ़ आंदोलन, ज्यादा स्वायत्तता की माँग के आंदोलन और अलग देश बनाने की माँग करना-ऐसी ही कुछ अभिव्यक्तियाँ हैं। पूर्वोत्तर के मानचित्र पर इन तीनों के लिए अलग-अलग रंग भरिए और दिखाइए कि किस राज्य में कौन-सी प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल है।
3. पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
4. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे?
5. जम्मू-कश्मीर की अंदरुनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए और बताइए कि इन विभिन्तताओं के कारण इस राज्य में किस तरह अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया है।
6. कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष क्या हैं? इनमें कौन-सा पक्ष आपको समुचित जान पड़ता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
7. असम आंदोलन सांस्कृतिक अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली-जुली अभिव्यक्ति था। व्याख्या कीजिए।
8. हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी माँग की तरफ अग्रसर नहों होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या कीजिए।
9. भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से ‘विविधता में एकता’ के सिद्धांत की अभिव्यक्ति होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए।
10. नीचे लिखे अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछेे गए प्रश्नों के उत्तर दें:
हजारिका का एक गीत… एकता की विजय पर है; पूर्वोत्तर के सात राज्यों को इस गीत में एक ही माँ को सात बेटियाँ कहा गया है… मेघालय अपने रास्ते गई… अरुणाचल भी अलग हुई और मिजोरम असम के द्वार पर दूल्हे को तरह दूसरी बेटी से ब्याह रचाने को खड़ा है… इस गीत का अंत असमी लोगों की एकता को बनाए रखने के संकल्प के साथ होता है और इसमें समकालीन असम में मौजूद छोटी-छोटी कौमों को भी अपने साथ एकजुट रखने की बात कही गई है… करबी और मिजिंग भाई-बहन हमारे ही प्रियजन हैं। -संजीब बरुआ
(क) लेखक यहाँ किस एकता की बात कह रहा है?
(ख) पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के कुछ राज्य क्यों बनाए गए?
(ग) क्या आपको लगता है कि भारत के सभी क्षेत्रों के ऊपर एकता की यही बात लागू हो सकती है? क्यों?