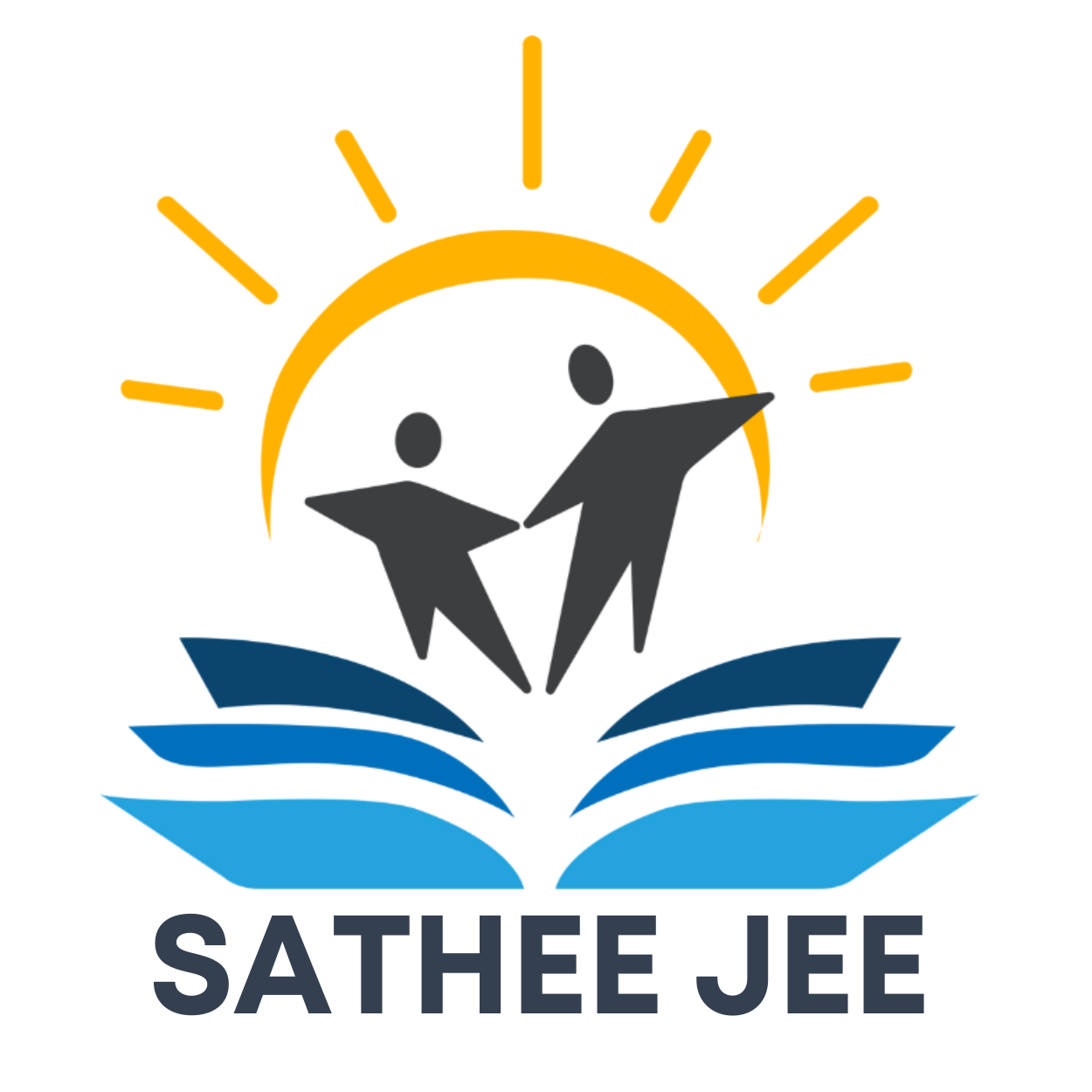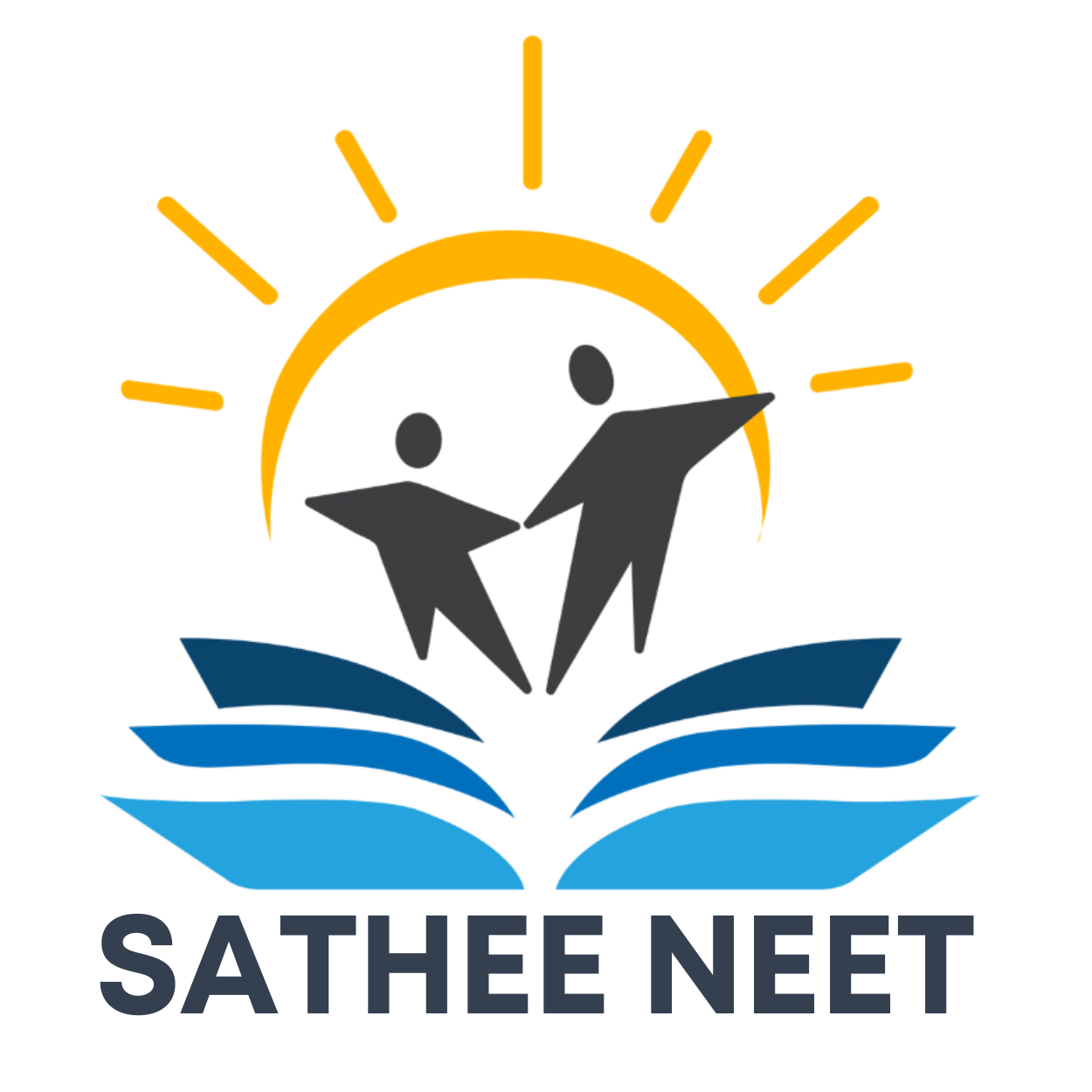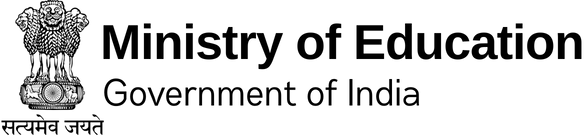अध्याय 06 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
आपातकाल की पृष्ठभूमि
1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गाँधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थीं और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुँचाने वाले कल्याण-कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे, उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गाँधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे।
आर्थिक संदर्भ
1971 के चुनाव में कांग्रेस ने ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया था। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक-आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमरीका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ीं। 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23 फीसदी और 1974 में 30 फीसदी का इज़ाफ़ा हुआ। इस तीव्र मूल्यवृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई।
औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ी थी। खर्च को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8 प्रतिशत कम हो गया। आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन-विरोध की अगुवाई की। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज़्यादा सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है!

अच्छा तो यही होता कि 1973 का यह साल जितनी जल्दी हो सके, बीत जाता।

गरीब जनता पर सचमुच भारी मुसीबत आई होगी। आखिर गरीबी हटाओ के वादे का हुआ क्या?
प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूँजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्यविरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी-लेनिनवादी (अब माओवादी) अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए।
गुजरात और बिहार के आंदोलन
गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र-आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आंदोलन छेड़ दिया। छात्र-आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ भी शरीक हो गईं और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की माँग की। कांग्रेस (ओ) के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल पर बैठ जाऊँगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गाँधी के मुख्य विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र-आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई।
सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है।
1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा
1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण (जेपी) को बुलावा भेजा। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र-आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्र्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की माँग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में ‘सम्पूर्ण क्रांति’ का आह्बान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में ‘सच्चे लोकतंत्र’ की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ़ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल, सरकार ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया।
इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा
कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ (1974) ने यह नारा दिया था।

आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्नान किया। इससे देश के रोज़मर्रा के कामकाज़ के ठप्प हो जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में जेपी ने जनता के ‘संसद-मार्च’ का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर-कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण ( जेपी ) ( 1902-1979) : युवावस्था में मार्क्सवादी; कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव; 1942 के भारत-छोड़ो आंदोलन के नायक नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए; नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार; 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ी; गाँधीवादी बनने के बाद भुदान आंदोलन में सक्रिय; नगा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की; कश्मीर में शांति प्रयास किए; चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया; बिहार आंदोलन के नेता; आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए थे; जनता पार्टी के गठन के प्रेरणास्रोत।
इन दलों ने जेपी को इंदिरा गाँधी के विकल्प के रूप में पेश किया। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनायी गई जन-प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएँ भी मुखर हुईं। गुजरात और बिहार, दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ़ नहीं बल्कि इंदिरा गाँधी के नेतृत्व के खिलाफ़ चलाए गए हैं। इंदिरा गाँधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हैं।
1974 की रेल हड़ताल
यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? एक या दो दिन नहीं, बल्कि हफ़्ते भर से ज़्यादा समय तक रेलगाड़ियाँ न चलें तो? निश्चित ही बहुत-से लोगों का आना-जाना दूभर हो जाएगा, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था ठप्प हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ज़्यादातर ढुलाई होती है।
क्या आप जानते हैं कि 1974 में ठीक ऐसा ही वाकया पेश आया था? रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नान्डिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्बान किया। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी माँगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का यह आह्बान किया गया था।
सरकार इन माँगों के खिलाफ़ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मज़दूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से मज़दूरों के अधिकार जैसे मसले तो उठे ही, यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी माँगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार दिया। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की माँगों को मानने से इनकार कर दिया। उसने इसके कई नेताओं को गिरफ़्तार किया और रेल लाइनों की सुर्का में सेना को तैनात कर दिया। ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई।

क्या ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’ और ‘प्रतिबद्ध नौकरशाही’ का मतलब यह है कि न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हों?
न्यायपालिका से संघर्ष
न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था। इस क्रम में तीन संवैधानिक मसले उठे थे: क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा यह कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छाँट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार, संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरे, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति-निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। आपको याद होगा कि इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढाँचा है और संसद इन ढाँचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है।
दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढ़ाया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फ़ैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फ़ैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेज़ी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे एक ऐसी ‘प्रतिबद्ध’ न्यायपालिका तथा नौकरशाही की ज़रूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। इस संघर्ष का चरमबिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया।
आपातकाल की घोषणा
12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फ़ैसला सुनाया। इस फ़ैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति ने यह फ़ैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण, इंदिरा गाँधी के खिलाफ़ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव-प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले का मतलब यह था कि कानूनन अब इंदिरा गाँधी सांसद नहीं रहीं और अगर अगले छह महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होतीं, तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकतीं। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फ़ैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गाँधी सांसद बनी रहेंगी; लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं।
संकट और सरकार का फ़ैसला
एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गाँधी के इस्तीफ़े के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गाँधी से इस्तीफ़े की माँग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्नान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज के ठप्प हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज़ अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ़ हो गया।
यह तो सेना से सरकार के खिलाफ़ बगावत करने को कहने जैसा जान पड़ता है! क्या यह बात लोकतांत्रिक है?

सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में ‘आपातकाल’ की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा ज़रूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना
आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बँटवारे का संघीय ढाँचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में चली आती हैं। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

यह कार्टून आपातकाल की घोषणा के चंद रोज़ पहले छपा था। इसमें मौजूदा राजनीतिक संकट की आहटों को पढ़ा जा सकता है। कुर्सी को पीछे से सहारा देता हाथ कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ का है।


सरकार की शक्तियों के दायरे में था क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सबेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था।
परिणाम
सरकार के इस फ़ैसले से विरोध-आंदोलन एकबारगी रुक गया; हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचारपत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मम्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ।

क्या राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफारिश के बगैर आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए थी? कितनी अजीब बात है।
सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ़्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है बल्कि इसके विपरीत, इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ कीं। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया गया। वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई ज़रूरी नहीं है। अनेक उच्च न्यायालयों ने फ़ैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी हो। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फ़ैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फ़ैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे़ बंद हो गए। इस फ़ैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फ़ैसलों में एक माना गया।
अरे! सर्वोच्च न्यायालय ने भी साथ छोड़ दिया! उन दिनों सबको क्या हो गया था?

आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएँ घटीं। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे ‘भूमिगत’ हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ़ मुहिम चलायी। ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘स्टेट्समैन’ जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। ‘सेमिनार’ और ‘मेनस्ट्रीम’
जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज़लेटर और लीफ़लेट्स निकले। पद्मभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी-अपनी पदवी लौटा दी। बहरहाल, मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए।

जिन चंद लोगों ने प्रतिरोध किया, उनकी बात छोड़ दें- बाकियों के बारे में सोचें कि उन्होंने क्या किया! क्या कर रहे थे बड़े-बड़े अधिकारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक-धार्मिक नेता और नागरिक …?
संसद ने संविधान के सामने कई नयी चुनौतियाँ खड़ी कों। इंदिरा गाँधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42 वाँ संशोधन पारित हुआ। आप पढ़ चुके हैं कि इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42 वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक था-देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई थी। इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को एक साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे।
…डी. ई. एम. ओ’क्रेसी की मृत्यु पर उनकी पत्नी टी. रूथ, उनके बेटे एल. आई. बर्टी और उनकी बेटियों फेथ, होप और जस्टिस ने शोक व्यक्त किया।
1975 में आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक गुमनाम विज्ञापन।
आपातकाल के सबक
आपातकाल से एकबारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियाँ उजागर हो गईं। हालाँकि बहुत-से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है।
दूसरे, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब ‘अंदरूनी’ आपातकाल सिर्फ़ ‘सशस्त्र विद्रोह’ की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे।
आज भारत की आजादी का दिन है… भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने न पाए।
फ्री जेपी कैम्पेन यह विज्ञापन द टाइम्स (लंदन) में 15 अगस्त 1975 को छपवाया गया था।
तीसरे, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए।
बहरहाल, आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोज़मर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सधा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ऐसे विरोध की सीमा क्या मानी जाए?
दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के ज़रिए हुआ। ये संस्थाएँ स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाईं। इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औज़ार बनाकर इस्तेमाल किया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहों हुई।
आपातकाल के बाद की राजनीति
जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे ज़रूरी और कीमती सबक राजव्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत-संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खासतौर पर क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज़्यादा महसूस किया गया था। विपक्ष ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ़ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र-विरोधी माना उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975-77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई।

मोरारजी देसाई ( 1896-1995) : स्वतंत्रता सेनानी, गाँधीवादी नेता; खादी, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक; बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री; 1967-1969 के बीच उप-प्रधानमंत्री; पार्टी में टूट के बाद कांग्रेस (ओ) में शामिल; 1977-1979 तक एक गै-कांग्रेसी दल की तरफ़ से प्रधानमंत्री रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को
लोकसभा के चुनाव-1977
18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फ़ैसला किया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज़ थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियाँ एक-दूसरे के नज़दीक आ रही थीं। चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। नयी पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया।

देखिए कि एक कार्टूनिस्ट ने 1977 के चुनावों में हारने और जीतने वालों को किस तरह देखा है। आम आदमी के साथ खड़े हुए लोगों में जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और अटलबिहारी वाजपेयी को दिखाया गया है।
कांग्रेस के कुछ नेता भी, जो आपातकाल के खिलाफ़ थे, इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नयी पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम ‘कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी’ था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई।
1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव-प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज़्यादतियों पर ज़ोर दिया। हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर-कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिलकुल साफ़ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी।
लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आज़ादी के बाद लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थीं। उसे 35 प्रतिशत से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिलों। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ़ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट न पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक-एक सीट मिली। इंदिरा गाँधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गाँधी अमेठी से चुनाव हार गए।
बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नज़र दौड़ाएँ, तो पाएँगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक-टोक चला था। इसके कई कारण रहे। पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एकसमान नहीं पड़ा था। लोगों को ज़बरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा ज़बरन नसबंदी करने का काम ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए थे। उत्तर भारत का मध्यवर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था और मध्यवर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े। इस अर्थ में देखें, तो 1977 के चुनाव सिर्फ़ आपातकाल की कथा नहीं कहते हैं, बल्कि इसके आगे की भी कुछ बातों का संकेत करते हैं।
जनता सरकार
1977 के चुनावों के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। मोरारजी देसाई 1966-67 से ही इंदिरा गाँधी के प्रतिद्वंद्धी थे। चरण सिंह, भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म न हुई।

1977 में बनी गैर-कांग्रेसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। चित्र में जयप्रकाश नारायण, जे. बी. कृपलानी, मोरारजी देसाई और अटलबिहारी वाजपेयी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।

नोटः यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए।

अगर उत्तर और दक्षिण के राज्यों में मतदाताओं ने इतने अलग करें पर मतदान किया, तो हम कैसे " कहें कि 1977 के चुनावों का जनादेश क्या था?
इस मानचित्र में उन जगहों को चिह्नित करें, जहाँ
- कांग्रेस हारी
- कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई
- ऐसे राज्य जहाँ कांग्रेस और उसके साथी दलों को भारी विजय मिली।
उत्तर भारत में वे कौन से निर्वाचन क्षेत्र हैं जिन्हें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही?



जनता पार्टी की गुटबाजी पर बहुत-से कार्टून बने। उसकी कुछ बानगी यहाँ आप भी देखें। ये कार्टून अंग्रेज़ी भाषा के अखबार और पत्रिकाओं में छपे।

चौधरी चरण सिंह( 1902-1987 ) : जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री; स्वतंत्रता सेनानी; उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय; ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक; कांग्रेस छोड़ी और 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन; उत्तर प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री; बाद में 1977 में जनता पार्टी के संस्थापको में से एक, उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री (1977-79); लोकदल के संस्थापक।

मैं समझ गया! आपातकाल एक तरह से तानाशाही निरोधक टीका था। इसमें दर्द हुआ और बुखार भी आया, लेकिन अंततः हमारे लोकतंत्र के भीतर क्षमता बढ़ी।
आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फ़ैसला किया। इस वज़ह से चरण सिंह की सरकार मात्र चार महीने तक सत्ता में रही। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को ज़बरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनावों वाली कहानी दुहराते हुए भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिलीं और वह सत्ता में आई। 1977-79 के चुनावों ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया-सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं।

जगजीवन राम (
) : स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेसी नेता; के बीच भारत के उप-प्रध ानमंत्री; संविधान सभा के सदस्य; 1952 से मृत्युपर्यंत सांसद; स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री; 1952 से 1977 के बीच अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी; विद्वान और कुशल प्रशासक।
विरासत
लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ़ इंदिरा गाँधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भर था? 1977 और 1980 के चुनावों के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद से कांग्रेस का सबको समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ। 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गति-मति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेटकर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और ग़रीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू किया। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ़ कितना खींच पाती है। इसके साथ-साथ यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर हुई। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल ‘गैर-कांग्रेसवाद’ की राजनीति की तरफ़ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ़-साफ़ नज़र आने लगी कि चुनावों में गैर-कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज़ ने 1977 के चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाई।
अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। हमने ऊपर गौर किया था कि 1977 के चुनाव-परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था, खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनावों के बाद, 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में ‘अन्य पिछड़ी जातियों’ के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद

यह कार्टून 1980 के चुनावों के बाद छपा था।
केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया। इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज़्यादा विस्तार से आप अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। आपातकाल के बाद हुए चुनावों ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी।
आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ़ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था।
आइए एक फिल्म देखें

सिद्धार्थ, विक्रम और गौत्ता मेधायों और सामाजिक सरोकार वाले छात्र हैं। दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तीनों अलग-अलग राह पर निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ सामाजिक बदलाव के लिए क्रांतिकारी विचारधारा का हिमायती है। विक्रम की दलील जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की है, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करने निकले इन लोगों के सुख-दुख के इर्द-गिर्द यह कहानी चलती है।
फ़िल्म की पृष्ठभूमि सत्तर के दशक की है। इस फ़िल्म के युवा चरित्र उस दौर की अपेक्षाओं और आदर्शवाद की उपज हैं। सिद्धांत क्रांति के अपने मकसद में सफल नहीं होता है, लेकिन वह गरीबों के दुख-दर्द इस तरह अपना चुका है कि उसे क्रांति की जगह ऐसे लोगों की हालत में थोड़ी बेहतरी ला पाना भी अच्छा लगने लगता है। दूसरी तरफ, विक्रम एक आमफहम राजनीतिक तिकड़मबाज बन जाता है। लेकिन अपने इस काम को लेकर उसका मन कचोटता रहता है।
वर्ष : 2005
निर्देशक : सुधीर मिश्र
पटकथा : रुचि नारायण, शिव कुमार, सुब्रह्मण्यम
अभिनय: के. के. मेनन, शाइनी आहूजा, चित्रांगदा सिंह
सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। फिर भी, इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप्प करने का फ़ैसला किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए ही करेगी। इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुँमुखी शक्तियाँ दे दी गईं। इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ। यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज़्यादा संगीन था।
इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतःस्फूर्त जन-भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नज़र आया। इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। आगे के अध्याय में हम इस तनाव की कुछ अभिव्यक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में हम विशेष रूप से क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी बहसों के बारे में पढ़ेंगे।
प्रश्नावली
1. बताएँ कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत-
(क) आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गाँधी ने की।
(ख) आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए।
(ग) बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र आपातकाल की घोषणा की गई थी।
(घ) आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
(ङ) सी.पी.आई. ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया।
2. निम्नलिखित में से कौन-सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ से मेल नहीं खाता है:
(क) ‘संपूर्ण क्रांति’ का आहवान
(ख) 1974 की रेल-हड़ताल
(ग) नक्सलवादी आंदोलन
(घ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला
(ङ) शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष
3. निम्नलिखित में मेल बैठाएँ
(क) संपूर्ण क्रांति
(ख) गरीबी हटाओ
(ग) छात्र आंदोलन
(घ) रेल हड़ताल
(i) इंदिरा गाँधी
(ii) जयप्रकाश नारायण
(iii) बिहार आंदोलन
(iv) जॉर्ज फर्नाडिस
4. किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े?
5. जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे?
6. 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे?
7. 1977 के चुनावों के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ?
8. हमारी राजव्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ?
- नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर इसका असर
- कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध
- जनसंचार माध्यमों के कामकाज
- पुलिस और नौकरशाही की कार्रवाइयाँ
9. भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से करें।
10. निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें-
1977 के चुनावों के दौरान भारतीय लोकतंत्र, दो-दलीय व्यवस्था के जितना नज़दीक आ गया था उतना पहले कभी नहीं आया। बहरहाल अगले कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया। हारने के तुरंत बाद कांग्रेस दो टुकड़ों में बँट गई….. जनता पार्टी में भी बड़ी अफरा-तफरी मची……..डेविड बटलर, अशोक लाहिड़ी और प्रणव रॉय - पार्था चटर्जी
(क) किन वज़हों से 1977 में भारत की राजनीति दो-दलीय प्रणाली के समान जान पड़ रही थी?
(ख) 1977 में दो से ज़्यादा पार्टियाँ अस्तित्व में थीं। इसके बावज़ूद लेखकगण इस दौर को दो-दलीय प्रणाली के नज़दीक क्यों बता रहे हैं?
(ग) कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से टूट पैदा हुई?