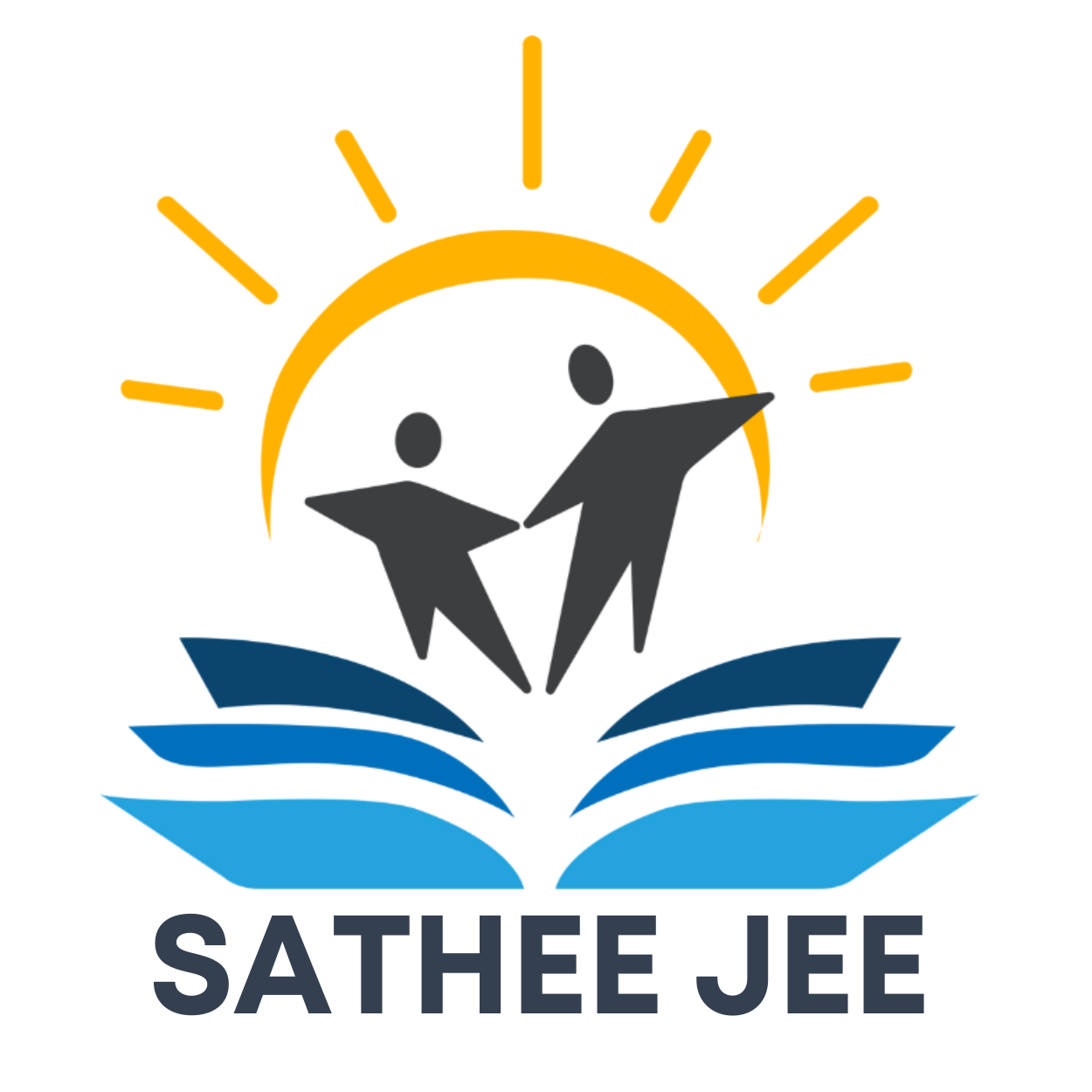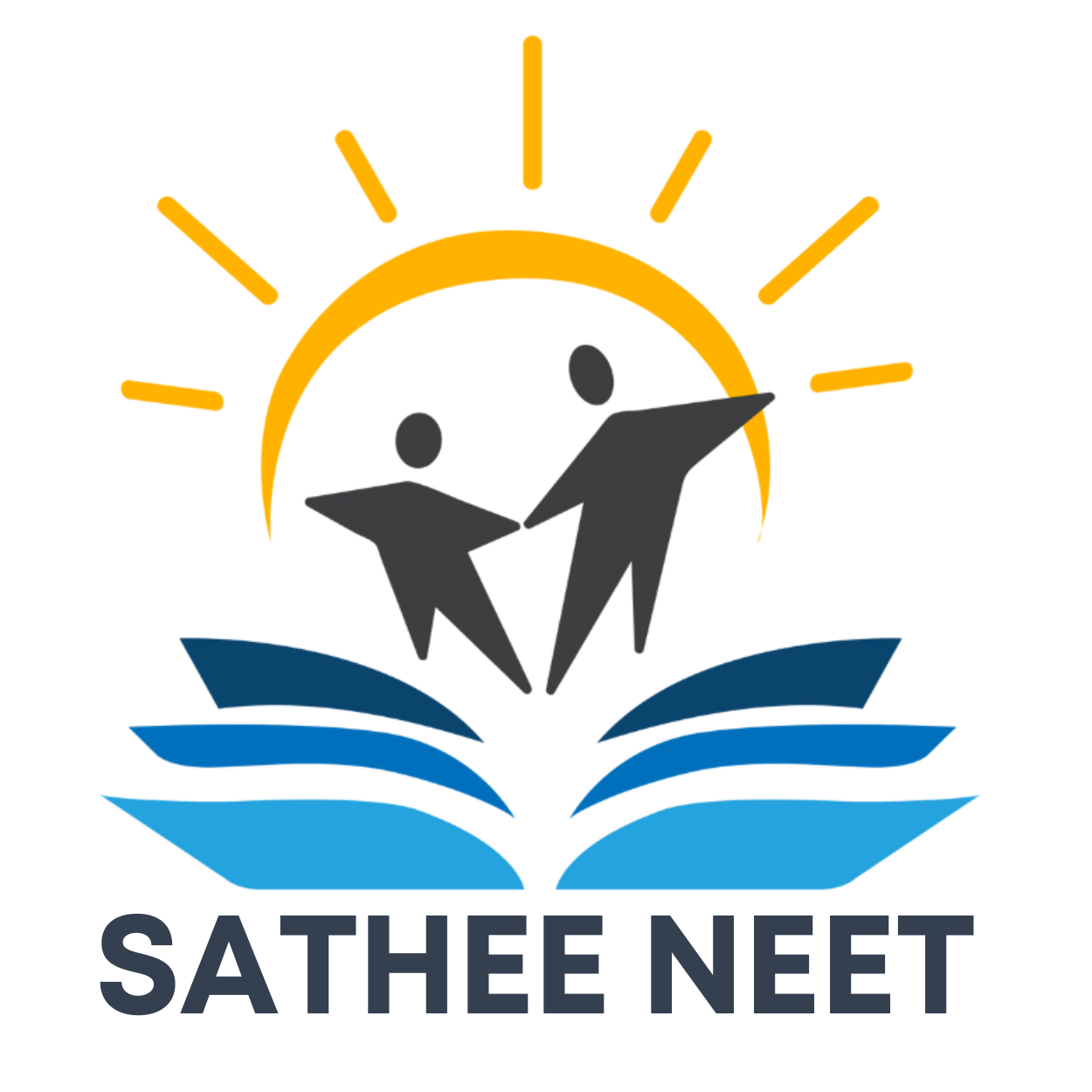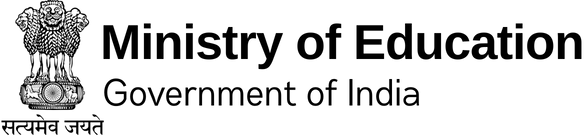अध्याय 08 भारत की जीवंत कला परंपराएँ
भारत में विभिन्न पारंपरिक कलाएँ हैं जो गाँव-शहर, रेगिस्तान, पहाड़ तक फैली हैं। ये कलाएँ आज भी जनमानस द्वारा अपनाई जा रही हैं। अब तक, हमने कला का अध्ययन समय के सापेक्ष किया है। कला अवधि का नामकरण किसी स्थान या राजवंशों के नाम पर किया गया है, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर कई वर्षों तक शासन किया। परंतु आम लोगों का क्या? क्या वे रचनात्मक नहीं थे? क्या उनके आसपास कोई कला मौजूद नहीं थी? राजदरबार या कला संरक्षकों के पास कलाकार कहाँ से आते थे? शहरों में आने से पहले वे कहाँ कार्य करते थे? या अभी भी वे अज्ञात कलाकार कौन हैं जो दूर रेगिस्तान, पहाड़, गाँव और ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्प बना रहे हैं, जिन्होंने कभी भी कला विद्यालय अथवा डिज़ाइन संस्थान या यहाँ तक कि किसी विद्यालय से औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली।
भारत में हमेशा स्वदेशी (देशज या स्थानीय) ज्ञान का भंडार रहा है, जो एक पीढ़ी से दसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण (स्थानांतरित) होता रहा है। प्रत्येक पीढ़ी में कलाकारों ने उपलब्ध सामग्री और तकनीक से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण किया है। असंख्य विद्वानों ने इन कला रूपों को लघुकला, उपयोगिता कला, लोक कला, जनजातीय कला, जनसाधारण कला, संस्कार कला, शिल्प और इसी तरह के कई नाम दिए हैं। हम जानते हैं कि ये कला अति प्राचीन काल (स्मरणातीत) से अस्तित्व में हैं। पूर्व-ऐतिहासिक काल के भित्ति चित्र और सिंधु काल के मिट्टी के बरतनों, टेराकोटा, कांस्य, हाथी दाँत की कलाकृतियों के उत्कृष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रारंभिक इतिहास और उसके बाद के समय के दौरान, हमें हर जगह कलाकारों के समुदाय के संदर्भ (निशान) मिलते हैं। उन्होंने बरतन और कपड़े, आभूषण और अनुष्ठान या मन्नत की मूर्तियों का सृजन किया है। उन्होंने अपनी दीवारों और फ़र्श को सजाया और कई कलात्मक कार्य अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किए। इसके साथ ही स्थानीय बाज़ारों में अपने कलाकृतियों की आपर्ति भी की। उनकी रचनाओं में स्वाभाविक (प्राकृतिक) सौंदर्यबोध की अभिव्यक्ति है। इनमें प्रतीकात्मकता, रूपांकन का विशेष उपयोग, सामग्रियों, रंग और बनाने की विधियों का विशिष्ट उपयोग लोक कला के निर्माण में किया जाता है। लोक कला और शिल्प के बीच एक पतली रेखा है। इन दोनों में रचनात्मकता, अंत: प्रेरणा (स्वाभाविक), आवश्यकताएँ और सौंद्यबोध शामिल हैं।

आज भी कई क्षेत्रों में हमें ऐसी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में, भारत और पश्चिम (यूरोप) में एक नया परिप्रिक्य आधुनिक कलाकारों के मध्य उत्पन्न हुआ जब उन्होंने अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए अपने आसपास की लोक कला (पारंपरिक कला) को प्रेरण के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद हस्तकला उद्योग का पु-रुद्धार हुआ। यह क्षेत्र व्यावसायिक उत्पादन के लिए भी संगठित हो गया। इस कला ने एक विशिष्ट पहचान भी प्राप्त की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के साथ, उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित राज्य के विक्रय केंद्र (एम्पोरिया) में अपनी विभिन्न अद्वितीय कलाओं और उत्पादों का प्रदर्शन किया है। भारत की कला और शिल्प परंपराएँ भारत के पाँच हज़ार सालों से अधिक की मूर्त (वास्तविक) विरासत के इतिहास को प्रदर्शित करती हैं। हालाँकि हम इनमें से कई को जानते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर, धार्मिक या अनुष्ठानिक कृतियों में समृद्ध प्रतीक हैं और साथ ही उपयोगी और सजावटी सामग्री जिन्हें हम दिनचर्चा में उपयोग में लाते हैं, उनका निर्माण भी किया जाता है।
चित्रकारी परंपरा
मिथिला या बिहार की मधुबनी पेंटंग, महराष्ट्र की वरली पेंटंग, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की पिथोरो पेंटंग, राजस्थान की पाबूजी की फड़ पेंटिंग, नाथद्वारा की पिछावई, मध्य प्रदेश की गोंड और सांवरा पेंटिंग, ओडिशा और बंगाल की पटचित्र आदि चित्रकला (लोक कला) के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ, उनमें से कुछ पर चर्चा की गई है।
मिथिला कला
मिथिला कला सबसे प्रसिद्ध समकालीन चित्रकला रूपों में से एक है जिसका नामकरण मिथिला प्रदेश के नाम पर आधारित है। मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था और ज़िला मधुबनी के नाम पर इसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। यह एक (व्यापक रूप से) मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध लोक कला परंपरा है। यह माना जाता है कि सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाएँ औपचारिक अवसरों, विशेष रूप से विवाह के अवसर पर अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर आकृतियों से अलंकरण करती हैं। इस क्षेत्र के लोग इस कला की उत्पत्ति का समय राजकुमारी सीता और भगवान श्रीराम के विवाह से मानते हैं।

चमकीले रंगों की विशेषता वाले इन चित्रों को मुख्य रूप से घर के तीन क्षेत्रों में चित्रित किया जाता है- केंद्रीय या बाहरी आँगन, घर का पूर्वी भाग (जो कुलदेवी का निवास स्थान है), आमतौर पर, काली और अलग से एक कमरा (जो दक्षिणी भाग में स्थित हो), जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र का चिर्रण किया जाता है। इस कमरे में विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित देवता के चित्र का चित्रण किया जाता है। पशु या महिलाओं की काम करते हुए छवियों को जैसे कि पानी के बरतन ले जाती हुईं, सुप से अनाज साफ करती हुईं इत्यादि, को बाहरी केंद्रीय प्रांगण में चित्रित किया गया है। भीतर के बरामदे (पारिवारिक देवस्थान या गोसाईं का स्थान है), वहाँ गृह देवता और कुलदेवता का चित्रण किया जाता है। हाल के दिनों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कपड़े, कागज़, बरतन आदि पर इस प्रकार के कई चित्रांकन किए जा रहे हैं।
सबसे असाधारण और रंगीन चित्रण घर के उस हिस्से में किया जाता है जिसे कोहबर घर या भीतरी कमरा नाम से जाना जाता है, जिससे कोहबर की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। कमरे के नए पलस्तर पर एक संपूर्ण खिला हुआ कमल अपने डंठल के साथ दीवारों पर चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही देवी-देवताओं का भी चित्रण किया जाता है।
अन्य विषयों में भागवत पुराण, रामायण, शिव-पार्वती की कहानियाँ, दुर्गा, काली और राधा-कृष्ण की रास-लीला के प्रसंग भी चित्रित किए जाते हैं। मिथिला के कलाकारों को रिक्त (खाली) स्थान पसंद नहीं हैं। वे समस्त स्थानों को पक्षियों, फूलों, जानवरों, मछली, साँप, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकृति के तत्वों से अंकित करते हैं, जिसमें अकसर प्रतीकात्मक अर्थ होता है। यह प्रेम, जुनून, उर्वरता, अनंत काल, कल्याण और समृद्धि का प्रतीक है। महिलाएँ बाँस की टहनियों में कपास, चावल का भूसा या रेशों को लगाकर चित्रण करती हैं। पूर्वकाल में वे खनिज, पत्थर और जैविक सामग्री जैसे कि फालसा और कुसुम के फूल, बिल्व के पत्ते, काजल, हल्दी आदि से रंग बनाती थीं।
वरली चित्रकला
वरली समुदाय उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के आसपास के उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र में विशाल संख्या में निवास करते हैं। यह क्षेत्र ठाणे ज़िले में है। विवाहित महिलाएँ चौक नामक चित्राकंन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, जहाँ विशेष अवसरों पर वह चौक बनाती हैं। यह शादी, प्रजनन, फ़सल और बुवाई-कटाई के रीति-रिवाज़ों से संबंधित है। चौक देवी माँ पालघाट की आकृति पर आधारित होती है, जिसे मुख्य रूप से प्रजनन की देवी के रूप में पूजा जाता है जो मकई की देवी, कंसारी का प्रतिनिधित्व करती है।

कंसारी देवी को एक छोटे वर्ग के फ्रेम में लगाया जाता है जिसके बाहरी किनारों को नुकीले कड़ी (शेवरॉन) से सजाया गया है। यह बाहरी किनारा हरियाली देवता, अर्थात् पौधों के देवता का प्रतीक है। कंसारी देवी के प्रहरी और अभिभावक की कल्पना, एक बिना सिर वाले योद्धा के रूप में की जाती है, वे घोड़े पर सवार या उन पर खड़े होते हैं जिनके गले से पाँच मकई के पौधे उगते हुए चित्रण किया जाता है और इसलिए इन्हें पंच सिर्या देवता (पाँच सिर वाले भगवान) कहा जाता है। यह खेत्रपाल या खेतों के संरक्षक का भी प्रतीक माना जाता है।
वरली चित्रकार अपने आसपास रोज़र्रा के क्रियाकलाप, मुंबई जीवन, चलती बसें, मछली पकड़ना, खेती, पौराणिक कहानियों के किरदार, नृत्य आदि का चित्रण करते हैं। इन चित्रों को पारंपरिक रूप से चावल के आटे से अपने घरों के भूरंगों के दीवारों पर चित्रित किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए, मृतकों को संतुष्ट करने के लिए और आत्माओं की माँगों को पूरा करने के लिए इन चित्रों का चित्रण किया जाता है। एक बाँस की छड़ी के एक सिरे को चबाकर तलिका के रूप में उपयोग किया जाता है।
गोंड चित्रकला
मध्य प्रदेश के गोंड की लोक कला मध्य भारत की एक विख्यात चित्रकला है। वे प्रकृति की पूजा करते थे। मंडला के गोंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में जानवरों, मनुष्यों और वनस्पतियों के रंगीन चित्रों का चित्रण किया जाता है। ज्यामितीय आकार के धार्मिक चित्रों को झोपड़ियों की दीवारों पर चित्रित किया जाता है। इन चित्रों में कृष्ण को गायों और गोपियों से घिरा हुआ चित्रित किया जाता है। जिनमें गोपियों के सिर पर घड़ा होता है जिसे बालक एवं बालिकाएँ कृष्ण को भेंट कर रहे होते हैं।


पिठोरो चित्रकला
गुजरात में पंचमहल क्षेत्र के राठवा भीलों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में झाबुआ में चित्रित इन चित्रों को घरों की दीवारों पर विशेष अवसर या धन्यवाद उत्सवों पर चित्रित किया जाता है। ये बड़े भित्ति चित्र हैं, जहाँ पंक्तियों मे कई भव्य रंगीन देवताओं को घोड़े पर सवार दर्शाया जाता है।
घोड़ा सवार देवताओं की पंक्तियाँ, राठवाओं के ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे ऊपर घुड़सवार देवताओं का खंड, स्वर्गीय निकायों और पौराणिक प्राणियों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। एक अलंकृत लहराती रेखा इस खंड को निचले खंड (क्षेत्र) से अलग करती है, जहाँ पिठोरो की शादी की बारात जिसमें गौण देवता, राजाओं, देवियों, एक आदर्श किसान, घरेलू जानवरों इत्यादि को पृथ्वी पर दर्शाया जाता है।


पट चित्रकला
चित्रकला का एक और रूप पटचित्र है जिसे कपड़े, ताड़ के पत्ते या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिम में गुजरात और राजस्थान और पूर्व में ओडिशा और बंगाल में प्रचलित कला रूप है। इसे पट, पचीसी, फड़ आदि के नाम भी जाना जाता है।
बंगाल के पट में कपड़े (पट) पर चित्रकारी होती है जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कहानी कहने का कार्य करते हैं। यह सबसे अधिक सुनने वाली मौखिक परंपरा है, जो लगातार नए विषयों की और दुनिया में प्रमुख घटनाओं पर प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करती हैं।
लंबबत् चित्रित पट, पटुआ कलाकार द्वारा पट चित्रकला में इस्तेमाल किया जाता है। पटुआ, जिसे चित्रकार भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बीरभूम और बांकुरा क्षेत्रों के आसपास एवं बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बसे समुदायों से संबंधित हैं। पट चित्रण और रखरखाव (संभालना) उनका वंशानुगत पेशा है। वे गाँवों में घूमते हैं, चित्रों को प्रदर्शित करते हैं और चित्रित किए गए आख्यानों को गाते हैं। प्रदर्शन गाँव के साझा (या सामान्य) स्थानों पर होते हैं। पटुआ हर बार तीन से चार कहानियाँ सुनाता है। प्रदर्शन के बाद, पटुआ को नकद या उपहार दिया जाता है।

पुरी पट या चित्रका, मंदिरों का शहर पुरी, ओडिशा की विख्यात लोक कला है। इसमें शुरुआत में मुख्यतः पट पर चित्रण किया जाता था, लेकिन अब कागज़ पर भी चित्रण किया जाता है। इसमें विभिन्न विषयों का चित्रण किया जाता है, जैसे कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दैनिक और विशेष अवसरों की वेशभूषा (पोशाक), (जैसे— बड़ा भृंगार वेश (परिधान), रघुनाथ वेश, पद्म वेश, कृष्ण-बलराम वेश, हरिहरन वेश आदि); रस चित्र, अंसारा पट्टी (गर्गशृह के देवी-देवताओं का प्रतीकात्मक चित्रण जिन्हें, सफ़ाई और स्नानायात्रा के समय नई रंगाई के लिए हटाया जाता है); जात्री पटी (तीर्थयात्रियों के लिए यादगार के रूप में और उन्हें घर के व्यक्तिगत मंदिरों में रखने के लिए), जगन्नाथ की पौराणिक कथाओं की भृंखलाओं, जैसे—कांची कावेरी पटा और थिया-बड़हिया पटा, मंदिर के हवाई और पार्श्व दृश्य का संयोजन के साथ देवी-देवताओं और मंदिर के आसपास या त्यौहारों का चित्रण किया जाता है।

पटचित्रों को सूती कपड़े की छोटी-छोटी पट्टियों या टुकड़ों पर किया जाता है, जिसे मुलायम सफ़ेद पत्थर के चूरन (पाउडर) और इमली के बीजों से बने गोंद के साथ कपड़े के सतह द्वारा तैयार किया जाता है। सबसे पहले किनारों को बनाने की प्रथा है। सीधे तूलिका के उपयोग से आकृतियों की संरचना की जाती है और सपाट रंग भरे जाते हैं। आमतौर पर सफ़ेद, काला, पीला और लाल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रण पूरा होने के बाद, चित्र को कोयले की आग के ऊपर रखा जाता है और सतह पर लाह को लगाया जाता है जिससे चित्र पानी प्रतिरोधी और चमक उत्पन्न कर सके। रंग, जैविक और स्थानीय रूप से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, काला को दीप से, पीला और लाल को क्रमशः हरिताली और हिंगल पत्थर से, सफ़ेद रंग शंख के चूर्ण से प्राप्त किया जाता है। ताड़ की पांडुलिपियों को एक विशेष प्रकार के ताड़, जिसे खर-ताड़ के नाम से जाना जाता है, पर चित्रित किया जाता है। इन पर तूलिका से चित्रण नहीं किया जाता है, वल्कि एक लोहे की कलम से आकृतियों को उकेरा जाता है, फिर स्याही से भरा जाता है और कभी-कभी इनमें रगंों को भी भरा जाता है। इन चित्रों के साथ कुछ लेखन भी संकलन हो सकते हैं। ताड़ पत्र पर चित्रण की कला परंपरा को लोक कला माना जाए या परिष्कृत कला के अंग के रूप में स्वीकार्य किया जाए जिसका संबंध देश के पूर्वी और अन्य हिस्सों की भित्ति और ताड़ पत्र चित्रण की परंपराओं से है, यह एक चर्चा का विषय है।
राजस्थान की फड़ लोक कला
फड़, लंबे, क्षैतिज, कपड़े के पटचित्र होते हैं, जिस पर भीलवाड़ा क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदाय के लोग लोक देवता का चित्रण करते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पशुधन को सुर्कित रखना होता है। इस तरह के विचार उनकी कहानियों, किंवदंतियों और पूजा पद्धतियों में प्रतिबिंबित होते हैं। उनके देवताओं के साथ उन बहादुर वीरों का भी चित्रण किया जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर मवेशियों को लुटेों से बचाया। इन्हें भोमिया कहा जाता है। इन नायकों को उनके कार्यों और बलिदान या शहादत के लिए सम्मानित, पूजा और याद किया जाता है। भोमिया, जैसे- गोगाजी, जेजाजी, देव नारायण, रामदेवजी और पाबूजी की व्यापक पंथ की परंपरा का राबरिया, गुर्जर, मेघवाल, गैगर और अन्य समुदाय के लोग अनुसरण करते हैं।
इन भोमियाओं की वीरतापूर्ण कहानियों को फड़ पर दर्शाते हैं। भोपों यात्रा करते समय अपने साथ फड़ रखते हैं और भोमियों की वीर गाथाएँ या कथाएँ सुनाते समय इन्हें प्रस्तुत करते हैं। भोपों रात भर चलने वाले कथा प्रदर्शनों में इन नायक-देवताओं से जुड़े भक्ति गीत गाते हैं। जिन चित्रों के बारे में बात की जा रही होती है, उन्हें रोशन करने के लिए फड़ के उस अंश पर एक दीपक से प्रकाश किया जाता है। भोपा और

उसका साथी रावणनाथ और वीणा जैसे वाद्ययंत्रों के साथ प्रस्तुति करते हैं और गायन की खयाल शैली का गान करते हैं।
हालाँकि, फड़ को भोपों द्वारा चित्रित नहीं किया जाता है। उन्हें पारंपरिक रूप से ‘जोशीस’ नामक एक जाति द्वारा चित्रित किया जाता है, जो राजस्थान के राजाओं के दरबार में चित्रकार होते थे। राजदरबार इन चित्रकारों को लघुचित्रों के निर्माण के लिए संरक्षण प्रदान करते थे। इसलिए, कुशल व्यवसायी का संघ, कवि संगीतकार और दरबारी कलाकार फड़ को अन्य सांस्कृतिक परंपराओं से उच्च स्थान प्रदान करते हैं।
मार्तिकला परंपरा
मूर्तिकला परंपरा, मिट्टी (मृण्मूर्ति), धातु और पत्थर से मूर्तियाँ बनाने की लोकत्रिय परंपराओं से संबंधित है। देशभर में ऐसी अनेक लोक कला परंपराएँ हैं। उनमें से कुछ पर यहाँ चर्चा की गई है।
डोकरा कास्टिंग
लोकप्रिय मूर्तिकला परंपराओं में, कांस्य की ढलाई या सेरे पर्दु तकनीक से बनाई गई डोकरा या धातु की मूर्तियाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के सबसे प्रमुख धातु शिल्पों में से एक है। इसमें पिघला हुआ मोम विधि के माध्यम से कांस्य की ढलाई शामिल है। बस्तर के धातु कारीगरों को गढ़वा कहा जाता है। लोकप्रिय शब्दावली में ‘गढ़वा’ शब्द का अर्थ है आकार देना और बनाने की क्रिया। शायद इसी कारण कलाकारों को गढ़वा नाम दिया गया है। परंपरागत रूप से गढ़वा कारीगर ग्रामीणों के दैनिक उपयोग के बरतनों की आपूर्ति के अलावा, आभूषण, स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित देवताओं की मूर्ति और मन्नत के चढ़ावा में साँप, हाथी, घोड़े, अनुष्ठान के बरतन आदि का निर्माण करते हैं। इसके बाद समय के साथ समुदाय में बरतन और पारंपरिक आभूषणों की माँग में कमी आने के बाद, इन शिल्पकारों ने नए (गैर-पारंपरिक) रूपों और कई सजावटी वस्तुओं का निर्माण शुरू किया।
डोकरा की ढलाई एक विस्तृत प्रक्रिया है। नदी के किनारे से काली मिट्टी को चावल की भूसी के साथ मिलाकर पानी से गूंधा जाता है। मुख्य आकृति (कोर फ़िगर) या मोल्ड को इसी से बनाया जाता है। सूखने के बाद इस पर गोबर में मिट्टी मिलाकर इसे दूसरी परत से ढक दिया जाता है। साल के पेड़ से एकत्रित राल को तब तक मिट्टी के बरतन में गर्म किया जाता है जब तक कि वह तरल न हो जाए, इसमें कुछ सरसों का तेल भी मिलाकर उबाला जाता है। उबलते तरल को एक कपड़े के माध्यम से छान लिया जाता है और पानी के ऊपर एक धातु के बरतन में इकट्ठा कर रखा जाता है। परिणामस्वरूप राल जम जाता है लेकिन नरम और मुलायम रहता है।

फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग कर दिया जाता है, कोयले की धीमी आँच पर इन्हें थोड़ा गर्म किया जाता है और फिर उत्कृष्ट धागे या कुंडल में फैलाया जाता है। ऐसे धागे पद्टियाँ बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। सूखी मिट्टी के आकार के ऊपर इन राल के पट्टियों या कुंडल को मढ़ा या जोड़ा जाता है और फिर सभी सजावटी विवरण, जैसे— आँखें, नाक आदि को आकृति के साथ बनाया जाता है। उसके बाद मिट्टी के ढाँचे से ढक दिया जाता है। सबसे पहले महीन मिट्टी की परत से, फिर मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण की परत से और अंत में, चावल की भूसी के साथ चींटियों द्वारा बनाए गए मिट्टी के टीलों से प्राप्त मिद्टी की परत चढ़ाते हैं। फिर उसी मिट्टी से बनाए गए एक पात्र को आकृति के निचले हिस्से में जोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ, धातु के टुकड़ों से भरे एक कप को मिट्टी-चावल की भूसी के मिश्रण से बंद कर दिया जाता है। भही में आग के लिए, साल की लकड़ी या उसके कोयले को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। धातु युक्त कप को नीचे मिट्टी के साँचे के साथ रखा जाता है और जलाऊ लकड़ी और बरतन से ढक दिया जाता है। धातु को पिघले हुए अवस्था में बदलने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे तक हवा को भह्ही में लगातार भरा या उड़ाया जाता है। साँचे को चिमटे की मदद से बाहर निकाला जाता है, फिर उसे उलटा कर दिया जाता है, इसके साथ एक तेज़ झटका दिया जाता है और धातु को पात्र (रिसेप्टेक) के माध्यम से डाला जाता है। राल के स्थान पर पिघला हुआ धातु प्रवाहित होता है, जो अब तक वाष्पित हो चुका होता है। साँचे को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और धातु की छवि को प्रकट करने के लिए मिट्टी की परत को तोड़ दिया जाता है।
मृण्मूर्ति
देशभर में सर्वाधिक प्रचलित सर्वव्यापी मूर्तिकला मृण्मूर्ति (टेराकोटा) है। आमतौर पर कुम्हारों द्वारा बनाए गए मृण्मूर्ति मन्नत की पूर्ति पर स्थानीय देवताओं को चढ़ाए जाते हैं या अनुष्ठान और त्यौहारों के दौरान उपयोग किए जाते हैं। वे नदी किनारे या तालाबों पर पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी से बने होते हैं। मृण्मूर्तियों को स्थायित्व के लिए पकाया जाता है। उत्तर-पूर्म में मणिपुर हो या असम, पश्चिमी भारत में कच्छ, उत्तर में पहाड़ियाँ, दक्षिण में तमिलनाडु, गंगा के मैदान या मध्य भारत हो, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की मृण्मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। उन्हें ढाला जाता है, हाथों से बनाया जाता है या कुम्हार के चाक पर बनाया जाता है फिर रंगा या सजाया जाता है। उनके रूप और उद्देश्य अकसर समान होते हैं। वे प्राय: देवी या देवताओं की आकृतियाँ होती हैं, जैसे — गणेश, दुर्गा या स्थानीय देवता, पशु, पभ्षी, कीड़े आदि।