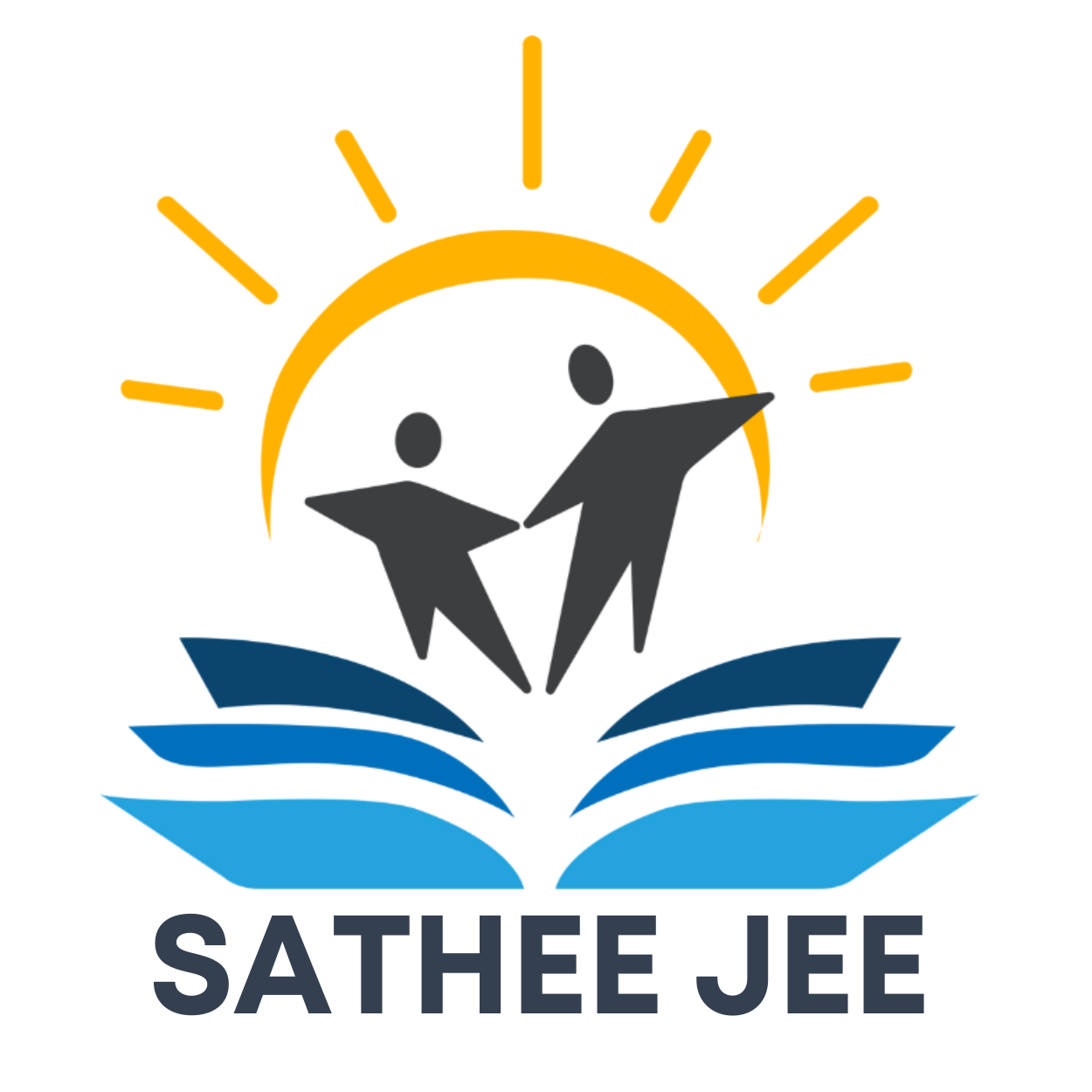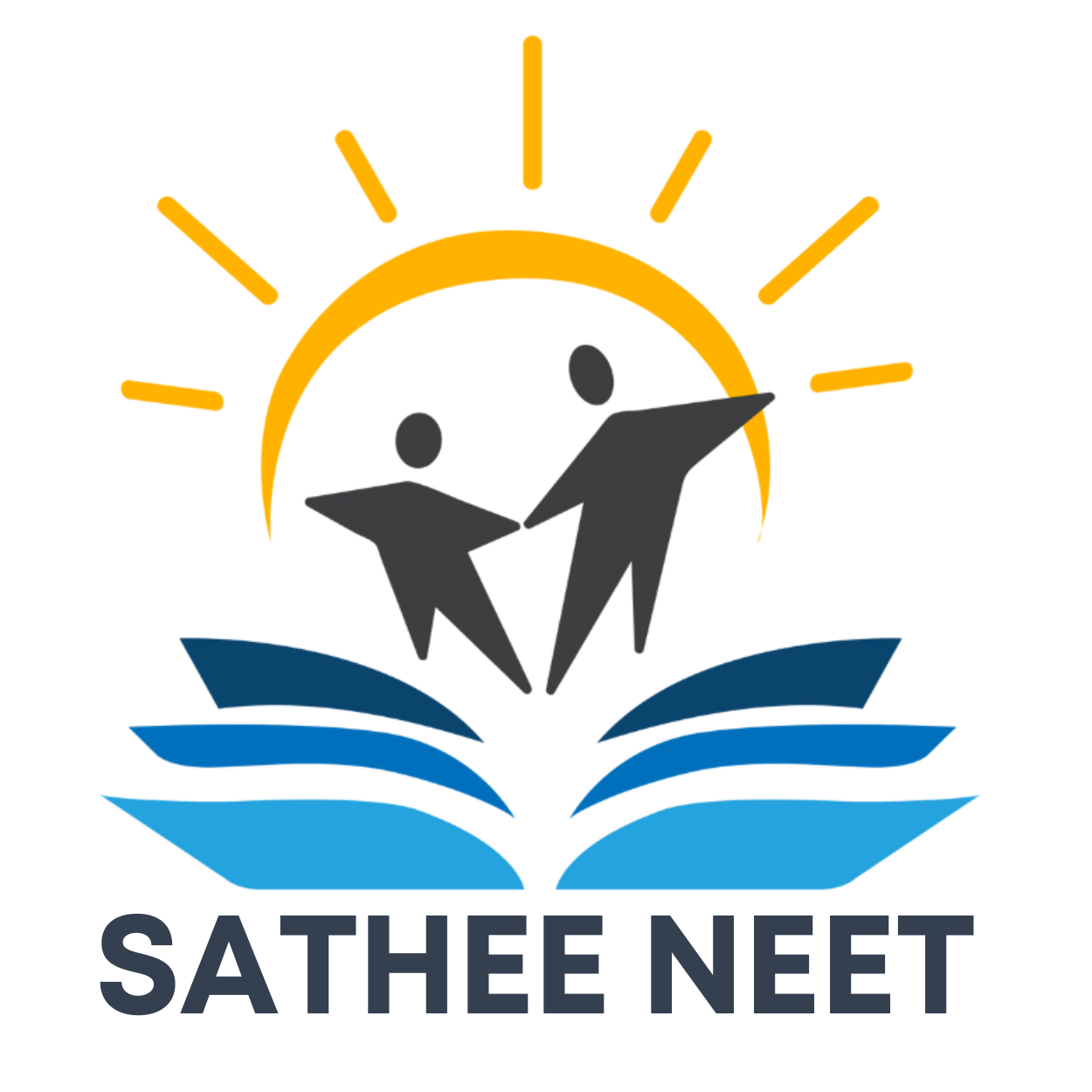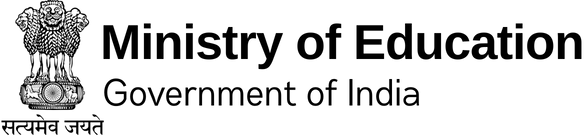अध्याय 01 पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा
पाँचवीं शताब्दी में रचित विष्णुधर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में ‘चित्रसूत्र’ नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चिर्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अध्याय आकृति बनाने की कला से संबंधित है, जिसे ‘र्रतिमा लक्षण’ कहते हैं, जो कि चित्रकला के धर्मसूत्र हैं। इसी खंड में तकनीक, उपकरण, सामग्रियों, सतह (दीवार या भित्ति), धारणा, परिप्रेक्ष्य और मानव आकृतियों के त्रि-आयामों की संरचना का उल्लेख किया गया है। चित्रण के विभिन्न अंग, जैसे— रूप-भेद या दृश्य और आकार, प्रमाण या परिमाप; अनुपात और संरचना; भाव या अभिव्यंजना; लावण्य योजना या सौंर्य रचना; सदृश और वार्णिकभंगा या तूलिका और रंगों के उपयोग की विस्तारपूर्वक उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। इनमें से प्रत्येक के कई उप-भागों का भी उल्लेख किया गया है। कई शताब्दियों से इन धर्मसूत्रों को कलाकारों द्वारा पढ़ा, समझा और अनुसरण किया जाता रहा है। इस प्रकार यह चित्रकला की सभी भारतीय शैलियों और चित्रशालाओं का आधार बना।
मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण ‘लघु चित्रकारी’ के नाम से जाना गया। छोटे आकार का होने के कारण इन लघु चित्रारियों का हाथों में लेकर करीब से अवलोकन किया जाता था। कला संरक्षकों के महलों या राजदरबारों की दीवारों को अकसर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था। इसलिए इन लघु चित्रों का उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था।
चित्रकला का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है, जिनमें महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न विहित, साहित्यिक, संगीत ग्रंथों (पांडुलिपियाँ) का चित्रण किया गया है। चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था। कभी-कभी विषयवस्तु को लेखचित्र के मुख्य पृष्ठ पर न लिखकर पीछे की तरफ़ लिखा जाता था।
पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्थित रूप से विषय अनुसार विभिन्न भागों में रचित किया गया था (प्रत्येक भाग में कई बंधनमुक्त चित्र या पर्ण या पृष्ठ शामिल होते थे)। चित्रकला के प्रत्येक पर्ण (फ़ोलियो) का संबंधित लेख, उस चित्र के ऊपरी भाग के सीमांकित स्थान पर या उसके पीछे अंकित किया गया था। तद्नुसार, किसी के पास रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला आदि के चित्रों का संकलन होगा। प्रत्येक संग्रह को कपड़े के टुकड़े से लपेटकर, राजा या संरक्षक के पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में संग्रहित किया जाता था।
मेवाड़ के विजयसिंह का श्रावक्रत्रत्रमसूत्र कर्णी-कमलचंद्र द्वारा लिखित, 1260 , संग्रह, बोस्टन

संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पर्ण-पृष्ठ (फ़ोलियो पृष्ठ) पुष्पिका पृष्ठ (कोलोफ़ोन पृष्ठ) होता है, जिसमें संरक्षक के नाम की जानकारी, कलाकार या लेखक, तिथि और संग्रह बनाने का स्थान या कार्य या चित्रण पूरा होने की तिथि और इस तरह का अन्य महत्वपूर्ण विवरण लिखा जाता था।
हालाँकि, समय के साथ, पुष्पिका पृष्ठ लुप्त या नष्ट हो चुके हैं। विद्यानों ने उनकी विशेषता के आधार पर इनका विवरण किया है। चित्रकला किसी भी तरह की आपदाओं, जैसे — आग, नमी और अन्य आपदाओं के प्रति अतिसंवेदनशील होती है। शिल्पकृतियों को अनमोल और कीमती माना गया है और यह सुवाह्य भी होती थीं, जिन्हें प्राय: राजकुमारियों के विवाह में उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। राजाओं व दरबारियों के बीच उपहार और कृतज्ञता के रूप में भी चित्रों और कलाकृतियों का आदान-प्रदान बड़े व्यापक एवं व्यावहारिक तौर पर होता था। चित्र तीर्थयात्रियों, भिक्षु, साहसी खोजकर्ता, व्यापारी और पेशेवर कथावाचक के साथ दूरदराज़ के क्षेत्रों में ले जाए जाते थे। उदाहरणस्वरूप, बूँदी के राजा के पास मेवाड़ के चित्रों का संग्रह या इसके विपरीत मेवाड़ के राजा के संग्रह में बूँदी के चित्र मिल सकते हैं।
चित्रकलाओं के इतिहास का पुरर्निर्माण एक अभूतपूर्व कार्य है। दिनांकित की तुलना में अदिनांकित कलाकृतियाँ कम हैं। कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने पर, इनके मध्य कई स्थान रिक्त हैं जिसके बारे में किसी के भी द्वारा इस तरह के चित्रण के विकास या समृद्धि या गतिविधि का अनुमान लगाया जा सकता है। स्थिति की जटिलता तब अधिक बढ़ जाती है, जब ये बिखरे पृष्ठ अपने मूल
भाग का हिस्सा न रहकर विभिन्न संग्रहालयों और निजी संग्रहों में बिखर गए, जो इधर-उधर समय-समय पर देखने को मिलते हैं। ये परिभाषित समय को चुनौती देते हैं और विद्वानों को पुनः कालक्रम में संशोधन करने और उसे पुनर्परिभाषित करने के लिए विवश करते हैं। इस प्रकार अदिनांकित चित्रकलाओं के समूहों को उनकी शेली के आधार और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता रहा है।
पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली
भारत के पश्चिमी भाग में जो चित्रकला शैली फली-फूली, उसे ‘पश्चिम भारतीय चित्रकला’ के नाम से जाना जाता है। गुजरात इसका प्रमुख केंद्र था। इसके साथ-साथ राजस्थान का दक्षिणी भाग और मध्य भारत का पश्चिमी भाग भी इसमें सम्मिलित है। गुजरात में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण इस भू-भाग से अनेक व्यापारिक मार्ग जाते थे। परिणामस्वरूप यहाँ अनेक संपन्न व्यापारी व स्थानीय सामंत प्रमुख हुए, जो आर्थिक संपन्नता के कारण, कला के भी सशक्त संरक्षक बने। मुख्य रूप से जैन समुदाय के व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को संरक्षित किया। जैन विषयों और पांडुलिपियों पर आधारित पश्चिम भारतीय शैली का यह भाग जैन चित्रकला के नाम से जाना जाता है।
शास्त्र दान की परंपरा के कारण जैन शैली के विकास को और प्रोत्साहन मिला। जैन समुदाय में, सचित्र पांडुलिपि को मठ के पुस्तकालय, जिसे भंडार कहा जाता था, में दान करना एक परोपकार, सदाचार व धार्मिक कृत्य माना जाता था।

महावीर का जन्म, कल्पसूत्र, पन्द्रहवीं शताब्दी, जैन भंडार, राजस्थान
कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकत्रिय चित्र ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के चौबीस तीर्थकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो कलाकारों को उनके जीवन चरित्र को चित्रित करने के लिए विषय प्रदान करता है। उनके जीवन की पाँच प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है, — गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश और महानिर्वाण—तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित अन्य घटनाओं के अधिकतम भाग कल्पसूत्र में शामिल हैं।
महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं को स्वप्न में देखा। ये 14 वस्तुएँ थीं- हाथी, बेल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चन्द्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राजाध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत और गुरु होगा।
त्रिशला के 14 स्वप्न, कल्पसूत्र, पश्चिमी भारत

लोकप्रिय चित्रित ग्रंथों में कालकाचार्यकथा और संग्राहिणी सूत्र उल्लेखनीय हैं। कालकाचार्यकथा में आचार्य कालका की कहानी का वर्णन है, जो एक दुष्ट राजा से अपनी अपहृत बहन (एक जैन तपस्विनी) को बचाने पर आधारित है। यह विभिन्न रोमांचकारी घटनाक्रम और कालका की रोमांचपूर्ण यात्रा को प्रस्तुत करता है, जैसे- वह अपनी लापता बहन का पता लगाने के लिए भूमि का परिमार्जन कर रहे हैं, अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन, अन्य राजाओं के साथ संबंध स्थापित करते हुए और अंत में, दुष्ट राजा से युद्ध कर रहे हैं।
उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। वहीं संग्राहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है, जिसकी रचना बारहवीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएँ शामिल हैं।
जैनियों ने इन ग्रंथों की कई प्रतियाँ लिखवाईं। इन ग्रंथों में या तो बहुत कम अथवा अत्यधिक चित्र मिलते हैं। इस प्रकार, एक विशिष्ट पृष्ठ पोथी या चित्र को लेखन और चित्रण के लिए वर्गों में विभाजित किया जाता था। पांडुलिपि या पोथी चित्र के पृष्ठों को एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर और नीचे पटलिस नामक लकड़ी के आवरण का उपयोग किया जाता था और जोड़ने के लिए एक छोटा-सा छेद बनाया जाता था जिससे उसे एक डोर के द्वारा बाँध दिया जाता था ताकि वे संरक्षित रहें।
कालकाचार्यकथा, 1497, एन. सी. मेहता संय्रह, अहमदाबाद, गुजरात

इस चित्र में कालका को दाहिनी ओर नीचे और उनकी बंदी बनाई गई बहन को बायों ओर ऊपर दिखाया गया है। जादुई शक्ति वाले गधे को कालका की सेना पर मुँह से बाणों की वर्षा करते हुए दिखाया गया है। दुष्ट राजा को वृत्त के अंदर से नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है।
चौदहवीं शताब्दी में कागज़ के आने से पहले, प्रांरिभिक जैन चित्रकला, परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनायी जाती थी। भारत के पश्चिमी भाग से प्राप्त ताड़ के पत्ते की सर्वप्रथम पांडुलिपि, ग्यारहवीं शताब्दी की है। ताड़ के पत्तों को चित्रण से पहले तैयार किया जाता था और तेज नुकीले सुलेख उपकरण के उपयोग से पत्तियों पर लेखन का कार्य कुशलता से किया जाता था।

ग्रह और उनके बीच की दूरी संय्रहिणी सूत्र, सखहवीं शताब्दी, एन.सी. मेहता, अहमदाबाद, गुजरात
ताड़ के पत्तों पर संकीर्ण और छोटे स्थान के कारण, आरंभ में चित्रण मात्र पटलिस तक ही सीमित था, जहाँ देवी-देवताओं की आकृतियों और जैन आचार्यों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का चित्रण चमकदार रंगों से किया जाता था।
जैन चित्रकला में विशेष प्रकार के संयोजन (योजनाबद्ध) और सरलीकृत भाषा का विकास हुआ, अधिकांश चित्रों में विभिन्न घटनाओं को समायोजित करने के लिए चित्र पटल को वर्गों में विभाजित किया गया। चित्रों में चमकीले रंग और कपड़े के अलंकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संयोजन में पतली, लहरदार रेखाओं का प्रबल प्रभाव है और चेहरे को तीन-आयामों में दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त आँख का उपयोग देखने को मिलता है। चित्रों में वास्तुशिल्प में सल्तनत कालीन गुंबद और नुकीले मेहराब का चित्रण, गुजरात, मांडू, जौनपुर और पाटन के क्षेत्रों में सुल्तानों की राजनीतिक उपस्थिति को दर्शाते हैं, जहाँ ये चित्र बने। कपड़े के चंदवा या शामियानों और पर्दों, मेज़, कुर्सी आदि वेशभूषा, उपयोगी वस्तुओं इत्यादि पर स्वदेशी और स्थानीय जीवन शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। भू-दृश्य या प्रकृति-दृश्य के स्वरूपों का चित्रण विस्तृत रूप में न होकर मात्र सांकेतिक या साधारणत: किया गया है। लगभग
इंर्र द्वारा देवसानो पाड़ो की स्तुति कल्पसूत्र, गुजरात, लगभग 1475 , संग्रह, बोस्टन

इन चित्रों को स्वर्ण और लाजवर्त के प्रचुर उपयोग से चित्रित किया गया है, जो इन चित्रों के निर्माणकर्ता या संरक्षकों की संपन्नता और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है।
इन धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त, तीर्थपट, मंडल, और गैर-धार्मिक कहानियों को भी जैन समुदाय के लिए चित्रित किया जाता था।
जैन चित्रों के अतिरिक्त, इनका निर्माण या संरक्षण धनी व्यापारियों और समर्पित भक्तों द्वारा करवाया जाता था। पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामंतों, ज़मींदारों, धनी नागरिकों और ऐसे अन्य लोगों के बीच चित्रकला की एक समानांतर परंपरा मौजूद थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और साहित्यिक विषयों के चित्रण शामिल थे। यह चित्रकला स्वदेशी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका निर्माण राजस्थान के राजदरबार की शैलियों और मुगलों के प्रभाव के आने से पहले हुआ था।
इसी समय में, हिंदू और जैन विषयों के अनेक चित्रों को चित्रित किया गया जैसे- महापुराण, चौरपंचाशिका, महाभारत का अरण्यक पर्व, भागवत पुराण, गीत गोविंद और अन्य कुछ चित्रांकन, जो इस स्वदेशी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस काल और शैली को साधारण रूप से पूर्व-मुगल या पूर्व-राजस्थानी शैली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे स्वदेशी शैली भी कहा जा सकता है।

चौरपंचाशिका, गुजरात, पन्द्रहवीं शताब्दी, एन. सी. मेहता संग्रह, अहमदाबाद, गुजरात
इसी काल के दौरान इन चित्रों के समूह में एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। इनमें मानव संरचना की एक विशेष शैली का विकास देखने को मिलता है, साथ ही साथ पारदर्शी वस्त्रों के चित्रण में विशिष्ट रुचि दृष्ट्रिंचर होती है। नायिका के सिर पर गुब्बारे की तरह से ओढ़नी का चित्रण है, जिसे कड़े और नुकीले किनारों की तरह ढाँका गया है। वास्तुकला का चित्रण प्रासंगिक परंतु सांकेतिक है। विभिन्न प्रकार की रेखाओं से जल निकायों और विशेष रूप से क्षितिज, वनस्पतियों, जीवों आदि का चित्रण किया गया है। ये सभी औपचारिक तत्व, सत्रहवीं शताब्दी की आरंभिक राजस्थानी चित्रकला को प्रभावित करते हैं।
उत्तर, पूर्व और पश्चिम के कई क्षेत्रों पर बारहवीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया के सल्तनत राजवंशों के शासन में आने के बाद, स्पष्टत:

मीठाराम, भागवत पुराण, 1550

निमतनामा, मांडू, 1550 , ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन
फ़ारसी, तुर्क और अफ़गान के प्रभाव को चित्रों में देखा जा सकता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहाँ सुल्तानों द्वारा चित्रों का निर्माण करवाया गया, जैसे कि मालवा, गुजरात, जौनपुर और अन्य सल्तनत शासित क्षेत्र। इन राजदरबारों में कुछ मध्य एशियाई कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों द्वारा चित्रों के निर्माण से, स्वदेशी शैलियों और फ़ारसी शैलियों के परस्पर मिश्रण से एक नई शैली का उदय हुआ, जिसे सल्तनत चित्रकला के रूप में जाना जाता है।
यह एक शैली की तुलना में पद्धति का अधिक प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर फ़ारसी मिश्रण का प्रभाव है- स्वदेशी चित्रण पद्धति, चित्तरंजक रूप से स्वदेशी तत्वों के साथ, फ़ारसी तत्वों, जैसे कि रंग, शरीर-रचना, अलंकरण सूक्ष्मता के साथ सरल प्राकृतिक दृश्य या भू-दृश्य इत्यादि एक साथ दिखाई दे रहे हैं।
नासिर शाह खिलजी (1500-10 ई.) के शासन काल के दौरान मांडू में चित्रित, निमतनामा (पकवानों की किताब) इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह व्यंजनों की पुस्तक है, जिसके एक खंड में शिकार का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही साथ दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र के निर्माण और उनके उपयोग के दिशानिर्देश भी दिए गए हैं।
सूफी विचारों पर आधारित कहानियाँ और लौराचंदा चित्रकला इस पद्धति के उदाहरण हैं।
पाल चित्रकला शैली
जैन साहित्य एवं चित्रकला की भाँति पूर्वी भारत के पाल शासकों के समय में लिखित सचित्र पांडुलिपियाँ, ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी की आंरभिक चित्रकला के उदाहरण हैं। पाल काल ( 750 से बारहवीं शताब्दी के मध्य) बौद्ध कला का अंतिम प्रमुख काल था। नालन्दा एवं विक्रमशिला जैसे महाविहार (विश्वविद्यालय) बौद्ध ज्ञान एवं कला के महान केंद्र थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित असंख्यक पांडुलिपियाँ एवं वज्रयान बौद्ध देवी-देवताओं के चित्र ताड़पत्र पर चित्रित किए गए।
इन केंद्रों में कांस्य मूर्तियों की ढलाई के लिए भी कार्यशालाएँ थीं। दक्षिण-पूर्व एशिया के छात्र और तीर्थ यात्री शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के लिए इन केंद्रों या
महाविहार (विश्वविद्यालयों) में आए और पालकालीन बौद्ध कला के कांस्य और सचित्र पांडुलिपियों के नमूने अपने साथ वापस ले गए। इस प्रथा ने पाल कला का विभिन्न स्थानों उदाहरणस्वरूप नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा देशों में सुगमता से प्रसार किया।

लोकेश्वर, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारामिता, पाल, 1050, राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्ली
जैन चित्रकला की कोणीय रेखाओं के विपरीत लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएँ तथा हलकी रंग योजना पाल शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएँ हैं। अजन्ता की तरह, पाल शैली में मठों में मूर्तिकला पद्धति और चित्रों में समांतर कला शैली का अनुभव होता है। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारामिता’ (बौदलेन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड) या आठ हज़ार पंक्तियों में लिखी गई बुद्धिमत्ता की पूर्णाता ताड़पत्र पर निर्मित पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण है।
इस पोथी का चित्रण नालन्दा विश्वविद्यालय में, पाल शासक रामपाल के पंद्रहवें राजवर्ष अर्थात् ग्यारहवीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में हुआ। इसमें छह पृष्ठ चित्रित हैं एवं दोनों ओर चित्रित लकड़ी के आवरण हैं। ये आवरण पांडुलिपि के पृष्ठों के ऊपर-नीचे लगाकर फीते से बाँधे जाते थे ताकि पांडुलिपि सुरक्षित रहे।
मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के पश्चात् पाल राजवंश कमजोर होता गया। अंततोगत्वा तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पाल कला का अंत हो गया, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया।
अभ्यास
- पांडुलिपि चित्रकला क्या है? दो स्थानों का नाम बताएँ जहाँ पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा प्रचलित थी?
- हमारी भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों में से किसी एक से एक अध्याय लें तथा चयनित पाठ का सचित्र लेखन करें (न्यूनतम पाँच पृष्ठ)।