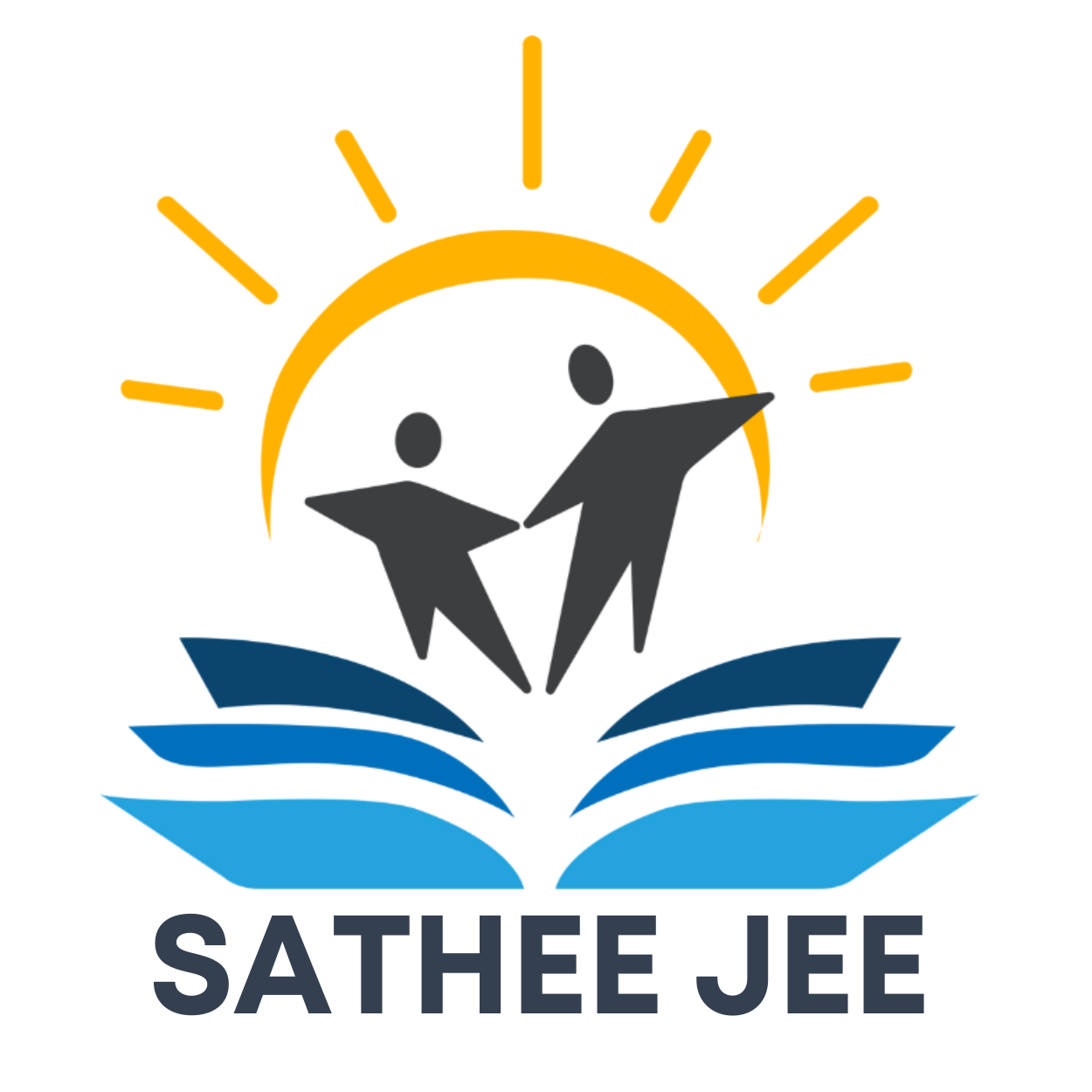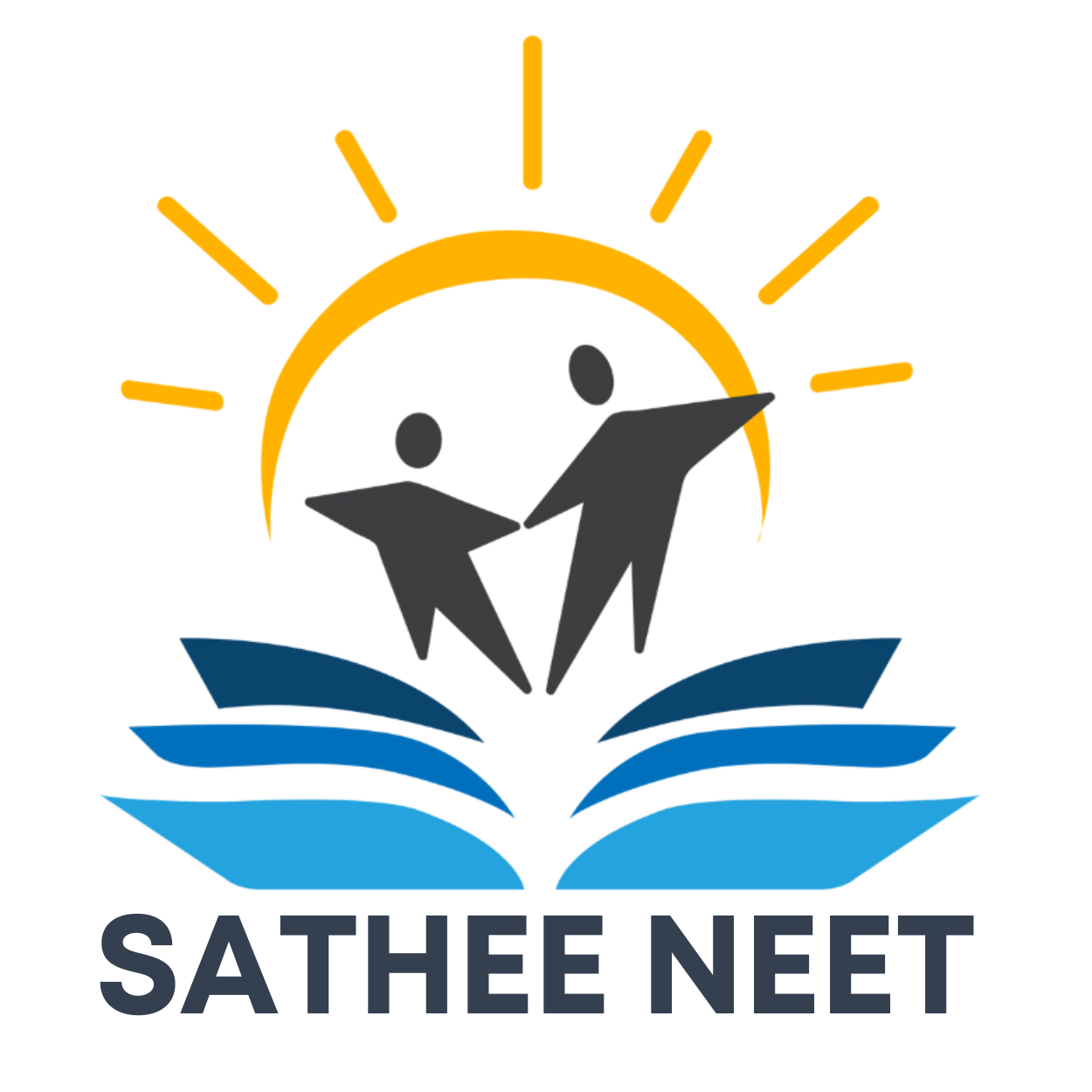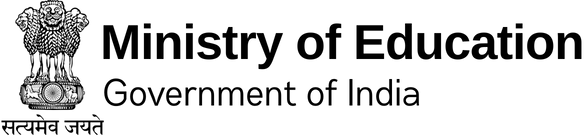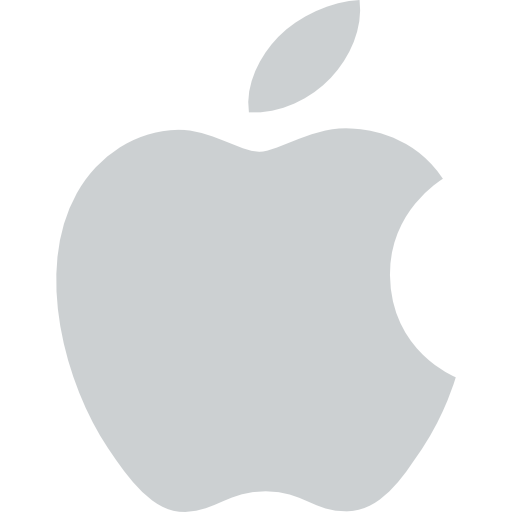अध्याय 04 तीन वर्ग
इस अध्याय में, हम नौवों और सोलहवीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था।
किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्रायः युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था। इस प्रकार से सामाजिक ढाँचे का केंद्र-बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। इसकी विशेषताएँ जर्मन रीति-रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थीं। ईसाई धर्म, जो चौथी सदी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे-धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था।
तीन वर्ग - जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु हैं, से हमारा अभिप्राय तीन सामाजिक श्रेणियों से है: ईसाई पादरी, भूमिधारक अभिजात वर्ग और कृषक। इन तीन वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्त्वपूर्ण कारक थे।
पिछले सौ वर्षों में, यूरोपीय इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों के इतिहासों, यहाँ तक कि प्रत्येक गाँव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भू-स्वामित्व के विवरणों, मूल्यों, और कानूनी मुकद्दमों जैसी बहुत सारी सामग्री दस्तावेज़ों के रूप में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए, चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवारों और जनसंख्या की संरंना को समझा जा सका। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी और गीत व कहानियों द्वारा हमें त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ।
इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, दीर्घकालीन (जैसे जनसंख्या में वृद्धि) अथवा अल्पकालीन (जैसे कृषक विद्रोहों) परिवर्तनों को समझने में किया जा सकता है।
सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक (Marc Bloch) थे। मार्क ब्लॉक (1886-1944) फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषयवस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्त्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर ज़ोर दिया जिससे कि लोगों के समूहों का व्यवहार और रुख समझा जा सके।
ब्लॉक का सामंती समाज यूरोपियों, विशेषकर 900 से 1300 के मध्य, फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों और श्रेणियों, भूमि प्रबंधन और उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देता है।
द्वितीय विश्वयुद्ध में नाज़ियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध व अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लग गया।
सामंतवाद का परिचय
इतिहासकारों द्वारा ‘सामंतवाद’ (fuedalism) शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधि क, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। यह जर्मन शब्द
‘मध्यकालीन युग’ शब्द पाँचवीं और पन्द्रहवीं सदी के मध्य के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है।

मानचित्र 1: पश्चिमी यूरोप।
‘फ़्यूड’ से बना है जिसका अर्थ ‘एक भूमि का टुकड़ा है’ और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ।
आर्थिक संदर्भ में, सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत (Lord) और कृषकों (peasents) के संबंधों पर आधारित है। कृषक, अपने खेतों के साथ-साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम-सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। इसके साथ-साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया।
यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शॉर्लमेन (Charlemagne, 742-814) के काल में पाई गईं, तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में ग्यारहवीं सदी के उत्तरार्ध में हुई।
फ्रांस और इंग्लैंड
गॉल (Gaul), जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, में दो विस्तृत तट-रेखाएँ, पर्वत-श्रेणियाँ, लंबी नदियाँ, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे।
*कुंस्तुनतुनिया में रहने वाले पूर्वी चर्च के प्रधान के भी बाइज़ेंटियम के सम्राट के साथ समान संबंध थे।
जर्मनी की एक जनजाति, फ्रैंक (Franks) ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। छठी सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिश अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे जो पोप द्वारा राजा शॉर्लमेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मज़बूत हो गए।*
एक संकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड-स्काटलैंड द्वीपों को ग्यारहवों सदी में फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी (Normandy) के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था।
| 481 |
| 486 |
| 496 |
| 714 |
| 751 |
| 768 |
| 808 |
| 840 |
तीन वर्ग
फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर तीन वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा “यहाँ वर्ग क्रम में, कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं।” इस तरह समाज मुख्य रूप से तीन वर्ग पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से बना था।
बारहवीं सदी में, बिंगेन के आबेस हिल्डेगार्ड (Hildegard) ने लिखा : कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा? इसलिए मनुष्यों में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है जिससे वे एक दूसरे को तबाह न करें… ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है चाहे स्वर्ग पर अथवा पृथ्वा पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है परंतु उनमें कोई समानता नहीं है।
‘ऑबे’ शब्द सीरिया के अबा से लिया गया है जिसका अर्थ पिता है। ऐबी, एबट या एबेस से संचालित था।
दूसरा वर्ग-अभिजात वर्ग
पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था। परंतु वास्तव में, सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। यह वैसलेज (Vassalage) नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ।
फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे ‘वैसलेज’ कहते थे और यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक थे, में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भू-स्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे जबकि कृषक भू-स्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी (Seigneur-शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का Senior) मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे- सेन्योर/लॉर्ड (लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला जिसका अर्थ था रोटी देने वाला) दास (Vassal) की रक्षा करता था और बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति-रिवाजों और शपथों का विनिमय शामिल था जो कि चर्च में बाईबल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास (vassal) को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी (staff) या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था।
अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी। उनका अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे (जो सामंती सेना, feudal levies, कहलाती थी)। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे।
वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे जिसमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत व चरागाह और उनके असामी-कृषकों (Tenant-peasant) के घर और खेत होते थे। उनका घर ‘मेनर’ कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करता पड़ता था।

फ्रांसीसी अभिजात शिकार पर जाते हुए, पंद्रहवों सदी को पेंटेंग।
मेनर की जागीर
लॉर्ड का अपना मेनर-भवन होता था। वह गाँवों पर नियंत्रण रखता था - कुछ लॉर्ड, अनेक गाँवों के मालिक थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी अनाज खेतों में उगाये जाते थे, लोहार और बढ़ई लॉर्ड के औज़ारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें वस्त्र कातती एवं बुनती थीं और बच्चे लॉर्ड की मदिरा सम्पीडक में कार्य करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्यभूमि और वन होते थे जहाँ लॉर्ड शिकार करते थे। उनके यहाँ चरागाह होते थे जहाँ उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहाँ पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था।

तेरहवों सदी के इंग्लैंड के मेनर की एक जागीर।
तेरहवीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा जिससे वे नाइट (knight) के परिवार का निवास स्थान बन सकें। वास्तव में, इंग्लैंड में नॉरमन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहों थी और इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था।
मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और मँहगे साजो-सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीज़ों को इन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था।
क्रियाकलाप 1
विभिन्न मानकों;जैसे - व्यवसाय,भाषा, धन और शिक्षा पर आधारित श्रेणीबद्ध सामाजिक ढाँचे की चर्चा कीजिए। मध्यकालीन फ्रांस की तुलना मेसोपोटामिया और रोमन साम्राज्य से करें।
नाइट
नौवीं सदी से, यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। शौकिया कृषक-सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स (Knights) कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार सम्बद्ध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से सम्बद्ध था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग (जिसे फ़ीफ़ कहा गया) दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फ़ीफ़ (fief) को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। यह 1000-2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पनचक्की और मदिरा संपीडक के अतिरिक्त, उसके व उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। सामंती मेनर (feudal manor) की तरह, फ़ीफ़ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में, नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए, नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने/घेराबंदी करने और पुतलों से रणकौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएँ अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी।
बारहवीं सदी से गायक फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियाँ, गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थीं। उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े-लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियाँ भी अधिक नहीं थीं, ये घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक मेनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था जहाँ मेनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी जो कि संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी।
“अगर मेरे प्पारे लॉर्ड को काट दिया जाता है उसकी तकदीर का मैं भागीदार बनूंगा, अगर वह लटका दिया जाता है तब मुझे भी उसके साथ लटका दें, अगर उसे अग्न दंड दिया जाता है तो मैं भी उसके साथ जल जाऊँगा; और अगर उसे डुबा दिया जाता है तो मुझे भी उसके साथ डुबा दिया जाए।"
तेरहवीं सदी में गाई जाने वाली फ्रांसीसी कविता ‘डून दे मयान्स’ जो नाइटों के साहस की याद दिलाती है।
प्रथम वर्ग-पादरी वर्ग
कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थीं जिनसे वे कर उगाह सकते थे। इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, जो रोम में रहते थे। यूरोप में इसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गाँवों में अपने चर्च हुआ करते थे जहाँ पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे।
प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था जैसे कृषि-दास पर, प्रतिबंध था शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थीं और वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का दसवाँ भाग लेने का अधिकार था जिसे ‘टीथ’ (Tithe) कहते थे। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत था।
चर्च के औपचारिक रीति-रिवाज की कुछ महत्त्वपूर्ण रस्में, सामंती कुलीनों की नकल थीं। प्रार्थना करते वक्त, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफ़ादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल था। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति-रिवाजों और तौर-तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था।
भिक्षु
चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति, पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गाँवों में रहते थे, एकांत ज़िदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें ऐबी (Abbeys) या मोनैस्ट्री* (monastery) मठ कहते थे और जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट (St. Benedict) था और दूसरा 910 में बरगंडी (Burgundy) में स्थापित क्लूनी (Cluny) था।
क्रियाकलाप 2
मध्यकालीन मेनर, महल और पूजा के स्थान पर विभिन्न सामाजिक-स्तर के व्यक्तियों से अपेक्षित व्यवहार के तरीकों की उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए।
भिक्षु अपना सारा जीवन ऑबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी-कार्य के विपरीत भिक्षु की ज़िदगी पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही अपना सकते थे - ऐसे पुरुषों को मोंक (Monk) तथा स्त्रियाँ नन (Nun) कहलाती थीं। कुछ ऑबों को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग ऑबे थे। पादरियों की तरह, भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकती थे।
*मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ‘मोनोस’ से बना है जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो।
दस या बीस पुरुष/ स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए जिसमें बड़ी इमारतें और भू-जागीरों के साथ-साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल समबद्ध थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। आबेस हिल्डेगार्ड (देखिए पृष्ठ 135) एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। तेरहवों सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें फ़्रायर (friars) कहते थे उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे।

इंग्लैंड के फार्नबरो में सेंट माईकेल को बेनेडिक्टीन ऑवे।
बेनेडिक्टीन (Benedictine) मठों में, भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे। इसका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा। इस पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार हैं:
अध्याय 6 : भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी-कभी ही दी जानी चाहिए।
अध्याय 7 : विनम्रता का अर्थ है आज्ञा पालन।
अध्याय 33 : किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए।
अध्याय 47 : आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए।

पांडुलिपि पर कार्य करते हुये एक बेनेडिक्टीन भिक्षु का काष्ठचित्र
अध्याय 48 : मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएँ -जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हों।
चौदहवीं सदी तक आते-आते, मठवाद के महत्त्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएँ व्याप्त होने लगीं। इंग्लैंड में, लैंग्लैंड (Langland) की कविता पियर्स प्लाउमैन (1360-70 ई.) में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गड़रियों और गरीब मजदूरों के ‘विशुद्ध विश्वास’ से तुलना की गई है। इंग्लैंड में भी चॉसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी (नीचे बॉक्स में उद्धरण देखिए) जिसमें भिक्षुणी (nun), भिक्षु (monk) और फ़्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया है।
चर्च और समाज
यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति-रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ बन गए थे। 25 दिसम्बर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व-रोमन त्योहार का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर-पंचांग (solar calendar) के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसने चन्द्र-पंचांग (lunar calendar) पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था जो लंबी सर्दी के पश्चात् बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप में, उस दिन प्रत्येक गाँव के व्यक्ति अपने गाँव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा पर अब वे उसे ग्राम के स्थान पर ‘पैरिश’ (Parish - एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र) कहने लगे। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों/छुट्टियों (Holy days/Holidays) का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था परन्तु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज-मस्ती करने और दावतों में बिताते थे।
तीर्थयात्रा, ईसाइयों के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा थी, और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे।
*दूर-दूर तक विभिन्न तीर्थस्थलों का भ्रमण करने वाला भिक्षु।
“अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेद जाती है और जब नन्हीं चिड़ियाँ संगीत सुनाती हैं
जो कि उन्निद्र चक्षु में रात बिता देती हैं….
(इस तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है और उनके हृदय को आकर्षित करती है);
तब लोग तीर्थयात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं,
और घुमक्कड़ भिक्षु
दूरस्थ उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं।
और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से
कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं।”
- जेफ़्री चॉसर (1340-1400 ई.), द कैंटरबरी टेल्स। इस काव्य-कृति की रचना मूल रूप से मध्यकालीन अंग्रेज़ी में की गई थी। यहाँ उसका हिंदी रूपांतरण करने का प्रयास किया गया है।
तीसरा वर्ग-किसान, स्वतंत्र और बंधक
अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले दो वर्गों का भरण-पोषण करते थे। काश्तकार दो तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ़ जिन्हें हिंदी में कृषि-दास कहा जाता है। सर्फ़ अंग्रेज़ी की क्रिया टू सर्व (To serve) से बना है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था (वर्ष में कम से कम चालीस दिन)। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के तीन या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन जिसे ‘श्रम-अधिशेष’ (Labour rent) कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त, उनसे अन्य श्रम कार्य; जैसे- गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्टी करना, बाड़ बनाना और सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी और इनके लिए उन्हें कोई मज़दूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त, स्त्रियों व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत कातते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते और लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकाल कर मदिरा तैयार करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर ‘टैली’ (Taille) था जिसे राजा कृषकों पर कभी-कभी लगाते थे। (पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे)।
कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे। इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। इसके लिए उन्हें कोई मज़दूरी नहीं
मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे हालाँकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी। सर्फ़ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेंक सकते थे और उनकी मदिरा संपीडक में ही आसवन-मदिरा और बीयर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परन्तु इसके लिए वह शुल्क लेता था।

एक अंग्रेज़ कृषक सोलहवों सदी का रेखाचित्र।
इंग्लैंड
सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में ग्याहरवों सदी से हुआ।
छठी सदी में मध्य यूरोप से एंजिल (Angles) और सैक्सन (Saxons) इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम ‘एंजिल लैंड’ का रूपांतरण है। ग्याहरवीं सदी में नारमैंडी (Normandy) के ड्यूक, विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल (English
*इंग्लैंड की वर्तमान रानी विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी है।

तेरेहवीं सदी के इंग्लैंड का हेवर दुर्ग।
channel) को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय, फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्राय: युद्ध होते रहते थे।
विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉरमन अभिजातों में बाँट दिए। यही लॉर्ड, राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे जिनसे वह सैन्य-सहायता की उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भमि उपहार में देने लगे जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे जैसी वे राजा की करते थे। किंतु वे नाइटों का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो-सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भू-स्वामियों के काश्तकार बन गए।
सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक
यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहाँ अनेक प्रक्रियाएँ थीं जो व्यवस्था को बदल रही थीं। इनमें से कुछ, जैसे पर्यावरण में परिवर्तन, धीरे-धीरे और लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। हम इन प्रक्रियाओं की बारी-बारी से जाँच करेंगे।
पर्यावरण
पाँचवों से दसवीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था। अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसके साथ ही, अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहाँ से भाग कर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इससे सर्दियाँ प्रचंड और लंबी अवधि की हो गईं। फसलों का उपज काल छोटा हो गया और इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई।
ग्यारहवीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसत तापमान बढ़ गया जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ।
भूमि का उपयोग
प्रारंभ में, कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म थी। कृषक को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का हल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच ही सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्रायः चार वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था और उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी।
साथ ही फ़सल-चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को दो भागों में बाँट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूँ बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को परती या खाली रखा जाता था। अगले वर्ष परती भूमि पर राई बोई जाती थी जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण, मिट्टी की उर्वरता का धीरे-धीरे ह्रास होने लगा और प्रायः अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी-बारी से पड़ने लगे जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया।
इन कठिनाइयों के बावजूद, लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मेनरों की जागीर (Manorial estate) की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे। चूँकि वे खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे और उस मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे बेगार करने से बचने लगे। चरागाहों व वन-भूमि के कारण उनका उन लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझते थे जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपदा मानते थे।
नयी कृषि प्रौद्योगिकी
ग्याहरवीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं।
मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और साँचेदार पटरे (Mould boards) का उपयोग होने लगा। ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और साँचेदार पटरे सही ढंग से उपरि मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा।
पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार हुआ। गले (Neck harness) के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बाँधा जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक जलशक्ति और वायुशक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित हो रहे थे।
भूमि के उपयोग के तरीके में भी बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी था दो खेतों वाली व्यवस्था से तीन खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन। इस व्यवस्था में कृषक तीन वर्षों में से दो वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था बशर्ते वह एक फ़सल शरत् ऋतु में और उसके डेढ़ वर्ष पश्चात दूसरी बसंत में बोता। इसका अर्थ था कि कृषक अपनी जोतों को तीन खेतों में बाँट सकते थे। वे मानव उपभोग के लिए एक खेत में शरत ऋतु में गेहूँ या राई बो सकते थे। दूसरे में, बसंत ऋतु में मनुष्यों के उपभोग के लिए मटर, सेम और मसूर तथा घोड़ों के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे, तीसरा खेत परती यानि खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष वे तीनों खेतों का प्रयोग बदल-बदल कर करते थे।
इन सुधारों के कारण, भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। भोजन की उपलब्धता दुगुनी हो गई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय के आहार में अधिक प्रोटीन का तथा उनके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया। फलस्वरूप कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगा। वे अब कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। तेरहवों सदी तक एक कृषक के खेत का औसत आकार सौ एकड़ से घटकर बीस से तीस एकड़ तक रह गया। छोटी जोतों पर अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी और उसमें कम श्रम की आवश्यकता थी। इससे कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिला।
इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी बदलावों में अत्यधिक धन लगता था। कृषकों के पास पनचक्की और पवनचक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था इसलिए इस मामले में पहल लॉर्डों द्वारा की गई। परन्तु कृषक भी कई अन्य क्षेत्रों में पहल करने में सक्षम रहे, जैसे कि खेती योग्य भूमि का विस्तार करने में। उन्होंने फ़सलों की तीन-चक्रीय व्यवस्था को अपनाया और गाँवों में लोहार की दुकानें और भट्ठियाँ स्थापित कीं, जहाँ पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने और मरम्मत करने के काम को सस्ती दरों पर किया जाने लगा।
ग्यारहवीं सदी से, व्यक्तिगत संबंध, जो सामंतवाद का आधार थे कमज़ोर पड़ने लगे क्योंकि आर्थिक लेन-देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। लॉर्डों को लगान, उनकी सेवाओं के बजाए नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा और कृषकों ने अपनी फ़सल व्यापारियों को मुद्रा में (उन्हें वस्तुओं से बदलने के स्थान पर) बेचना शुरू कर दिया जो पुनः उन वस्तुओं को शहर में बेच देते थे। धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा जो खराब फ़सल के समय बहुत अधिक हो जाती थीं। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच कृषि मूल्य दुगुने हो गए थे।
चौथा वर्ग? नए नगर और नगरवासी
कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबद्ध तीन क्षेत्रों - जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख थी बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन-अवधि था। तेरहवीं सदी तक एक औसत यूरोपीय आठवों सदी की तुलना में दस वर्ष अधिक जी सकता था। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन-अवधि छोटी होती थी क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे।
रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे। परन्तु ग्यारहवों सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई तो नगर फिर से बढ़ने लगे। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहाँ वे अपना एक बिक्री केन्द्र स्थापित कर सकें और जहाँ से वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सकें। इस ज़रूरत ने मियादी हाट-मेलों को बढ़ावा दिया, और छोटे विपणन केन्द्रों का विकास किया जिनमें धीरे-धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे - एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहाँ पर व्यापारी, घर और दुकानों का निर्माण कर सकें और एक कार्यालय जहाँ से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सकें। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास, बड़े दुर्गों, बिशपों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा।
नगरों में लोग, सेवा के स्थान पर, उन लॉर्डों को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे, कर देने लगे। नगरों ने कृषक परिवारों के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएँ प्रदान कीं।
‘नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है’ एक प्रसिद्ध कहावत थी। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भाग कर नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नज़रों से एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषिदास थे जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों

रेम्स, फ्रांसीसी कथीड्रल नगर, सत्रहवीं सदी का नक्शा।
क्रियाकलाप 3
उपर्युक्त नक्शे और नगर के चित्र को ध्यान से देखिए। मध्यकालीन यूरोपीय नगरों के कौन से महत्त्वपूर्ण लक्षण आपको उनमें दिखाई पड़ते हैं। वे अन्य स्थानों व अन्य काल के नगरों से किस प्रकार भिन्न थे?
जैसे साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग तीस हज़ार होती थी। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था।
आर्धिक संस्था का आधार ‘श्रेणी’ (Guild) था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक ‘श्रेणी’ के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। ‘श्रेणी सभागार’ प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। यह आनुष्ठानिक समारोहों के लिए था जहाँ गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे, संगीतकारों को प्रीतिभोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था और सरायवाले यात्रियों की देखभाल करते थे।
ग्यारहवों सदी आते-आते, पश्चिम एशिया के साथ नवीन व्यापार-मार्ग विकसित हो रहे थे (विषय 5 देखिए )। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले में फ़र और शिकारी बाज़ लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्री यात्रा करते थे और अंग्रेज़ व्यापारी राँगा बेचने के लिए आते थे। बारहवों सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले, दस्तकारों को एक मेनर से दूसरे मेनर में जाना पड़ता था पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे-जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजात्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे।
कथीड्रल-नगर
चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। बारहवीं सदी से फ्रांस में कथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। कथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ-स्थल बन गए। इस प्रकार, उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए।

सॉल्सबरी कथीड्रल, इंग्लैंड।
“दावत के दिनों में हमारे द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली कमी, जगह की संकीर्णता, अत्यधिक यंत्रणा और शोर के कारण भाग कर स्त्रियों का पुरुषों के सिरों के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना - ये सब कुछ ऐसे कारण थे कि हमने पवित्र चर्च को विस्तृत एवं व्यापक बनाने का निर्णय लिया…
विभिन्न क्षेत्रों से आए अनेक विशेषजों के अति कुशल हाथों से तरह-तरह की शानदार नयी खिड़कियों की पुताई कराई, क्योंकि ये खिड़कियाँ अपने अद्भुत निष्पादन और बहुत मँहगे रंजित व सफ़ायर काँच के कारण बहुत मूल्यवान थीं इसलिए उनकी रक्षा के लिए हमने एक सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार की नियुक्ति की, वे अपनी तनख्वाह वेदिका से सिक्कों के रूप में और आटा अपने भाईबंधुओं के सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे; वे उन कला वस्तुओं की देखरेख के कर्तव्यों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते थे।”
— एबट सुगेर (Abbot Suger) (1081-1151) ने पैरिस के निकट सेंट डेनिस में स्थित ऑवे के बारे में लिखा। 
अभिरोंजित काँच की खिड़की, कारटेस कथीड्रल, फ्रांस, पंद्रहवीं सदी।
चौदहवीं सदी का संकट
चौदहवों सदी की शुरुआत तक, यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा तीन कारकों की वजह से हुआ।
इसके साथ-साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चाँदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु-मुद्रा में भारी कमी आई जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चाँदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा।
इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। बारहवीं व तेरहवीं सदी में जैसे-जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ-साथ चूहे आए - जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण (Black death) लाए। पश्चिमी यूरोप, जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग-थलग रहा था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20 % भाग इसमें काल-कवलित हो गया जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहाँ की जनसंख्या का 40 % तक थी।
“कितने बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने कुटुंबियों के साथ नाश्ता कर उसी रात्रि को दूसरी दुनिया में अपने पूर्वजों के साथ रात्रि भोजन किया होगा। लोगों की हालत दयनीय थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। वे हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे, और बिना किसी मदद के मर जाते थे। अनेक खुली गालियों में मरते थे और बाकी अपने घरों में मरते थे इसका पता उनके सड़े शरीर की बदबू से चलता था। चूँकि पवित्र कब्रिस्तान इतनी अधिक संख्या में शरीरों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थे अतः उनको सैकड़ों की संख्या में बड़ी-बड़ी खंदकों में डाल दिया जाता था, जैसे कि पोत में सामान को भरा जाता है, और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती थी।”
- जिओवानी बोकाचियो (Giovanni Boccacio) (1313-75), इतालवी लेखक
व्यापार केन्द्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए। बंद समुदाय में, जैसे मठों और आभ्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था तो सबको इससे बीमार होने में देर नहीं लगती थी और लगभग प्रत्येक मामले में कोई भी नहों बचता था। प्लेग, शिशुओं, युवाओं और बुर्जुगों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएँ हुईई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई।
इस विनाशलीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मज़दूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई थी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि-उत्पादों के मूल्यों में कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मज़दूरों, विशेषकर कृषि मज़दूरों की भारी माँग के कारण मज़दूरी की दरों में 250 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों से दुगुने की माँग कर सकता था।
सामाजिक असंतोष
इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मज़दूरी की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था और उन्होंने पुरानी मज़दूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसका कृषकों विशेषकर पढ़े-लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स (Flanders) में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए।
यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया पर महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीकों से उन स्थानों पर हुए जहाँ पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावज़ूद कृषक विद्रोहों की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। धन अर्थव्यवस्था (money economy) काफी अधिक विकसित थी जिसे पलटा नहीं जा सकता था। इसलिए, यद्यपि लॉर्ड विद्रोहों का दमन करने में सफल रहे, परन्तु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि दासता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे।
| 1066 | नॉरमन लोगों की एंग्लो-सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय |
| 1100 | के पश्चात् फ्रांस में कथीड्रलों का निर्माण |
| 1315-17 | यूरोप में महान अकाल |
| 1347-50 | ब्यूबोनिक प्लेग (Black Death) |
| 1338-1461 | इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य “सौ-वर्षीय युद्ध” |
| 1381 | कृषकों के विद्रोह |
क्रियाकलाप 4
तिथियों के साथ दी गई घटनाओं और प्रक्रियाओं को पढ़िए और उनका विवरणात्मक लेखा-जोखा दीजिए।
राजनीतिक परिवर्तन
राजनीतिक हलकों में हुए विकास, सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ होते रहे। पंद्रहवीं और सोलहवों सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए नए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्त्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को ‘नए शासक’ (the new monarchs) कहने लगे। फ्रांस में लुई ग्यारहवें, आस्ट्रिया में मैक्समिलन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में ईसाबेला और फरडीनेंड, निरकुंश शासक थे जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नयी संभावनाओं की शुरुआत की। (देखिए विषय 8)
बारहवीं और तेरहवीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी (Vassalage) और सामंतशाही (lordship) वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी (देखिए विषय 5)। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े-टुकड़े हो गया।

इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम, पिकनिक मनाते हुए, सोलहवीं सदी के अंतिम दशकों में।
| नए शासक | |
|---|---|
| 1461-1559 | फ्रांस में नए शासक |
| 1474-1556 | स्पेन में नए शासक |
| 1485-1547 | इंग्लैंड में नए शासक |
करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएँ रख सके। इस तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार किया तथा राजसत्ता के प्रति होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को दबाया। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि केंद्रीयकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध नहीं किया। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुए जिनका 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में दमन कर दिया गया। फ्रांस में लुई XI (1461-83) को ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अवर कोटि के अभिजातों और अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्ती हड़पे जाने का विरोध किया। सोलहवीं सदी में फ्रांस में होने वाले ‘धर्म-युद्ध’ कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे।

नेमूर का दुर्ग, पंद्रहवरं सदी
अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए एक चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया। नई शासन-व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्दी ही अपने को राजभक्तों में बदल लिया। इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। वास्तव में, लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा में शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए। परन्तु नयी शासन व्यवस्था कई महत्त्वपूर्ण तरीकों में अलग थी। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहाँ राजभक्ति विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता-अनुयायी तंत्र का केंद्र-बिंदु था। सभी राजतंत्र, चाहे वे कितने भी कमज़ोर या शक्तिशाली हों, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे, जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया या प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए, धन ग़ैर-अभिजात वर्गों जैसे व्यापारियों और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गया। वे राजाओं को धन उधार देते थे जो इसका उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे। शासकों ने इस प्रकार राज्य-व्यवस्था में ग़ैर सामंती तत्त्वों के लिए स्थान बना दिया।
फ्रांस और इंग्लैंड का बाद का इतिहास इन शक्ति संरचचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बनना था। 1614 में बालक शासक लुई XIII के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे एस्ट्ट्ट जनरल कहते थे (जिसके तीन सदन थे, जो तीन वर्गों - पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग तथा अन्य का प्रतिनिधित्व करते थे), का एक अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात दो सदियों, 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया क्योंकि राजा तीन वर्गों के साथ अपनी शक्ति बाँटना नहीं चाहते थे।
इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉरमन विजय से भी पहले एंग्लो-सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे व हाउस ऑफ कामन्स, जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम (1629-40) ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए ग्यारह वर्षों तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। परन्तु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहों चल पाई और राजतंत्र की पुन: स्थापना हुई; परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी।
वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्र है। इसका कारण यह है कि सत्रहवों सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग-अलग दिशाएँ अपनाईं।
अभ्यास
संक्षेप में उत्तर दीजिए
1. फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के दो लक्षणों का वर्णन कीजिए।
2. जनसंख्या के स्तर में होने वाले लंबी-अवधि के परिवर्तनों ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया?
3. नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ?
4. मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था?
संक्षेप में निबंध लिखिए
5. मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए और इसका वर्णन कीजिए।
6. फ्रांस के सर्फ़ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए।