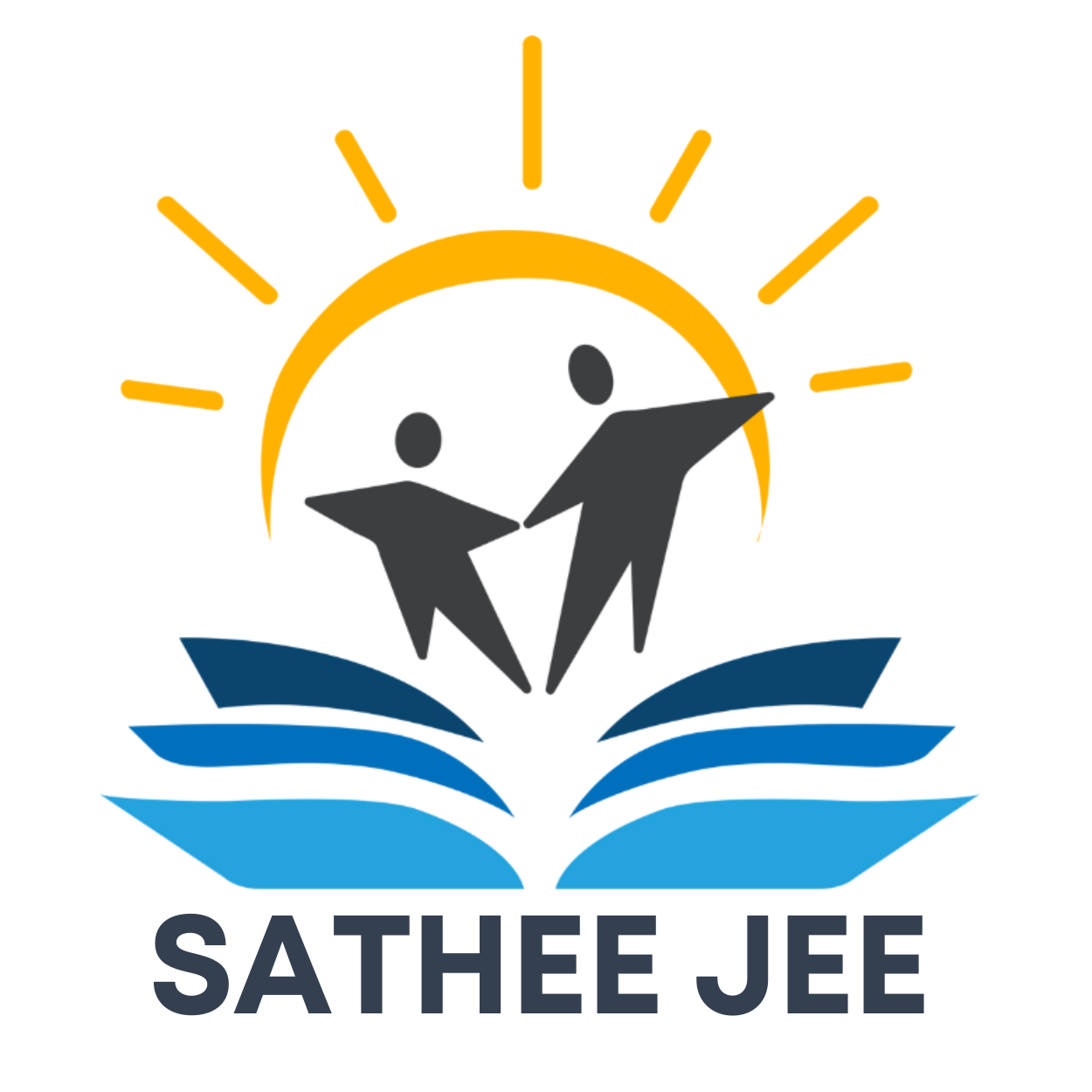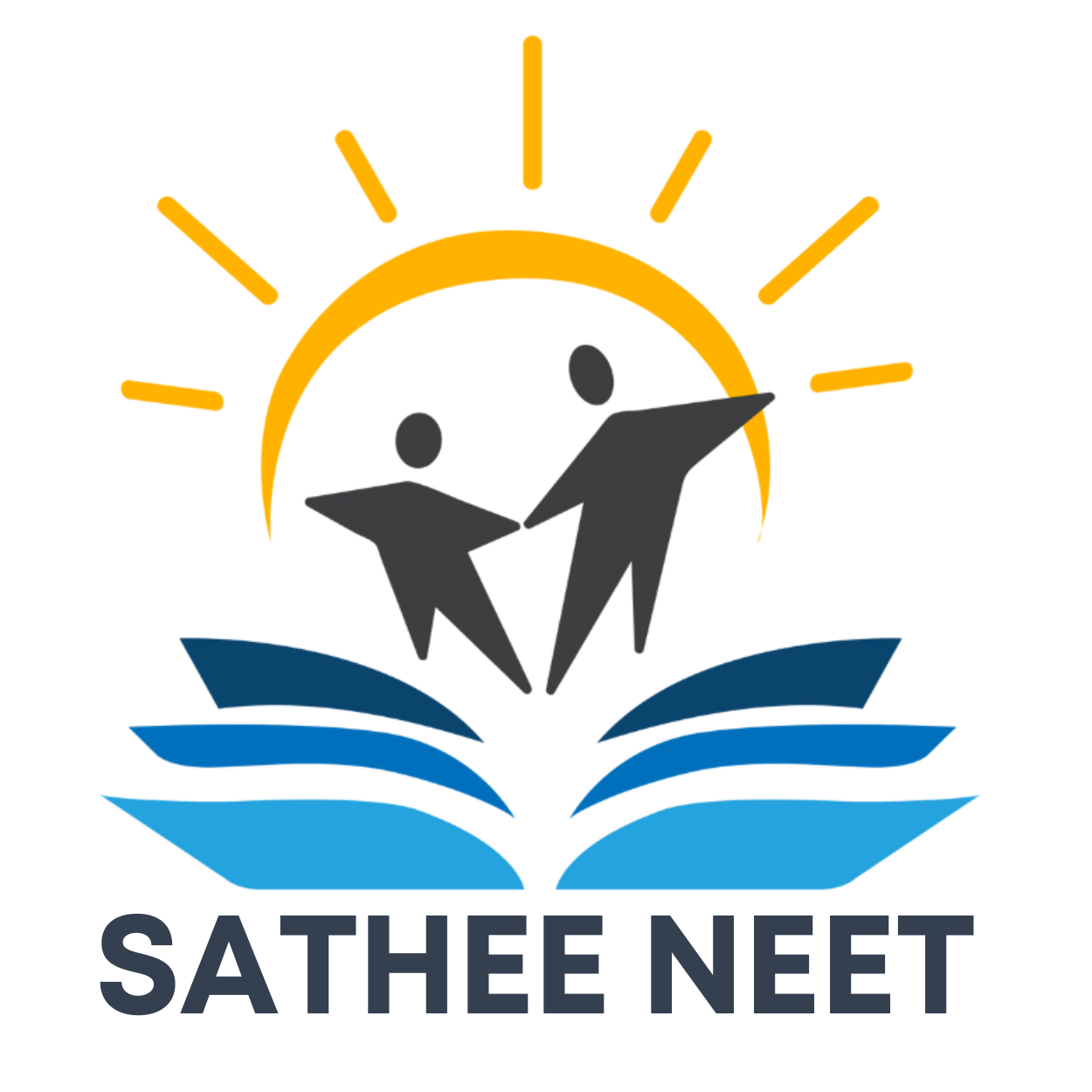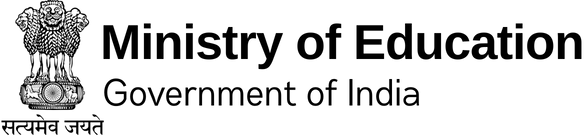अध्याय 05 भारतीय समाजशास्त्री
जैसा कि आपने प्रथम भाग की पाठ्यपुस्तक समाजशास्त्र परिचय के पहले अध्याय में देखा कि यूरोपियन संदर्भ में भी यह विषय काफी नया है जिसकी स्थापना लगभग सौ वर्षों पहले की गई। भारत में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच-विचार सौ वर्षों से भी कुछ पुराना है लेकिन विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 ई. में बंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। सन् 1920 में दो अन्य विश्वविद्यालयों-कलकत्ता तथा लखनऊ-ने भी समाजशास्त्र तथा मानवविज्ञान में शिक्षण तथा शोधकार्य प्रारंभ किया। आज प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक मानवविज्ञान अथवा मानवविज्ञान विभाग हैं और ज्यादातर इनमें से एक से अधिक का प्रतिनिधित्व होता है।
अन्य कई संस्थापित विषयों की तरह ही आजकल समाजशास्त्र को भी भारत में स्वीकारा जाता है लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने प्रारंभिक काल में यह बिलकुल स्पष्ट नहीं था कि भारतीय समाजशास्त्र का प्रारूप क्या तथा कैसा होगा और क्या वास्तव में भारत को समाजशास्त्र जैसे किसी विषय की आवश्यकता थी भी या नहीं? 20 वीं शताब्दी के पहले पच्चीस सालों में जिन लोगों ने इस विषय में रुचि दिखाई, उन्हें यह स्वयं तय करना था कि भारत में उसकी क्या भूमिका होगी। इस अध्याय में आपका परिचय भारत के कुछ प्रारंभिक संस्थापक समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा। इन विद्वानों ने इस विषय को आकार देने और इसको ऐतिहासिक तथा सामाजिक परित्रेक्ष्य के अनुकूल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भारतीय संदर्भ की विशिष्टता ने कई प्रश्न खड़े किए। सर्वप्रथम यदि पाश्चात्य समाजशास्त्र का उद्भव आधुनिकता को समझने के प्रयास के रूप में हुआ, तो भारत जैसे देश में इसकी क्या भूमिका होगी? भारत भी आधुनिकता द्वारा लाए गए परिवर्वनों को महसूस कर रहा था परंतु यहाँ एक महत्त्वपूर्ण अंतर था और वह था एक उपनिवेश के रूप में भारत। भारत में आधुनिकता का पहला अनुभव और औपनिवेशिक पराधीनता का अनुभव दोनों आपस में घुले-मिले थे। दूसरा, यदि मानवविज्ञान का उद्भव यूरोपियन समाज की ‘आदिम संस्कृतियों’ को जानने की उत्सुकता के संदर्भ में हुआ तो भारत में उसकी क्या भूमिका हो? भारत स्वयं एक प्राचीन एवं विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता था लेकिन इसमें ‘आदिम’ (या आदिवासी) समाज भी पाए जाते थे। अंत में भारत जैसे संपन्न, स्वतंत्र, नवराष्ट्र जो नियोजित विकास तथा प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है, वहाँ समाजशास्त्र की क्या महत्त्वपूर्ण भूमिका हो?
भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं ढूँढ़ने थे बल्कि उन्हें अपने लिए नए प्रश्नों को भी तलाशना था। भारतीय संदर्भ में यह सिर्फ़, ‘करने’ के अनुभव से ही संभव था-जिससे समाजशास्त्रीय प्रश्नों को एक आकार मिला; यह पूर्व निर्मित रूप में उपलब्ध नहीं थे जैसा कि देखा जा सकता है। भारतीय समाजशास्त्री तथा मानवविज्ञानी, अधिकतर अचानक ही बन गए। उदाहरण के तौर पर, भारत के बेहतरीन तथा सर्वप्रथम सामाजिक मानवविज्ञानी श्री एल.के. अनन्तकृष्ण अय्यर (1861-1937) ने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की; फिर स्कूली शिक्षक और उसके बाद कोचीन रजवाड़े के महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, जो आज केरल राज्य का एक भाग है। सन् 1902 में कोचीन के दीवान द्वारा इन्हें राज्य के नृजातीय सर्वेक्षण (एथनोग्रैफिक सर्वे) में मदद के लिए कहा गया। ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों तथा इलाकों में करवाना चाहती थी जो प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आते थे। अनन्तकृष्ण अय्यर ने इस कार्य को पूर्णरूपेण एक स्वयंसेवी के रूप में किया। महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में, एरनाकुलम स्थित महाराजा कॉलेज में पढ़ाते हुए, इसके लिए उन्होंने सप्ताहांतों में नृजातीय विभाग में अवैतनिक सुपरिंटेंडेंट के रूप में कार्य किया। उनके काम की अपने समय के ब्रिटिश मानवविज्ञानी तथा प्रशासकों ने काफ़ी प्रशंसा की तथा बाद में उन्हें इसी प्रकार के सर्वेक्षण में सहायता करने के लिए मैसूर रजवाड़े में आमंत्रित किया गया।
अनन्तकृष्ण अय्यर संभवतः पहले शिक्षित मानवविज्ञानी थे, जिन्हें एक विद्वान तथा शिक्षाविद् के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय रूप में ख्याति मिली। उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई, जहाँ उन्होंने भारत के सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानवविज्ञान विभाग की स्थापना करने में मदद की। सन् 1917-1932 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही रहे। हालाँकि, मानवविज्ञान में उनके पास कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, परंतु उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के नृजातीय विभाग का अध्यक्ष चुना गया। यूरोपियन विश्वविद्यालयों में अपने भाषणों तथा भ्रमण के दौरान जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्ट्रेट की मानद उपाधि दी गई। कोचीन रजवाडे़ की तरफ़ से उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया।
कानूनविद् शरत चंद्र रॉय (1871-1942) एक अन्य मानवविज्ञानी हैं जो भारत में इस वर्ग के अग्रणी थे तथा अकस्मात मानवविज्ञानी बने। कलकत्ता के रिपन कॉलेज से कानून की डिग्री लेने से पूर्व, रॉय ने अंग्रेज़ी विषय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी। कुछ दिनों कानून की प्रैक्टिस करने के बाद सन् 1898 में राँची जाकर ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेज़ी के शिक्षक के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने उनके भावी जीवन को बदल दिया, क्योंकि अगले 44 वर्षों तक वे राँची में रहे तथा छोटानागपुर प्रदेश (आज का झारखंड) में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति तथा समाज के विशेषज्ञ बने। रॉय की मानवविज्ञान में रुचि तब बढ़ी जब उन्होंने स्कूल का काम छोड़ दिया तथा राँची की अदालत में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। आगे चलकर उन्हें सरकारी दुभाषिए के रूप में अदालत में नियुक्त किया गया।
रॉय की रुचि जनजातीय समाज में बढ़ी जो वास्तव में उनकी नौकरी की आवश्यकताओं का प्रतिफल था क्योंकि अदालत में वे जनजातियों की परंपरा तथा कानूनों को दुभाषित करते थे। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया तथा उनके बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया। यह सभी कार्य शौकिया आधार पर किया गया परंतु उनकी मेहनत तथा बारीकियों को ध्यानपूर्वक देखने तथा समझने के कौशल ने शोधकार्य के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य तथा लेखन सामग्री तैयार की। अपने पूरे सेवाकाल में रॉय के सौ से अधिक लेख राष्ट्रीय तथा ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित हुए। इसके साथ ही इनके द्वारा ओराँव, मुंडा तथा खरिया जनजातियों पर किया गया सर्वप्रसिद्ध लेखन कार्य भी प्रकाशित हुआ। शीघ्र ही रॉय भारत तथा ब्रिटेन में जाने-माने मानवविज्ञानी के रूप में विख्यात हुए तथा ‘छोटा नागपुर’ के विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान बनी। 1922 में उन्होंने मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की, जो कि अपने समय तथा प्रकार का पहला जर्नल था तथा आज भी जिसका प्रकाशन भारत में होता है।
अनन्तकृष्ण अय्यर तथा शरतचंद्र रॉय-दोनों सही मायनों में इस क्षेत्र के अग्रणी विद्वान थे। 1900 के प्रारंभ में ही उन्होंने एक ऐसे विषय पर कार्य करना प्रारंभ किया जो भारत में न तो अभी तक विद्यमान था और न ही कोई ऐसी संस्था थी जो इसे किसी प्रकार का संरक्षण देती थी। दोनों-अय्यर तथा रॉय-का जन्म तथा मृत्यु अंग्रेज़ों द्वारा शासित भारत में हुई। इस अध्याय में आपका परिचय चार भारतीय समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा, जिन्होंने अय्यर तथा रॉय के एक पीढ़ी बाद जन्म लिया। ये सभी औपनिवेशिक भारत में जन्मे परंतु इनका कार्य स्वतंत्र भारत में चलता रहा तथा इन्होंने पहली औपचारिक संस्थाओं की रूपरेखा बनाई जिस पर आगे चल कर भारतीय समाजशास्त्र जैसी औपचारिक संस्थाओं को स्थापना की गई। जी.एस. घूर्य तथा डी.पी. मुकर्जी का जन्म 1890 के दशक में हुआ जबकि ए.आर. देसाई तथा एम.एस. श्रीनिवास का जन्म इनसे लगभग पंद्रह वर्ष बाद अर्थात बीसवीं सदी के दूसरे दशक में हुआ हालाँकि ये सब बहुत गहराई से समाजशास्त्र की पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित थे। ये उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम थे जोकि कुछ अग्रणी विद्वानों द्वारा पूछे जा सकते थे कि विशिष्ट भारतीय समाजशास्त्र किस प्रकार का आकार लेगा।
जी. एस. घूर्ये को भारत में समाजशास्त्र को एक संस्थागत रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने
गोविंद सदाशिव घूर्ये (1893-1983)
गोविंद सदाशिव घूर्ये का जन्म 12 दिसंबर 1893 को मालवान, पश्चिम भारत के कोंकण तटीय प्रदेश के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार एक संपन्न व्यापारी था, लेकिन बाद में उसका पतन हो गया।
1913 : एलफिंस्टन कॉलेज, मुंबई में प्रवेश। संस्कृत (ऑनर्स) में स्नातक। स्नातकोत्तर की उपाधि संस्कृत तथा अंग्रेज़ी में, इसी कॉलेज से 1918 में।
1919 : समाजशास्त्र में विदेश में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति के लिए चयनित। प्रारंभ में लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनामिक्स में एल.टी. हॉबहाऊस, अपने समय के प्रमुख समाजशास्त्री, के द्वारा पढ़ाए गए। बाद में केम्ब्रिज में डब्लू.एच.आर. रिवर्स द्वारा पढ़ाए गए और उनके प्रसारवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए।
1923 : 1922 में रिवर्स के अकस्मात निधन के पश्चात ए. सी. हैडन के निर्देशन में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। मई में मुंबई वापस आए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पीएच.डी. पर आधारित पांडुलिपि पर केम्ब्रिज में पुस्तकों की एक शृंखला प्रकाशित करने के लिए स्वीकृत हुई।
1924 : थोड़े समय तक कोलकाता में रहने के पश्चात, बंबई विश्वविद्यालय में रीडर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। जहाँ अगले 35 वर्ष तक रहे।
1936 : बंबई विश्वविद्यालय के विभाग में पीएच.डी. की उपाधि प्रारंभ की, भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्रथम पीएच.डी. उपाधि, घूर्ये के निर्देशन में जी.आर. प्रधान को प्रदान की गई। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को पुनरावृत्त किया और 1945 में पूर्णकालीन 8 -कोर्स में समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया।
1951 : घूर्ये द्वारा ‘इंडियन सोशयोलॉजिकल सोसायटी, की स्थापना की गई तथा वे इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। ‘द इंडियन सोशयोलॉजिकल सोसायटी’ ने 1952 में अपने जर्नल, सोशयोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन प्रारंभ किया।
1959 : 1959 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन शैक्षिक जीवन में क्रियाशील रहे, मुख्य रूप से प्रकाशन के क्षेत्र में- 30 में से 17 पुस्तकें उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद लिखीं।
मृत्यु : 1983 में 90 वर्ष की आयु में जी. एस. घूर्ये का निधन हो गया।
सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विभाग में शिक्षण कार्य की अध्यक्षता की तथा पैंतीस वर्षों तक इस विभाग में कार्य किया। उनके निर्देशन में बड़ी संख्या में काम करने वाले शोध विद्यार्थी आज भी इस विषय में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर कार्यरत हैं। इन्होंने ‘इंडियन सोशयोलॉजिकल सोसायटी’ की स्थापना की तथा सोशयोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल भी निकाला। उनके शैक्षणिक लेख न केवल बहुसर्जक होते थे बल्कि जिन विषयों पर उन्होंने लेखन किया वे काफ़ी विस्तृत होते थे। ऐसे समय में जबकि विश्वविद्यालय शोध के लिए दी जाने वाली वित्तीय तथा संस्थागत सहायता काफ़ी सीमित थी; घूर्य ने समाजशास्त्र का एक भारतीय विषय के रूप में पोषण किया। घूर्ये द्वारा स्थापित बंबई विश्वविद्यालय विभाग ऐसा पहला विभाग बना, जिसने सर्वप्रथम सफलतापूर्वक दो मुख्य कार्यक्रमों (विषयों) को लागू किया जिन्हें आगे चलकर उत्साहपूर्वक इनके उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। ये थे-सक्रिय रूप से शिक्षण तथा शोधकार्य का एक ही संस्था में किया जाना, तथा सामाजिक मानवविज्ञान और समाजशास्त्र को एक बृहत वर्ग के रूप में स्थापित करना।
घूर्ये की पहचान जाति और प्रजाति पर उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों से होती है लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने बृहत विषयों; जैसेजनजाति, नातेदारी, परिवार और विवाह; संस्कृति, सभ्यता और नगरों की ऐतिहासिक भूमिका; धर्म; तथा संघर्ष और एकीकरण का समाजशास्त्र। बौद्धिक तथा संदर्भगत सरोकारों जिन्होंने घूर्ये को प्रभावित किया; उनमें सबसे प्रमुख हैं-प्रसारवाद, हिंदू धर्म तथा सिद्धांत पर प्राच्य छात्रवृत्ति, राष्ट्रवाद तथा हिंदू अभिन्नता के सांस्कृतिक पक्ष।
एक प्रमुख विषय जिस पर घूर्ये ने कार्य किया वह था ‘जनजाति’ अथवा ‘आदिवासी’ संस्कृति। वास्तव में इस विषय पर इनका लेखन, और मुख्य रूप से वेरियर एलविन के साथ हुए वाद-विवाद ने इन्हें समाजशास्त्र तथा शिक्षा की दुनिया से बाहर एक पहचान दी। सन् 1930 और 1940 के दशकों में इस विषय पर काफ़ी वाद-विवाद हुआ कि भारत में जनजातीय समाज का क्या स्थान हो और राज्य उनसे किस प्रकार का व्यवहार करे। कई ब्रिटिश प्रशासकमानवविज्ञानी भारतीय जनजातियों में रुचि रखते थे और उनका मानना था कि ये आदिम लोग थे जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी जो हिंदू मुख्यधारा से काफ़ी अलग थी। उनका मानना था कि सीधे-सादे जनजातीय लोग हिंदू समाज तथा संस्कृति से न केवल शोषित होंगे बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उनका पतन होगा। इस कारण को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वे जनजातियों को संरक्षण दें ताकि वे अपनी जीवन-पद्धति तथा संस्कृति को बनाए रख सकें क्योंकि उन पर लगातार यह दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्यधारा में अपना समायोजन करें (अपने आपको मुख्यधारा में मिला लें)।
हालाँकि, राष्ट्रवादी भारतीय भी भारत की एकता तथा भारतीय समाज तथा संस्कृति को आधुनिक बनाने की आवश्यकता को लेकर उतने ही उत्तेजित थे। उनका यह मानना था कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे और आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य वास्तव में गुमराह करने की कोशिश थी। इसके परिणामस्वरूप जनजातियों के पिछड़ेपन को आदिम संस्कृति के ‘संग्रहालय’ के रूप में ही बनाए रखा गया था। हिंदुत्व की कई विशेषताओं को वे स्वयं पिछड़ा हुआ मानते थे और जिनमें सुधार की आवश्यकता थी; उन्हें लगा कि जनजातियों को भी विकास की आवश्यकता थी। घूर्ये राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनजातियों को ‘पिछड़े हिंदू समूह’ के रूप में पहचाना जाए न कि एक भिन्न सांस्कृतिक समूह के रूप में। इस कार्य के लिए उन्होंने विस्तार से जनजातीय संस्कृति के कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, यह प्रमाणित करने के लिए कि वे काफ़ी लंबे समय से हिंदुत्व से आपसी अंतःक्रिया द्वारा जुड़े रहे हैं। जिस समायोजन प्रक्रिया से सभी भारतीय जातियों को गुज़रना पड़ा, उसी प्रक्रिया में जनजातीय वर्ग साधारणतः अन्य भारतीय समुदाय से पीछे रह गए थे। एक मुख्य विवाद-कि भारतीय जनजाति एक ऐसी आदिम जाति थी जो शायद ही कभी अलग-थलग रही हो, जिसका वर्णन शास्त्रीय मानवविज्ञान की पुस्तकों में हुआ है-विवादास्पद नहीं रहा। इस तथ्य पर मतभेद था कि मुख्यधारा की संस्कृति का उस पर क्या प्रभाव पड़ा और इसकी जाँच की गई। ‘संरक्षणवादियों’ का यह विश्वास था कि समायोजन का परिणाम जनजातियों के शोषण तथा उनकी संस्कृति की विलुप्तता के रूप में सामने आएगा। दूसरी तरफ़ घूर्ये तथा राष्ट्रवादियों ने यह तर्क दिया कि ये दुष्परिणाम मात्र जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित न होकर भारतीय समाज के सभी पिछड़े तथा दलित वर्गों में समान रूप में देखे जा सकते हैं। विकास के मार्ग में आने वाली ये वे आवश्यक कठिनाइयाँ हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता।
क्रियाकलाप 1
आज भी हम उसी प्रकार के विवादों में पड़े हैं। किसी भी प्रश्न के विभिन्न पक्षों की उनके समकालीन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर समीक्षा कीजिए, उदाहरण के लिए, अधिकतर जनजातीय आंदोलन अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहचान पर बल देते हैं। वास्तव में झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण इसी प्रकार के आंदोलनों का फल है। विकास के नाम पर बड़े-बड़े बाँधों, खदानों तथा फैक्ट्रियों के निर्माण के कारण जनजातीय वर्गों पर एक असमान दबाव पड़ता है, जिस पर काफ़ी मतभेद है। ऐसे और कितने संघर्षों के बारे में आप जानते हैं? पता लगाइए कि इन संघर्षों के पीछे कौन से मुद्दे थे। आप और आपके सहपाठी इन समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं?
जाति तथा प्रजाति पर घूर्ये के विचार
घूर्ये की शैक्षिक साख उनके द्वारा केम्ब्रिज में किए गए डॉक्ट्रेट के शोध निबंध के आधार पर बनी जो आगे चल कर 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। घूर्ये के कार्य ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया क्योंकि इन्होंने समकालीन भारतीय मानवविज्ञान के मुद्दों को संबोधित किया था। इस पुस्तक में घूर्ये ने जाति तथा प्रजाति के संबंधों पर प्रचलित सिद्धांतों की विस्तारपूर्वक आलोचना की। इस सर्वप्रचलित विचार के प्रमुख उद्घोषक हरबर्ट रिजले थे, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे और मानवविज्ञान के मामलों में बेहद रुचि रखते थे। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए जैसे-खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई, अथवा कपाल का भार या खोपड़ी का वह हिस्सा जहाँ दिमाग की स्थिति होती है-अलग तथा भिन्न प्रजातियों में बाँटा गया है।
रिजले तथा अन्य लोगों की यह मान्यता थी कि भारत विभिन्न प्रजातियों के उदाविकास के अध्ययन की एक विशिष्ट ‘प्रयोगशाला’ था क्योंकि जाति एक लंबे समय से विभिन्न समूहों के बीच एक लंबे समय से अंतर्विवाह निषिद्ध करती है। रिजले का मुख्य तर्क था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ होगा क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं। सामान्य रूप से उच्च जातियाँ तकरीबन भारतीय-आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं से मिलती हैं, जबकि निम्न जातियों में अनार्य जनजातियों, मंगोल अथवा अन्य प्रजातियों के गुण देखने को मिलते हैं। विभिन्न वर्गों की भिन्नताओं के औसतन आधार पर जैसे नाक की लंबाई, कपाल का आकार आदि, रिजले तथा अन्य लोगों ने यह सुझाव दिया कि निम्न जातियाँ ही भारत की वास्तविक आदि निवासी हैं। उन्हें आर्यों द्वारा दबाया गया जो कहीं बाहर से आकर भारत में बस गए थे।
रिजले द्वारा दिए गए तर्कों से घूर्ये असहमत नहीं थे लेकिन वे उसे केवल अंशतः सत्य मानते थे। उन्होंने उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जो केवल औसत के आधार पर, बिना परिवर्तनों को ध्यान में रखे किसी भी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू कर दिए जाने से होती हैं। घूर्ये का यह विश्वास था कि रिजले के शोध प्रबंध में उच्च जातियों को आर्य तथा निम्न जातियों को अनार्य बताया गया है, यह व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए ही सही है। भारत के अन्य भागों में, अंतरसमूहों की भिन्नताएँ मानवमिति माप बहुत व्यापक अथवा व्यवस्थित नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ कि अधिकांश भारत में, सिंधु-गंगा के मैदान छोड़कर, विभिन्न प्रजातीय वर्गों का आपस में काफ़ी लंबे समय से मेल-मिलाप था। अतः ‘प्रजातीय शुद्धता’ केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी क्योंकि वहाँ अंतर्विवाह निषिद्ध था। शेष भारत में अन्तःविवाह (जाति विशेष में ही विवाह करना) का प्रचलन उन वर्गों में हुआ जो प्रजातीय स्तर पर वैसे ही भिन्न थे।
आज जाति के इस प्रजातीय सिद्धांत को नहीं माना जाता, परंतु बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में इसे सच माना जाता था। इतिहासकारों में आर्यों तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उनके आगमन को लेकर मतभेद है। हालाँकि, जिस समय घूर्य इस विषय पर लिख रहे थे, उस समय इस विषय के ये मुद्दे महत्त्वपूर्ण थे, इसी कारण से इनके लेखों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
घूर्ये जाति की एक विस्तृत परिभाषा दिए जाने के कारण भी जाने जाते हैं। उनकी परिभाषा छह महत्त्वपूर्ण विशेषताओं पर बल देती है।
1. जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जातीय समाज कई बंद, पारस्परिक अनन्य खंडों में बँटा है। प्रत्येक जाति ऐसा ही एक खंड है। यह बंद है क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। एक विशिष्ट जाति के बच्चे हमेशा उसी जाति के होंगे। दूसरे शब्दों में, जाति की सदस्यता केवल जन्म के आधार पर मिलती है। संक्षेप में, किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म से, जन्म के समय होता है। इससे न तो बचा जा सकता है और न ही बदला जा सकता है।
2. जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होते हैं। प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है अर्थात प्रत्येक जाति दूसरी से उच्च अथवा निम्न होती है। सैद्धांतिक रूप से (प्रचलन में नहीं) कोई भी दो जातियाँ समान नहीं होतीं।
3. संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने पर। किस प्रकार के खाद्य पदार्थ को विभिन्न जातियों के बीच बाँटा जा सकता है; इसके विस्तृत नियम हैं। ये नियम पवित्रता तथा अपवित्रता के विचार से संचालित होते हैं। यही तथ्य सामाजिक अंतःक्रिया पर भी लागू होते हैं; यह विशेष नाटकीय रूप से अस्पृश्यता के क्षेत्र में दिखाई देता है, जहाँ किसी जाति विशेष के व्यक्ति द्वारा छू जाने मात्र से इनसान अपवित्र हो जाता है।
4. सोपानिक तथा प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांतों को मानते हुए जाति में विभिन्न जातियों के लिए भिन्न-भिन्न अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित होते हैं। उनके अधिकार तथा कर्तव्य केवल धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित न रहकर धर्मनिरपेक्ष विश्व तक फैले हुए हैं। जैसा कि नृजातीय वर्णन जातिगत समाज की दिनचर्या को दिखाता है, विभिन्न जातियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया इन्हीं नियमों से चालित होती है।
5. जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है जो जाति की तरह, जन्म पर आधारित तथा वंशानुगत होता है। समाज के स्तर पर, जातिगत श्रम विभाजन में कठोरता देखी जाती है तथा विशिष्ट व्यवसाय कुछ विशिष्ट जातियों को ही दिए जाते हैं।
6. जाति, विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंतःविवाह (जाति में ही विवाह), के साथ ही ‘बहिर्विवाह’ के नियम भी जुड़े रहते हैं, अथवा किसकी शादी किससे नहीं हो सकती है। इस प्रकार की योग्यता और निर्योग्यता के समूहों के नियम जाति प्रथा को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
घूर्ये की परिभाषा जाति के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक है। उनकी परिभाषा अवधारणात्मक थी जो शास्त्रीय पुस्तकों पर आधारित थी। वास्तविक रूप से, जाति के बहुत से रूपों में परिवर्तन हो रहा था हालाँकि वे सब किसी न किसी रूप में अस्तित्व में हैं। आगे आने वाले कई दशकों में नृजातीय क्षेत्र के अध्ययनों ने इस विषय पर महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित करने में मदद की है कि स्वतंत्र भारत में इस क्षेत्र में (जाति) क्या कुछ हो रहा है।
1920 तथा 1950 ई. के मध्य भारत में समाजशास्त्र के दो प्रमुख विभाग मुंबई तथा लखनऊ में खुले। दोनों का प्रारंभ समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के मिले-जुले विभाग के रूप में हुआ। जहाँ मुंबई विभाग इस समय जी.एस. घूर्ये द्वारा संचालित हो रहा था वहीं दूसरी ओर लखनऊ विभाग प्रसिद्ध ‘त्रिदेव’ राधाकमल मुकर्जी (संस्थापक), डी.पी. मुकर्जी तथा डी.एन. मजूमदार द्वारा चलाया जा रहा था। वैसे तीनों ही जाने-माने थे तथा अपने कार्यों के लिए पहचाने जाते थे परंतु डी.पी. मुकर्जी इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय थे। वास्तव में डी.पी. मुकर्जी, ज्यादातर डी.पी. के नाम से ही जाने जाते थे जो न केवल समाजशास्त्र में बल्कि शिक्षण के अलावा बौद्धिक तथा जनजीवन में भी अपने समय के सर्वाधिक प्रभावशाली विद्वान रहे हैं। इनका प्रभाव तथा सार्वजनिक लोकप्रियता इनके विद्वातापूर्ण लेखन से उतनी नहीं मिली जितनी शिक्षण, शैै्षणिक घटनाओं पर उनके भाषण, मीडिया में उनके द्वारा किए गए कार्य जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों के लेख तथा रेडियो प्रोग्राम, से मिली। डी.पी. ने समाजशास्त्र से पहले इतिहास तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था तथा इन विविध विषयों में उनकी अभिरुचि थी, जिसका विस्तार क्षेत्र साहित्य, संगीत, फ़िल्म, पाश्चात्य तथा भारतीय दर्शन, मार्क्सवाद, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, तथा विकास को योजना थी। मार्क्सवाद से वे बेहद प्रभावित थे, हालाँकि इसके राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा इसके सामाजिक विश्लेषण के तरीकों
ध्रुजटि प्रसाद मुकर्जी (1894-1961)
5 अक्तूबर 1894 को एक मध्यमवर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्म, जहाँ कि उच्च शिक्षा की लंबी परंपरा थी। विज्ञान में स्नातक; कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।
1924 : लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति।
1938-41 : ब्रिटिश भारत के यूनाइटेड प्रोविंस की कांग्रेस गठित सरकार में (वर्तमान उत्तर प्रदेश) सूचना मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्ति
1947 : यू.पी. लेबर एंक्वायरी कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य किया।
1949 : लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्ति; (उप-कुलपति के विशेष आदेश पर )
1953 : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्ति।
1955 : नवनिर्मित इंडियन सोशयोलॉजिकल सोसायटी में अध्यक्षीय भाषण।
1956 : स्विट्ज्जरलैंड में गले के कैंसर की सर्जरी, 5 दिसंबर 1961 को निधन।
में उनका विश्वास अधिक था। डी.पी. ने अंग्रेज़ी तथा बंगाली में काफ़ी पुस्तकें लिखीं। उनके द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक इस विषय में एक श्रेष्ठ कार्य है जो इस वर्ग की कालजयी रचना मानी जाती है।
परंपरा एवं परिवर्तन पर डी.पी. मुकर्जी के विचार
डी.पी. मुकर्जी भारतीय इतिहास तथा अर्थव्यवस्था के प्रति अपने असंतोष के कारण समाजशास्त्र की ओर मुड़े। उनका यह मानना था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका निर्णायक एवं विशिष्ट लक्षण है और इसलिए, यह प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक है कि वह इस संदर्भ में इससे जुड़ा हो। भारतीय संदर्भ में निर्णायक पक्ष उसका सामाजिक पक्ष है- इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र पश्चिम के मुकाबले भारत में कम विकसित थे; उसका सामाजिक आयाम अधिकाधिक विकसित था। डी.पी. लिखते हैं-“मेरा यह मानना है कि भारत में सामाजिकता का बाहुल्य है, इसके अलावा और सब कुछ बहुत कम है। वास्तव में सामाजिकता की अधिकता भारत की विशेषता ही है। भारत का इतिहास, इसका अर्थशास्त्र, यहाँ तक कि इसका दर्शन सामाजिक समूहों के इर्द-गिर्द घूमता है, ज़्यादा से ज़्यादा यह भी कह सकते हैं कि यह समाजीकृत व्यक्तियों के इर्द-गिर्द है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।” (मुकर्जी
भारत में समाज की केंद्रीय स्थिति को देखते हुए, भारतीय समाजशास्त्री का यह प्रथम कर्तव्य था कि वह सामाजिक परंपराओं के बारे में पढ़े तथा जाने। डी.पी. के लिए परंपरा का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं था बल्कि वह परिवर्तन की संवेदनशीलता से भी जुड़ा था। अतः परंपरा एक जीवंत परंपरा थी, जिसने अपने आपको भूतकाल से जोड़ने के साथ ही साथ वर्तमान के अनुरूप भी ढाला था और इस प्रकार समय के साथ अपने आपको विकसित कर रही थी। जैसा कि उन्होंने लिखा, “…सिर्फ़ भारतीय समाजशास्त्री के लिए एक समाजशास्त्री होना काफ़ी नहीं होता है। बल्कि उसकी प्रथम आवश्यकता एक भारतीय होना है क्योंकि वह लोकरीतियों, रूढियों, प्रथाओं तथा परंपराओं से जुड़कर ही अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंदर तथा उसके आगे क्या है, को समझा पाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, उनका मानना था कि समाजशास्त्रियों को भाषा को सीखना तथा भाषा की उच्चता-निम्नता और संस्कृति की पहचान हो-न केवल संस्कृत, फ़ारसी अथवा अरबी भाषाएँ बल्कि स्थानीय बोलियों की भी जानकारी हो।”
डी.पी. ने यह तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति तथा समाज पाश्चात्य अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं हैं। एक औसत भारतीय की आकांक्षाओं का रूप, कम या अधिक, उसके सामाजिक-सांस्कृतिक वर्ग द्वारा तय किया जाता है और वह शायद ही उससे विचलित होता है। अतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था की दिशा मुख्यतः समूह, संप्रदाय तथा जाति के क्रियाकलापों द्वारा निर्धारित होती है न कि ‘स्वैच्छिक’ व्यक्तिगत कार्यों द्वारा। हालाँकि ‘स्वैच्छिकता’ ने शहरी मध्यम वर्ग को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके आने से भारतीय समाज को अध्ययन के लिए एक रोचक विषय मिल गया था। परंपरा शब्द का मूल अर्थ संचारित/प्रेषित करना है-डी.पी. ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इसका समतुल्य संस्कृत शब्द परंपरा है, जोकि, उत्तराधिकार; अथवा आतिथ्य है, जिसका मूल आधार वही है जो इतिहास का है। अतः परंपरा की मज़बूत जड़ें भूतकाल में होती हैं और उन्हें कहानियों तथा मिथकों द्वारा कहकर और सुनकर जीवित रखा जाता है। हालाँांक परिवर्तन भी भूतकाल से उसके संबंध को नहों तोड़ पाया। बल्कि यह अनुकूलन की प्रक्रिया को इंगित करता है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन के आंतरिक तथा बाह्य स्रोत हमेशा मौजूद रहते हैं। पाश्चात्य समाज में आंतरिक परिवर्तन का अत्यधिक सामान्य स्रोत अर्थव्यवस्था है परंतु यह भारत में उतना प्रभावशाली नहीं है। जैसा कि डी.पी. मानते थे कि भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष जातीय परंपराओं से प्रभावित होता है और उसे अपने में सम्मिलित कर लेता है। भारत में नवीन वर्ग संघर्ष अभी स्पष्ट रूप में उभर कर नहीं आया है। इस समझ के आधार पर, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक गैर आर्थिक कारणों को देखना होगा।
डी.पी. की यह मान्यता थी कि भारतीय परंपरा में परिवर्तन के तीन सिद्धांतों को मान्यता दी गई है-श्रुति, स्मृति तथा अनुभव। इन सब में आखिरी-अनुभव अथवा व्यक्तिगत अनुभवक्रांतिकारी सिद्धांत है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्वप्रमुख सिद्धांत सामान्यीकृत अनुभव अथवा समूहों का सामूहिक अनुभव था। उच्च परंपराएँ स्मृति तथा श्रुति में केंद्रित थीं परंतु समय-समय पर उन्हें समूहों तथा संप्रदायों के सामूहिक अनुभवों द्वारा चुनौती दी जाती रही है, उदाहरणत: भक्ति आंदोलन। डी.पी. ने बल देकर कहा कि यह केवल हिंदुओं के लिए ही सही नहीं है बल्कि भारत को इस्लामी संस्कृति के लिए भी सही है। भारतीय इस्लाम में, सूफियों ने पवित्र ग्रंथों की अपेक्षा प्रेम तथा अनुभव पर अधिक बल दिया है; जिसने परिवर्तन लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अत: डी.पी. के लिए भारतीय संदर्भ में बुद्धि-विचार, परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है; बल्कि ऐतिहासिक रूप से अनुभव और प्रेम परिवर्तन के उत्कृष्ट कारक हैं।
भारतीय संदर्भ में संघर्ष तथा विद्रोह सामूहिक अनुभवों के आधार पर कार्य करते हैं। परंतु परंपरा का लचीलापन इसका ध्यान रखता है कि संघर्ष का दबाव परंपराओं को बिना तोड़े उनमें परिवर्तन लाए। अतः हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभावी रूढ़िवाद को लोकप्रिय विद्रोहों द्वारा चुनौती दी जाती है जो आगे चलकर रूढ़िवाद को परिवर्तित करने में सफल तो हो जाती हैं परंतु ये परिवर्तन आखिरकार परंपरा में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह चक्र लगातार अपने आप को दोहराता रहता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया-जहाँ संघर्ष परंपरा की सीमाओं में रहता है-ठेठ जातिगत समाज का लक्षण है, जहाँ वर्गों के बनने तथा वर्ग-चेतना को अवरोधित कर दिया गया है। डी.पी. के परंपरा और परिवर्तन संबंधी विचारों ने पाश्चात्य देशों से बिना सोचे-समझे बौद्धिक परंपराओं को ग्रहण करने के कारण विकास योजनाओं जैसे संदर्भों की भी आलोचना की। परंपरा को न तो पूजना चाहिए और न ही इसको अनदेखा करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे आधुनिकता आवश्यक तो है लेकिन अंधानुकरण के लिए नहीं। डी.पी. परंपरा के समीक्षक थे जो उन्हें विरासत में मिली थी और साथ ही वे आधुनिकता के प्रशंसक आलोचक भी थे जिसके कारण उनके स्वयं के बौद्धिक परिप्रेक्ष्य को आकार प्राप्त हुआ।
ए. आर. देसाई ऐसे विरले भारतीय समाजशास्त्री हैं जो सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों से औपचारिक सदस्य के रूप में राजनीति से जुड़े थे। देसाई आजीवन मार्क्सवादी रहे तथा मार्क्सवादी राजनीति में उनकी सक्रियता बड़ौदा में स्नातक की पढ़ाई करते हुए हुई, हालाँकि बाद में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अपने व्यवसाय के अधिकांश भाग में वे गैर-मुख्यधारा के मार्क्सवादी राजनीतिक समूहों से जुड़े थे। देसाई के पिता बड़ौदा राज्य में माध्यमिक स्तर के प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन साथ ही वे एक जाने-माने उपन्यासकार भी थे तथा उनके मन में भारतीय राष्ट्रवाद (गांधीवाद) तथा समाजवाद-दोनों के लिए हमदर्दी थी। देसाई की माता का देहांत उनके जीवन के प्रारंभिक काल में हो गया था तथा उनकी देखभाल उनके पिता ने की। पिता के बड़ौदा के विभिन्न स्थानों में लगातार होने वाले स्थानांतरण के कारण देसाई ने प्रवासीय जीवन जिया।
क्रियाकलाप 2
‘जीवंत परंपरा’ से क्या तात्पर्य है-विचार कीजिए। डी.पी. मुकर्जी के अनुसार यह एक परंपरा है जो भूतकाल से कुछ ग्रहण कर उससे अपने संबंध बनाए रखती है और साथ ही नयी चीज़ों को भी ग्रहण करती है। अतः एक जीवंत परंपरा पुराने तथा नए तत्त्वों का मिश्रण है। आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब आप विभिन्न पीढ़ी के लोगों से, चाहे वे आपके पड़ोसी हैं या परिवार के सदस्य, यह जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में वे कौन सी चीज़ें हैं जो परिवर्तित हो चुकी हैं या फिर वे जो आज भी परिवर्तित नहीं हुई हैं। यहाँ इस विषय से संबंधित एक सूची दी जा रही है जिस पर आप काम कर सकते हैं; आप अपने मनपसंद विषय को भी चुन सकते हैं। जैसे-आपके उम्र के बच्चों द्वारा खेला जाने वाला खेल। (लड़का/लड़की)
-किसी लोकप्रिय त्योहार को मनाने के तरीके।
-पुरुषों और स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला पहनावा।
…इसके अतिरिक्त आपकी रुचि के अन्य विषय…इनके लिए ज़रूरी है कि आप ढूँढ़े-जहाँ तक आपकी सोच जाती है ऐसे कौन से पहलू हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आया है? किन पहलुओं में परिवर्तन हो गया है? इस व्यवहार में समानता और असमानता क्या है (क) 10 वर्ष पश्चात, (ख) 20 वर्ष पश्चात, (ग) 40 वर्ष पश्चात, (घ) 60 या अधिक वर्ष पश्चात। अपने निष्कर्षों की चर्चा कक्षा में कीजिए।
अक्षय रमनलाल देसाई (1915-1994)
1915 में जन्म, प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में, फिर सूरत तथा मुंबई में।
1934-39 : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य; ट्रोटस्की ग्रुप से संबद्ध।
1946 : जी. एस. घूर्ये के निर्देशन में बंबई विश्वविद्यालय से पीएच.डी.।
1948 : देसाई की पीएच.डी. शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित-सोशल बैकग्राउंड ऑफ़ इंडियन नेशनलिज्म।
1951 : बंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में नियुक्ति।
1953-1981 : रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य।
1961 : रूरल ट्रांज़ीशन इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित।
1967 : प्रोफ़ेसर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।
1975 : स्टेट एंड सोसायटी इन इंडिया : एसेज़ इन डीसेंट प्रकाशित।
1976 : समाजशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त।
1979 : पेज़ेंट स्ट्रगल इन इंडिया प्रकाशित।
1986 : एग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रकाशित।
निधन-12 नवंबर 1994
बड़ौदा में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद देसाई ने बंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रवेश लिया जहाँ घूर्ये उनके गुरु थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक पहलुओं पर अपने डॉक्ट्रेट का शोधग्रंथ लिखा जिस पर 1946 में उन्हें डिग्री प्रदान की गई। 1948 में उनकी थीसिस द सोशल बैकग्राउंड ऑफ़ इंडियन नेशनलिज़्म प्रकाशित हुई जो उनके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे बेहतरीन है। इस पुस्तक में देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी विश्लेषण किया, जिसमें आर्थिक प्रक्रियाओं एवं विभाजनों को महत्त्व दिया गया है, यह ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय हालात कैसे थे। हालाँकि इसकी आलोचना हुई पर फिर भी यह पुस्तक बेहद प्रसिद्ध हुई और इसका कई बार पुनर्मुद्रण भी हुआ। अन्य विषय जिन पर देसाई ने काम किया वे हैं-किसान आंदोलन तथा ग्रामीण समाजशास्त्र; आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्धे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य के स्वरूप और मानवाधिकार। चूँकि मार्क्सवाद भारतीय समाजशास्त्र में बहुत प्रभावशाली या महत्त्वपूर्ण नहीं था अतः ए.आर. देसाई को अपने विषय की तुलना में बाहर ज़्यादा नाम मिला। हालाँकि
देसाई को कई पदवियों से सम्मानित किया गया तथा वे ‘इंडियन सोशयोलॉजिकल सोसायटी’ के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय समाजशास्त्र में देसाई एक अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व रहे।
राज्य पर ए.आर. देसाई के विचार
आधुनिक पूँजीवादी राज्य एक महत्त्वपूर्ण विषय था, जिसमें ए.आर. देसाई की रुचि थी। हमेशा की तरह, इस विषय को समझने में भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। ‘द मिथ ऑफ़ द वेलफेयर स्टेट’ नामक निबंध में देसाई ने विस्तारपूर्वक इसकी विवेचनात्मक समीक्षा की है तथा इसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समाजशास्त्रीय साहित्य की प्रमुख परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, देसाई ने कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं-
1. कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है। इसका अर्थ है कि वह उदारवादी राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत की लेसेज़ फेयर (Lassiez faire) नीति से भिन्न होता है। कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता जो कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। बल्कि कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपीय राज्य होता है और समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक नीतियों को तैयार तथा लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग सक्रिय रूप से करता है।
2. कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य के जन्म के लिए लोकतंत्र की एक अनिवार्य दशा होती है। औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं, विशेषकर बहुपार्टी चुनाव, कल्याणकारी राज्य की पारिभाषिक विशेषता समझी जाती है। यही कारण है कि उदारवादी चिंतकों ने समाजवादी तथा कम्युनिस्ट राज्यों को इस परिभाषा से बाहर रखा है।
3. कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निजी पूँजीवादी कंपनियाँ तथा राज्य अथवा सामूहिक कंपनियाँ-दोनों साथ साथ कार्य करती हों। एक कल्याणकारी राज्य न तो पूँजीवादी बाज़ार को ही खत्म करना चाहता है और न ही यह उद्योगों तथा दूसरे क्षेत्रों में जनता को निवेश करने से रोकता है। कमोबेश कल्याणकारी राज्य ज़रूरत की वस्तुओं और सामाजिक अधिसंरचना पर ध्यान देता है जबकि उपभोक्ता वस्तुओं पर निजी उद्योगों का वर्चस्व होता है।
देसाई कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिसके आधार पर कल्याणकारी राज्य द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण किया जा सके। ये हैं-
1. क्या कल्याणकारी राज्य गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति तथा अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखता है?
2. क्या कल्याणकारी राज्य आय संबंधित असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाता है; जैसे-धन के जमाव को रोककर अथवा अमीरों की आय के कुछ भाग को गरीबों में पुनः बाँटना आदि?
3. क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करता है, जहाँ पूँजीवादियों की अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर, समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई जा सकती हो?
4. क्या कल्याणकारी राज्य स्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी तथा तेज़ी से मुक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है?
5. क्या यह सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है ?
इस आधार को ध्यान में रखते हुए देसाई उन देशों के कार्यों का परीक्षण करते हैं जिनको अकसर कल्याणकारी राज्य कहा जाता है; जैसे-ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोप के अधिकांश भाग और हम यह पाते हैं कि उनके द्वारा काफ़ी बढ़ा-चढ़ा कर दावे किए गए थे। अतः अधिकांश आधुनिक पूँजीवादी राज्य, यहाँ तक कि विकसित देश भी, अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे हैं। वे आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं हो पाए हैं और अधिकांशतः उसे प्रोत्साहित ही करते हैं। तथाकथित कल्याणकारी राज्य बाज़ार के उतार-चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में भी असफल रहे हैं। अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अत्यधिक बेरोज़गारी इसकी कुछ अन्य असफलताएँ हैं। अपने इन तर्कों के आधार पर देसाई ने यह निष्कर्ष निकाला कि कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है।
ए.आर. देसाई ने राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर भी लेखन कार्य किया। उनके इन लेखों में हम देख सकते हैं कि देसाई एकांगी दृष्टिकोण को लेकर नहीं चलते हैं बल्कि कम्युनिस्ट राज्यों की कमियों की आलोचना भी करते हैं। उन्होंने कई मार्क्सवादी चिंतकों के उदाहरणों द्वारा इस तथ्य पर बल दिया है कि कम्युनिज्म के तहत भी लोकतंत्र का महत्त्व होता है तथा राजनीतिक उदारता एवं कानून का राज प्रत्येक वास्तविक समाजवादी राज्य में बने रहना चाहिए।
क्रियाकलाप 3
ए.आर. देसाई कल्याणकारी राज्य की आलोचना मार्क्सवादी तथा सोशलिस्ट दृष्टिकोण से करते हैं। वे चाहते हैं कि पाश्चात्य पूँजीवादी कल्याणकारी राज्यों ने जो किया है, राज्य अपने नागरिकों के लिए उससे अधिक करे। आज इसके विपरीत ये तर्क दिए जा रहे हैं कि राज्य अपनी भूमिकाओं को निरंतर कम करे और इन भूमिकाओं और दायित्व के निर्वाह का बड़ा भाग स्वतंत्र बाज़ार के हवाले कर देना चाहिए। कक्षा में इन दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए और दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनिए।
अपने आस-पड़ोस में राज्य तथा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सूची बनाइए; शुरुआत अपने विद्यालय से कीजिए। लोगों से पता करने के लिए पूछिए कि आज के संदर्भ में क्या यह सूची बढ़ी है या छोटी हुई है-क्या राज्य पहले की अपेक्षा आज अधिक कार्य कर रहा है या कम? आपको क्या लगता है-यदि राज्य इन कार्यों को करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या आपका पड़ोस/विद्यालय की स्थिति खराब/अच्छी, अथवा वैसी ही रहेगी, उस पर
कोई प्रभाव नहीं पडेगगा? अगर राज्य अपने कुछ क्रियाकलापों को रोक दे तो अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग तथा गरीब व्यक्ति के विचार वैसे ही रहेंगे अथवा उन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा?
आपके पड़ोस में राज्य द्वारा दी गई सुविधाओं एवं सेवाओं की एक सूची बनाइए। सरकार द्वारा ये सुविधाएँ रोक दी जाएँ अथवा चलाई जाएँ-इस विषय पर विभिन्न वर्गों के विचार किस प्रकार से अलग हो सकते हैं उसे देखिए। (उदाहरणतः सड़क, पानी, बिजली, सड़क की बत्तियाँ, विद्यालय, सफाई, पुलिस सेवाएँ, अस्पताल, बस, ट्रेन वायु परिवहन….। कुछ अन्य चीज़ों को सोचिए जो आपके संदर्भ में अनिवार्य हों)
स्वतंत्र भारत के बेहतरीन भारतीय समाजशास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास ने डॉक्ट्रेट की उपाधि दो बार प्राप्त की-एक बंबई विश्वविद्यालय से तथा दूसरी ऑक्सफोर्ड से। श्रीनिवास मुंबई में घूर्ये के शिष्य थे। ऑक्सफोर्ड के सामाजिक मानवविज्ञान विभाग में अध्ययन के दौरान इनके बौद्धिक अभिविन्यास में बदलाव आया। उस समय ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञान, पाश्चात्य मानवविज्ञान में एक प्रभावी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था और श्रीनिवास, स्वयं विषय के महत्त्वपूर्ण ‘केंद्र’ में रहकर उसके अध्ययन से प्रसन्न थे। श्रीनिवास के डॉक्ट्रेट के शोध निबंध का प्रकाशन रिलीजन एंड सोसायटी एमंग द कुर्गस ऑफ़ साऊथ इंडिया के नाम से हुआ। इस पुस्तक में श्रीनिवास ने ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञान में प्रभावी संरचनात्मक-प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य पर कार्य किया। इस पुस्तक ने पूरे विश्व में श्रीनिवास का सम्मान बढ़ाया। ऑक्सफोर्ड में नवस्थापित भारतीय समाजशास्त्र विभाग में प्रवक्ता के रूप में श्रीनिवास की नियुक्ति की गई, परंतु 1951 में इस्तीफा देकर वे भारत लौट आए जहाँ महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा में नवस्थापित समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार सँभाला। 1959 में वे दिल्ली आए जहाँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की जो शीघ्र ही पूरे भारत में समाजशास्त्र का महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया।
श्रीनिवास अकसर यह शिकायत करते थे कि उनका अधिकांश समय संस्थाओं को बनाने में ही बीत जाता है और स्वयं उनके पास शोधकार्य के लिए बहुत ही कम समय रह जाता है। इन कठिनाइयों के रहते हुए भी, श्रीनिवास ने कुछ विषयों पर महत्त्वपूर्ण कार्य किए जैसे-जाति, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाएँ, ग्रामीण समाज इत्यादि। श्रीनिवास ने अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान तथा सहयोगियों की मदद से भारतीय समाजशास्त्र को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया। उनकी ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञान तथा अमेरिकन मानवविज्ञान, विशेष तौर पर शिकागो विश्वविद्यालय में ज़बरदस्त पहचान थी जो उस समय विश्व मानवविज्ञान में एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर रहा था। जी.एस. घूर्ये तथा लखनऊ के विद्वानों की तरह श्रीनिवास ने भी नयी पीढ़ी के समाज को तैयार किया जो आने वाले दशकों में अपने विषय के दिग्गजों के रूप में स्थापित होने वाले थे।
एम.एन. श्रीनिवास के गाँव संबंधी विचार
एम.एन. श्रीनिवास की रुचि भारतीय गाँव तथा ग्रामीण समाज में जीवनभर बनी रही। यद्यपि वे गाँवों में कई बार सर्वेक्षणों तथा साक्षात्कार के लिए जा चुके थे, लेकिन एक वर्ष तक मैसूर के निकट के एक गाँव में कार्य करने के पश्चात ही इन्हें ग्रामीण समाज के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। गाँव में रहकर कार्य करने का अनुभव इनके व्यवसाय तथा बौद्धिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हुआ। 1950-60 के दौरान श्रीनिवास ने ग्रामीण समाज से संबंधित विस्तृत नृजातीय ब्यौरों के लेखे-जोखों को तैयार करने में सामूहिक परिश्रम को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि उसका समन्वय भी किया। श्रीनिवास ने
मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास (1916-1999)
16 नवंबर 1916 को मैसूर के आयंगार ब्राह्मण परिवार में जन्म। इनके पिता ज़मींदार थे और मैसूर के ऊर्जा तथा बिजली विभाग में कार्यरत थे। प्रारंभिक शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय में, बाद में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु मुंबई गए जहाँ घूर्ये इनके गुरु थे।
1942 : स्नातकोत्तर शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित विषय-‘मैरिज एंड फैमिली एमंग द कुर्गस’
1944 : पीएच.डी शेधकार्य (2 भाग में) बंबई विश्वविद्यालय से घूर्ये के निर्देशन में किया।
1945 : ऑक्सफोर्ड गए; पहले रैडक्लिफ्फ ब्राउन तथा फिर इवान्स प्रीचर्ड द्वारा शिक्षा ग्रहण।
1947 : ऑक्सफोर्ड से सामाजिक मानवविज्ञान में डी.फिल कर वापस भारत आए।
1948 : ऑक्सफोर्ड में भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति; इसी समय (1948) रामपुरा में क्षेत्रकार्य किया।
1951 : ऑक्सफोर्ड से इस्तीफा दिया तथा महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा में प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्ति तथा समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की।
1959 : दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनोमिक्स में प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्ति; समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की।
1971 : दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ा। बैंगलोर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकॉनोमिक चेंज के सह-संस्थापक।
निधन-30 नवंबर 1999

एस.सी. दुबेे तथा डी.एन. मजूमदार जैसे विद्वानों के साथ मिलकर भारतीय समाजशास्त्र में उस समय के ग्रामीण अध्ययन को प्रभावशाली बनाया।
गाँव पर श्रीनिवास द्वारा लिखे गए लेख मुख्यतः दो प्रकार के हैं। सर्वप्रथम, गाँवों में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का नृजातीय ब्यौरा और इन ब्यौरों पर परिचर्चा। द्वितीय प्रकार के लेखन में भारतीय गाँव सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में कैसे कार्य करते हैं-इस पर ऐतिहासिक तथा अवधारणात्मक परिचर्चाएँ। द्वितीय प्रकार के लेखन में गाँव की एक अवधारणा के रूप में उनकी उपयोगिता के प्रश्न पर श्रीनिवास का विवाद हुआ। ग्रामीण अध्ययन के खिलाफ, कुछ सामाजिक मानवशास्त्रियों जैसे लुई ड्यूमों का मानना था कि जाति जैसी सामाजिक संस्थाएँ गाँव की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण थीं क्योंकि गाँव केवल कुछ लोगों का समूह था जो एक विशेष स्थान पर रहते थे। गाँव बने रह सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं और लोग एक गाँव को छोड़ दूसरे गाँव को जा सकते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक संस्थाएँ, जैसे जाति अथवा धर्म, सदैव उनके साथ रहते हैं और जहाँ वे जाते हैं वहाँ सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण से ड्यूमों का मानना था कि गाँव को एक श्रेणी के रूप में महत्त्व देना गुमराह करने वाला हो सकता है। इसके विरुद्ध, श्रीनिवास का यह मानना था कि गाँव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है। ऐतिहासिक साक्ष्य यह दिखाते हैं कि गाँवों ने अपनी एक एकीकृत पहचान बनाई है और ग्रामीण एकता ग्रामीण सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्त्वपूर्ण है। श्रीनिवास ने ब्रिटिश प्रशासक मानव वैज्ञानिकों की आलोचना की जिन्होंने भारतीय गाँव का स्थिर, आत्मनिर्भर, छोटे गणतंत्र के रूप में चित्रण किया था। ऐतिहासिक तथा सामाजिक साक्ष्य द्वारा, श्रीनिवास ने यह दिखाया कि वास्तव में गाँवों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। यहाँ तक कि गाँव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे और विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों से क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े हुए थे।
गाँव ग्रामीण शोधकार्यों के स्थल के रूप में भारतीय समाजशास्त्र को कई तरह से लाभान्वित करते हैं। इसने नृजातीय शोधकार्य की पद्धति के महत्त्व से परिचित कराने का एक मौका दिया। नव-स्वतंत्र राष्ट्र जब विकास की योजनाएँ बना रहा था, ऐसे समय में इसने भारतीय गाँवों में तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के बारे में आँखों देखी जानकारी दी। ग्रामीण भारत से संबंधित इन विविध जानकारियों की उस समय काफ़ी प्रशंसा हुई क्योंकि नगरीय भारतीय तथा नीति निर्माता इससे अनुमान लगा सकते थे कि भारत के आंतरिक हिस्सों में क्या हो रहा था। इस प्रकार ग्रामीण अध्ययन ने समाजशास्त्र जैसे विषय को स्वतंत्र राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक नयी भूमिका दी। मात्र आदिम मानव के अध्ययन तक सीमित न रहकर, इसे आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकता है।
क्रियाकलाप 4
मान लीजिए कि आपका कोई मित्र दूसरे ग्रह अथवा सभ्यता का है अर पहली बार पृथ्वी पर आया है और उसने कभी गाँव के बारे में नहीं सुना है। आप उन्हें ऐसे कौन से पाँच सुराग देंगे ताकि वे कभी गाँव को देखें तो उसे पहचान सकें।
इसे छोटे-छोटे समूहों में आयोजित कीजिए और विभिन्न समूहों द्वारा दिए गए सुरागों की तुलना कीजिए तथा देखिए कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो बार-बार उभर कर सामने आती हैं। क्या इसके आधार पर आप गाँव की परिभाषा दे सकते हैं? (आपकी परिभाषा एक अच्छी परिभाषा है या नहीं इसे देखने के लिए अपने आप से एक सवाल कीजिए-क्या ऐसा कोई गाँव है जहाँ आपके द्वारा दी गई परिभाषा की सभी या ज़्यादातर चीज़ें अनुपस्थित हैं?)
क्रियाकलाप 5
1950 में नगरीय भारतीयों में ग्रामीण अध्ययन के प्रति काफ़ी रुचि थी जिसे समाजशास्त्रियों ने उस समय शुरू किया था। क्या आपको लगता है कि नगर के लोग आज भी गाँव में रुचि रखते हैं? टी.वी., फ़िल्म अथवा अखबारों में गाँव पर कितनी बार चर्चा की जाती है? अगर आप नगर में रहते हैं तो क्या आपका परिवार आज भी अपने गाँव के रिश्तेदार के संपर्क में है? इस प्रकार के संपर्क आपके पिता अथवा दादा की पीढ़ी में थे? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नगर छोड़ गाँव में जाकर बस गया हो? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो वापस जाना चाहता हो? अगर हाँ, तो वे कौन से कारण हैं जिनके लिए ये नगर छोड़ गाँव में जाकर बसना चाहते हैं? अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो अपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग गाँव में नहीं रहना चाहते हैं? अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, जो गाँव का रहने वाला है, पर नगर में रहना चाहता है, तो वे गाँव छोड़ने के क्या कारण देते हैं?
उपसंहार
इन चार समाजशास्त्रियों ने, इस विषय (समाजशास्त्र) को नव-स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्र के संदर्भ में एक अलग पहचान देने को कोशिश की। किन विभिन्न तरीकों से समाजशास्त्र को ‘भारतीय’ बनाया गया इसके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अतः घूर्ये ने उन प्रश्नों से शुरुआत की जो पाश्चात्य मानवशास्त्रियों द्वारा उठाए गए थे लेकिन यहाँ उन्होंने शास्त्रीय पुस्तकों से अर्जित अपने ज्ञान तथा एक शिक्षित भारतीय सोच का उपयोग किया। एक भिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले, पूर्णरूपेण पाश्चात्य डी.पी. मुकर्जी जैसे आधुनिक बुद्धिजीवी ने भारतीय परंपरा की महत्ता को पुन: खोजा, बिना इसकी कमियों को नज़रअंदाज़ करते हुए। मुकर्जी की ही तरह ए.आर. देसाई भी मार्क्सवाद से अत्यधिक प्रभावित थे और भारतीय राष्ट्र की समालोचना ऐसे समय में की, जब इस प्रकार की आलोचनाएँ दुर्लभ थीं। पाश्चात्य सामाजिक मानवशास्त्र के प्रभावी केंद्रों में रह कर प्रशिक्षण प्राप्त एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय संदर्भ में इसका प्रयोग किया और बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समाजशास्त्र की नवीन कार्यसूची को तैयार करने में मदद की।
यह किसी भी विभाग की शक्ति के लिए शुभ लक्षण हैं जब उसकी एक पीढ़ी अपने पूर्वजों से ज्ञान पाकर उनसे भी आगे निकल जाती है। भारतीय समाजशास्त्र मे ऐसा होता रहा है। आने वाली पीढ़ियों ने इन अग्रदूतों के कार्यों की सकारात्मक आलोचना भी की ताकि यह विषय और अधिक विकसित हो सके। सीखने की इस प्रक्रिया के चिह्न तथा समालोचक केवल इस पुस्तक में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाजशास्त्र में देखे जा सकते हैं।
शब्दावली
प्रशासक-नृशास्त्री- यह पद उन ब्रिटिश प्रशासकों के लिए प्रयुक्त होता है जो 19 वीं तथा प्रारंभिक ब्रिटिश भारतीय सरकार के भाग थे तथा जिन्होंने नृजातीय अनुसंधानों को प्रारंभ करने में अत्यधिक रुचि ली विशेषकर सर्वे तथा जनगणना। इनमें से कुछ सेवानिवृत्ति के पश्चात नामी नृशास्त्री बने। प्रमुख नामों में एडगर थर्सटन, विलियम क्रूक, हरबर्ट रिज़ले तथा जे.एच. हट्टन हैं।
मानवमिति / नृमिति- नृशास्त्र का एक विभाग जो मनुष्य की प्रजाति का अध्ययन उसके शरीर के माप, विशेषकर उसकी खोपड़ी के भार, सिर की चौड़ाई तथा नाक की लंबाई के आधार पर करता है।
समायोजन- वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति (विशेषतः बड़ी अथवा अधिक प्रभावी) दूसरी संस्कृति को अपने अंदर समा लेती है तथा पहली संस्कृति में मिल जाती है, ताकि यह प्रक्रिया के अंत में जीवित या अलग से दिखाई न दे।
अंतर्विवाह- सामाजिक संस्था जहाँ वैवाहिक रिश्ते केवल अपनी बिरादरी में ही किए जाते हैं; इस सीमांकित वर्ग के बाहर विवाह निषेध होते हैं। इसका आम उदाहरण जाति विवाह है, जहाँ विवाह अपनी ही जाति के व्यक्ति से होता है।
बहिर्विवाह- सामाजिक संस्था जहाँ कुछ वर्गों में वैवाहिक संबंध निषिद्ध होते हैं। विवाह इन निषिद्ध वर्गों के बाहर होना चाहिए। आम उदाहरण हैं-खून के रिश्तेदारों में विवाह निषेध (सपिंड बाहिर्विवाह), एक गोत्र में विवाह निषेध (सगोत्र बाहिर्विवाह) अथवा एक ही गाँव अथवा क्षेत्र में विवाह निषेध (गाँव/क्षेत्र बहिर्विवाह) है।
मुक्त व्यापारः फ्रांसीसी मुहावरा (शाब्दिक अर्थ ‘जैसा है’ अथवा ‘अकेला छोड़ो’) जो राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांत के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक संबंधों में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करता है; मुक्त बाज़ार की दक्षता तथा नियामक शक्तियों की मान्यता से जुड़ा है।
अभ्यास
1. अनन्तकृष्ण अय्यर तथा शरतचंद्र रॉय ने सामाजिक मानवविज्ञान के अध्ययन का अभ्यास कैसे किया?
2. ‘जनजातीय समुदायों को कैसे जोड़ा जाए’-इस विवाद के दोनों पक्षों के क्या तर्क थे?
3. भारत में प्रजाति तथा जाति के संबंधों पर हरबर्ट रिज़ले तथा जी.एस. घूर्ये की स्थिति की रूपरेखा दें।
4. जाति की सामाजिक मानवशास्त्रीय परिभाषा को सारांश में बताए।
5. ‘जीवंत परंपरा’ से डी.पी. मुकर्जी का क्या तात्पर्य है? भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपनी परंपरा से जुड़े रहने पर बल क्यों दिया?
6. भारतीय संस्कृति तथा समाज की क्या विशिष्टताएँ हैं तथा ये बदलाव के ढाँचे को कैसे प्रभावित करते हैं?
7. कल्याणकारी राज्य क्या है? ए.आर. देसाई कुछ देशों द्वारा किए गए दावों की आलोचना क्यों करते हैं?
8. समाजशास्त्रीय शोध के लिए ‘गाँव’ को एक विषय के रूप में लेने पर एम.एन. श्रीनिवास तथा लुई ड्यूमों ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क दिए हैं?
9. भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्त्व है? ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में एम.एन. श्रीनिवास की क्या भूमिका रही?