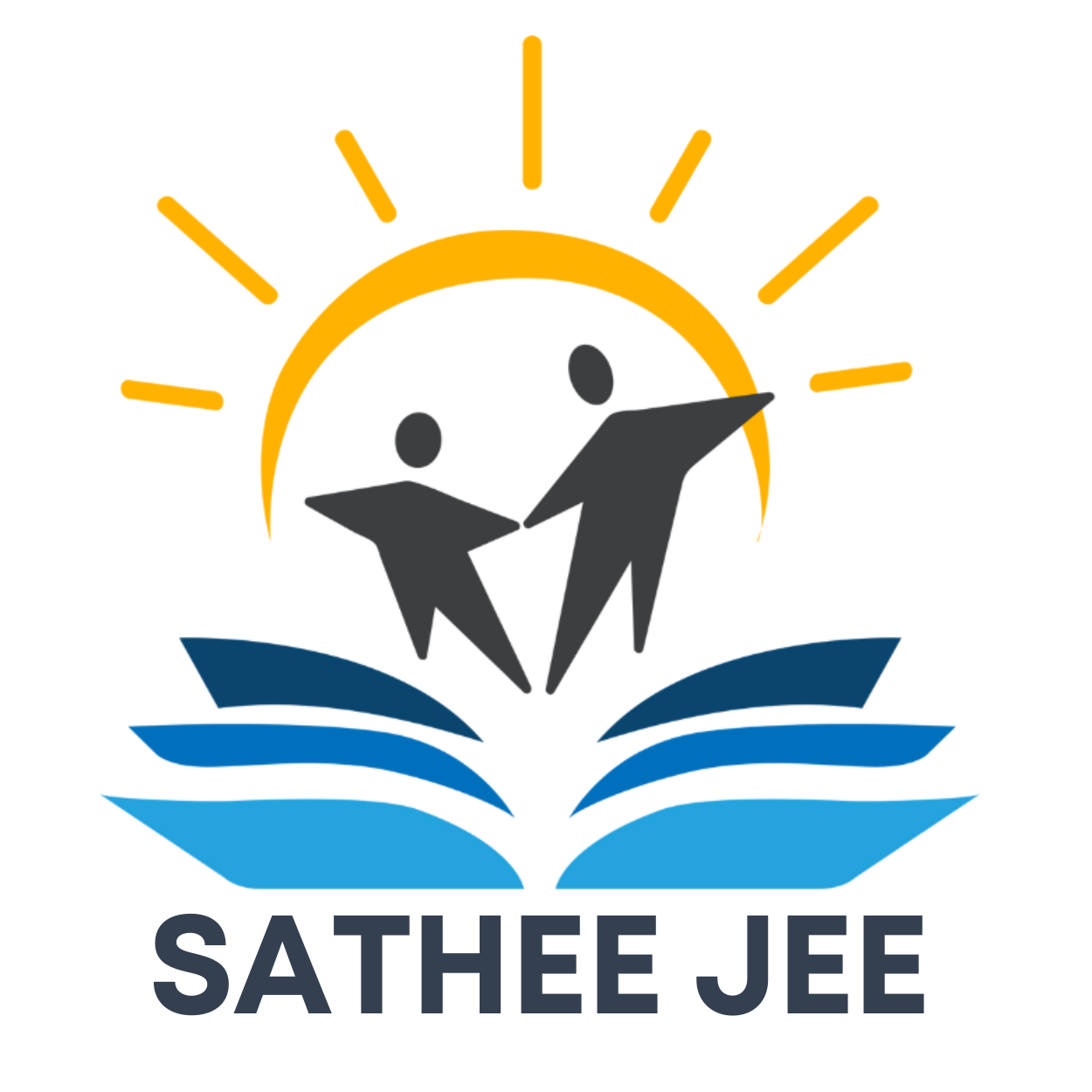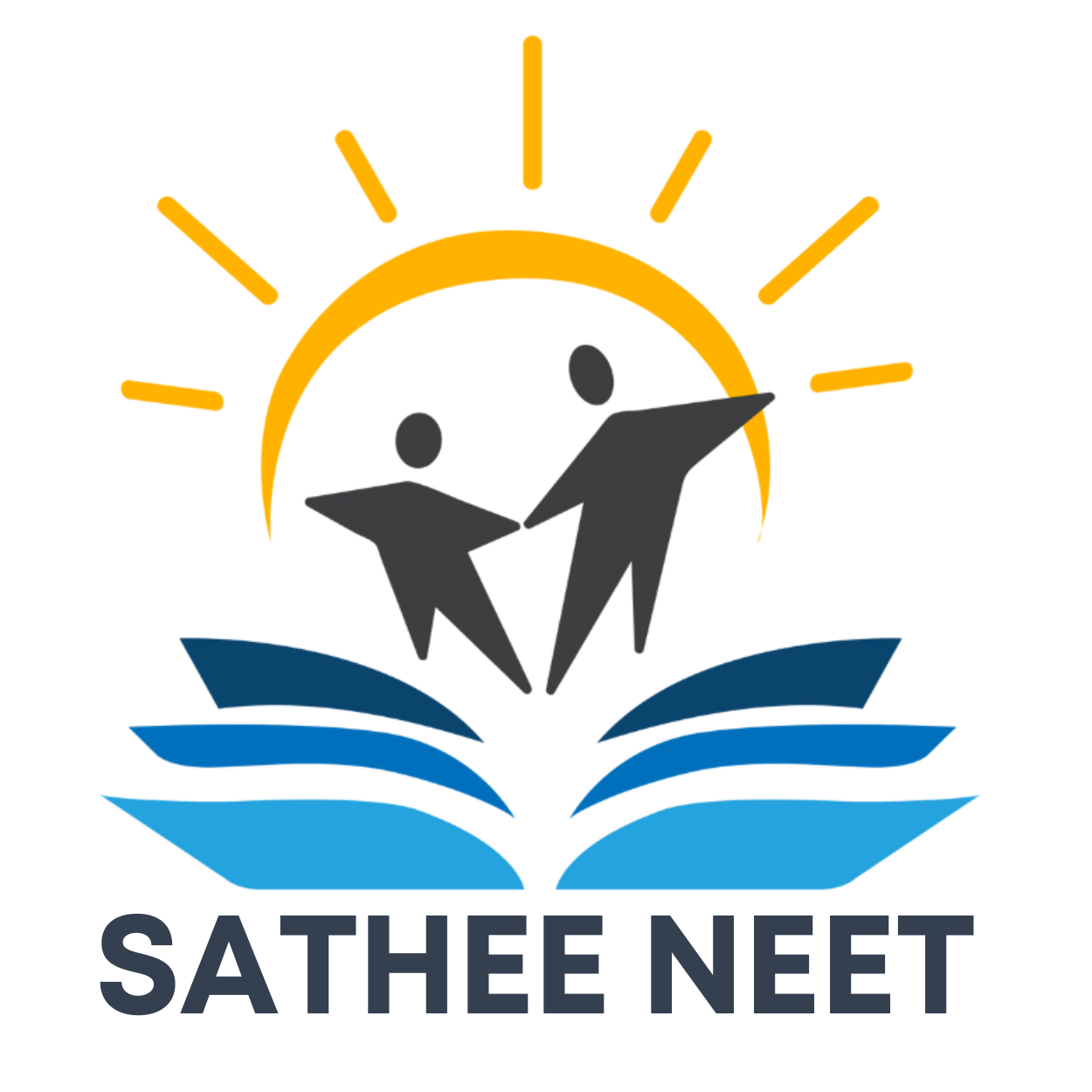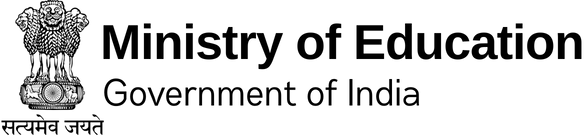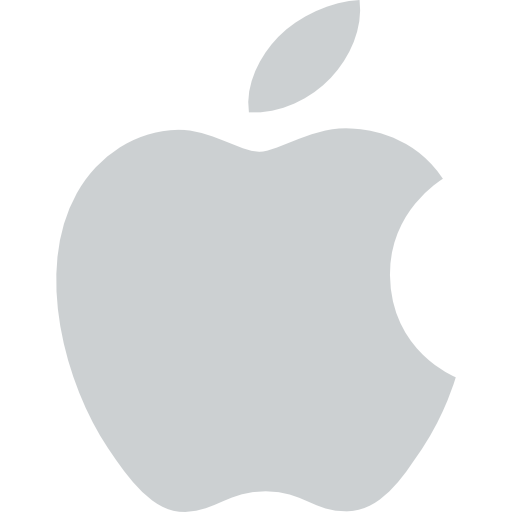अध्याय 11 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन
विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकडों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आँकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बाँटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण तीन वृहत् उपगमनों द्वारा किया गया है। वे हैं - आनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। आनुभविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आँकड़ों पर आधारित होता है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।
कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति
वी. कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आँकड़ों पर आधारित यह एक आनुभविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया। सन् 1918 मे विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है।
कोपेन ने पाँच प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए जिनमें से चार तापमान पर और एक वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं को सारणी 11.1 में दिया गया है।
सारणी 11.1 कोपेन के अनुसार जलवायु समूह
| समूह | लक्षण |
|---|---|
| A. उष्णकटिबंधीय | सभी महीनों का औसत तापमान |
| B. शुष्क जलवायु | वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। |
| C. कोष्ण शीतोष्ण | सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान |
| D. शीतल हिम-वन जलवायु | वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान शून्य अंश तापमान से |
| E. शीत | सभी महीनों का औसत तापमान |
| H. उच्चभूमि | ऊँचाई के कारण शीत। |
बड़े अक्षर
सारणी 11.2 : कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार
| समूह | प्रकार | कूट अक्षर | लक्षण |
|---|---|---|---|
| A उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु |
उष्णकटिबंधीय आर्द्र उष्णकटिबंधीय मानसून उष्णकटिबंधीय आर्द्र एंव शुष्क |
Af Am Aw |
कोई शुष्क ऋतु नहीं। मानसून, लघु शुष्क ऋतु जाड़े की शुष्क ऋतु |
| B शुष्क जलवायु | उपोष्ण कटिबंधीय स्टैपी उपोष्ण कटिबंधीय मरूस्थल मध्य अक्षांशीय स्टैपी मध्य अक्षांशीय मरूस्थल |
BSh BWh BSk BWk |
निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क निम्न अक्षांशीय शुष्क मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क मध्य अक्षांशीय शुष्क |
अक्षांशीय जलवायु) |
आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय समुद्री पश्चिम तटीय |
Cfa Csa Cfb |
मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क अथवा शुष्क शुष्क गर्म ग्रीष्म कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म |
हिम-वन जलवायु |
आर्द्र महाद्वीपीय उप-उत्तर ध्रुवीय |
Df Dw |
कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण |
| टुंड्रा ध्रुवीय हिमटोपी |
सही अर्थो में कोई ग्रीष्म नहीं सदैव हिमाच्छादित हिम |
||
| उच्च भूमि | हिमाच्छादित उच्च भमियाँ |
मानसून जलवायु को
समूह
उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के
उष्णकटिबंधीय आर्द जलवायु (Af)
उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत् वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊँचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग
उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु (Am)
उष्णकटिबंधीय मानूसन जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूर्वी भाग तथा उत्तरी आस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायवी विवरण ‘भारत : भौतिक पर्यावरण’, एन.सी.आर.टी., 2006 में दिया गया है।
उष्णकटिबंधीय आर्र एवं शुष्क जलवायु (Aw)
उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु Af प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में
शुष्क जलवायु-B
शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है जो विषुवत् वृत्त से
उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी (BSh) एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरूस्थल (BWh) जलवायु
उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी (BSh) एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरूस्थल (BWh) जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र एंव शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरूस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है जो विरल घासभूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरूस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरूस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरूस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्मऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊँचा होता है। लीबिया के अल-अजीज़िया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान
कोष्ण शीतोष्ण (मध्य अक्षांशीय) जलवायु - C
कोष्ण शीतोष्ण (मध्य अक्षांशीय) जलवायु
आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु (Cwa)
आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह जलवायु
भूमध्यसागरीय जलवायु (Cs)
जैसा कि नाम से स्पष्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से
आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु (Cfa)
आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस प्रदेश में वायुराशियाँ प्रायः अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष वर्षा करती हैं। यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर-पूर्वी अर्जेटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 से.मी. के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ितझंझा और शीतऋतु में वाताग्री वर्षण सामान्य विशेषताएँ हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग
समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु (Cfb)
समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं - उत्तर-पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी केलिफोर्निया, दक्षिण चिली, दक्षिण-पूर्वी आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। गर्मी के महीनों में औसत तापमान
शीत हिम-वन जलवायु (D)
शीत हिम-वन जलवायु उत्तरी गोलार्द्ध में
आर्द जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु (Df)
आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टैपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फोले होते हैं। तुषार-मुक्त ऋतु छोटी होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियाँ अधिक उग्र होती हैं।
शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु (DW)
शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर-पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रतिचक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यार्वन की मानसून जैसी दशाएँ उत्पन्न करते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होती है। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं, जहाँ वर्षा के सात महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता हैं। वार्षिक वर्षा कम होती है जो 12 से 15 से.मी. के बीच होती है।
ध्रुवीय जलवायु (E)
ध्रुवीय जलवायु
टुण्ड्रा जलवायु (ET)
टुण्ड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकान तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। यह स्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। लघुवर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुण्ड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है।
हिमटोप जलवायु (EF)
हिमटोप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती जाती है जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिम शैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक में
उच्च भूमि जलवायु (F)
उच्च भूमि जलवायु भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊँचे पर्वतों में थोड़ी-थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों व उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊँचाई के साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं।
जलवायु परिवर्तन
जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम अब कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10 हज़ार वर्षों से अनुभव की जा रही है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर-हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू-आकृतिक लक्षण, विशेषतः ऊँचाईयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिह्न प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है।
भारत में भी आर्द एवं शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरस्थल की जलवायु आर्द एवं शीतल थी। ईसा से 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2,000 से 1,700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएँ तभी से गहन हुई हैं।
लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भू-वैज्ञानिक काल के कैंब्रियन, आर्डोविसियन तथा सिल्युरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियाँ रही हैं। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था।
अभिनव पूर्व काल में जलवायु
सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएँ घटित हुई हैं। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में, जिसे ‘धूल का कटोरा’ कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें से महत्त्वपूर्ण प्रसंग 10 वीं और 11 वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे। यूरोप ने सन् 1550 से सन् 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया है। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है।
जलवायु परिवर्तन के कारण
जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का सबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौर्यिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं, जो एक चक्रीय, ढंग से घटते-बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कंलकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण एवं शुष्क दशाएँ उत्पन्न होती हैं यद्यपि ये खोजें आँकड़ों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।
एक अन्य खगोलीय सिद्धांत ‘मिलैंकोविच दोलन’ है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यातप में परिवर्तन ला देते हैं। जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है।
ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ऐरोसोल फेंक देता है। ये ऐरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाले सौर्यिक विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था।
जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण मानवोद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इससे भूमंडलीय ऊष्मन हो सकता है।
भूमंडलीय ऊष्मन
ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीनहाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का पारेषण भी करता है किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम् दीर्घ तंरगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, ग्रीनहाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ‘ग्रीनहाउस प्रभाव’ (Green house effect) कहा जाता है।
ग्रीनहाउस शब्द का साम्यानुमान उस ग्रीनहाउस से लिया गया है। जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीनहाउस काँच का बना होता है। काँच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी। इस प्रकार काँच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तंरगों वाले विकिरण को काँच घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीनहाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाज़ों व खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। यह ग्रीनहाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है।
ग्रीनहाउस गैसें (GHGs)
वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीनहाउस गैसें कार्बन डाईऑक्साइड
इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उबरने में उतना अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीनहाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाईईक्साइड का है।
वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ है जिसकी उद्घोषणा सन् 1997 में की गई थी। सन् 2005 में प्रभावी हुई इस उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया है क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को

परिबद्ध किया कि वे सन् 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5 प्रतिशत की कमी लायें।
वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता। तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को कुप्रभावित कर सकते हैं। हिमटोपियों व हिमनदियों के पिघलने से ऊँचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को आप्लावित कर सकता है। इससे सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होंगी। विश्व समुदाय के लिए यह गहरी चिंता का एक और विषय है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संसार रहने के लायक रह सकेगा।
आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है, आइए देखें कि दर्ज तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है।
पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग
तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20 वीं शताब्दी में दिखाई दी। 20 वों शताब्दी में सबसे अधिक तापन दो अवधियों में हुआ है-1901-44 और 1977-99। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन
अभ्यास
1. बहुवैकल्पिक प्रश्न :
(i) कोपेन के
(क) सभी महीनों में उच्च वर्षा
(ख) सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक
(ग) सभी महीनों का औसत मासिक तापमान
(घ) सभी महीनों का औसत तापमान
(ii) जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है-
(क) अनुप्रयुक्त
(ख) व्यवस्थित
(ग) जननिक
(घ) आनुभविक
(iii) भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा-
(क) “Af”
(ख) “BSh”
(ग) “Cfb”
(घ) “Am”
(iv) निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है-
(क) 1990
(ख) 1998
(ग) 1885
(घ) 1950
(v) नीचे लिखे गए चार जलवायु के समूहों में से कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता हैं?
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए :
(i) जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन के द्वारा किन दो जलवायविक चरों का प्रयोग किया गया है ?
(ii) वर्गीकरण की जननिक प्रणाली आनुभविक प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है?
(iii) किस प्रकार की जलवायुओं में तापांतर बहुत कम होता है?
(iv) सौर कलंकों में वृद्धि होने पर किस प्रकार की जलवायविक दशाएँ प्रचलित होंगी?
3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
(i)
(ii)
(iii) ग्रीनहाउस गैसों से आप क्या समझते हैं? ग्रीनहाउस गैसों की एक सूची तैयार करें?
परियोजना कार्य
भूमंडलीय जलवायु परिवर्तनों से संबंधित ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित कीजिए।