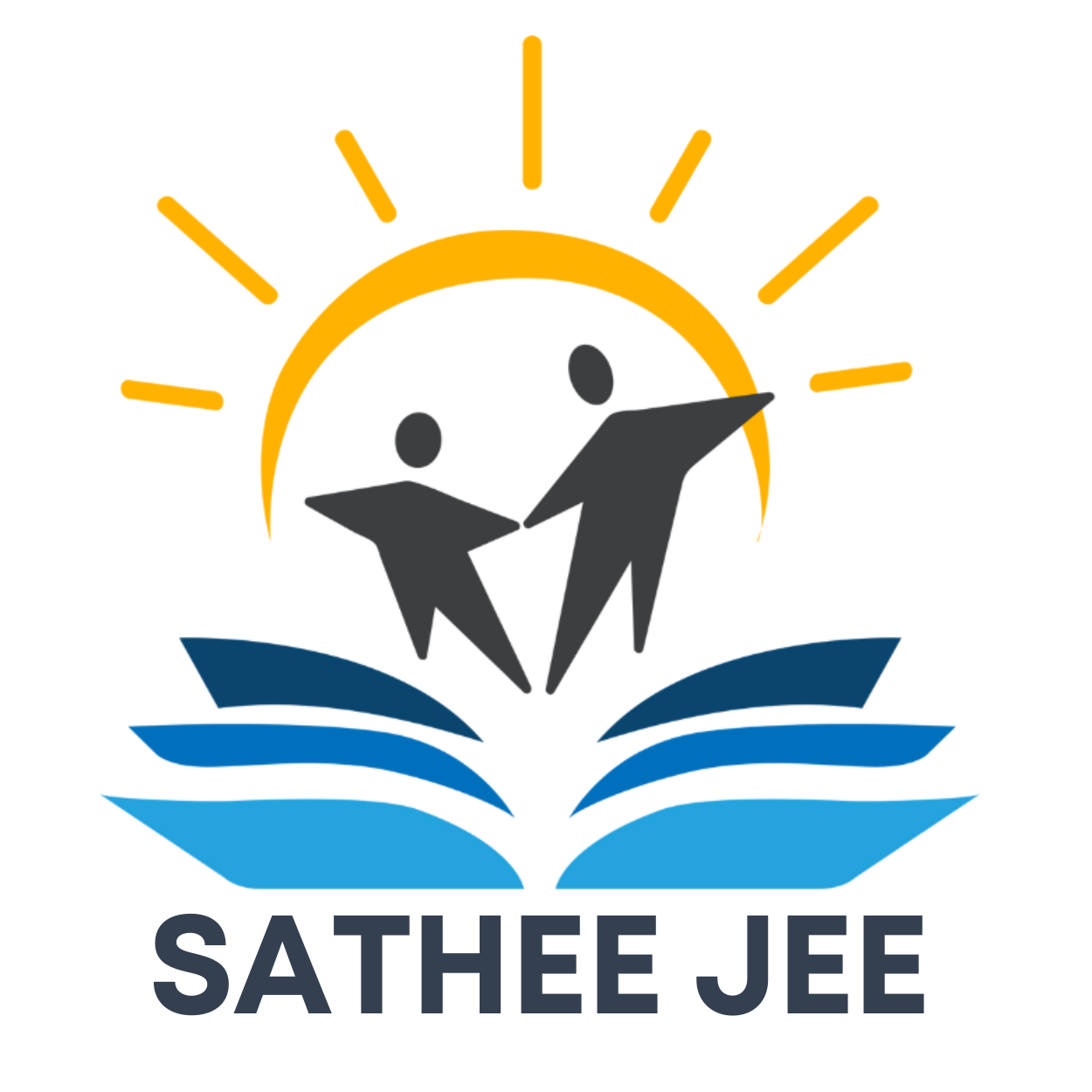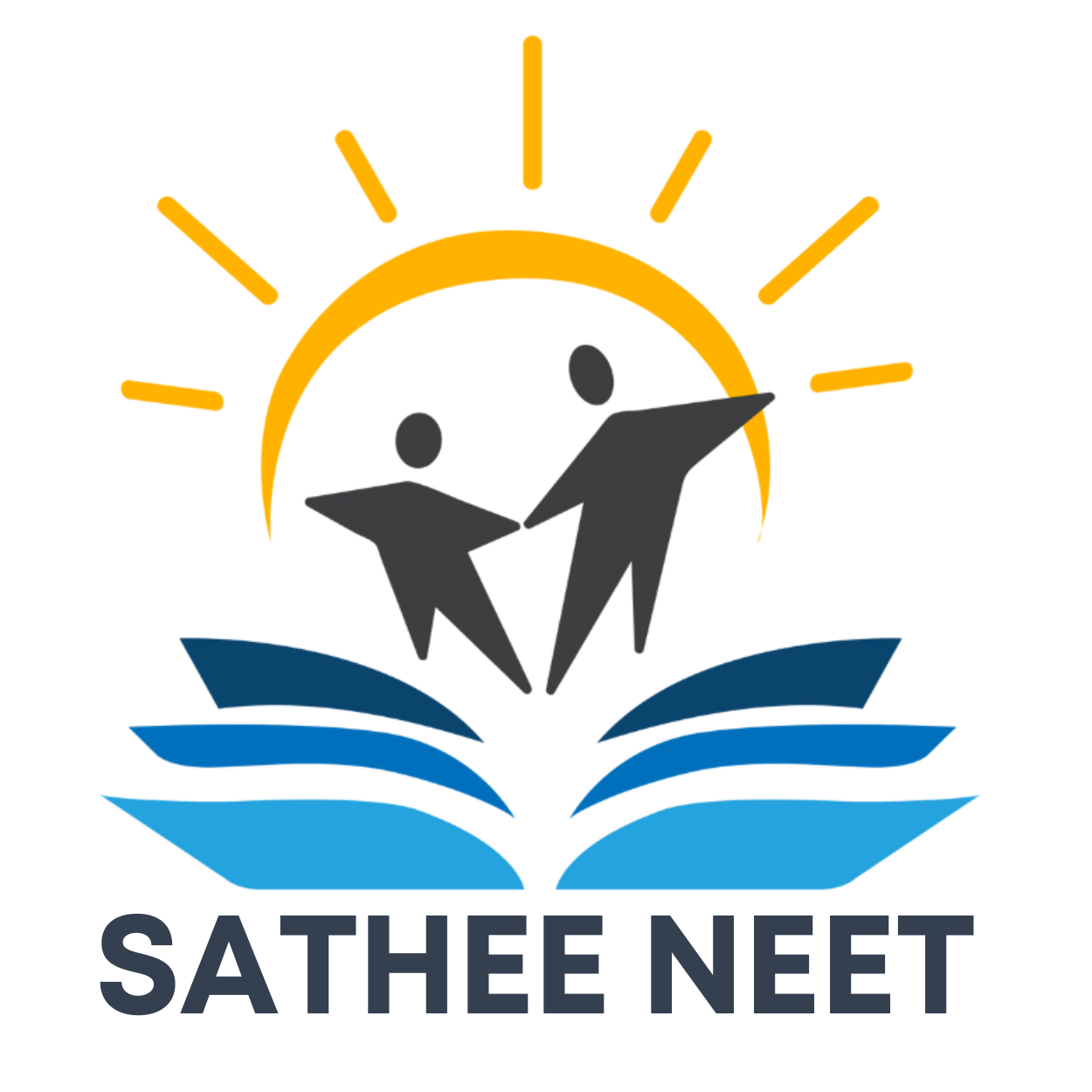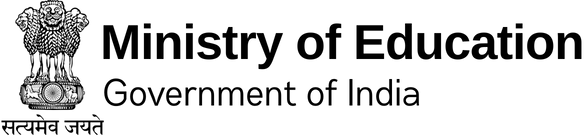अध्याय 07 भारतीय कांस्य प्रतिमाएँ
भारतीय मूर्तिकारों ने पकी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने और पत्थर तराशने-उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने और उससे मूर्तियाँ आदि बनाने के कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेर्डु यानी ‘लुप्त-मोम’ की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्रधातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्रधातु को कांस्य (कांसा) कहते हैं।
बौद्ध, हिंदू और जैन देवी-देवताओं की कांस्य प्रतिमाएँ भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएँ आनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थीं, लेकिन ये रूप एवं सौौर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट हैं। इसी के साथ-साथ, धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों, जैसे कि पकाने, खाने-पीने आदि के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जाता रहा है। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेते हैं।
संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्ककी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है जिसका काल 2500 ई.पू. माना जाता है। इस नारी प्रतिमा के अंग-प्रत्यंग और धड़ सारणी रूप में साधारण हैं। ऐसी ही अनेक छोटी-छोटी प्रतिमाओं का समूह दाइमाबाद (महाराष्ट्र) में हुई पुरातात्विक खुदाइयों में प्राप्त हुआ है। इन्रत्रतिमों का काल 1500 ई.पू बताया जाता है। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलाकार हैं जबकि उसके चालक (मानव) की आकृति को लंबा बनाया गया है और उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं, वे प्रबल तरीके से सांचे गये हैं।
बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएँ पाई गई हैं जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुशाण काल की बताई जाती हैं। तीर्थंकरों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था इसलिए इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुखुों के अंग-प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है जिसे उनके कंधों पर फैली हुई लंबी केश लटों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थंकर छोटे घुंघराले केश में दिखाए जाते हैं।

कालियामर्दन, चोल कालीन कांस्य, तमिलनाडु
गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं जिनका काल पाँचवीं शताब्दी के अंत से सातवीं शताब्दी के अंत तक का माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमाएँ प्रारंभ में लुप्त-मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थीं और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आँखें, मुकुट और वे वस्त्र बना दिए गए जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएँ बिहार में चौसा से भी मिली हैं जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभालकर रखा गया है। इसी प्रकार हरियाणा में हाँसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएँ मिली हैं।
वडोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पाई गई हैं, उनसे यह सिद्ध हो गया है कि छठी से नौवीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की हैं। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया जिसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या तीन से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा, कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएँ भी बनाई जाने लगीं। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थीं। चक्रेश्वरी, आदिनाथ की शासनदेवी और अंबिका, नेमिनाथ की शासनदेवी हैं।
बुद्ध की अनेक प्रतिमाएँ खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएँ गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी पाँचवीं, छठी और सातवीं शताब्दियों में उत्तर भारत विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थीं। इनमें संघति यानी भिक्षु के परिधान (वेश-भूषा) से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। यह परिधान

शिव परिवार, दसवीं शताब्दी ईसवी, बिहार

गणेश, सातवीं शताब्दी ईसवी, कश्मीर
एक ओर दाहिनी भुजा को ढके हुए है और उसका दूसरा सिरा बाईं भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है और उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुनटें पकड़ी हुई हैं। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला है, आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है जिससे वस्त्र की पतली किस्म का भी बोध होता है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। यह आकृति कुशाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई और समानुपातिक प्रतीत होती है। धानेसरखेड़ा (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तहें मथुरा शैली जैसी ही बनाई गई हैं यानी उसमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाई देते हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तहें नहीं दिखाई देतीं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुलतानगंज, बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है जोकि एक काफ़ी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रामाणिक उदाहरण है।

देवी, चोल कालीन कांस्य प्रतिमा, तमिलनाडु
फोफनार, महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएँ गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन हैं। उनमें ईसा की तीसरी शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफ़ी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है इसलिए वस्त शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर सतत प्रवाही रेखा दिखाई देती है। बुद्ध की
लुप्त-मोम प्रक्रिया (लॉस्ट-वैक्स प्रोसेस)
लॉस्ट-वैक्स यानी लुप्त-मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। इसके लिए पहले मोम को आग से पिघलाते हैं और फिर एक महीन कपड़े से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन में उसे निकालते हैं। यहाँ यह पुनः ठोस हो जाता है, फिर इसे पिचकी या फरनी से दबाते हैं जिससे मोम तार/धागे के आकार में आ जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा (आकृति) के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इसके एक खुले सिरे पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है। इसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से दस गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांशतः यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं, उस समय मिट्टी से ढके सांचे को आग पर रखे रहने देते हैं। जैसे ही अंदर की मोम पिघलती है, धातु नालिकाओं में नीचे की ओर बहती है और मोम की प्रतिमा का आकार ले लेती है। धातु ढलाई की समूची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। बाद में प्रतिमा को छेनी एवं रेती से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफी मेहनत का काम है और इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी-कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए पाँच धातुओं- सोना, चांदी, तांबा, पीतल और सीसे के मिश्रण का उपयोग होता है।


गणेश, सातवीं शताब्दी ईसवी, कश्मीर
आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्टतः वक्ररेखीय मोड़ बनाता है, जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है।
गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वे सुबाह्य थीं और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया।
हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी-देवताओं की कांस्य प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं। इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ आठवीं, नौवीं और दसवीं शताब्दियों की बनी पाई गईं हैं। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। इनमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएँ नाना रूपों में बनाई जाने लगीं। इन क्षेत्रों में चार सिरों वाले अर्थात् चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। यह व्यूह सिद्धांत पर आधारित है और ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी दो मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियाँ हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही हैं।

कांस्य प्रतिमा, हिमाचल प्रदेश
नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में, नौवीं शताब्दी के आस-पास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासन काल के दौरान, कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुर्किहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। इस काल की प्रतिमाओं में, चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियाँ अत्यन्त लोकप्रिय हो गईं। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है, उनके साथ एक टेढ़ी कमलनाल उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है।

नटराज, चोलकालीय, बारहवीं शताब्दी ईसवी
कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी-देवताओं की कांस्य प्रतिमाएँ बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुँच गया था। यद्यपि पल्लव काल में आठवीं तथा नौवीं शताब्दियों के दौरान कांस्य प्रतिमाएँ बहुतायत में बनाई जाने लगी थीं लेकिन दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासन काल में कुछ अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएँ बनाई गईं। कांस्य प्रतिमाएँ बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत, विशेष रूप से कुंभकोणम् में प्रचलित है। तथापि दसवीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी सेंवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
नटराज
इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य ‘अपस्मार’ को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंगत्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं जो ‘तिरोभाव’ यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का परदा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएँ बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ ‘अभय हस्त’ की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां ‘दोलहस्त’ मुद्रा में दाहिने हाथ की ‘अभयहस्त’ मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों और छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था और उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए। शिव को इस ब्रह्माण्ड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से ही जुड़ी है। तथापि, शिव अपने अनन्य भक्त के दृष्टिजगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। यह पौराणिक कथा चिंदबरम् से जुड़ी है इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है।

आठवीं शताब्दी की पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्द्धपर्यक आसन में (एक टांग को झुलाते हुए) बैठा हुआ दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है, जो यह दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं।
हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्त्ता, धर्ता और संहर्ता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतीकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप की भिन्न-भिन्न कांस्य प्रतिमाएँ बनाई जाती रहीं।

तमिलनाडु के तंजावुर (तंजौर) क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए। इस संदर्भ में नौवीं शताब्दी की कल्याणसुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें पाणिग्रहण यानी विवाह संस्कार को दो अलग-अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव (वर) अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती (वधू) के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्द्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी-बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियाँ भी मिलती हैं जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है।

सोलहवीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएँ बनाने का प्रयास भी किया। तिरुपति में, कांस्य की आदमकद प्रतिमाएँ बनाई गईं जिनमें कृष्ण देव राय को अपनी दो महारानियों तिर्मालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्त्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंग में भी दिखाई देती है जिससे शरीर रौबदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं।
अभ्यास
1. आपके विचार से क्या कांसे की ढलाई की तकनीक एक सतत प्रक्रिया है और इसका विकास आने वाले समय तक कैसे हुआ?
2. भारत में पत्थर और धातु से मूर्तियाँ बनाने की कला साथ-साथ चलती रही। आपकी राय में, इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच तकनीक, शैली और कार्य/उपयोग की दृष्टि से क्या-क्या समानताएँ और अंतर हैं?
3. चोल कालीन कांस्य प्रतिमाओं को सर्वाधिक परिष्कृत क्यों माना जाता है?
4. चोल काल के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से पायी गईं कांस्य प्रतिमाओं के मुद्रित चित्र खोजें।