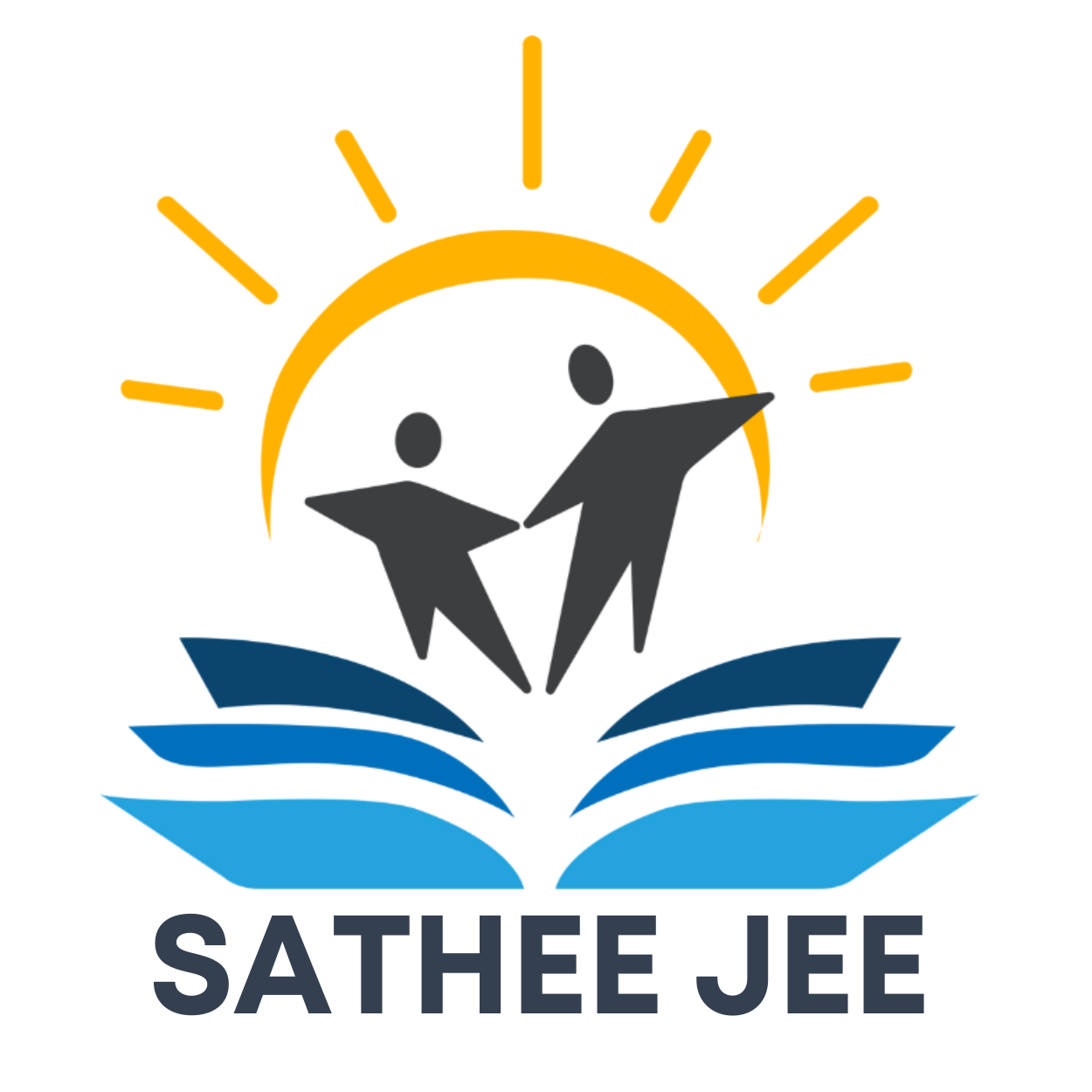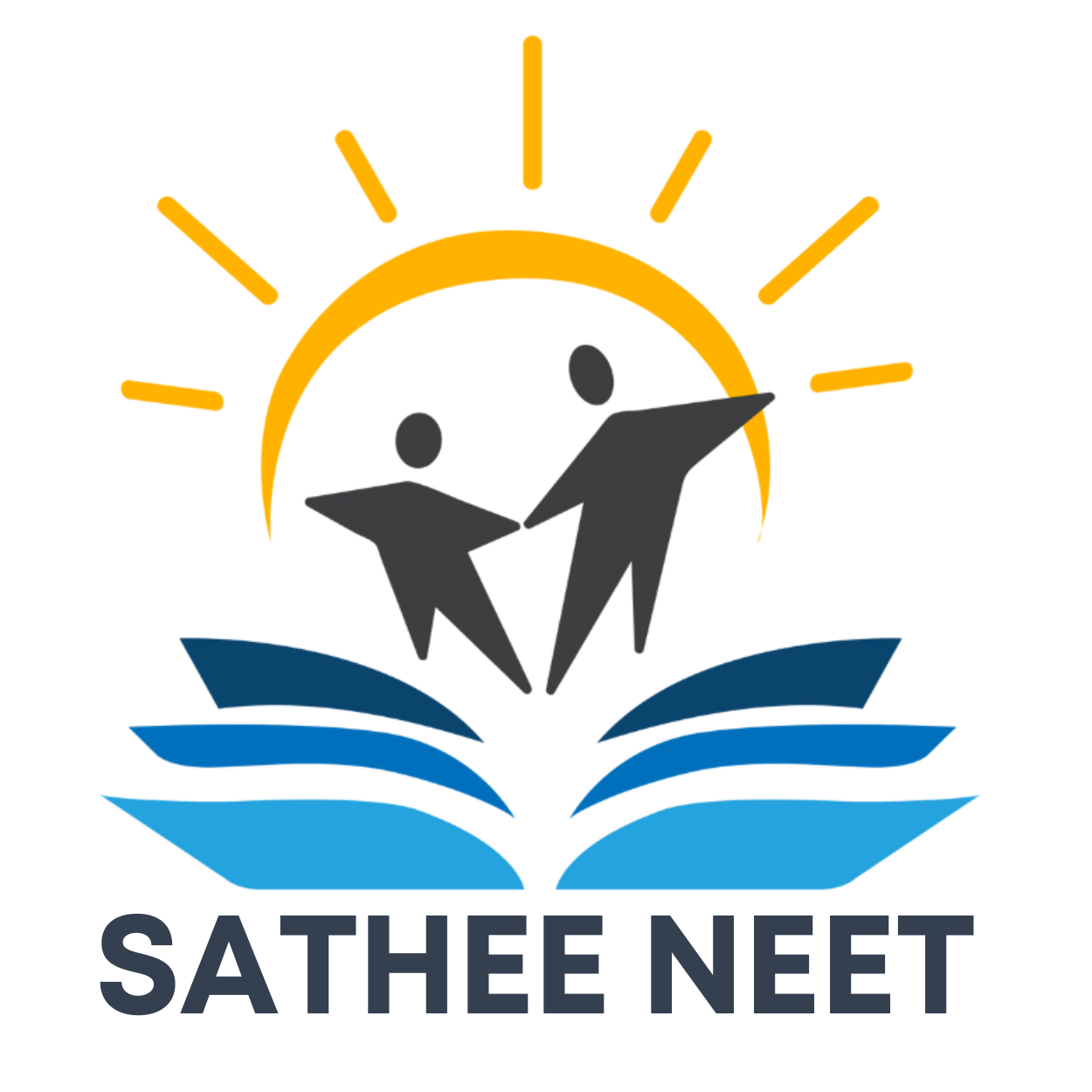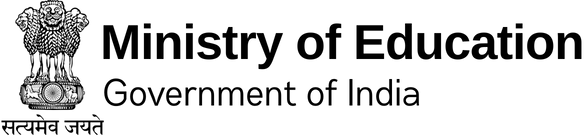अध्याय 05 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया
मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बग़ैर दुनिया की कल्पना हमारे कितनी मुश्किल है! हम अपने चारों तरफ़ जहाँ नज़र दौड़ाएँ, हमें कोई न कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी: किताबें, पत्र-पत्रिकाएँ, अख़बार, मशहूर तसवीरों की नक़लें, मेज़ पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएँ, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर, आदि-आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटंग देखते हैं, अख़बार पढ़ते हैं, और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायज़ा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं, यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है, और इस इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी?
इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे-कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे।

चित्र 1 - प्रिंट के आने से पहले पुस्तक-निर्माण, अख़लाक़-ए-नसीरी, 1595 , से।
भारत का एक शाही वर्कशॉप-भारत में छपाई आने से काफ़ी पहले। यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है, फिर तस्बीर बनाई जा रही है। पुस्तक-निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व्व था। छापेख़ाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, यह सोचने लायक है।
1 शुरुआती छपी किताबें
मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकररीबन 594 ई. से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख़्ती पर काग़ज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थीं। चूँकि पतले, छिद्रित काग़ज़ के दोनों तरफ़ छपाई संभव नहीं थी, इस पारंपरिक चीनी किताब ‘एकॉर्डियन’ शैली में, किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या ख़ुशनवीसी करनेवाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशख़त होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर-सुडौल अक्षरों में सही-सही कलात्मक लिखाई करते थे।
एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। सोलहवीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाज़ा, छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई।
सत्रहवीं सदी तक आते-आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने-फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ़ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे। व्यापारी अपने रोज़मर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शग़ल भी बन गया। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएँ, आत्मकथाएँ, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रूमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे।
पढ़ने की यह नयी संस्कृति एक नयी तकनीक के साथ आई। उन्नीसवीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियाँ स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट-संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे-धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली।
नए शब्द
खुशनवीसी : सुलेखन (Calligraphy)
1.1 जापान में मुद्रण
चीनी बौद्ध प्रचारक 768-770 ई. के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी, 868 ई. में छपी, पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ-साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तसवीरें अकसर कपड़ों, ताश के पत्तों और काग़ज़ के नोटों पर बनाई जाती थीं। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थीं।

चित्र 2(क) - डायमंड सूत्र का एक पन्ना।
अठारहवों सदी के अंत में, एदो (बाद में जिसे तोक्यो के नाम से जाना गया) के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है जिसमें हम चायघर के मजमों, कलाकारों, और तवायफ़ों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह-तरह की सामग्री - महिलाओं, संगीत के साज़ों, हिसाब-किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाज़ी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों - से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थीं।
13 वीं शताब्दी के मध्य में, त्रिपीटका कोरियाना, वुडब्लॉक्स (woodblocks) मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुडब्लॉक्स पर उकेरा गया था। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड राजस्टर में अंकित किया गया।

चित्र 2(ख) - त्रिपीटका कोरियाना
कितागावा उतामारो, 1753 ई. में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो (तैरती दुनिया के चित्र) नाम की एक नयी चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियाँ यूरोप और अमेरिका पहुँची और माने, मोने और वान गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। त्सुताया जुज़ाबूरो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का क़रार किया जाता फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद हुनरमंद वुडब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख़ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो ग़ायब हो जाता था, पर उसकी छपी नक़ल बच जाती थी।

चित्र 3 - कितागावा उतामारो की एक उकियो रचना।

चित्र 4 - सुबह का नज़ारा। रचयिता : शुन्मन कुबो, अठारहवीं सदी के अंत में।
2 यूरोप में मुद्रण का आना
सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। ग्यारहवों सदी में चीनी काग़ज़ भी उसी रास्ते वहाँ पहुँचा। कग़ज़ ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ई. में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्र चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास बुडब्लॉक (काठ की तख़ती) वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख़्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाक़ी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील माननेवाले कुलीन वर्गों और भिभ्षु-संघों के छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशक़ीमती वेलम (vellum) या चर्म-पत्र पर ही छपते थे। व्यापरी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें ख़रीदते थे।
किताबों की माँग बढ़ने के साथ-साथ यूरोप-भर के पुस्तक-विक्रेता विभिन्न देश्रों में निर्यात करने लगे। अलग-अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती माँग की आपूर्ति के हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ़ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक-विक्रेता भी अब उन्हें रोज़गार देने लगे। आम तौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे।
लेकिन किताबों की अबाध बढ़ती माँग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहों होने वाली थी। नक़ल उतारना बेहद ख़र्चीला, समयसाध्य और श्रमसाध्य काम था। पांडुलिपियाँ अकसर नाज़ुक होती थीं, उनके लाने-ले जाने, रख-रखाव में तमाम मुश्किलें थीं। इस उनका सर्कुलेशन-(चलन, गश्त) सीमित रहा तो किताबों की बढ़ती माँग के चलते वुड़्लॉक प्रिटिंग (तख़्ती की छपाई) उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। पंद्रहवीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख़ीी की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते, और छोटी-छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे।
ज़ाहिर है कि किताबें छापने के इससे भी तेज़ और सस्ती मुर्रण तकनीक की ज़रूरत थी। ऐसा छपाई की एक नयी तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता जो 1430 के दशक में स्ट्सैसर्ग के योहान गुटेन्बर्ग ने अंततः कर दिखाया।
नए शब्द
वेलम (Vellum) : चर्म-पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह।

चित्र 4(अ) - जिक्जी, कोरिया
कोरिया की जिक्जी (Jikji) मूवेबल मेटल टाइप (Movable metal type) के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से है। इसमें ज़ेन (Zen) बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएँ हैं। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इसे 14 वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया।
2.1 गुटेन्बर्ग और प्रिंटिंग प्रेस
गुटेन्बर्ग के पिता व्यापारी थे, और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल-बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरे की मशीनें (press) देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने
गतिविधि
कल्पना कीजिए आप मार्को पोलो हैं। चीन में आपने प्रिंट का कैसा संसार देखा, यह बताते हुए एक चिट्ठी लिखें।
में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना, और साँचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के किया गया। गुटेन्बर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी, वह थी बाइबिल। तक़रीबन 180 प्रतियाँ बनाने में उसे तीन साल लगे। जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था।
पर यह नयी तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई।
शुरू-शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग-रूप और साज-सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थीं। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिये पर फूल-पत्तियों की डिज़ाइन बनाई जाती थी, और चित्र अकसर पेंट किए जाते थे। अमीरों के बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिये की जगह बेल-बूटों के ख़ाली छोड़ दी जाती थी। हर ख़रीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिज़ाइन और पेंटर खुद तय करके उसे सँवार सकता था।
करोब सौ सालों के दरम्यान (1450-1550) यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापेख़ाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापेख़ाने खुलवाया करते थे। छपाईख़ाने की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोत्तरी हुई। पंद्रहवों सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाज़ार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आईं। यह संख्या सोलहवों सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई।
नए शब्द
प्लाटेन : लेटर्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है, जिसे काग़ज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा।

चित्र 5 - योहान गुटेन्बर्ग का चित्र ( 1584 )।

चित्र 6 - गुटेन्बर्ग प्रिंटिंग प्रेस।
एक्कू से लगा लंबा हैंडल देखों। इसकी मदद से स्कू घुमाकर प्लाटेन को गीले काग़ज़ पर दबा दिया जाता था। गुटेन्वर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के टाइप बनाए, और जुगत लगाई कि इन्हें इधर-उधर ‘मूव’ कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सकों लिहाज़ा, इसे ‘मूूवेबल टाइप प्रिंटंग मशीन’ के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई को बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के तख़्ती पर ख़ास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब कितावों का इस तरह छापना निहायत तेज़ हो गया। गुटेन्नर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने (एक साइड) छाप सकता था।

चित्र 7 - यूरोप की पहली छपी किताब, गुटेन्बर्ग की बाइबिल से कुछ पन्ने।
गुटेन्बर्ग ने कुल 180 प्रतियाँ छापी थीं, पर उनमें से 50 ही बच पाई हैं। आइए गुटेन्बर्ग की बाइबिल के इन पन्नों को ध्यान से देखें। ये केवल नयी तकनीक की देन नहीं थे। इन्हें गुटेन्बर्ग प्रेस को धातुई टाइप से छापा ज़रूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी की थी। कोई दो प्रतियाँ एक-जैसी नहीं थीं। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहाँ पहली नज़र में वे एक-जैसे लगे भी, गौर से तुलना करने पर फ़र्क़ पता चल जाएगा। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इस विशिष्टता को पसंद किया। जो उनके पास था, वह अनोखा था, वे यह दावा कर सकते थे, क्योंकि किसी और के पास उसकी हू-ब-हू नक़ल नहीं थी।
आप इबारत में देखेंगे कि कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं। इसके दो फायदे थे। पन्ना रंगीन हो जाता था, और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज़्यादा दर्शनी और महत्त्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेन्बर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के जगह छोड़ दी।

चित्र 8 - एक मुद्रक की वर्कशॉप, सोलहवीं सदी।
इस तसवीर से पता चलता है कि सोलहवों सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखायी देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाएँ छोर पर अगले हिस्से में कम्पोज़ीटर काम कर रहे हैं। बाएँ सिरे पर गैलीज़ा तैयार किए जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। पृष्ठभूमि में प्रिंटर्स प्रेस के पेंच कस रहे हैं और उन्हीं के पास पूऱरीडर काम में जुटे हैं। बिलकुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये दो-दो पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है।
नए शब्द
कम्पोज़ीटर : छपाई के इबारत कम्पोज़ करने वाला व्यक्ति।
गैली : धातुई फ्रेम, जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी।
3 मुद्रण क्रांति और उसका असर
मुद्रण क्रांति क्या थी? छापेख़ाने का आविष्कार महज़ तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक-उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की ज़िदगी बदल दी: इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोकचेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नज़रिया।
3.1 नया पाठक वर्ग
छापेख़ाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था, वह कम हो गया, और बड़ी तादाद में प्रतियाँ छापना आसान हो गया। बाज़ार किताबों से पट गई, पाठक वर्ग भी बृहत्तर होता गया।
किताबों तक पहुँच आसान होने से पढ़ने की एक नयी संस्कृति विकसित हुई। अब तक आमलोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा-गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे, और किस्से भी उनके बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन-देन ही होता था। लोगबाग समूह में ही दास्तान सुनते, या कोई आयोजन देखते, आए थे। आप आठवें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में, या ख़ामोशी से, पढ़ने के आदी नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल मँहगी थीं, बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबक़ों तक पहुँच सकती थीं। अगर पहले की जनता श्रोता थी, तो कह सकते हैं कि अब पाठक-जनता अस्तित्व में आ गई थी।
लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ़ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में बीसवों सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रकाशकों के सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएँ? इसके उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुँच का ध्यान रखना थाः जो नहीं पढ़ पाते थे, वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ़ तो उठाते ही थे। इस मुद्रकों ने लोकगीत और लोककथाएँ छापनी शुरू कर दीं, और ऐसी किताबें आमतौर पर तसवीरों से ख़ूब सजी-धजी यानी सचित्र होती थीं। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराबघरों में गाया-सुनाया जाता था।
इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाख़िल हुई, और छपी सामग्री मौखिक अंदाज़ में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुँधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक-दूसरे में घुल-मिल गए।
गतिविधि
मान लीजिए आप नव-मुद्रित सस्ती किताबों का इश्तेहार देना चाहते हैं। अपनी दुकान के बाहर लगाने के एक पोस्टर बनाएँ।
नए शब्द
गाथा-गीत (Ballad) : लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान, जिसे गाया या सुनाया जाता है।
शराबघर (Tavern) : वह जगह जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात-विचार के आते थे।
3.2 धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर
छापेख़ाने से विचारों के व्यापक प्रचार-प्रसार और बहस-मुबाहिसे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के ज़रिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के मना सकते थे, या कोई कार्रवाई करने के प्रेरित कर सकते थे। ज़ाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्त्व था।
हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था, जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आमलोगों के ज़ेहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ‘मूल्यवान’ साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव-मुद्रित और नव-प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए, देखें कि जीवन के एक क्षेत्र-धर्म-में इसका क्या असर हुआ।
धर्म-सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी पिच्चानवे स्थापनाएँ लिखीं। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाज़े पर टाँगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्मसुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ़्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियाँ बिक गईं, और तीन महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहेदिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, “मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा।” कई इतिहासकारों का यह खयाल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म-सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली।

चित्र 9 - जे.वी. श्ले, लाम्प्रीमेरी ( छापाख़ाना) 1739
यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। देखें कि छापाख़ाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है। इस देवी के आजू-बाजू मिनवा (विद्या की देवी) और मर्करी (दूत-देव, विवेक का भी प्रतीक) हैं। तसवीर के आगे के हिस्से में अलग-अलग देशों के छः अग्रणो मुद्रकों की छवियाँ औरतें हैं। बीच में बाईई ओर घरे के अंदर गुटेन्वर्ग की तसवीर है।
3.3 मुद्रण और प्रतिरोध
छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग-अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। सोलहवीं सदी की इटली के एक
नए शब्द
प्रोटेस्टेंट धर्मसुधार : सोलहवीं सदी यूरोप में रोमन कैथलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएँ निकलीं।
किसान मेनोकियो ने अपने इलाकेे में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए, और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म-विरोधी विचारों को दबाने के रोमन चर्च ने जब इन्क्वीज़ीशन (धर्म-द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था) शुरू किया तो मेनोकियो को दो बार पकड़ा गया और आख़िरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाईं, और 1558 ई. से प्रतिबंधित किताबों की सूरी रखने लगे।

चित्र 10 - द मैकॅबर डान्स (वीभत्स नाच)।
इस सोलहवीं सदी की तसवीर में, छपाई का ख़ौफ़ किस नाटकीयता से पेश किया जा रहा था, यह देखा जा सकता है। इस बेहद दिलचस्प वुडकट (तख़ती-छाप) तसवीर में मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया है। मुद्रक के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया है। मुद्रक और उसके मज़दूर कंकालों के नियंत्रण में हैं, और उनसे मनचाही चीज़ों छपवाते हैं।
चर्चा करें
छपाई से विरोधी विचारों के प्रसार को किस तरह बल मिलता था? संक्षेप में लिखें।
नए शब्द
इन्क्वीज़ीशन (धर्म-अदालत) : विधर्मियों की शिनाख़्त करने और सज़ा देने वाली रोमन कैथलिक संस्था।
धर्म-विरोधी : इनसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्म-द्रोह के प्रति सख़्त था, उसे लगता था कि लोगों की आस्था, उनके विश्वास पर सिर्फ़ उसका अधिकार है, और उसकी बात ही अंतिम है।
किताब का डर
लातिन के विद्वान और कैथलिक धर्मसुधारक इरैस्मस - जिसने कैथलिक धर्म की ज़्यादतियों की आलोचना की, पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी- प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडेजेज़ (1508) में लिखा-
‘किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन-सा कोना है, जहाँ ये नहीं पहुँच जातीं? हो सकता है कि जहाँ-तहाँ, एकाध जानने लायक चीज़ें भी बताएँ, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्धता के हानिकारक ही है। बेकार ढेर हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक ही है, इनसे बचना चाहिए… (मुद्रक) दुनिया को सिर्फ़ तुच्छ (जैसे कि मेरी लिखी) चीज़ों से ही नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीख़ेज़, धर्मविरोधी, अज्ञानी, और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं, और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता।’
4 पढ़ने का जुनून
पूरे सत्रहवीं और अठारहवीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग-अलग संप्रदाय के चर्चों ने गाँवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों-कारीगरों को शिक्षित करने लगे। अठारहवों सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80 प्रतिशत तक हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थीं, इस मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे।
नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए क़िस्म-क़िस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गाँव-गाँव जाकर छोटी-छोटी किताबें बेचने वाले फेरीवालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक-गाथाएँ और लोकगीतों की हुआ करती थीं। लेकिन जल्द ही मनोरंजन-प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुँचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैपबुक्स या एकपैसिया किताबें बेचनेवालों को चैपमेन कहा जाता था। इन किताबों को ग़रीब तबक़े भी ख़रीदकर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोधीक ब्ल्यू का चलन था, जो सस्ते काग़ज़ पर छपी और नीली जिल्द में बँधी छोटी किताबें हुआ करती थीं। इसके अलावा चार-पाँच पन्ने की प्रेम-कहानियाँ थीं, और अतीत की थोड़ी गाथाएँ थीं, जिन्हें ‘इतिहास’ कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग-अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार-प्रकार थे।
अठारहवों सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की ख़बर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अख़बार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की ख़बरें होती थीं।
उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुँच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंध संकलित किए गए, और नक्शों के साथ-साथ वैज्ञानिक ख़ाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइज़ैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके विज्ञान-बोध में पगा एक बड़ा पाठक-वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वॉल्तेयर और ज़्याँ ज़ाक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगीं। ज़ाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे।
नए शब्द
संप्रदाय : किसी धर्म का एक उप-समूह।
पंचांग : चाँद, सूरज की गति, ज्वार-भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देता वार्षिक प्रकाशन।
चैपबुक (गुटका) : पॉकेट बुक के आकार की किताबों के इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। इन्हें आमतौर पर फेरीवाले बेचते थे। ये सोलहवीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए।
1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉकिंग्टन ने अपनी डायरी में यह लिखा-
पिछले बीस सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। गरीब किस्म के किसान, या गाँव के लोग जो पहले अपनी शामें डायन-जोगिन, और भूत-प्रेत की कहानियाँ सुनते हुए बिताते थे…. अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रूमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़े की रातों को छोटी करने लगे हैं। अगर जॉन शहर जा रहा है, तो उसे सख़्न हिदायत की जाएगी कि वह पेरेग्रिन पिकल्स ऐंडवंचर लेकर आए… और अगर डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता है कि वह द हिस्ट्री ऑफ़ जोज़ेफ़ ऐण्डू़ज़ लेकर ही वापस लौटे।
4.1 दुनिया के ज़ालिमों, अब हिलोगे तुम!
अठारहवों सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के ज़रिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से
समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएँगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। अठारहवीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिएँ मर्सिए ने घोषणा की, “छापाख़ाना प्रगति का सबसे ताक़तवर औज़ार है, इससे बन रही जनमत की आँधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा।” मर्सिए के उपन्यासों में नायक अकसर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं, और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेख़ाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिए ने कहा, “हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे काँपने का वक्त आ गया है! आभासी लेखक की क़लम के ज़ोर के आगे तुम हिल उठोगे!”
मर्सिए ने अपनी एक किताब में छपे शब्द की ताक़त को यूँ बयान किया-
‘अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताज़ा पानी मिलने पर गटगट पीने लगता है… बड़े एहतियात से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था। और वाक और अर्थ के प्रवाह में मैं पन्ता-दर-पन्ना बहता चला जाता था, अनायास और अनजान। ख़ामोशी के साये में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तेल ख़त्म होने से मेरी लालटटन की लौ पीली पड़ने लगती थी, पर मैं था कि पढ़ता जाता। मैं बत्ती उठाने की ज़हमत भी नहीं लेता था, कि मेरे आनंद में व्यवधान न पड़े। और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर मे घुसते थे! मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी!’
रॉवर्ट डार्नटन की किताब द फ़ौरबिडेन बेस्ट-सेलर्स ऑफ़ प्री-रेवॉलूशननी फ्रांस, 1995 से उद्धत।
4.2 मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति
कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ़ांसीसी क्रांति के अनुकूल परिस्थितियाँ रचीं। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं?
मूलतः तीन तरह के तर्क देखने लायक हैं:
पहला : छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति-रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया, और माँग की कि हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वॉल्तेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक-वर्ग था, और उनके पाठक एक नए, आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नज़रिये से दुनिया को देखने लगे थे।
दूसरा : छपाई ने वाद-विवाद-संवाद की नयी संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और क़ायदों पर आम जनता के बीच बहस-मुबाहिसे हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताक़त से परिचित यह नयी ‘पब्लिक’ धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी ‘सार्वजनिक दुनिया’ से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ।
तीसरा : 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मज़ाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों (व्यंग्य चित्रों) में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फँसी है जबकि राजशाही भोग-विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के ख़िलाफ़ भड़काया।
हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की। लेकिन याद रहे कि लोग-बाग़ हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ़ वे अगर रूसो और वॉल्तेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ़
नए शब्द
निरंकुशवाद : राजकाज की ऐसी व्यवस्था, जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, और उस पर न क़ानूनी पाबंदी लगी हो, न ही संवैधानिक।
चर्च और राज्य का प्रोपगैंडा या प्रचार भी। वे हर पढ़ी या देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे, तो कुछ को नकारते भी थे। फ़िर चीज़ों की अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह, मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएँ ज़रूर खोलीं।
गतिविधि
मान लीजिए कि आप क्रॉंति-पूर्व फ़्रांस में एक कार्ट्निस्ट या व्यंग्य-चित्रकार हैं। किसी परचे के लिए एक कार्टून बनाएँ।

चित्र 11 - फ़्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आम जन, अठारहवीं सदी के अंत का एक कार्टून।
इस व्यंग-चित्र में दिखाया गाया है कि जनसाधारण-किसान, कारीगर और मज़दूर - किस तरह मुश्किल हालात में थे, जबकि ज़िदगी के मज़े लेने वाला कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है। इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिल-दिमाग़ पर ख़ास असर हुआ।
चर्चा करें
कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ़्रांसीसी क्रांति के ज़मीन तैयार की?
5 उन्नीसवीं सदी
उन्नीसवीं सदी में यूरोप ने जन-साक्षरता की दिशा में लंबी-लंबी छलाँगे लगाईं, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठकवर्ग तैयार हुआ।
5.1 बच्चे, महिलाएँ और मज़दूर
उन्नीसवीं सदी के आख़िर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे, पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन महत्त्वपूर्ण हो गया। फ़्रांस में 1857 में सिर्फ़ बाल-पुस्तकें छापने के एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नयी, दोनों तरह की परी-कथाओं और लोक-कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक-कथाएँ जमा कीं। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ, फ़िर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के अनुपयुक्त सामग्री, या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थीं, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोककथाओं को नया रूप मिला-छपने से वे दर्ज तो हुईं, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गईं।
महिलाएँ पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई। पेनी मैगज़ींस या एकपैसिया पत्रिकाएँ (देखें, चित्र 12) खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थीं, वैसे ही जैसे कि सही चाल-चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएँ। उन्नीसवीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएँ उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएँ अग्रणी थीं: जेन ऑस्टिन, ब्रॉण्ट बहनें, जॉर्ज इलियट, आदि। उनके लेखन से नयी नारी की परिभाषा उभरी : जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझ-बूझ थी, और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छाशक्ति थी।

चित्र 12 - पेनी या एकपैसिया मैग्ज़ीन का आमुख।
पेनी मैग्ज़ीन का प्रकाशन इंग्लैड में 1832-1850 के बीच सोसायटी फ़ॉर द डिफ्यूज़न ऑफ़ यूज़फ़ुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मज़दूर वर्ग के थी।
सत्रहवों सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। उन्नीसवों सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद-कॉलर मज़दूरों, दस्तकारों और निम्नवर्गीय लोगों को शिक्षित करने के किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मज़दूरों को अपने सुधार और आत्म-अभिव्यक्ति के थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे, और आत्मकथाएँ लिखीं।
5.2 नए तकनीकी परिष्कार
अठारहवीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी उन्नीसवीं सदी के दौरान छापेख़ाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। उन्नीसवों सदी के
मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम.हो. ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफ़सेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ छह रंग की छपाई मुमकिन थी। बीसवीं सदी के शुरू से ही, बिजली से चलनेवाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेज़ी से होने लगे। एक-दो और चीज़ें हुईं। काग़ज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर-रील और रंगों के फ़ोटो-विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी-छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग-रूप ही बदल गया।
यॉर्कशायर के एक मेकैनिक थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अख़बार ख़रीदकर शाम के व़्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के पैसे नहीं होते थे। ग़रीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुर्किल हालात में पढ़ने के जद्दोजहद करते थे: बीसवों सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की की मेरा बचपन और मेंरे विश्वविद्यालय इन संघोषों की कहानियाँ हैं।
मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए। उन्नीसवों सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा जिससे उपन्यास लिखने की एक ख़ास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती शृंखला-शिलिंग श्रृंखला-के तहत छापी गईं। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी बीसवों सदी की तकनीकी नवइयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ। लिहाज़ा, पाठकों की जेब का ख़याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या अजिल्द संस्करण छापे।
गतिविधि
चित्र 13 को देखें। ऐसे विज्ञापनों का लोगों के मन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या आपको लगता है कि छपी हुई चीज़ को देखकर हर व्यक्ति की एक-जैसी प्रतिक्रिया होती है?

चित्र 13 - इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन, अल्फ्रेड कॉन्कानेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ, 1874
छपी हुई सूचनाएँ और इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लैटफ़ॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे।
6 भारत का मुद्रण संसार
आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई, और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे।
6.1 मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ
भारत में संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्त-लिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने काग़ज़ पर नक़ल कर बनाई जाती थीं। कभी-कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तसवीरें भी बनाई जाती थीं। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख़याल से तख़्तियों की जिल्द में या सिलकर बाँध दिया जाता था। उन्नीसवीं सदी के अंत तक, छपाई के आने के बाद भी, पांडुलिपियाँ छापी जाती रहीं।
लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुुक होती थीं, काफ़ी मँहगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे, लिपियों के अलग-अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इस उनका व्यापक

चित्र 14 - जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने, अठारहवीं सदी।
यह एकॉर्डियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है।

चित्र 15 - हाफ़िज़ के दीवान के कुछ पन्ने, 1824
चौदहवों सदी के शायर हाफ़िज़ की संपूर्ण शायरो दीवान में संकलित है। पेज पर खुशनवीसी, नक्काशी और डिज़ाइन देखें। लेटर्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियाँ अमीरों के बनाई जाती रहीं।
दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालाँकि पूर्व-औपनिवेशिक बंगल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे, और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई-सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे।

चित्र 16 - ॠवेद के कुछ पन्ने।
प्रिंट के आगमन के काफ़ी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ प्रकाशित की जाती रहीं। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में अठारहवों सदी में बनाई गई।
6.2 छपाई भारत आई
प्रिंटिंग प्रेस पहले-पहल सोलहवीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगालीधर्म-प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएँ छापीं। 1674 ई. तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थीं। कैथलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी, और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म-प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापों, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थीं।
अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था, यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्रहवीं सदी के अंत तक छापेख़ाने का आयात शुरू कर दिया था।
जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गज़ट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूँ परिभाषित किया, ‘हर किसी के खुली एक व्यवसायिक पत्रिका, जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलानेवाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद, निजी अंग्रेज़ी उद्यम थी, और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे। लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज़ अधिकारियों से जुड़ी गपबाज़ी भी छापता था। इससे नाराज़ होकर गवर्नर जेनरल वॉरेन हेंस्टिंग्स ने हिक्की पर मुक़दमा कर दिया, और ऐसे सरकारी आश्रय-प्राप्त अख़बारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सकें। अठाहरवीं सदी के अंत तक कई-सारी पत्र-पत्रिकाएँ छपने लगीं। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अख़बार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राममोहन राय के क़रीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गज़ट।
विलियम बोल्ट्स नामक व्यक्ति को, 1768 ई. में भी, इस तरह की सूचना कलक्ता के एक सार्वजनिक इमारत में टाँगने की ज़रूरत महसूस हुई-
‘जनसाधारण के : मि. बोल्ट्स पल्लिक को यह बताने के इस तरीक़े का सहारा ले रहे हैं कि चूँकि शहर में छापेख़ाने की घोर कमी से नुक़सान होता है….इस वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे,, जो छपाई में माहिर हो।’
पर जल्द ही बोल्ट्स महोदय इंग्लैंड चले गए और यह वादा हवा में लटका रहा।
7 धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें
जैसा कि आप जानते हैं, उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाज़ार गर्म था। अलग-अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए, धर्म की अपनी-अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति-रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज-सुधारकों के तर्कों के ख़लाफ़ खड़े थे। ये सारे वाद-विवाद प्रिंट में, सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अख़बारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार-प्रसार किया बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन-समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत ज़ाहिर कर सकता था। इस तरह के मत-मंतातर से नए विचार उभरे।
यह वह समय था जब समाज और धर्म-सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा-दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारीवर्ग और मूर्ति-पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज़ बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे-जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अख़बारों के ज़ारिए तरह-तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने के ख़याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राममोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अख़बारजाम-ए-जहाँ नामा और शम्सुल अख़बार - भी 1882 में प्रकाशित हुए।
उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दें, या मुस्लिम क़ानून न बदल डालें। इससे निबटने के उन्होंने सस्ते लिथोग्राफ़ी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्मग्रंथों के फ़ारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अख़बार तथा गुटके निकाले। सन् 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हज़ारों फ़तवे जारी किए। पूरी उन्नीसवीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए, धर्म को लेकर सबकी अपनी-अपनी व्याख्याएँ थीं, हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था।
हिंदुओं के बीच भी छपाई से ख़ास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की सोलहवीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफ़ी संस्करणों से उत्तर भारत का बाज़ार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपों। मुद्रित और लाने-ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी,
नए शब्द
उलमा : इस्लामी क़ानून और शरिया के विद्वान।
फ़तवा : अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में, इस्लामी क़ानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती, के द्वारा की जानेवाली वैधानिक घोषणा।
किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हे अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल-बोल कर भी पढ़ा जा सकता था।
मतलब यह कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन-समुदाय तक पहुँच रही थीं, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच, और उनके अंदर, बहस-मुबाहिसे, और वाद-विवाद-संवाद की नयी स्थिति बन गई थी।
लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ़ मत-मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को अंदर से, और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया।
अख़बार क्यों?
‘पूना के कृष्णाजी त्रिम्बक राणाडे मराठी का एक अख़बार निकालना चाहते हैं, जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी ख़बरों को जगह मिल सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक्-विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर, और दक्कन पर ख़ासतौर पर जानकारियाँ होंगी… ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदेन है, जो ज्ञान के प्रसार और जनकल्याण के इच्छुक हैं।’
बॉम्बे टेलीग्राफ़ एंड कोरियर, 6 जनवरी 1849
‘देसी अख़बारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है, जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ़ कॉमन्स में विपक्ष की होती है। यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कर, लोगों के हित साधने में अक्षम हिस्सों को निकालें और सुधार करें, तथा उनको तेज़ी से लागू करने का काम करें।
इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के ख़ास मुदों पर नाना तरह की सूचनाएँ जमा करें और क्या संभव और वांछित सुधार हैं, वह बताएँ, इन कार्यों का काफ़ी असर होगा।’
नेटिव ओपिनियन, 3 अप्रैल, 1870
8 प्रकाशन के नए रूप
छापेख़ाने से नए तरह के लेखन के भूख जागी। जैसे-जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी ही इसने अपनी एक ख़ास भारतीय शक्ल और शैली अख़्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया।
दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएँ, जैसे-गीत, कहानियाँ, सामाजिक-राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग-अलग तेवरों में इन्होंने इनसानी ज़िदगी और अंतरंग भावनाओं, और उन सामाजिक-राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था।
उन्नीसवों सदी के अंत तक, एक नयी तरह की दृश्य-संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापेख़ानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नक़लें या प्रतियाँ अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थीं। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के तसवीरें बनाईं। काठ की तख़्ती पर चित्र उकररने वाले ग़रीब दस्तकारों ने लैटरप्रेस छापेखा़नों के करीब अपनी दुकानें लगाईं, और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाज़ार में सुलभ सस्ती तसवीरें और कैलेंडर ख़रीदकर ग़रीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तसवीरों ने आहिस्ता-आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार-लोक को गढ़ना शुरू किया।
1870 के दशक तक पत्र-पत्रिकाओं में सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मज़ाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्यचित्रों में राष्ट्रवादियों का मज़ाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे।

चित्र 17 - राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा रवि वर्मा का चित्र।
राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए, जो उनके अपने, रावि वर्मा प्रेस, में छपती थीं।
8.1 महिलाएँ और मुद्रण
महिलाओं की ज़िदगी और उनकी भावनाएँ बड़ी साफ़गोई और गहनता से लिखी जाने लगीं। इस मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, और उन्नीसवीं सदी के मध्य में जब बड़े-छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी-शिक्षा की ज़रूरत को बार-बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था, और ज़रूरत के मुताबिक़ पाठ्य-सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के किया जा सकता था।
लेकिन सारे परिवार उदार-दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी-लिखी कन्याएँ विधवा हो जाती हैं, और इसी तरह दक्रियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफ़साने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएँगी। कभी-कभार बाग़ी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दक़ियानूसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है, जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ़ पढ़ना सीखा, बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ़ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाज़ा उसने वह ज़बान पढ़ने की ज़िद की, जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में, उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में, कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रशसुन्दरी देबी ने रसोई में छिप-छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीबन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म-कहानी थी।
चूँकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इस महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आपबीती के प्रति कुतूहल तो था ही।
कैलाशबाशिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया-कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर-भर के काम का बोझ उठाती हैं, और जिनकी सेवा वे करती हैं, वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बँधी औरत के पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, ‘बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है… मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई हैं..।

चित्र 18 - इंडियन शारिवारी का आवरण पृष्ठ।
इंडियन शारिवारी उन्नीसवों सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग्य और विद्रूप (कैरिकेचर) विधा के कई पत्रों में से एक था।
गौरर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज़ की छवि ठीक बीचोबीच है। सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना वह देसी लोगों को, वे क्या करें, क्या नहीं, इसकी हिदायत दे रहा है। उसके दोनों ओर बैठे देसीजन गुलामों की नत मुद्रा में हैं। भारतीयों को व्यंग्य-चित्रों के अंग्रेज़ी पत्र, द पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो, ‘यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्करण निकालो।’
उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट-संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी-शिक्षण को समर्पित हुआ। बीसवों सदी के आरंभ में महिलाओं के मुद्रित, और कभी-कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएँ
जानी-मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रोकैया शेखावत हुसैन ने 1926 में, बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए, धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के पुरुषों की निंदा की-
‘नारी-शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएँ उद्दंड हो जाएँगी…
‘छिः! ये खुद को मुसलमान बताते हैं, और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक़ देने के बुनियादी उसूल के ख़िलाफ़ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़-लिखकर नहीं भटकते, तो महिलाएँ क्यों बिगड़ जाएँगी, भला?’
लोकप्रिय हो गईं। इनमें औरतों की तालीम, विधवा-जीवन, विधवा-विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फ़ैशन के नुस्खे बताने के साथ-साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के ज़रिए मनोरंजन परोसा।
पंजाब में भी बीसवीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियाँ बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट-सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसायटी (खालसा पुस्तिका सभा) ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएँ छापीं। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया।
बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाक़ा-बटाला-लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज़ समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। उन्नीसवीं सदी के अंत तक, ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख़्ती और लिथोग्राफ़ी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तसवीरें उकेरी जा रही थीं। फेरीवाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर-घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फ़ुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई।

चित्र 19 - घोर कलि (प्रलयकाल), उन्नीसवीं सदी के अंत का रंगीन काष्ठचित्र।
पारिवारिक संबंधों के नष्ट-भ्रष्ट होने की कल्पना। पत्नी, जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है। और वह खुद अपनी माँ को ज़ंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है।
8.2 प्रिंट और ग़रीब जनता
उन्नीसवों सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक-चौराहों पर बेची जा रही थीं, जिसके चलते ग़रीब लोग भी बाज़ार से उन्हें ख़रीदने की

चित्र 20 - एक भारतीय दंपति, सफ़ेद-स्याह काष्ठचित्र
इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट-पुलट गई है। मर्द वीणा बजा रहा है, और औरत हुक्का खींच रही है। उन्नीसवीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न-भिन्न हो जाने की आशंका तेज़ हो गई।

चित्र 21 - एक यूरोपीय दंपति, उन्नीसवीं सदी का काष्ठचित्र
इस तसवीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे हैं, और मेमसाहब वायलिन बजा रही हैं।
स्थिति में आ गए थे। बीसवों सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुँच निस्संदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अकसर शहरों या क़्बों में होते थे, या यदा-कदा संपन्न गाँवों में भी। स्थानीय अमीरों के पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी।
उन्नीसवीं सदी के अंत से जाति-भेद के बारे में तरह-तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। ‘निम्न-जातीय’ आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी (1871) में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। बीसवीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ई.वी. रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर ज़ोरदार क़लम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्मग्रंभों की आलोचना करते हुए, नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाएँ और गुटके छापे।
कारखानों में मज़दूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था, और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल-मज़दूर काशीबाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल-मज़दूर का लेखन सच्ची कविताएँ नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगलौर के सूती-मिल-मज़दूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख़याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बंबई के मिल-मज़दूरों से मिली थी। समाज-सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मज़दूरों के बीच नशाख़ोरी कम हो, साक्षरता आए, और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे।
गतिविधि
चित्र 19,20 और 21 को गौर से देखें।
समाज में हो रहे बदलाव को लेकर चित्रकार क्या कह रहा है?
वे कौन से बदलाव हो रहे थे, कि चित्रकार ने ऐसी प्रतिक्रिया दी?
क्या आप चिर्रकार के मत से सहमत हैं?

चित्र 22 - लक्ष्मीनाथ बेज़बरुवा (1868-1938)
वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आइर साधु (दादी को कहानियाँ) उनकी उल्लेखनीय किताबों में से है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ‘ओ मोर अपुनर देश’ (ओ मेरी प्यारी भूमि) भी लिखा।
9 प्रिंट और प्रतिबंध
ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती क़दम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दें।
कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ क़ानून पास किए, और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अख़बारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेज़ी और देसी भाषाओं के अख़बार-संपादकों द्वारा गुहार और अर्ज़ी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जेनरल बेंटिंक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के राज़ी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफ़सर टॉमस मेकॉले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए क़ानून बनाए।
1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेज़ों ने ‘देसी’ प्रेस का मुँह बंद करने की माँग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज़ होने लगी। आइरिश प्रेस कानून के तर्त़ पर 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक़ मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अख़बारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बाग़ी करार दिया जाता था तो अख़बार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अख़बार को ज़ब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थीं।
लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अख़बार देश के हर कोने में बढ़ते-फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताक़तों की हौसला-अफज़ाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में कालापानी भेजा गया तो बालगंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कै़द कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत-भर में व्यापक विरोध हुए।
कभी-कभी वफ़ादार अख़बारों के संपादक खोजना सरकार के मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अख़बार स्टेट्समैन के संपादक-पद के सैंडर्स को बुलया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ़्रेंड ऑफ़ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इस इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के मजबूर होना पड़ेगा।
मुद्रित शब्द की ताक़त का अंदाज़ा अकसर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र-पत्रिकाओं पर नज़र रखता था।
पहले विश्वयुद्ध के दौरान, भारतीय रक्षा नियम के तहत, 22 अख़बारों को ज़मानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अख़बारों के ख़िलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख़्त बना दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत पर, भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया, ताकि युद्ध-संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थीं। अगस्त 1942 में तक़रीबन 90 अख़बारों का दमन किया गया।
गांधी ने 1922 में कहा-
‘वाणी की स्वतंत्रता…. प्रेस की आज़ादी…. सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन तीन ताक़तवर औज़ारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज, ख़िलाफत… की लड़ाई, सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है।’
संक्षेप में लिखें
1. निम्नलिखित के कारण दें-
(क) वुडब्लॉक प्रिंट या तख़्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई।
(ख) मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की।
(ग) रोमन कैथलिक चर्च ने सोलहवीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी।
(घ) महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस, और सामूहिकता के लड़ाई है।
2. छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएँ-
(क) गुटेन्बर्ग प्रेस
(ख) छपी किताब को लेकर इरैस्मस के विचार
(ग) वर्नाक्युलर या देसी प्रेस एक्ट
3. उन्नीसवीं सदी में भारत में मुद्रण-संस्कृति के प्रसार का इनके क्या मतलब था-
(क) महिलाएँ
(ख) ग़रीब जनता
(ग) सुधारक
चर्चा करें
1. अठारहवीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत, और ज्ञानोदय होगा?
2. कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक-एक उदाहरण लेकर समझाएँ।
3. उन्नीसवीं सदी में भारत में ग़रीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ?
4. मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की?
परियोजना कार्य
पिछले सौ सालों में दुद्रण संस्कृति में हुए अन्य बदलावों का पता लगाएँ। फिर इनके बारे में यह बताते हुए लिखें कि ये क्यों हुए और इनके कौन से नतीजे हुए?