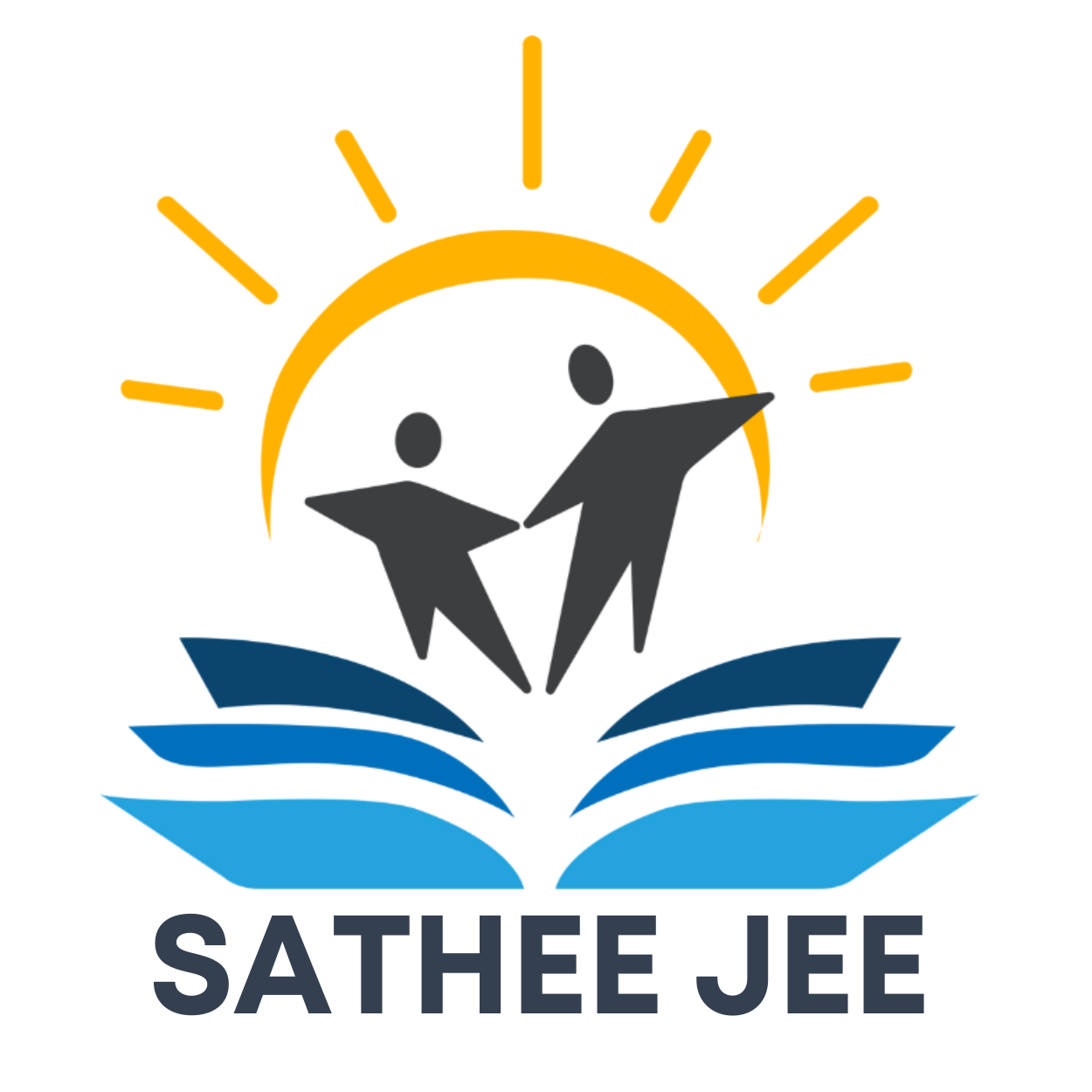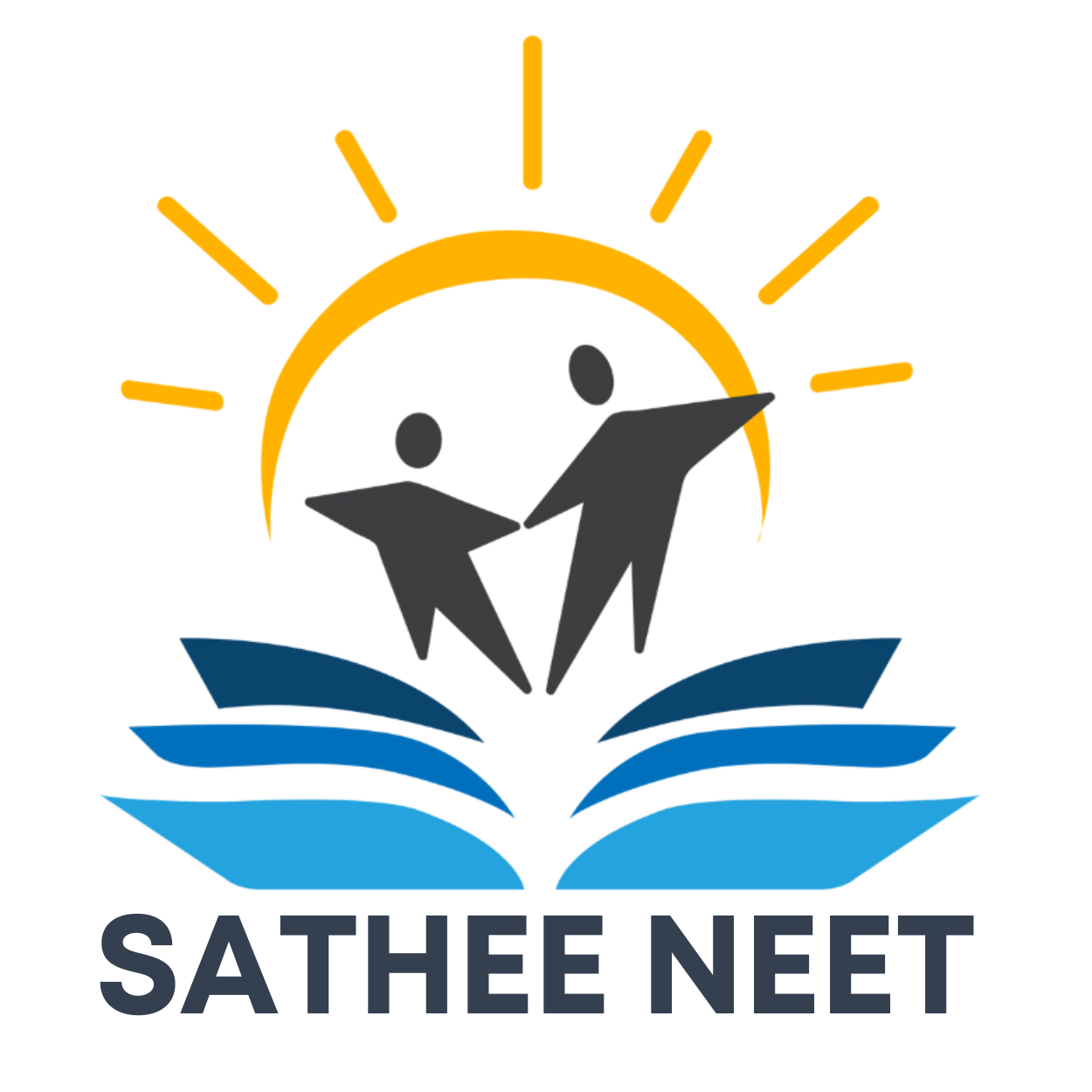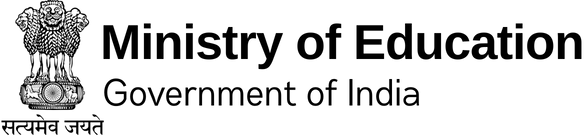अध्याय 04 औद्योगीकरण का युग

चित्र 1 - डॉन ऑफ़ द सेंचुरी, ई.टी. पॉल म्यूज़िक कंपनी, न्यूयॉर्क (अमेरिका) एवं इंग्लैंड, 1900
ई.टी. पॉल म्यूज़िक कंपनी ने सन् 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर दी गई तसवीर में ‘नयी सदी के उदय’ (डॉन ऑफ़ द सेंचुरी) (चित्र 1) का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तसवीर के मध्य में एक देवी जैसी तसवीर है। यह देवी हाथ में नयी शताब्दी की ध्वजा प्रगति का फ़रिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पाँव पंखों वाले पहिये पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिह्न तैर रहे हैं : रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारख़ाना।
मशीन और तकनीक का यह महिमामंडन एक अन्य तसवीर में और भी ज़्यादा साफ़ दिखाई देता है। यह तसवीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर सौ साल से भी पहले छपी थी (चित्र 2)। इस तसवीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य (Orient) इलाके का अलादीन है जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़ कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है।
नए शब्द
प्राच्य : भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नज़ारिये में प्राच्य इलाके पूर्व-आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे।
नीचे एक आधुनिक मेकैनिक है जो अपने आधुनिक औज़ारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज़, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है; मेकैनिक पश्चिम और आधुनिकता का।
ये तसवीरें आधुनिक विश्व की विजयगाथा कहती हैं। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्पपोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगीकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है।
अब ये छवियाँ और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज़ औद्योगीकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहों लगता कि रेलवे और फ़ैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का घ्योतक होता है? ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई हैं? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगीकरण के तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनोंदिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगीकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के हमें औद्योगीकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा।
इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र-व्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगीकरण का अध्ययन करेंगे जहाँ औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था।
गतिविधि
दो ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ आधुनिक विकास से प्रगति की बजाय समस्याएँ पैदा हुई हैं। आप चाहें तो पर्यावरण, आणविक हथियारों व बीमारियों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं।

चित्र 2 - दो जादूगर, इनलैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित, 26 जनवरी 1901
1 औद्योगिक क्रांति से पहले
औद्योगीकरण को अकसर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फ़ैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। और जब हम औद्योगिक मज़दूरों की बात करते हैं, तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों से ही होता है। औद्योगीकरण के इतिहास अकसर प्रारंभिक फ़ैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं।
पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल, इंग्लैंड और यूरोप में फ़ैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंर्राष्ट्रीय बाज़ार के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फ़क्ट्टियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगीकरण के इस चरण को आदि-औद्योगीकरण (protoindustrialisation) का नाम देते हैं।
नए शब्द
आदि : किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत।
सत्बवीं और अठारहवीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों की तरफ़ रुख़ करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की माँग बढ़ने लगी थी। इस माँग को पूरा करने के केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स का़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पदकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्बरूप, नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे। इस वे गाँवों की तरफ़ जाने लगे।
गाँवों में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्युप्तक में देखा है, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोज़ी-रोटी के साझा ज़मीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियाँ, सब्जियाँ, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान (कॉटेज़र) और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत दूँढ़ रहे थे। बहुतों के पास छोटे-मोटे खेत तो थे लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसी, जब सौदागर वहाँ आए और उन्होंने माल पैदा करने के पेशगी रकुम दी तो किसान फ़ौरन तैया हो गए। सौदागरों के काम करते हुए वे गाँव में ही रहते हुए अपने छोटे-छोटे खेतों को भी सँभाल सकते थे।

चित्र 3 - अठारहवीं सदी में कताई।
आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है।
इस आदि-औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौक़ा भी मिल गया।
इस व्यवस्था से शहरों और गाँवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे लेकिन उनके काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेप्लर्स (Staplers) से ऊन खरीदते थे और उसे सूत कातने वालों के पास पहुँचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फ़ुलर्ज़ (Fullers), और रंगसाज़ों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच देते थे। इसी लंदन को तो फ़िनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा था।
यह आदि-औद्योगिक व्यवस्था व्यवसायिक आदान-प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मज़दूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मज़दूर काम करते थे।
नए शब्द
स्टेपलर : ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को ‘स्टेपल’ करता है या छाँटता है।
फुलर : ऐसा व्यक्ति जो ‘फुल’ करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है।
कार्डिंग : वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के तैयार किया जाता है।
1.1 कारख़ानों का उदय
इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारख़ाने खुले लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इज़ाफ़ा अठारहवीं सदी के आखिर में ही हुआ।
कपास (कॉटन) नए युग का पहला प्रतीक थी। उन्नीसवीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुँच गया। यह इज़ाफ़ा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे।
अठारहवीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया (कार्डिंग, ऐंठना व कताई, और लपेटने) के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मज़दूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने-अपने घर पर ही करते थे। लेकिन अब मँहगी नयी मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रियाएँ एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थीं। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मज़दूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गाँवों में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे।

चित्र 4 - लंकाशायर की एक कॉटन मिल, सी.ई. टर्नर द्वारा बनाया चित्र, दि इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, 1925
कलाकार ने कहा : ‘अगर उस नम मौसम की नज़र से देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के सबसे आदर्श स्थान बनता है तो शाम के धुँधलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है।’
उन्नीसवों सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल, और नयी प्रौद्योगिकी की ताक़त इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आँखें चौंधिया जाती थीं। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आँखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप्स में अभी भी उत्पादन चालू है।
गतिविधि
जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप की बजाय औद्योगीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास हुए हैं वे इस बात से तय होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ़ कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसे आपके माता-पिता या शिक्षक आदि वयस्क लोग महत्त्वपूर्ण नहीं मानते लेकिन आपको वह महत्त्वपूर्ण लगती है।
1.2 औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार
औद्योगीकरण की प्रक्रिया कितनी तेज़ थी? क्या औद्योगीकरण का मतलब केवल फ़ैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है?

चित्र 5 - औद्योगिक मैनचेस्टर, एम. जैक्सन का चित्र, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, 1857
धुआँ छोड़ती चिमनियाँ औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थीं।
पहला : सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते-फूलते उद्योग थे। तेज़ी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पौंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी।
दूसरा : नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। उन्नीसवीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों की संख्या कुल मज़दूरों में 20
गतिविधि
चित्र 4 और 5 को देखें। क्या आपको दोनों तसवीरों में औद्योगीकरण को दर्शाने के ढंग में कोई फ़र्क़ दिखाई देता है? अपना दृष्टिकोण संक्षेप में व्यक्त करें।
प्रतिशत से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था।
तीसरा : यद्यपि ‘परंपरागत’ उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, काँच के काम, चर्मशोधन, फ़र्नीचर और औज़ारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे ग़ैर-मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्क़ी हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे-छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी।

चित्र 6 - इंग्लैंड में एक रेलवे कारख़ाने में फ़िटिंग शॉप, दि इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़्र, 1849
इस फ़िटिंग शॉॅप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुरानों की मरम्मत की जाती थी।
चौथा : प्रौद्योगिकीय बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेज़ी से नहीं फैले। नयी तकनीक मँहगगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूँक-फूँक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अकसर खराब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थीं जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था।
इस बात को समझने के आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वॉट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बूल्टन ने किया। पर, सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ़ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 ऊन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मज़दूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे।
अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि उन्नीसवों सदी के मध्य का औसत मज़दूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बाल्कि परंपरागत कारीगर और मज़ूदूर ही होता था।

चित्र 7 - 1830 की एक कताई फ़ैक्ट्री।
आप देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकृत से चलने वाले विशालकाय पहिये एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे।
2 हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति
विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं। इसी, उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मज़दूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो।
बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की माँग मौसमी आधार पर घटती-बढ़ती रहती थी। गैसघरों और शराबखानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज्यादा मज़दूरूं की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मज़दूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ़-सफ़ाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन

चित्र 8 - काम की तलाश में निकले लोग, दि इलस्ट्रेटे लंदन न्यूज़, 1879
कुछ लोग छोटी-मोटी चीज़ें बेचते और अस्थायी काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे।
घटता-बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मज़दूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे।
विल थोर्न मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मज़दूरों में से एक थे। उन्होंने ईंटें ढोईं और अन्य छोटे-मोटे काम किए। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे -
‘मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों को पढ़कर और मज़बूत हो जाती थी… वह ओल्ड केंट रोड गैस वर्क्स में काम करता है… आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया… नवंबर 1881 में। दो दोस्तों के साथ मैं सफ़र पर निकल पड़ा। हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहाँ पहुँचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोज़गार मिल जाएगा।. .. जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के खाने और रात को ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिन हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे… तीसरे दिन हमारे पैसे खत्म हो गए… दो रातें हमने बाहर ही सोते हुए गुजारीं… एक बार भूसे के ढेर तले और एक बार खेत में बने एक शेड में… लंदन पहुँचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूँढ़ने का प्रयास किया।… लेकिन नाकामयाब रहे। पैसा तो जा ही चुका था। इस अब हमारे पास देर रात तक यहाँ-वहाँ भटकते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूँढ़ते थे। हमने एक पुरानी इमारत ढूँढ़ी और एक रात उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था। दोपहर बाद हम ओल्ड केंट गैस वर्क्स पहुँचे। वहाँ हमने काम के अर्ज़ी दे दी। यह देखकर मेरे अचरज की सीमा न रही कि हम जिसे ढ़ँढ़ रहे थे वह वहीं काम कर रहा था। उसने फ़ोरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया गया।’
एच.जे. ड्योस एवं माइकल वुल्फ (सं.) द विक्टोरियन सिटी : इमेजेज़ एंड रियेलिटीज़, 1973 में रेफ़ेल सेमुअल के लेख ‘ कमर्स एंड गोअर्स में उद्धत।
गतिविधि
कल्पना कीजिए कि आप सौदगर हैं और एक ऐसे सेल्समैन को चिट्री लिख रहे हैं जो आपको नयी मशीन खरीदने के राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। अपने पत्र में बताइए कि मशरी के बारे में आपने क्या सुना है और आप नयी प्रौद्योंगिकी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते।
बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। लेकिन बाज़ार में अकसर बारीक डिज़ाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी माँग रहती थी। उदाहरण के , ब्रिटेन में उन्नीसवों सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थीं। इन्हें बनाने के यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इनसानी निपुणता की ज़रूरत थी।
विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग-कुलीन और पूँजीपति वर्गहाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फ़िनिश अच्छी होती थी। उनको एक-एक करके बनाया जाता था और उनका डिज़ाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था।
जिन देशों में मज़दूरों की कमी होती है वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि कम से कम मज़दूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकें। उन्नीसवीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी। लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी।

चित्र 9 - लोहे की फैक्ट्री में मज़दूर, उत्तर-पूर्व इंग्लैंड, विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग, 1861
उन्नीसवों सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मज़दूरों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे। उन्हें राष्ट्र के कठिनाइयाँ और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था।
2.1 मज़दूरों की ज़िदगी
बाज़ार में श्रम की बहुतायत से मज़दूरों की ज़िदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गाँवों में पहुँची सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों

चित्र 10 - बेघर और भूखे, सेमुअल ल्यूक फिल्देस की पेंटिंग, 1874
इस पोंटंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक कामघर (Work house) में रात भर ठहरने के टिकट के अर्ज़ी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल ‘बेसहरा, सड़कों पर रहने वाले, आवाराओं और यहाँ-बहाँ भटकते’ लोगों के गररीब कुतून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्कहाउसों में रहना ज़िल्लत को बात थी। हरक की डाक्टरी जाँच करके ये पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहों है, उनका शररर पूरो तरह साफ़ है या नहों और उनके कपड़े मैले तो नहीं हैं। उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था।
की तरफ़ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी-दोस्ती, कुनबे-कुटुंब के ज़रिए जान-पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारख़ाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोज़गार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ़्तों इंतज़ार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन-बसेरों में राते काटते थे। कुछ बेरोज़गार शहर में बने निजी रैनबसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन क़ानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे।
बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच-बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीज़न गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाँवों में चले जाते थे जहाँ इस समय काम निकलने लगता था। लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा-मोटा काम ढूँढ़ने की कोशिश करते थे जो उन्नीसवीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था।

चित्र 11 - स्पिनिंग जेनी, टी.ई. निकल्सन द्वारा बनाया गया रेखाचित्र, 1835
ध्यान से देखिए कि एक ही पहिये से कितनी सारी तकलियाँ घूमने लगती थीं।
उन्नीसवों सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया। लेकिन इससे मज़दूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आँकड़ों से अलग-अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फ़र्क़ और साल-दर-साल होने वाले उतार-चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर, जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ों तो मज़दूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ों नहीं खरीद सकते थे। मज़दूरों की आमदनी भी सिर्फ़ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोज़गार की अवधि भी बहुत महत्त्वपूर्ण थी : मज़दूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने
एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मज़दूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के बुलाया गया था :
‘कोयला मज़दूरों और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण… क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था… शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। ऊन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते थे क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की माँग घटने वाली थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। आदमियों को समझाना आसान था इस कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के तैयार कर लिया गया।
जे.एल. हैमंड एवं बी. हैमंड, द स्किल्ड लेबरर 1760-1832, मैक्सिन बर्ग, दि एज ऑफ़ मैन्युफैक्चर्स में उद्धत।
चर्चा करें
चित्र 3,7 और 11 को देखिए। इसके बाद स्रोत-ख को दोबारा पढ़िए। अब बताइए कि बहुत सारे मज़दूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे।

चित्र 12 - मध्य लंदन में निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन, इलस्ट्रेटेड टाइम्स, 1868
1850 के दशक से पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। इसका मतलब था कि सुरंगे बनाने, बल्लियों की पाड़ लगाने, ईंट और लोहे का काम करने के बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत थी। रोज़गार चाहने वाले एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल तक जाते रहते थे।
कितने दिन काम किया है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10 प्रतिशत शहरी आबादो निहायत ग़रीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोज़गारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75 प्रतिशत तक पहुँच जाती थी।
बेरोजगारी की आशंका के कारण मज़दूर नयी प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन कातने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगीं। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा।
1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ीं। लोगों के नए रोज़गार पैदा हुए। सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गईं, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई।
नए शब्द
स्पिनिंग जेनी : जेम्स हर्रीज़ द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज़ कर दी और मज़दूरों की माँग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मज़दूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे।
3 उपनिवेशों में औद्योगीकरण
आइए अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगीकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ-साथ ग़ैर-मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा।
3.1 भारतीय कपड़े का युग
मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाज़ार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मीनियन और फ़ारसी सौदागर पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फ़ारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता-फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के ज़रिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपटनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण-पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था।
निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुँचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिये बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुँचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज़ मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल-भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे।
गतिविधि
एशिया के मानचित्र पर भारत से मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले कपड़ा व्यापार के समुद्री और सड़क संपर्कों को चिहिनत कीजिए।
1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था।
यूरोपीय कंपनियों की ताक़त बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल कों और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इज़ारेदारी अधिकार प्राप्त कर । इससे सूरत व हुगली, दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस क़र्ज़े से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे-धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। सत्रहवों सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपये था। 1740 के दशक तक यह गिर कर केवल 30 लाख रुपये रह गया था।

चित्र 13 - सूरत में एक इंग्लिश फ़ैक्ट्री, सत्रहवीं सदी का चित्र।
सूरत व हुगली कमज़ोर पड़ रहे थे और बंबई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्त्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताक़त का संकेत था। नए बंदरगाहों के ज़ारिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के ज़ारिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
इन बदलावों ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की ज़िदगी को किस तरह प्रभावित किया?
3.2 बुनकरों का क्या हुआ?
1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी माँग थी। इस कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी।

चित्र 14 - काम पर लगा एक बुनकर, गुजरात।
1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले इस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के फ़ांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ-साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल-भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊँची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफ़सरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊँचे दामों का बार-बार जिक्र किया है।
लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रबंधन और नियंत्रण की एक नयी व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया।
पहला : कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जाँचने के वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था।
दूसरा : कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके उन्हें पेशगी रक़म दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के क़र्ज़ा दे दिया जाता था। जो क़र्ज़ा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे।
जैसे-जैसे क़र्ज़े मिलते गए और महीन कपड़े की माँग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे-छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूततें पूरी कर लेते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे व औरतें, सभी कुछ न कुछ काम करते थे।
लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गाँवों में बुनकरों और गुमाश्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगीं। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अकसर बुनकर गाँवों में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का खयाल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद
करते थे। नए गुमाश्ता बाहर के लोग थे। उनका गाँवों से पुराना सामाजिक संबंध नहों था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सज़ा देते थे। सज़ा के तौर पर बुनकरों को अकसर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी पर वे क़र्ज़ों की वजह से कंपनी से बँधे हुए थे।
कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गाँव छोड़ कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गाँव में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफ़सरों का विरोध करते हुए गाँव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर क़र्ज़ा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मज़दूरी करने लगे।
उन्नीसवीं सदी आते-आते कपास बुनकरों के सामने नयी समस्याएँ पैदा हो गईई।
पटना के आयुक्त ने लिखा -
‘ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया है। जबकि बिहार में बहुत कम उत्पादन होता है। यह मैनचेस्टर में बनी सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं का परिणाम है जिनसे स्थानीय निर्माता प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।’
जे. कृष्णमूर्ति, ‘डोइंडस्ट्रियलाइजे़शन ऑफ़ गैंगटिक बिहार ड्यूरिंग द नाइनटींथ संचुरी’, दि इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिब्यू, 1985 , में उद्धत।
3.3 भारत में मैनचेस्टर का आना
1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफ़सर हेनरी पतूलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की माँग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि उन्नीसवों सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी जो लंबे समय तक जारी रही। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33 प्रतिशत था। 1850-51 में यह मात्र 3 प्रतिशत रह गया था।
ऐसा क्यों हुआ? उसके निहितार्थ क्या थे?
जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। दूसरी तरफ़ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में भी बेचे। उन्नीसवों सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। अठारहवीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते-आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31 प्रतिशत हो चुका था। 1870 तक यह आँकड़ा 50 प्रतिशत से ऊपर चला गया।
इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक-साथ दो समस्याएँ थीं। उनका निर्यात बाज़ार ढह रहा था और स्थानीय बाज़ार सिकुड़ने लगा था।
संसस रिपोर्ट ऑफ़ सेन्ट्रल प्रोविंसेज़ में बुनकरों के कोष्टि समुदाय के बारे में कहा गया था -
‘भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोष्टियों का भी बुरा समय चल रहा है। वे मैनचेस्टर से इतनी भारी तादाद में आने वाली आकर्षक चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हाल के सालों में वे बड़ी संख्या में यहाँ से जाने लगे हैं। वे मुख्य रूप से बिहार का रुख कर रहे हैं जहाँ दिहाड़ी मज़ूरूर के तौर पर उन्हें रोज़ी-रोटी मिल जाती है…’
सेंसस रिपोर्ट ऑफ़ संन्ट्रल प्रोविंसेज़, 1872, सुमित गुहा ‘द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया, 1825-1950’, दि इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, 1989, में उद्धत।

चित्र 15 - बॉम्बे हार्बर, अठारहवीं सदी के आख़िर का चित्र।
बंबई और कलकत्ता 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे थे। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था।
स्थानीय बाज़ार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी।
1860 के दशक में बुनकरों के सामने नयी समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृहयुद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मँगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था।
उन्नीसवीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाज़ार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह क़ायम रह सकता था?
4 फै़क्ट्रियों का आना
बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और दो साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी चार मिलें काम कर रही थीं। उनमें 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगीं। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई।
ये उद्योग कौन लगा रहा था? उनके पूँजी कहा से आ रही थी? मिलों में काम करने वाले कौन थे?

चित्र 16 - जमशेदजी जीजीभोये।
जीजीभोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज़रानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज़ और अमेरिकी जहाज़ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज़ बेचने पड़े।
4.1 प्रारंभिक उद्यमी
देश के विभिन्न भागों में तरह-तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये कौन लोग थे।
बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था, अठारहवीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज़ भारतीय अफ़ीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुँच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830-1840 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियाँ लगा ली थीं। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ-साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन उन्नीसवीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बंबई में डिनशॉ पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिड़ला के पिता और दादा ने किया।

चित्र 17 - द्वारकानाथ टैगोर।
द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगीकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाज़रानी, जहाज़ निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था।
पूँजी इकट्ठा करने के अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे जबकि कुछ के मध्य-पूर्व व पूर्वी अफ्रीका में संबंध थे। इनके अलावा भी कुछ वाणिज्यिक समूह थे लेकिन वे विदेश व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुँचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फ़क्ट्रियाँ लगा लीं।
जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे-वैसे भारतीय व्यावसायियों के जगह सिकुड़ती गई। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाजकच्ची कपास, अफ़ीम, गेहूँ और नील-का ही निर्यात कर सकते थे जिनकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी। धीरे-धीरे उन्हें जहाज़रानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया।
पहले विश्वयुद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियाँ भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थीं। इनमें बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल, और जार्डीन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियाँ थीं। ये एजेंसियाँ पूँजी जुटाती थीं, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ लगाती थीं और उनका प्रबंधन सँभालती थीं। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्तपोषक (फाइनेंसर) पूँजी उपलब्ध कराते थे जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फ़ैसले यूरोपीय एजेंसियाँ लेती थीं। यूरोपीय व्यापारियों-उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था।

चित्र 18 - साझेदारों की टोली - जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, सर आर.जे. टाटा और सर डी.जे. टाटा।
1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग के काफ़ी बाद शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज़्यादातर आयात ही किया जाता था। इस स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता था।
4.2 मज़दूर कहाँ से आए?
फ़ैक्ट्रियाँ होंगी तो मज़दूर भी होंगे। फ़ैक्ट्रियों के विस्तार से मज़दूरों की माँग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में $5,84,000$ मज़दूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर $24,36,000$ हो चुकी थी। ये मज़दूर कहाँ से आए?
ज़्यादातर औद्योगिक इलाक़ों में मज़दूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों-कारीगरों को गाँव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ़ जाने लगते थे। 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50 प्रतिशत से ज़्यादा मज़दूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के ही गाँवों से आते थे। मिल मज़दूर बीच-बीच में अपने गाँव जाते रहते थे। वे फ़सलों की कटाई व त्यौहारों के समय गाँव लौट जाते थे।
बाद में, जब नए कामों की खबर फैली तो दूर-दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के , संयुक्त प्रांत के लोग बंबई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के पहुँच रहे थे।

चित्र 19 - बंबई के एक मिल के युवा कामगार, बीसवों सदी की शुरुआत।
जब मज़दूर गाँव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे।
नौकरी पाना हमेशा मुश्किकल था। हालाँकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मज़दूरों की माँग भी बढ़ रही थी लेकिन रोज़गार चाहने वालों की संख्या रोज़गारों के मुक़ाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति नए मज़दूरों की भर्ती के प्राय: एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गाँव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताक़तवर और मज़बूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफ़ों की माँग करने लगे और मज़दूरों की ज़िदगी को नियंत्रित करने लगे।
समय के साथ फै़क्ट्री मज़दूरों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था।

चित्र 20 - मुख्य जॉबर।
इस चित्र में देखें कि उसका अंदाज और उसके कपड़ों से जॉबर की सत्ता का पता चलता है।
बंबई के एक मिल मज़दूर वसंत पारकर ने कहा -
‘मज़दूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के जॉबर को पैसा देते थे…। मिल मज़दूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसके गाँव से गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वह गाँव जाकर फ़सलों की कटाई करता था। कोंकणी लोग धान काटने और घाटी यानी गन्ना काटने गाँव में जाते थे। यह एक स्वीकृत व्यवस्था थी जिसके मिल वाले छुट्टी दे देते थे।
मीना मेनन एवं नीरा अदरकर, वन हंड्रेड इयर्स : वन हंड्रेड वॉइसेज़, 2004 इोत

चित्र 21 - अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मज़ादू औरतें।
औरतें मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम करती थीं।
नए शब्द
जॉबर : इन्हें अलग-अलग इलाक़ों में ‘सरदार’ या ‘मिस्त्री’ आदि भी कहते थे।
भाई भोसले बंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930-40 के दशकों में बिताए अपने बचपन को उन्होंने इस प्रकार याद किया -
‘उस जमाने में दस घंटे की शिफ्ट होती थी। शाम पाँच बजे से सुबह तीन बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की। उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए…। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गाँव चले गए।’
मीना मेनन एवं नीरा अदरकर, वन हंड्रेड इयर्स : वन हंड्रेड वॉइसेज़, 2004
5 औद्योगिक विकास का अनूठापन
भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर ज़मीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के आवश्यकता थी।
उन्नीसवीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाज़ार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था इस भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था।
बीसवीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगीकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाज़ारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप, भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया।
पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिलकुल नयी स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारख़ाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे इस भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाज़ारों को रातोंरात एक विशाल देशी बाज़ार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फ़ौज के जूट की बोरियाँ, फ़ौजियों के वर्दी के कपडे़, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए।

चित्र 22 - मद्वास चेम्बर ऑफफ कॉमर्स का पहला दफ़्तर।
उन्नीसवीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायो मिलकर चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक चिंता के मुदों पर फैसला ले सकें।
पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मज़दूरों को काम पर रखा गया और हरेक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा।
युद्ध के बाद भारतीय बाज़ार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पायी। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाज़ारों पर क़न्ज़ा कर लिया और धीर-धीरे अपनी स्थिति मज़बूत बना ली।
5.1 लघु उद्योगों की बहुतायत
हालाँकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इज़ाफ़ा हुआ लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर - 1911 में 67 प्रतिशत - बंगाल और बंबई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5 प्रतिशत और 1931 में 10 प्रतिशत थी। बाकी मज़दूर गली-मोहल्लों में स्थित छोटी-छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे।
कुछ मामलों में तो बीसवीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इज़ाफ़ा हुआ था। यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन-निर्मित धागे ने उन्नीसवीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। बीसवीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह तीन गुना हो चुका था।

चित्र 23 - हाथ से बुना कपड़ा।
हाथ से बुने कपड़े के महीन डिज़ाइन की मिलों में नक़ल नहीं को जा सकती थी।
ऐसा कैसे हुआ?
इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा न हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नयी तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इस, बीसवों सदी के दूसरे दशक तक आते-आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ़्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज़ हुआ और श्रम की माँग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35 प्रतिशत से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70-80 प्रतिशत तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे-छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुक़ाबला करने में मदद मिली।
नए शब्द
फ्लाई शटल : यह रस्सियों और पुलियों के ज़रिए चलने वाला एक यांत्रिक औज़ार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षैतिज धागे (ताना-the weft) को लम्बवत् धागे (बाना-the warp) में पिरो देती है। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली।
मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुक़ाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी माँग में भारी उतार-चढ़ाव आते थे। खराब फ़सल और अकाल के समय जब ग्रामीण ग़रीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नकद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर क़िस्म के कपड़े की माँग खाते-पीते तबके में ज्यादा थी। उसमें उतार-चढ़ाव कम आते थे। जब ग़रीब भूखों मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी, जैसा कि आप देख चुके है, मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नक़ल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के आसान नहीं था।
ऐसा भी नहीं है कि बीसवीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। उनकी ज़िदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन-रात काम करना पड़ता था। अकसर पूरा परिवार-बच्चे, बूढ़े, औरतें-उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फ़िक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे।

चित्र 24 - भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों वाले इलाके़, 1931
चित्र में बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के आकार को इंगित करते हैं।
6 वस्तुओं के लिए बाज़ार
हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाज़ार पर क़ब्ज़े के प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के माँग उठाई, अपने जगह बनाई और अपने माल के बाज़ार को फैलाने का प्रयास किया।
जब नयी चीज़ें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। इसके क्या किया गया?
नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीक़ा विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नयी ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ चारों तरफ़ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के परदे पर, सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगीकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाज़ार को फैलाने में और एक नयी उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है।

चित्र 25 - ग्राइपवॉटर का कैलेंडर, एम.वी. धुरंधर का चित्र, 1928
बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था।
जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में ‘मेड इन मैनचेस्टर’ लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था।

चित्र 26 (क)
चित्र 26 (ख)
चित्र 26 (क) - मैनचेे्टर के लेबल, बीसवीं सदी का प्रारंभ। आयातित कपड़ों के लेबलों पर असंख्य भारतीय देवी-देवताओं - कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था।
चित्र 26 (ख) - मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र। उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इस्तेमाल किया जा रहा था।
लेबलों पर सिऱ़् शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे। उन पर तस्वीरें भी बनी होती थीं जो अकसर बहुत सुंदर होती थीं। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब-किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीक़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
इन लेबलों पर भारतीय देवी-देवताओं की तसवीरें प्रायः होती थीं। देवी-देवताओं की तसवीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तसवीरों का फ़ायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी-पहचानी सी लगती थी।
उन्नीसवों सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़-लिखे लोग ही समझ सकते थे लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों व मध्यवर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज, पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के देवताओं की तसवीर होती थी।

चित्र 27 - सनलाइट साबुन का कैलेंडर, 1934 यहाँ भगवान विष्णु आसमान से रोशनी लाते दिखाए गए हैं।
देवताओं की तसवीरों की तरह महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों व नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थीं। इनका संदेश अकसर यह होता था : अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए; अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता।
जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ़ दिखाई देता था। इनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे।
निष्कर्ष
ज़ाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े-बड़े प्रौद्योगिकीय बदलाव आए हैं, फ़ैक्ट्रियों का उदय हुआ है और नयी औद्योगिक श्रमशक्ति अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आपने देखा है, इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
चित्र 1 और 2 को दोबारा देखिए। अब बताइए कि ये छवियाँ क्या दर्शाती हैं।

चित्र 28 - एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेबल।
इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही हैं और लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही हैं।
संक्षेप में लिखें
1. निम्नलिखित की व्याख्या करें -
(क) ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए।
(ख) सत्रहवों शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे।
(ग) सूरत बंदरगाह अठारहवों सदी के अंत तक हाशिये पर पहुँच गया था।
(घ) ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के गुमाश्तों को नियुक्त किया था।
2. प्रत्येक वक्तव्य के आगे ‘सही’ या ‘गलत’ लिखें -
(क) उन्नीसवों सदी के आखिए में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80 प्रतिशत तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था।
(ख) अठारहवों सदी तक महीन कपड़े के अंतराष्ट्रीय बाज़ार पर भारत का दबदबा था।
(ग) अमेरेकी गृद्युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई।
(घ) फ़्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ।
3. पूर्व-औद्योगीकरण का मतलब बताएँ।
चर्चा करें
1. उन्नीसवों सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे।
2. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के क्या किया।
3. कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश (Encyclopaedia) के लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर अपना लेख लिखिए।
4. पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा?
परियोजना कार्य
अपने क्षेत्र में किसी एक उद्योग को चुनकर उसके इतिहास का पता लगाएँ। उसकी प्रौद्योगिकी किस तरह बदली? उसमें मज़ूर कहाँ से आते हैं? उसके उत्पदों का विज्ञापन और मार्केटिंग किस तरह किया जाता है? उस उद्योग के इतिहास के बारे में उसके मालिकों और उसमें काम करने वाले कुछ मज़्दूरों से बात करके देखिए।