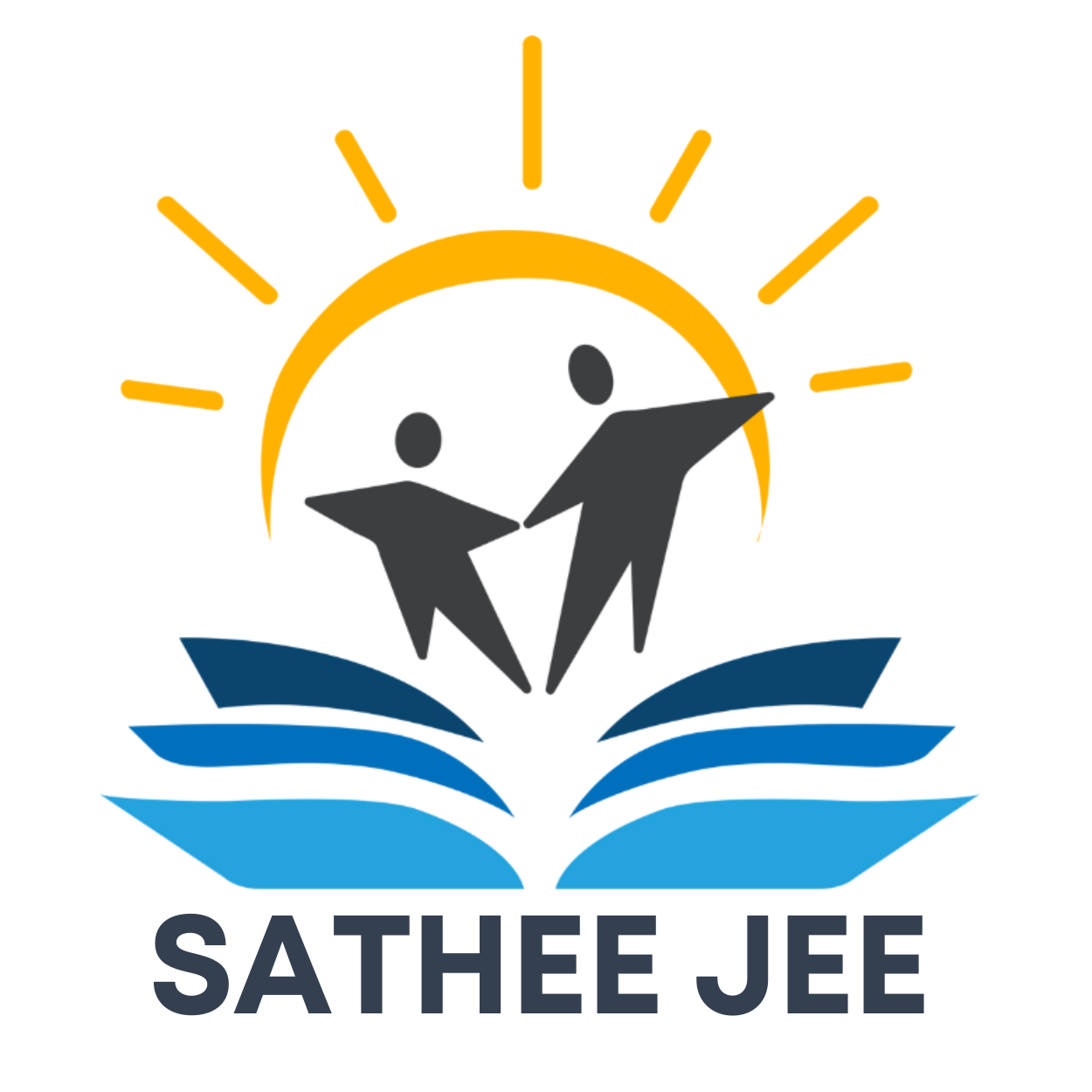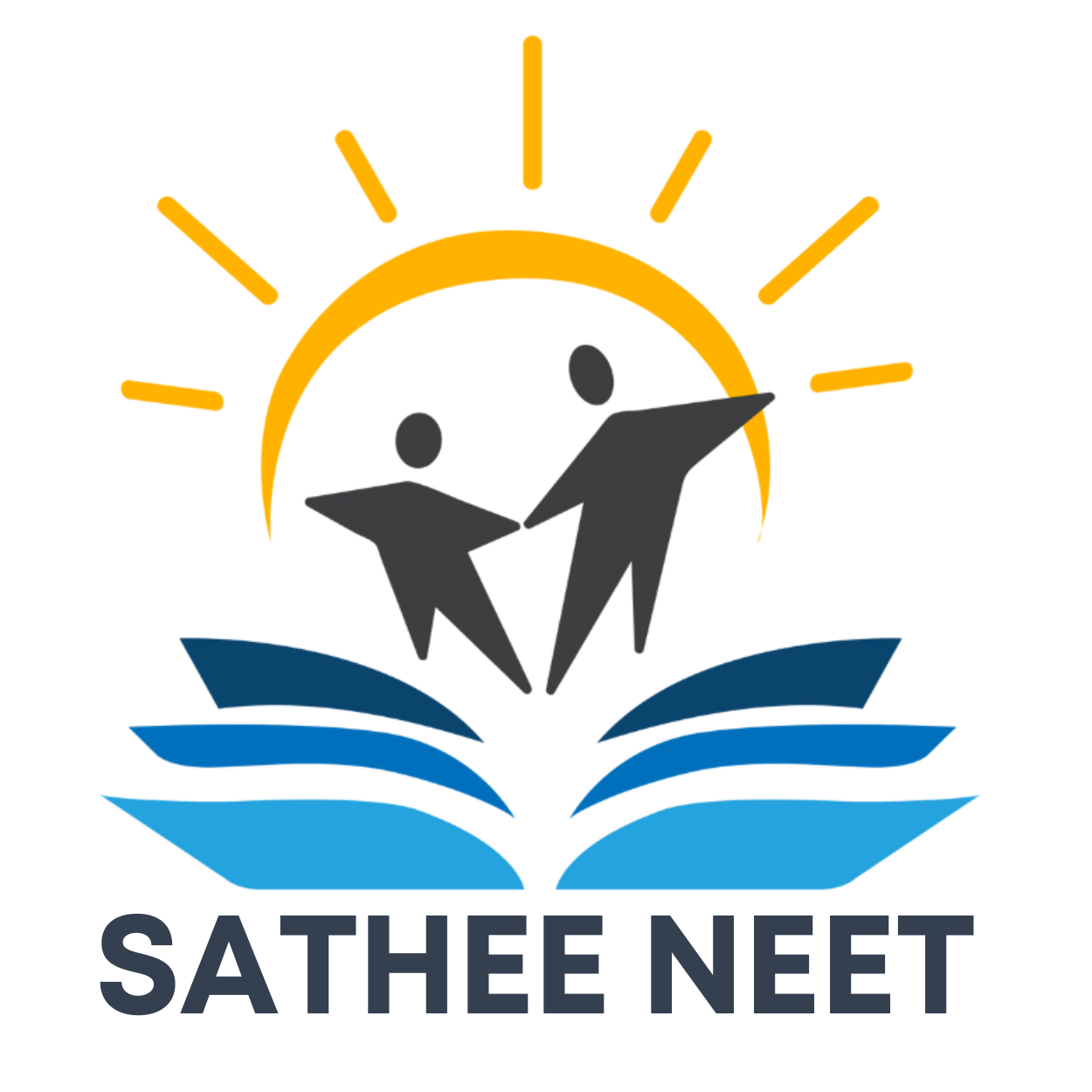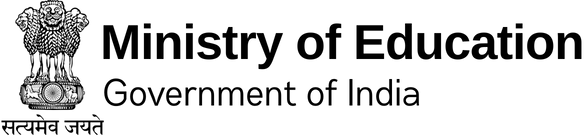अध्याय 03 भूमंडलीकृत विश्व का बनना
1 आधुनिक युग से पहले
जब हम ‘वैश्वीकरण’ की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग पचास सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया - व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूँजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का - एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुज़रते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है।
इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक-दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के या उत्पीड़न/यातनापूर्ण जीवन से बचने के दूर-दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह-तरह की चीजें, पैसा, मूल्य-मान्यताएँ, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे हैं। 3,000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाक़े से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। हज़ार साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ (जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था) चीन और पूर्वी अफ़्रीका तक पहुँचती रही हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर-दूर तक पहुँचने का इतिहास भी सातवीं सदी तक ढूँढ़ा जा सकता है। तेरहवों सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ़ देखा जा सकता है।

चित्र 1 - एक स्मृतिशिला पर पानी के एक जहाज़ का चित्र, गोवा संग्रहालय, दसवीं शताब्दी।
पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई नवों सदी के बाद की स्मृतिशिलाओं पर जलपोतों की तसवीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्त्व का पता चलता है।
1.1 रेशम मार्ग ( सिल्क रूट) से जुड़ती दुनिया
आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर-दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। ‘सिल्क मार्ग’ नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम (सिल्क) का कितना महत्त्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ज़मीन या समुद्र से होकर गुज़रने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम करते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग पंद्रहवों शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुँचते थे। वापसी में सोने-चाँदी जैसी कीमती धातुएँ यूरोप से एशिया पहुँचती थीं।
व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, दोनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलती थीं। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था।

चित्र 2 - चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग, आठवों सदी, गुफा 217, मोगाओ ग्राटोज़, गन्सू, चीन।
1.2 भोजन की यात्रा : स्पैघेत्ती और आलू
हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने-अनजाने वहाँ नयी फ़सलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले ‘झटपट तैयार होने वाले’ (Ready) खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पैघेत्ती (Spaghetti) और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पैघेत्ती का जन्म हुआ, या संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ पाँचवीं सदी में सिसली पहुँचा जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं इस हो सकता कि हम कभी यह न जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी, इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन-देन चल रहा होगा।
आलू, सोया, मूँगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग पाँच सौ साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस

चित्र 3 - वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए ब्यापारी चीजों की अदला-बदली करते हुए, मार्को पोलो, बुक ऑफ़ मार्वल्स, पंद्रहवीं सदी।
गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। (यहाँ ‘अमेरिका’ का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरीबियन द्वीपसमूह, सभी से है।) दरअसल, हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं।
कई बार नयी फ़सलों के आने से जीवन में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के ग़रीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फ़सल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुँह में चले गए।
1.3 विजय, बीमारी और व्यापार
सोलहवों सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूँढ़ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे तो पूर्व-आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता-फूलता व्यापार, तरह-तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएँ एक जगह से दूसरी जगह आ-जा रही थीं। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाक़े का भारी महत्त्व था। यूरोपीयों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ़ भी मुड़ने लगी।
अपनी ‘खोज’ से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन सोलहवीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फ़सलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप-रंग बदलने लगे।
आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली क़ीमती धातुओं, खासतौर से चाँदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। सत्रहवीं सदी के आते-आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन-संपदा के बारे में तरह-तरह के क़िस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए।
सोलहवीं सदी के मध्य तक आते-आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएँ केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत क़िस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफ़सरों के साथ वहाँ जा पहुँचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग-थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग-प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी।

चित्र 4 - आयरलैंड में आलू अकाल, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, 1849
फ़्रल कट जाने के बाद बचे-खुचे आलुओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे। 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग $10,00,000$ लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे और इससे दोगुने लोग काम की तलाश में घर-बार छोड़ कर दूसरे इलाकों में चले गए थे।
‘जैविक’ युद्ध?
न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स के कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के ईश्वर का वरदान है : ‘… देशी जनता … छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कीयत पर हमें मालिकाना दे दिया।’
अल्फ़्रेड क्रॉस्बी, इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म
फलस्वरूप, इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया।
बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के ख़लाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी।
उन्नीसवों सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। अठारहवीं सदी तक अमेरिका में अफ़्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाज़ारों के कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था।
अठारहवीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हों का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पंद्रहवों सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग-थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्त्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया।
नए शब्द
असंतुष्ट : जो स्थापित विश्वासों और तरीक़ों को नहीं मानता।
चर्चा करें
जब हम कहते हैं कि सोलहवीं सदी में दुनिया ‘सिकुड़ने’ लगी थी तो इसका क्या मतलब है।

चित्र 5 - गुलामों की खरीद-फरोो़़्न, न्यू ऑर्लियंस, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, 1851
एक खरीदार नीलामी के कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में चार औरतों और लंबी टोपियाँ पहने सात पुरुषों के साथ दो बच्चे भी बिकने के ख़ड़े हैं। अच्छों क्रीमत पाने के गुरालामों को अकसर बढ़िया कपड़े पहना कर बाज़ार में लाया जाता था।
2 उन्नीसवीं शताब्दी ( $1815-1914$ )
उन्नीसवीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया।
अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों या ‘प्रवाहों’ का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है जो उन्नीसवीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं (जैसे कपड़ा या गेहूँ आदि) के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा, श्रम का प्रवाह होता है। इसमें लोग काम या रोज़गार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूँजी का होता है जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के दूर-दराज़ के इलाक़ों में निवेश कर दिया जाता है।
ये तीनों तरह के प्रवाह एक-दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी-कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के , वस्तुओं या पूँजी की आवाजाही के मुक़ाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय: ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी, यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो उन्नीसवों सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं।
2.1 विश्व अर्थव्यवस्था का उदय
इस विषय को समझने के सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन उन्नीसवों सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवनस्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे?
अठारहवों सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की माँग भी बढ़ी। जैसे-जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की माँग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद मँहगे होने लगे। दूसरी तरफ़ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन क़ानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें ‘कॉर्न लॉ’ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊँची क़ीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फ़ौरन समाप्त कर दे।
कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप, ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की क़ीमत का मुक़ाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए। गाँवों से उजड़ कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे।
जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। उन्नीसवीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज़ रही जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ीं। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के ज़मीनों को साफ़ करके खेती की जाने लगी।
खेती के ज़मीन को साफ़ कर देना ही काफ़ी नहीं था। खेतिहर इलाक़ों को बंदरगाहों से जोड़ने के रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के नयी गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नयी जमीनों पर खेती करने के यह आवश्यक था कि दूसरे इलाक़ों के लोग वहाँ आकर बसें। यानी नए घर बनाना और नयी बस्तियाँ बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के पूँजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूँजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा यानी श्रम का प्रवाह होने लगा।
उन्नीसवीं सदी में यूरोप के लगभग पाँच करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग पंद्रह करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर-बार छोड़कर दूर-दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे।

चित्र 6 - अमेरिका को रवाना होते आप्रवासियों से लदे जहाज़ का चित्र, एम.डब्यूयू. रिडले, 1869

चित्र 7 - जहाज़ पर चढ़ने का इंतज़ार करते आयरिश आप्रवासियों का चित्र, माइकेल फिट्ज़जेराल्ड, 1874
1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूँजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या क़स्बे से नहीं बल्कि हज़ारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मज़दूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहाँ महज़ एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुँचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ़्रीका और कैरीबियाई द्वीपसमूह के मज़दूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था।
गतिविधि
कल्पना कीजिए कि आप आयरलैंड से अमेरिका में आए एक खेत मज़दूर हैं। इस बारे में एक पैराग्राफ़ लिखिए कि आपने यहाँ आने का फ़ैसला क्यों किया और अब आप अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के क्या करते हैं।
बहुत छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्द्ध-रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के गेहूँ और कपास की खेती की जा सके। नयी नहरों की सिंचाई वाले इलाक़ों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी (नहर बस्ती) कहा जाता था।
भोजन तो सिर्फ़ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की माँग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीजों के उत्पादन में विभिन्न इलाक़ों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा ‘प्राथमिक उत्पादों’ यानी गेहूँ और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था।
2.2 तकनीक की भूमिका
इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज़, टेलग्राफ़, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्त्वपूर्ण रहे। उनके बिना उन्नीसवीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अकसर चौतरफ़ा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के , औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनों, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर-दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुँचाया जा सके।
गतिविधि
फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाइए कि जब ब्रिटेन ने खाद्य पदार्थों के आयात का निर्णय लिया तो उसके कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन करने वालों की संख्या क्यों बढ़ने लगी?

चित्र 8 - द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाज़ार, 1851 , इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़।
मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहाँ ख़रीद-फ़रोख़्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाज़ार था। उन्नीसवों सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाज़ार खोला गया था जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें जाती थीं।
मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन ज़िंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वज़न गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक मँहगा सौदा था और यूरोप के ग़रीबों की पहुँच से बाहर था। दूसरी तरफ़, ऊँची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की माँग और उत्पादन भी कम रहता था। नयी तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था।
इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ़ आलू और ब्रेड होते थे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार (और मक्खन व अंडे) भी शामिल हो गया। जीवनस्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा।
2.3 उन्नीसवीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद
उन्नीसवों शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाज़ार तेज़ी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। व्यापार में इज़ाफ़े और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। उन्नीसवों सदी के आखिरी दशकों में यूरोपीयों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया।

चित्र 9 - मांस को अलेक्सांद्रा, जलपोत पर लादा जा रहा है, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, 1878
मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी।
ज़रा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। आप पाएँगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएँ तो बिलकुल सीधी लकीर जैसी हैं मानो उन्हें फुट्टा (Scale) रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश, यही हुआ भी था। अफ़्रीका पर क़ब्ज़े की कोशिश में लगी प्रतिद्वंद्धी यूरोपीय ताक़तों ने अपने-अपने इलाके बाँटने के प्राय: इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक़्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बाँट लिया गया था।
उन्नीसवों सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नयी औपनिवेशिक ताक़तों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्ज़े में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर क़ब्ज़ा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताक़त बन गया।
आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोज़ी-रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा।

चित्र 10 - उन्नीसवीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ़ीका का मानचित्र।
मध्य अफ़्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली
स्टैली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हैर्ल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ़्रीका गए लिविंग्स्टन नामक मिशनरी की खोज करने के भेजा था। उस ज़माने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भाँति स्टैनली भी हभियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहाँ जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ीं, अफ़ीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक़्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे। उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था।

चित्र 11 - मध्य अफ़ीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी टोली, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, 1871
2.4 रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग
अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताक़तों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हज़ारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नयी शक्ल में ढाल दिया।
प्राचीन काल से ही अफ़्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ़्रीकियों की ज़िदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। उन्नीसवों सदी के आखिर में अफ़्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ़्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते - जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी - तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के काम करने की क्या ज़रूरत है।

चित्र 12 ट्रांसवाल स्वर्ण खानों तक आवागमन, द ग्राफिक, 1887
विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुँचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विट्वॉटर्सरेंड में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाक़े की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते-आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20 प्रतिशत से भी ऊपर जा चुका था।
उन्नीसवों सदी के आखिर में यूरोपीय ताक़तें अफ़्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप को ओर आकर्षित हुई थीं। यूरोपीय लोग अफ़्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख़्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मज़दरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आज़मा कर देख लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था

चित्र 13 - दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते मज़दूर, द ग्राफ़िक, 1875
जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए क़ानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस क़ानून के ज़रिए परिवार के बाक़ी लोगों को श्रम बाज़ार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खानकर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। उनके खुलेआम घूमने-फिरने पर पाबंदी लगा दी गई।
तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया।
अफ़्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ़्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश अधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हों जानवरों के ज़रिए यहाँ पहुँची थी। अफ़्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी ‘जंगल की आग’ की तरह पश्चिमी अफ़्रीका की तरफ़ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ़्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुँची। पाँच साल बाद यह केप (अफ़्रीका का धुर दक्षिणी हिस्सा) तक भी पहुँच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90 प्रतिशत मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया।
पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ़्रीकियों के रोज़ी-रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मज़बूत करने तथा अफ़्रीकियों को श्रम बाज़ार में ढकेलने के वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे-खुचे पशु भी अपने क़ब्ज़े में ले । बचे-खुचे पशु संसाधनों पर क़ब्ज़े से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व ग़ुलाम बना लेने का बेहतरीन मौक़ा हाथ लग गया था।
उन्नीसवीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं।
2.4 भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना
भारत से अनुबंधित (गिरमिटिया) श्रमिकों को ले जाया जाना भी उन्नीसवीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज़ आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी।
उन्नीसवों सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के दूर-दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनंबुधों में यह शर्त होती थी कि यदि मज़दूर अपने मालिक के बागानों में पाँच साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं।
भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाक़ों से जाते थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य में इन इलाक़ों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे,
ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बँँाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे, उन पर क़र्ज़ा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर-बार छोड़ने पड़े।
भारतीय अनुब्धित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरीबियाई द्वीप समूह ( मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सुरेनाम), मॉरिशस व फ़िजी ले जाया जाता था। तमिल आप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुवाधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के भी ले जाया जाता था।

चित्र 14 - त्रिनिदाद के एक कोको (Cocoa) बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मज़़ूर, उन्नीसबीं सदी का प्रारंभ।
मज़दूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे आप्रवासी अपने गाँव में होने वाले उत्पीड़न और ग़रीबी से बचने के भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी आप्रवासियों को फुसलाने के झूठी जानकारियाँ देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा, और नयी जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे आप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मज़दूर अनुबंध के राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे।
उन्नीसवीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने ‘नयी दास प्रथा’ का भी नाम दिया है। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुँचने के बाद मज़दूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं हैं। नयी जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थीं और मज़दूरों के पास क़ानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मज़दूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के अपने तरीक़े ढूँढ़ निकाले। बहुत सारे तो भाग कर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मज़दूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नयी संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति के नए रूप खोज । त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को ‘होसे’ (इमाम हुसैन के नाम पर) नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मज़दूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानवाद (Rastafarianism) नामक विद्रोही धर्म (जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुँचा दिया) में भी भारतीय आप्रवासियों और कैरीबियाई द्वीपसमूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर ‘ चटनी म्यूज़िक’ भी भारतीय आप्रवासियों के वहाँ पहुँचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नयी वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग-अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल-मिल जाती थीं, उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएँ गुम हो जाती थीं और बिलकुल नया रूप सामने आता था।
चर्चा करें
राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं के महत्त्व पर चर्चा करें।

चित्र 15 - शिनाख़्न के गिरमिटिया मज़दूरों के चित्र।
मालिकों के इन मज़ूदूरों के नाम नहों बल्कि उनकी संख्या का ही महत्त्व होता था।
ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिता कर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी. एस. नायपॉल का नाम सुना है? आपमें से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिवनैरन चंद्रॉल और रामनरेश सरवन का नाम भी सुना ही होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबांधित मजदूरों के ही वंशज हैं।
बीसवीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुर्धिति मजदूरों के वंशज कैरीबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें ‘कुली’ मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। नायपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विछोह और परायेपन के इस अहसास को खूब देखा जा सकता है।

चित्र 16 - एक अनुबंधित श्रमिक (गिरमिटिया मज़दूर) के अनुबंध का फॉर्म।
2.5 विदेश में भारतीय उद्यमी
विश्व बाज़ार के खाद्य पदार्थ व फ़सलें उगाने के वास्ते पूँजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के तो बाज़ार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था। लेकिन छोटे-मोटे किसानों का क्या होता ?
यहीं से देशी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपूरी श्रॉफ और नट्टूकोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातन्नुखी खेती के कर्ज़े देते थे। इसके वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज़े लेते थे। उनके पास दूर-दूर तक पैसे पहुँचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर थे।
अफ़्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे-पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े-बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थीं। यह एक फलता-फूलता कारोबार था क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनोंदिन बढ़ने लगी थी।
एक गिरमिटिया मज़दूर की आपबीती
राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने बीसवों सदी की शुरुआत में डेमेरारा में दस साल काम किया था। उनके संस्मरण का एक अंश :
‘… तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। … कुछ ही दिनों के भीतर मेंरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ़्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया जिसके मुझेे सज़ा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। … नए आप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। … अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा न हुआ तो तनख़्वाह भी काट ली जाती है। इसी बहुत सारे लोगों को उसका पूरा वेतन नहीं मिल पाता है और उन्हें तरह-तरह से सज़ा दी जाती है। दरअसल मज़ूरूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्रिलों में बितानी पड़ती है..।
स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, आप्रवासन शाखा, 1916
2.6 भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था
भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगीकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप,

चित्र 17 - ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लंदन।
ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यहीं था।
ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा।
उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के नए-नए बाज़ार ढूँढ़ने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाज़ारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आँकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन् 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था जो 1815 में घट कर 15 प्रतिशत रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3 प्रतिशत रह गया था।
तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? आँकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5 प्रतिशत से बढ़ कर 35

चित्र 18 - सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य।
सत्रवों सदी के दौरान और अठारहवों सदी के शुरुती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा।
प्रतिशत तक पहुँच गया था। कपड़ों की रँगाई के इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था, 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफ़ीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफ़ीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफ़ीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफ़ीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था।
उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय बाज़ारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इज़ाफ़ा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा ‘व्यापार अधिशेष’ की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फ़ायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफ़े के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफ़ा कमा कर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने उन्नीसवीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी।
ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित ‘होम चार्जेज़’ ( देसी खर्चे) का निबटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफ़सरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी क़र्ज़े पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफ़सरों की पेंशन शामिल थी।

चित्र 19 - सत्रहवीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग।
3 महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था
पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया। लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्त्तपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को तीन दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। इस दौरान पुरी दुनिया में चौतरफ़ा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी।
3.1 युद्धकालीन रूपांतरण
जैसा कि आप जानते ही हैं, पहला विश्वयुद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ़्रांस और रूस थे तो दूसरे पाले में कंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। पर यह युद्ध तो चार साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा।
मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहों हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक-दूसरे से जूझ़ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी।
यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीनगनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थीं। युद्ध के दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भर कर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभिषिका रची उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहों की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए।
मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई।
युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के उद्योगों का पुर्ग्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो

चित्र 20 - प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान एक हथियार .फैक्ट्री में काम करते मज़़ूरू।
युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के हथियारों के उत्पादन में तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ।
उन कामों को सँभालने के घर की औरतों को बाहर आना पड़ा जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था।
युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताक़तों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक-दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी क़र्ज़ा लेना पड़ा। फलस्वरूप, इस युद्ध ने अमेरिका को क़र्ज़दार की बजाय कर्ज़दाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी।
3.2 युद्धोत्तर सुधार
युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाज़ार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुक़ाबला करना था, सो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के ब्रिटेन ने अमेरिका से जम कर क़र्ज़े थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्र्ज़ों में दब चुका था।
युद्ध के कारण आर्थिक उछाह का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि माँग, उत्पादन और रोज़गारों में भारी इज़ाफ़ा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाह शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोज़गारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी-भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोज़गार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर पाँच में से एक ब्रिटिश मज़दूर के पास काम नहीं था। रोज़गार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी।
बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएँ भी संकट में थीं। उदाहरण के , गेहू उत्पादकों की हालत पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाज़ार में गेहूँ की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त-व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गहूँ की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूँ की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेँूू की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे क़र्ज़ संकट में फँस गए।
3.3 बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग
अमेरिका में सुधार की गति तेज़ रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुँचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा लेकिन बीस के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्क़ी के रास्ते पर बढ़ने लगी।
1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहत उत्पादन (Mass Production) का चलन। बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो उन्नीसवों सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फ़ोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज़ पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठा कर निकलते जाते थे। यह देख कर फ़ोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे, दोनों के लिहाज़ से किफायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम - जैसे, कार के किसी खास पुर्ज़े को ही लगाते रहना - मशीनी ढंग से बार-बार करते रहना होता था। काम की रफ़्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ़्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मज़दूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मज़दूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और, इस व्यवस्था में मज़दूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहों कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ की हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर तीन मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ़्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी-मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी।

चित्र 21 - फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी टी-मॉडल गाड़ियाँ।
शुरुआत में फ़ोर्ड फ़ैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई क्योंकि वे उसकी रफ़्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मज़दूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के फ़ोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुना यानी 5 डॉलर प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी।
तनख़्वाह बढ़ाने से हेनरी फ़ोर्ड के मुनाफ़े में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के वे अपनी असेंबली लाइन की रफ़्तार बार-बार बढ़ाने लगे। उनके मज़दरूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फ़ैसले से फ़ोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि ‘लागत कम करने के ’ अपनी ज़िदगी में उन्होंने इससे अच्छा फ़ैसला कभी नहीं लिया।
फ़ोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। बीस के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नक़ल की जाने लगी। बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मज़दूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुँचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफ़ोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीजें ‘हायर-परचेज़’ व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थीं। यानी लोग ये सारी चीजें क़र्ज़े पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ़्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की माँग में इज़ाफ़ा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी क़र्ज़े पर ही की जा रही थी।
1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से रोज़गार और माँग बढ़ती थी तो दूसरी और उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के और ज़्यादा निवेश की जरूरत थी जिससे और नए रोज़गार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी।
1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूँजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा क़र्ज़दाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूँजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद दी। अगले छह साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया।
लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक क़ायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते-आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फँस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहों किया था।
3.4 महामंदी
आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट तीस के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोज़गार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इस हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पदों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही।
इस महामंदी के कई कारण थे। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरों और किसानों की आय घटने लगी तो आमदनी बढ़ाने के किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सकें।

चित्र 22 - महामंदी के दौरान एक आप्रवासी खेत मज़्दूर का बेघर और भूखा परिवार, 1936
सौजन्य : लायब्रेरी ऑफ़्फ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फ़ोटोग्राप्स डिविजन।यह चित्र लेने वाली डॉरोथी लेंग ने इस भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था -
‘मैंने इस भूखी, लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से खिंची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई…। मैंने न तो उसका नाम पूछा न उसके अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र पैंतीस साल है। उसने कहा कि वे लोग (यानी माँ और उसके सात बच्चे) आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सक्जियों और उन परिदोंों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उसके बच्चे मार लाते हैं…। वो वहाँ बैठी थी… अपने बच्चों को चिपटाए, शायद उसे लगता था कि मेरी तसवीर उसकी कोई मदद कर सकती है इस उसने मेरी मदद कर दी…।’
स्रोत : पॉपुलर फ़ोटोग्राफ़ी, फ़रवरी 1960
फलस्वरूप, बाज़ार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है, कीमतें और नीचे चली गईई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी-पड़ी सड़ने लगी।
दूसरा कारण : 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से क़र्ज़े लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से क़र्ज़ा जुटाना बहुत आसान था लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले छह माह तक विदेशों में अमेरिका का क़र्ज़ा एक अरब डॉलर था। साल भर के भीतर यह कर्ज़ा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी क़र्ज़े पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ।
भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो लेकिन अमेरिकी पूँजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर ज़रूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की क़ीमतें तेज़ी से लुढ़कने लगीं। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के आयातित पदार्थों पर दो गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फ़ैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़़ दी।
औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू क़र्ज़े देना बंद कर दिया। जो कर्ज़े दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज़ कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज़े चुकाने में नाकामयाब हो गए जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी ज़रूरी चीजें कुर्क कर ली गईं। बीस के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुबार की तरह रातोंरत काफ़ूर हो गई थी। बेरोज़गारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर-दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्ज़े वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूँजी न लौटा पाने के कारण हज़ारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आँकड़े सकते में डाल देने वाले हैं : 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन $1,10,000$ कंपनियाँ चौपट हो चुकी थीं।
यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो-दिमाग़ पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी।

चित्र 23 - बेरोज़गारी लाभ के क्तार में खड़े लोग, अमेरिका। डॉरोथी लेंग द्वारा लिया गया चित्र, 1938
सौजन्य : लायद्रोरी ऑफ़ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फ़ोटगग्गाफ्स डिविजन। जब एक बेरोजगारी जनगणना से पता चला कि देश में एक करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कोई काम नहीं है तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में स्थानीय प्रशासन की और से बेरेज़गगरों को छोटे-छोटे भत्ते दिए जाने लगे। ये लंबी क़तारें महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोज़गारी का प्रतीक थीं।
3.5 भारत और महामंदी
यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बीसवीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कँपकँपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुँच जाती थी और उससे दुनिया भर में लोगों की ज़िदगी, अर्थव्यवस्थाएँ और समाज प्रभावित हो उठते थे।
जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फ़ौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात-निर्यात घट कर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें गिरने लगीं तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूँ की कीमत 50 प्रतिशत गिर गई।
शहरी निवासियों के मुक़ाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुक़सान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ़ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाज़ार के उपज पैदा करते थे।
बंगाल के जूट/पटसन उत्पादकों को ही देखिए। वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियाँ बनाई जाती थीं। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60 प्रतिशत से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के उपज बढ़ाने के वास्ते क़र्ज़े ले थे उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनोंदिन और क़र्ज़ में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था -
चलो भाइयों, नक़द की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ
लागत और क़र्ज़े में पिसकर नाउम्मीदी पाओ
सारी पूँजी लगा-फँसाकर फ़सल खड़ी कर जाओ
…घर पर बैठे बनिये देंगे पाँच रुपये मन भाव
पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा क़र्ज़ में डूब गए। खर्च पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी, घर में जो भी गहने-ज़ेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हों सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समस महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा (सिविल नाफ़रमानी) आंदोलन शुरू किया।
यह मंदी शहरी भारत के इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जैसे, शहर में रहने वाले ज़मींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बँधा-बँधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेज़ी आई।
चर्चा करें
पटसन (जूट) उगाने वालों के विलाप में पटसन की खेती से किसके मुनाफ़े का ज़िक्र आया है? स्पष्ट करें।
4 विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण : युद्धोत्तर काल
पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल दो दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियाँ (मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान और इटली) थीं तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ़ांस और अमेरिका) के नाम से जाना जाता था। छह साल तक चला यह युद्ध ज़मीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया।
इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहों बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3 प्रतिशत था। करोड़ों लोग घायल हुए।
अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्च पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था।

चित्र 24 - रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियाँ,
जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्त्व की घटना थी।
युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नात्सी जर्मनी को हराने के सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियाँ दी थीं। जिस समय पूँजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था।

चित्र 25 - सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्तालिन्र्राद।
4.1 युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन-वुड्स संस्थान
दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिजों ने दो अहम सबक़ निकाले। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना क़ायम नहीं रखा जा सकता। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोज़गार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। स्थिर आय के पूर्ण रोज़गार भी ज़रूरी था।
लेकिन बाज़ार पूर्ण रोज़गार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोज़गार में आने वाले उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करने के सरकार का
दखल ज़रूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के ज़रिये ही सुनिश्चित की जा सकती थी।
दूसरा सबक़ बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोज़गार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूँजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताक़त उपलब्ध हो।
संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोज़गार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी।
सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ़.) की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के पैसे का इंतज़ाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है) का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और आई.एम.एफ़. को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन (ब्रेटन वुड्स की जुड़वाँ संतान) भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अकसर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है।
विश्व बैंक और आई.एम.एफ़. ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और आई.एम.एफ़. के किसी भी फ़ैसले को वीटो कर सकता है।

चित्र 26 - ब्रेटन वुड्स, अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल।
यही वह स्थान है जहाँ ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक-दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधरित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएँ, जैसे भारतीय मुद्रा- रुपया-डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बँधा हुआ था। एक डॉलर के बदले में कितने रुपये देने होंगे, यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बँधा हुआ था। एक डॉलर की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी।
नए शब्द
वीटो : निषेधाधिकार; इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है।
4.2 प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष
ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8 प्रतिशत से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी। उसमें ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोज़गारी औसतन 5 प्रतिशत से भी कम ही रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुँचने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। इसी उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूँजी का निवेश किया।
चर्चा करें
संक्षेप में बताएँ कि दो महायुद्धों के बीच जो आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा हुए उनसे अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने क्या सबक सीखे?
4.3 अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता
दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले दो दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र, स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन ये सभी देश ग़रीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएँ और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त-व्यस्त हो चुके थे।
आई.एम.एफ. और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था उसके कारण ये देश आई.एम.एफ. और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहों थे। इसी कारण पचास के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे।
दुनिया के अल्पविकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नवस्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के उन्हें ऐसे अंर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था।
अनौपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नवस्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ़्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका वहाँ के महत्त्वपूर्ण संसाधनों, जैसे खनिज संपदा और ज़मीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ़्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थीं।
कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थीं।
दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को पचास और साठ के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नयी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली (New International Economic Order-NIEO) के आवाज़ उठाई और समूह 77 (जी-77) के रूप में संगठित हो गए। एन.आई.ई.आ. से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिलें, और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के बेहतर पहुँच मिले।
एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम (मल्टोनेनल कॉर्पोरेन-एमएनसी) या बहुाराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। पचास व साठ के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिमी यूरोप एवं जापान भी विश्वयुद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे उस समय ऐसी बहुत सारी नयी कंपनियाँ समने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार पचास और साठ के दशक की एक विशेषता था। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज़्यादातर सरकरें बाहर से आने वाली चीजों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थीं जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहाँ वे अपने उत्पाद बेचना चाहती थीं। उन्हें ‘घेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था।
नए शब्द
आयात शुल्क (Tariff) : किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर।
4.4 ब्रेटन वुड्स का समापन और ‘वैश्वीकरण’ की शुरुआत
सालों की स्थिर और तेज़ वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। साठ के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई।
सत्तर के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश क़र्ज़े और विकास संबंधी सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से क़र्ज़ न लेने के बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय-समय पर क़र्ज़ संकट पैदा होने लगा जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी।
औद्योगिक विश्व भी बेरोज़गारी की समस्या में फँसने लगा था। सत्तर के दशक के मध्य से बेरोज़गारी बढ़ने लगी। नब्बे के दशक के प्रांरभिक वर्षों तक वहाँ काफी बेरोज़गारी रही। सत्तर के दशक के आखिर सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगीं जहाँ वेतन कम थे।
चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग-थलग ही था। परंतु चीन में नयी आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए।
चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाज़ारों पर अपना प्रभुत्व क़ायम करने के प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहाँ जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और खास तौर से वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है।
उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूँजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले दो दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है।
नए शब्द
विनिमय दर : इस व्यवस्था के जरिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक-दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर दो प्रकार की होती हैं : स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर।
स्थिर विनिमय दर : जब विनिमय दर स्थिर होती हैं और उनमें आने वाले उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करने के सरकारों को हस्क्षेप करना पड़ता है तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है।
लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर : इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाज़ार में विभिन्न मुद्राओं की माँग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांतत: सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती-बढ़ती रहती है।
संक्षेप में लिखें
1. सत्रहवों सदी से पहले होने वाले आदान-प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुने।
2. बताएँ कि पूर्व-आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी।
3. निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें:
(क) कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फ़ैसला।
(ख) अफ़्रीका में रिंडरपेस्ट का आना।
(ग) विश्वयुद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत।
(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव।
(ङ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फ़ैसला।
4. खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के इतिहास से दो उदाहरण दें।
5. ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है।
चर्चा करें
6. कल्पना कीजिए की आप कैरीबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मज़दूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखें।
7. अंर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक-एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें।
8. महामंदी के कारणों की व्याख्या करें।
9. जी-77 देशों से आप क्या समझते हैं। जी-77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वाँ संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। व्याख्या करें।
परियोजना कार्य
उन्नीसवीं सदी के दौरान दक्षिण अफ़्रीका में स्वर्ण हीरा खनन के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी करें। सोना और हीरा कंपनियों पर किसका नियंत्रण था? खनिक कौन लोग थे और उनका जीवन कैसा था?