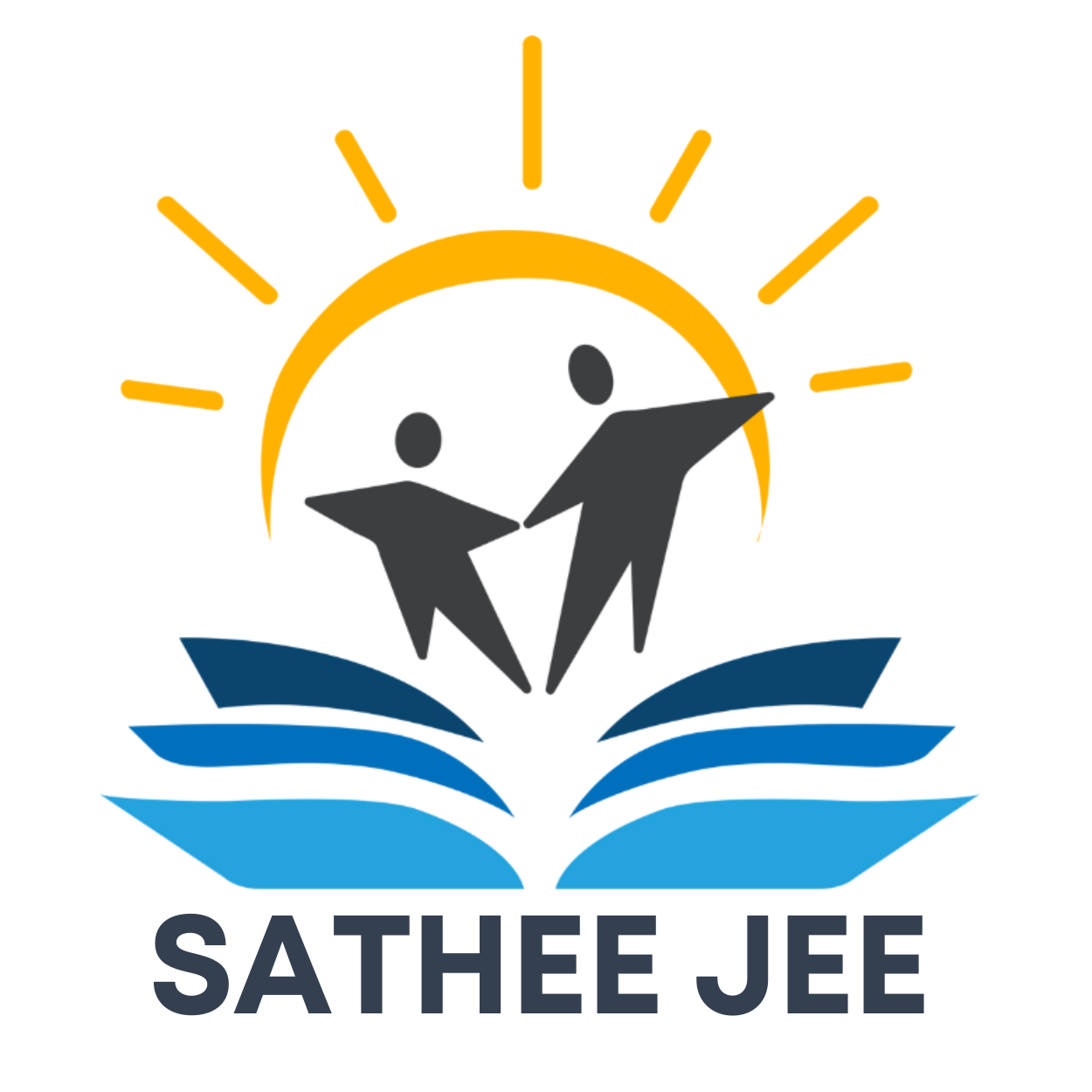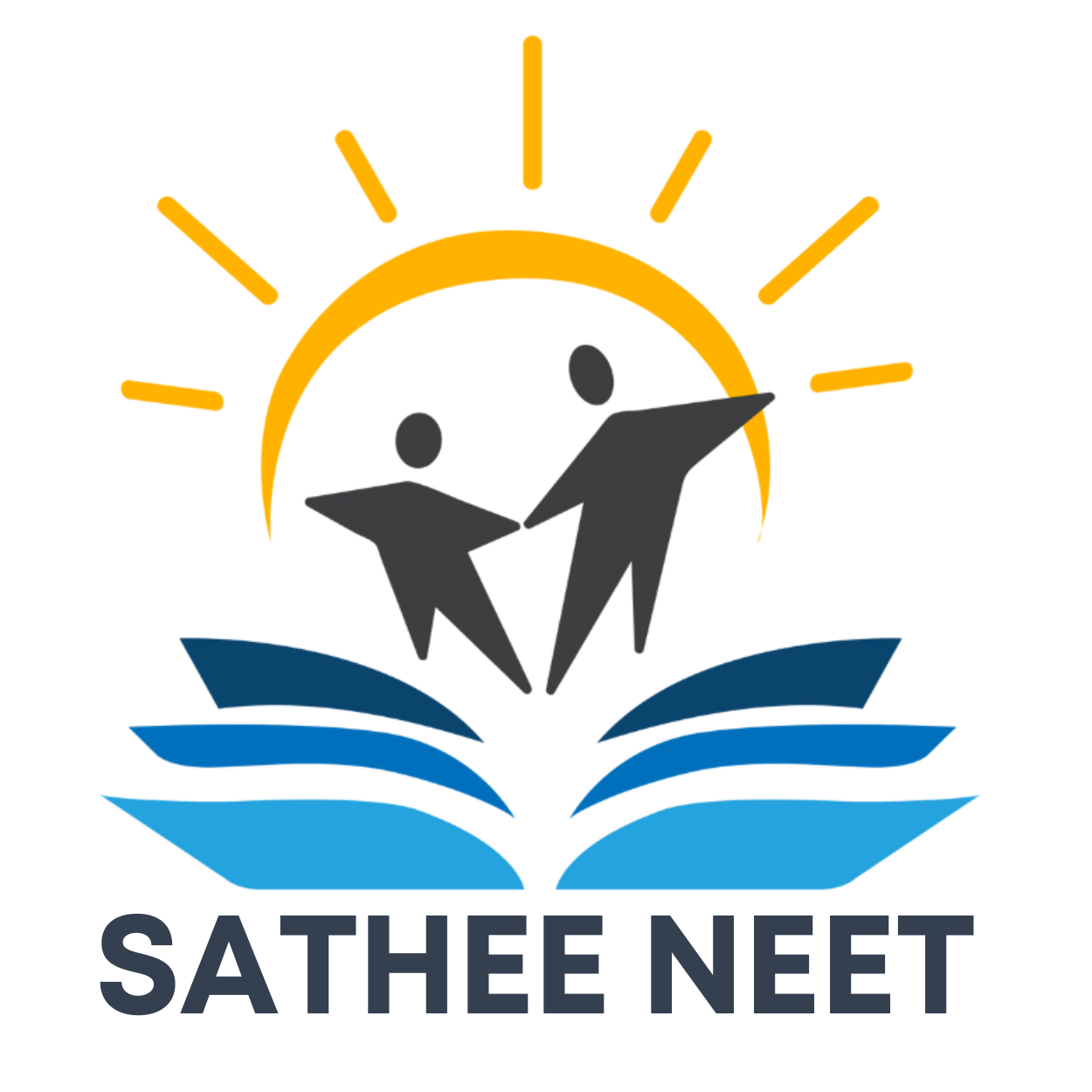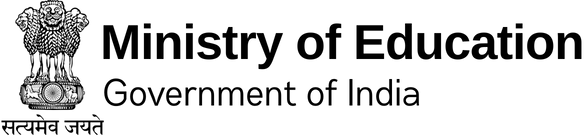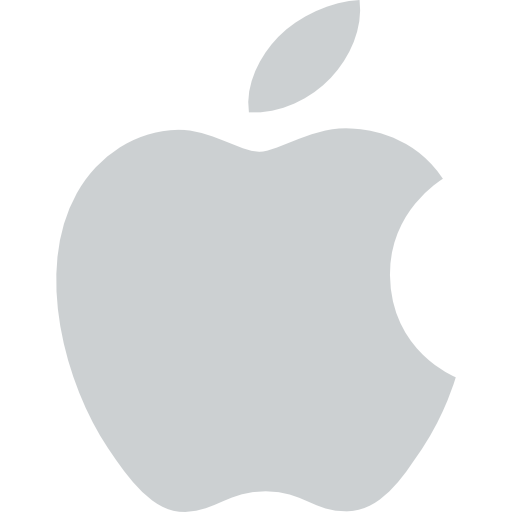अध्याय 05 जैव प्रक्रम
हम जैव (सजीव) तथा अजैव (निर्जीव) में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं? यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए अथवा गली में एक इन्सान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या इन्सान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं, लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें साँस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हममें से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियाँ हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में, हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है, जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु साँस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है।
अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, उदाहरण के लिएअणुओं की गतियाँ। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीवविज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति (जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं) नहीं होती है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं।
जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है; उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएँ होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ-साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएँ अणुओं से बनी होती हैं अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए।
सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए, खोजते हैं।
5.1 जैव प्रक्रम क्या है?
जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है, जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं।
क्योंकि क्षति तथा टूट-फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं।
चूँकि, पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एकसमान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रंखला की आवश्यकता है। उपचयन-अपचयन अभिक्रियाएँ अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है।
एक एक-कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान-प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएँ अपने आस-पास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकतीं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता।
हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न-भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है, यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन-तंत्र की आवश्यकता होती है।
जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुँचाने की होगी।
आइए, हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक-एक करके विचार करते हैं।
प्रश्न
1. हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है?
Show Answer
#missing2. कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे?
Show Answer
#missing3. किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है?
Show Answer
#missing4. जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे?
Show Answer
#missing5.2 पोषण
जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है।
सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं?
सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाईऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव-उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं।
5.2.1 स्वपोषी पोषण
स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है, जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौथे द्वारा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है? इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएँ होती हैं-

चित्र 5.1 एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट
(i) क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना।
(ii) प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन।
(iii) कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन।
यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, उदाहरण के लिए- मरुद्रिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है।
आइए, हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है।
यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे (चित्र 5.1) तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए, हम एक क्रियाकलाप करते हैं, जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।

चित्र 5.2 शबलित पत्ती (a) मंड परीक्षण से पहले (b) मंड परीक्षण के बाद
क्रियाकलाप 5.1
- गमले में लगा एक शबलित पत्ती (उदाहरण के लिए- मनीप्लांट या क्रोटन का पौधा) वाला पौधा लीजिए।
- पौधे को तीन दिन अँधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए।
- अब पौधे को लगभग छः घंटे के लिए सर्य के प्रकाश में रखिए।
- पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए। इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए।
- कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए।
- इसके बाद इसे एल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए।
- इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए, जब तक एल्कोहल उबलने न लगे।
- पत्ती के रंग का क्या होता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है?
- अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए।
- पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए।
- पत्ती के रंग (चित्र 5.2) का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए।
- पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?
अब हम अध्ययन करते हैं कि पौथे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र (चित्र 5.3) की चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान-प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान-प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएँ सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है।

(a)

(b)
चित्र 5.3(a) खुला तथा (b) बंद रंध्र
क्रियाकलाप 5.2
- लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे लीजिए।
- तीन दिन तक उन्हें अँधेरे कमरे में रखिए।
- अब प्रत्येक पौधे को अलग-अलग काँच-पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटैशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटैशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है।
- चित्र 5.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग-अलग बेलजार से ढक दीजिए।
- जार के तले को सील करने के लिए काँच-पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं, इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है।
- लगभग दो घंटों के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए।
- प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जाँच कीजिए।
- क्या दोनों पत्तियाँ समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं?
- घस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो?

चित्र 5.4 प्रायोगिक व्यवस्था (a) पोटैशियम हाइड्रोक्साइड के साथ (b) पोटैशियम हाइड्रोक्साइड के बिना
उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है?
अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है, जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं।
5.2.2 विषमपोषी पोषण
प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है, उदाहरण के लिए- यदि भोजन स्रोत अचल (जैसे कि घास) है, या गतिशील जैसे, हिरण है। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न-भिन्न है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफँदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव, पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरबेल, किलनी, जूँ, लीच और फीताकृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है।
5.2.3 जीव अपना पोषण कैसे करते हैं?
क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एककोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं, उदाहरण के लिए- अमीबा कोशिकीय सतह से अँगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका (चित्र 5.5) बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिकाद्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एककोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्ष्याभ की गति द्वारा पहुँचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं।

चित्र 5.5 अमीबा में पोषण
5.2.4 मनुष्य में पोषण
आहार नाल मूल रूप से मुँह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली है। चित्र 5.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है, उसका क्या होता है? हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं।
क्रियाकलाप 5.2
मंड का घोल ( ) दो परखनलियों ’ ’ तथा ’ ’ में लीजिए। - परखनली ’
’ में लार डालिए तथा दोनों परखनलियों को 20-30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। - अब प्रत्येक परखनली में कुछ बूँद तनु आयोडीन घोल की डालिए।
- किस परखनली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है?
- दोनों परखनलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में यह क्या इंगित करता है?
- यह लार की मंड पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है?
हम तरह-तरह के भोजन खाते हैं, जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे-छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दाँतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुँह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, जिसे लालारस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं, उसका दूसरा पहल, उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव-उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है, जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्ना भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है।
आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है।
मुँह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक बृहत अंग है, जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है।

चित्र 6.6 मानव पाचन तंत्र
ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को ‘एसिडिटी अथवा अम्लता’ की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है?
आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुट्रांत्र आहारनाल का सबसे लंबा भाग है, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुट्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्युलोज़ पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है। अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत्र छोटी होती है।
क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्न्याशय से स्रावण प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है, यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय अग्न्याशयिक रस का स्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है, जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज़ में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं।
पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक अँगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है।
बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिःक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
क्या आप जानते हैं?
दंतक्षरण
दंतक्षरण या दंतक्षय इनैमल तथा डैंटीन के शनैः-शनै: मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है, जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तब इनैमल मृदु या बिखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्यकणों के साथ मिलकर दाँतों पर चिपक कर दंतप्लाक बना देते हैं, प्लाक दाँत को ढक लेता है। इसलिए, लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुँच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे भोजनोपरांत दाँतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं।
प्रश्न
1. स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है?
Show Answer
#missing2. प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है?
Show Answer
#missing3. हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है?
Show Answer
#missing4. पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है?
Show Answer
#missing5. पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है?
Show Answer
#missing5.3 श्वसन
क्रियाकलाप 5.4
- एक परखनली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए।
- इस चूने के पानी में निःश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए [चित्र 5.7 (a)]।
- नोट कीजिए कि चूने के पानी को दधिया होने में कितना समय लगता है।
- एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परखनली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं [चित्र 5.7 (b)]।
- नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है।
- निःश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है?

चित्र 5.7
(a) चूने के पानी में नि:श्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है।
(b) चूने के पानी में पिचकारी/सिरिंज द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है।
क्रियाकलाप 5.5
- किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए। एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परखनली में इस मिश्रण को ले जाइए।
- कॉर्क में मुड़ी हुई काँच की नली लगाइए। काँच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली परखनली में ले जाइए।
- चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट कीजिए।
- किण्वन के उत्पाद के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है?
पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है कोशिकाएँ उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं- कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग, ग्लूकोज़ को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में, विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दसरे पथ (चित्र 5.8) का उपयोग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज़, एक छः कार्बन वाले अणु का तीन कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिकाद्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु (ऑक्सीजन) की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम तीन कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके तीन कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु (ऑक्सीजन) की उपस्थिति में होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी-कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है, यहाँ पायरुवेट एक अन्य तीन कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है।

चित्र 5.8 भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन
कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही ए.टी.पी. (ATP) नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। ए.टी. पी. के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मि (endothermic) क्रियाओं का परिचालन करती है।
यह भी जानिए!
ए.टी.पी.
अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ए.टी.पी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग ए.डी.पी. (ADP) तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ए.टी.पी. अणु बनाने में किया जाता है।
(P): फॉस्फेट
आंतरोष्मि प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी ए.टी.पी. का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद ए.टी.पी. में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो
के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है।
सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में ए.टी.पी. का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है।
क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान-प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतर्कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएँ वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान-प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में, जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान-प्रदान क्रिया है। दिन में, श्वसन के दौरान निकली
जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं, उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है।
क्रियाकलाप 5.6
- एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए। वे अपना मुँह खोलती और बंद करती रहती हैं। साथ ही आँखों के पीछे क्लोमछिद्र (या क्लोमछिद्र को ढकने वाला प्रच्छद) भी खुलता और बंद होता रहता है। क्या मुँह और क्लोमछिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है?
- गिनती करो कि मछली एक मिनट में कितनी बार मुँह खोलती और बंद करती है।
- इसकी तुलना आप अपनी श्वास को एक मिनट में अंदर और बाहर करने से कीजिए।
जो जीव जल में रहते हैं, वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुँह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुँचाती है, जहाँ विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है।
स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न-भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है, जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है।
क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर-पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है, उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है।
मनुष्य में (चित्र 5.9), वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो।
और अधिक जानें
तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटका आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआँ रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख कारक है। भारत में गुटका सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएँ बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहें बस तंबाकू से बने उत्पादों को न कहें!

चित्र 5.9 मानव श्वसन तंत्र
क्या आप जानते हैं?
धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वासनली के ऊपरी हिस्से में छोटी-छोटी बालों जैसी संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया साँस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआँ और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खाँसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं।
फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, इसके परिणामस्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
जैसे-जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, उन ऊतकों तक पहुँचाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है।
क्या आप जानते हैं?
- यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है।
- यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुँचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है।
प्रश्न
1. श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है?
Show Answer
#missing2. ग्लकोज़ के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं?
Show Answer
#missing3. मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है?
Show Answer
#missing4. गैसों के विनिमय के लिए मानव-फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है?
Show Answer
#missing5.4 वहन
5.4.1 मानव में वहन
क्रियाकलाप 5.7
- अपने आस-पास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है?
- क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है?
- क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है?
- अपने आस-पास के एक पशु चिकित्सा क्लीनिक का भ्रमण कीजिए। ज्ञात कीजिए कि पशुओं, जैसे भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है?
- क्या यह मात्रा बछड़ों में, नर तथा मादा जंतुओं में समान है?
- नर तथा मादा मानव में व जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए।
- यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे?
पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, इसमें कोशिकाएँ निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएँ ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपनयंत्र की आवश्यकता है, जो रुधिर को अंगों के आस-पास धकेल सके, नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है, जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट-फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके।
हमारा पंप-हदय
हृदय एक पेशीय अंग है, जो हमारी मुट्ठी के आकार (चित्र 5.10) का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर चित्र 5.10 मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बँटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है।

चित्र 5.10 मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य
हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों (चित्र 5.11) में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ- बायाँ अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायाँ अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायाँ निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायाँ निलय संकुचित होता है, तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायाँ कोष्ठ, दायाँ अलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायाँ अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ, दायाँ निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएँ निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं।
फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है।
हृदय का दायाँ व बायाँ बँटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बँटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में तीन कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल दो कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह दो बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं।

चित्र 5.11 ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण
यह भी जानिए!
रक्तदाब
रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रंकुचन (संकुचन) के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन (शिथिलन) के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लभगग
(पारा) तथा अनुशिथिलन दाब लगभग (पारा) होता है। 
स्फाईग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्रवण हो सकता है।
नलिकाएँ- रुधिर वाहिकाएँ
धमनी वे रुधिर वाहिकाएँ हैं, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हद्य से उच्च दाब से निकलता है। शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं।
किसी अंग या ऊतक तक पहुँचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी-छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आस-पास की केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। केशिकाएँ तब आपस में मिलकर शिराएँ बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं।
प्लेटलैट्स द्वारा अनुरक्षण
इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएँ और रक्तस्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलैट्स कोशिकाएँ होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं।
लसीका
एक अन्य प्रकार का द्रव है, जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसीका या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएँ बाहर निकलकर ऊतक के अंतर्कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसीका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्पमात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसीका अंतर्कोशिकीय अवकाश से लसीका केशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसीका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसीका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है।
5.4.2 पादपों में परिवहन
हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह
विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं, और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणामस्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती हैं।
पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित हैं। एक जाइलम है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा फ्लोएम, पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं।
जल का परिवहन
जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएँ तथा वाहिकाएँ आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएँ मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है।
जो हम आमतौर पर पादपों की ऊँचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊँचाई के बिंदु तक जल पहुँचाने की कोई और युक्ति करते हैं।
क्रियाकलाप 5.8
- लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मृदा वाले दो गमले लीजिए। एक में पौधा लगा दीजिए तथा दूसरे गमले में पौधे की ऊँचाई की एक छड़ी लगा दीजिए।
- दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए जिसमें नमी का वाष्पन न हो सके।
- दोनों गमलों को, एक को पौधे के साथ तथा दूसरे को छड़ी के साथ, प्लास्टिक शीट से ढक दीजिए।
- क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं?
यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है, उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है।
अतः वाष्पोत्सर्जन, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के उपरिमुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण, जाइलम में जल की गति के लिए, मुख्य प्रेरक बल होता है।

चित्र 5.12 एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति
भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण
अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह चित्र 5.12 एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में उपरिमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है।
जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में ए.टी.पी. से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है, जहाँ दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है, उदाहरण के लिए- बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
प्रश्न
1. मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं?
Show Answer
#missing2. स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है?
Show Answer
#missing3. उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं?
Show Answer
#missing4. पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है?
Show Answer
#missing5. पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है?
Show Answer
#missing5.5 उत्सर्जन
हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम, जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। बहुत से एककोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं।
5.5.1 मानव में उत्सर्जन
मानव के उत्सर्जन तंत्र (चित्र 5.13) में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है, जब तक मूत्रमार्ग से यह निकल नहीं जाता है।

चित्र 5.13 मानव उत्सर्जन तंत्र
मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फुफ्फुस में

चित्र 5.14 एक वृक्काणु की रचना
क्या आप जानते हैं?
कृत्रिम वृक्क (अपोहन)
उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग हैं। कई कारक, जैसे- संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह, वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पार्दों को रुधिर से अपोहन (dialysis) द्वारा निकालने की एक युक्ति है।

कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएँ अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनरवशोषण नहीं है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में एक या दो लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनरवशोषित हो जाता है।
क्या आप जानते हैं?
अंगदान
अंगदान एक उदार कार्य है, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है, जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। यह दान दाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता है। अंग और ऊतक दान में दान दाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति (दाता) के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति (ग्राही) के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थिमज्जा शामिल हैं। अधिकांशतः अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंगों, जैसे- गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है।
5.5.2 पादप में उत्सर्जन
पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों, जैसे- पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आस-पास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं।
प्रश्न
1. वृक्काणु (नेफ्रॉन) की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।
Show Answer
#missing2. उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं।
Show Answer
#missing3. मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है?
Show Answer
#missingआपने क्या सीखा
- विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है।
- जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक हैं।
- स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना है।
- विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है।
- मनुष्य में, खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांत्र में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है।
- श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज़ जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, जिससे ए.टी.पी. का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है।
- मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद सरीखे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएँ होती हैं।
- उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं।
- मनुष्य में, उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में वृक्काणु (नेफ्रॉन) द्वारा निकाले जाते हैं।
- पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए- अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं या गोंद व रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है या ये अपने आस-पास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं।
अभ्यास
1. मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो संबंधित है-
(a) पोषण
(b) श्वसन
(c) उत्सर्जन
(d) परिवहन
Show Answer
#missing2. पादप में जाइलम उत्तरदायी है-
(a) जल का वहन
(b) भोजन का वहन
(c) अमीनो अम्ल का वहन
(d) ऑक्सीजन का वहन
Show Answer
#missing3. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है-
(a) कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल
(b) क्लोरोफिल
(c) सूर्य का प्रकाश
(d) उपरोक्त सभी
Show Answer
#missing4. पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है-
(a) कोशिकाद्रव्य
(b) माइटोकॉन्ड्रिया
(c) हरित लवक
(d) केंद्रक
Show Answer
#missing5. हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है?
Show Answer
#missing6. भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है?
Show Answer
#missing7. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं?
Show Answer
#missing8. वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर हैं? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है।
Show Answer
#missing9. गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं?
Show Answer
#missing10. हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं?
Show Answer
#missing11. मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है?
Show Answer
#missing12. जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है?
Show Answer
#missing13. फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु (नेफ्रान) की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए।