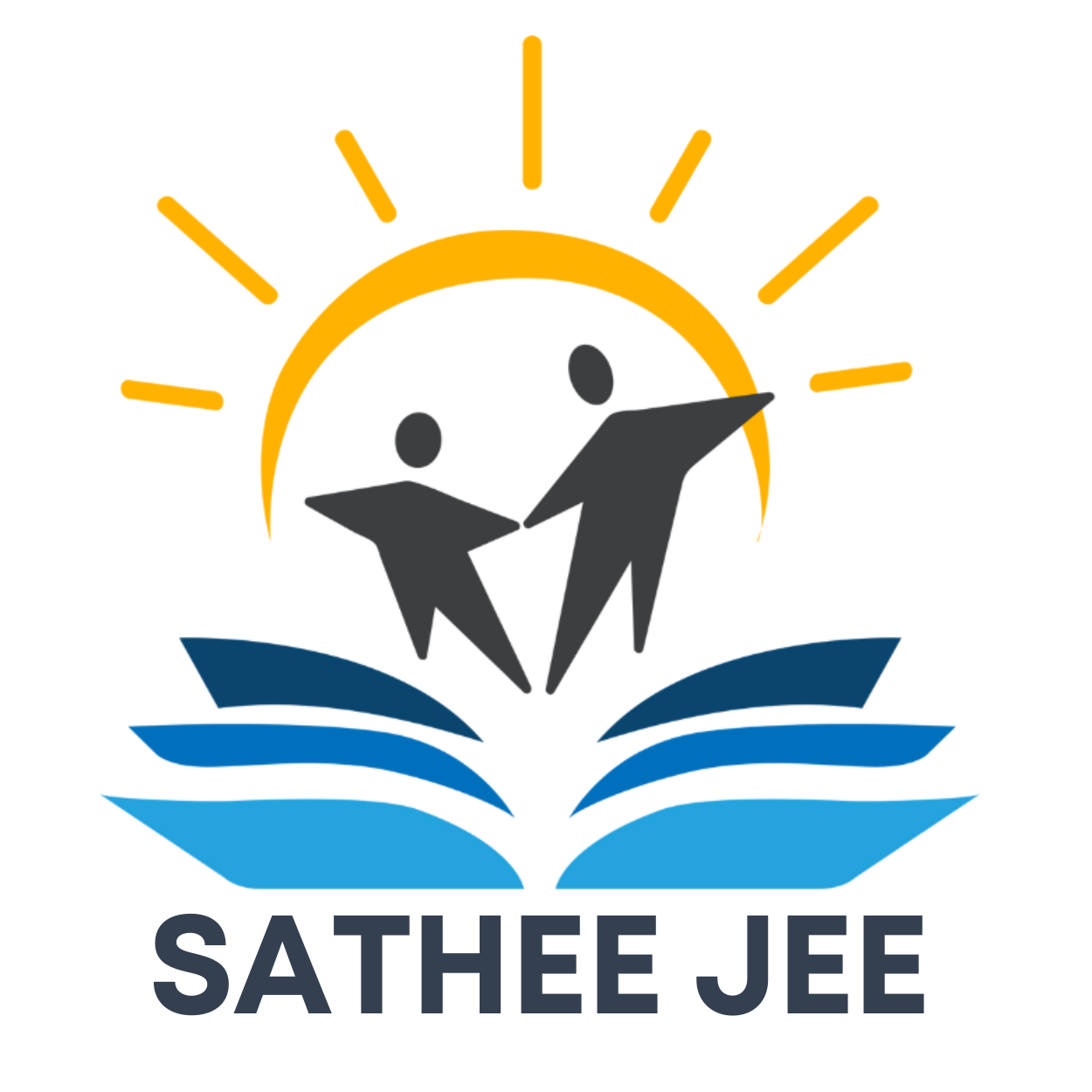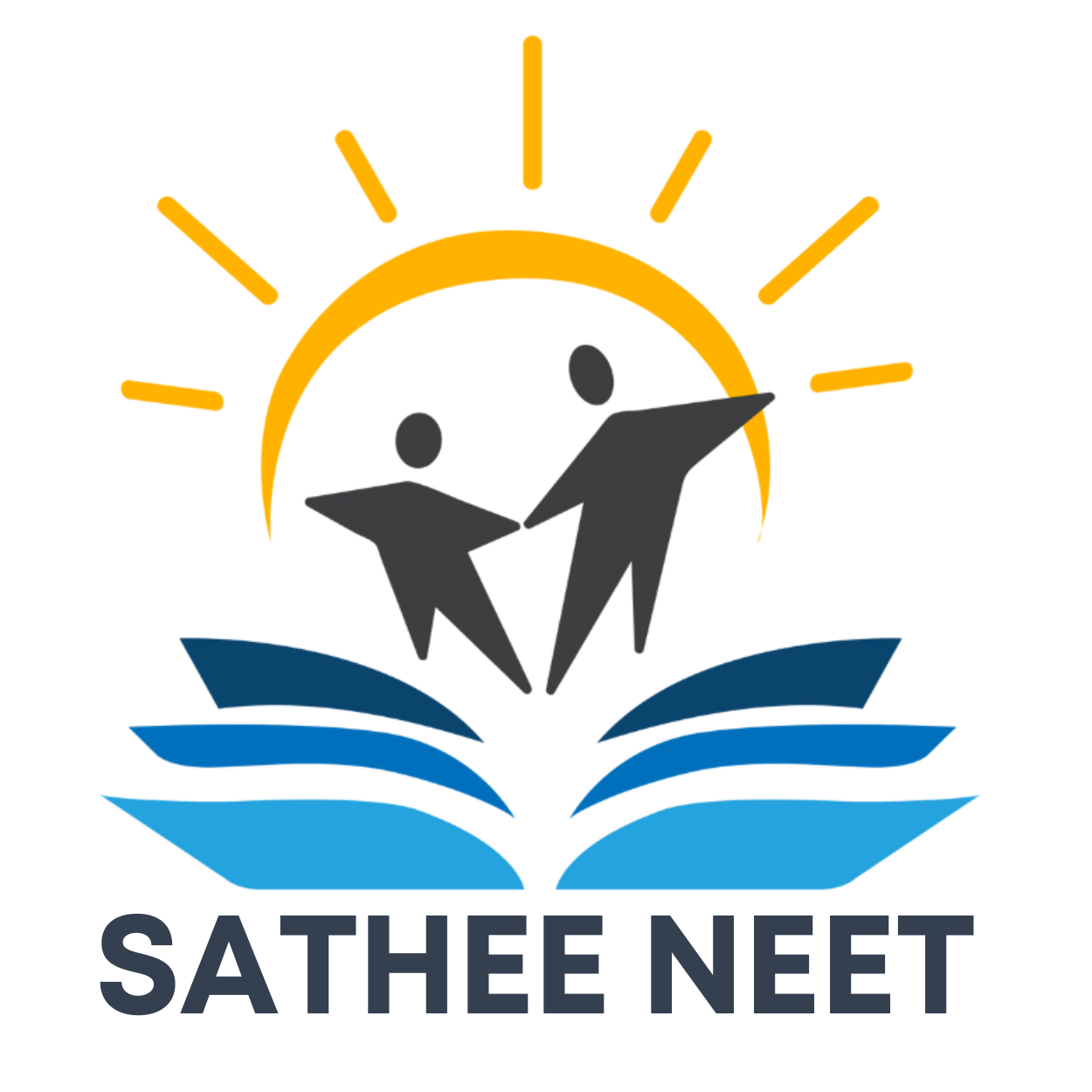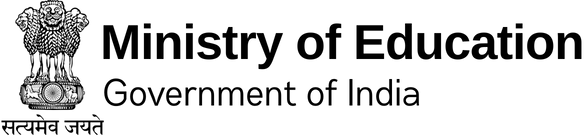अध्याय 04 वन्य समाज और उपनिवेशवाद
अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानें जो जंगल की हैं-इस किताब का कागज़, मेज़-कुर्सियाँ, दरवाज़े-खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफ़ेन रैपर, बीड़ियों के तेंदू पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्मशोधक (टैनिन) या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटियाँ-इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बाँस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएँ, फल-फूल, पशु-पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती हैं। ऐमेज़ॉन या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग-अलग प्रजातियाँ मिल जाती हैं।
यह विविधता तेज़ी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगीकरण के दौर में सन् 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3 प्रतिशत भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती-बाड़ी, चरागाहों व ईंधन की लकड़ी के साफ़ कर दिया गया।

चित्र 1 - यह छत्तीसगढ़ का एक साल वन है.
घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुँच पाती है। इस चित्र में आप पेड-पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियाँ देख सकते हैं।
1 वनों का विनाश क्यों?
वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन-विनाश कहते हैं। वन-विनाश कोई नयी समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए, भारत में वन-विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें।
1.1 ज़मीन की बेहतरी
सन् 1600 में हिंदुस्तान के कुल भू-भाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आँकड़ा बढ़ कर आधे तक पहुँच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गयी और खाद्य पदार्थों की माँग में भी वृद्धि हुई, वैसे-वैसे किसान भी जंगलों को साफ़ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेज़ी से फैलाव आया।

चित्र 2 - व्हेन द वैलीज़ वर फुल (जब घाटियाँ भरी पड़ी थीं)। जॉन डॉसन की पेंटंग.
लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह, जो इन विशाल उत्तर-अमेरिकी मैदानों में रहते थे, का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते, बीसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज़ आबादकारों ने बीसनों के विशाल भू-भाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई।
इसकी कई वजहें थीं। पहली, अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फ़सलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूँ व कपास के उत्पादन को जम कर प्रोत्साहित किया। उन्नीसवों सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के कच्चे माल की ज़रूरत थी।
बॉक्स 1
किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर-आबाद होना नहीं है। जब गारे आवादकार ऑस्ट्रेलिया पहुँचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में, ये आदिवासी पथ-प्रदर्शकों के नेतृत्व में, पुरातन रास्तों से इस भू-भाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगार्रिन्दज़ोरियों (Ngarrindjeri) को अपनी ज़मीन की आकृति इनके पहले पूर्वज, नगुरूनदेरी (Ngurunderi) के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह ज़मीन पाँच अलग-अलग प्राकृतिक प्रदेशों : खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदीतटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया करते थे।
लिहाज़ा इन फ़सलों की माँग में इजाफ़ा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य ज़मीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई।
स्रोत क
परती ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। यही वह विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया।
अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य-अमेरिका के हॉन्डूरास के बारे में लिखते हैं:
‘आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर-विकसित पड़ी ज़मीन का क्या किया जाए; क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए, जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। ये मध्य-अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध-बर्बरों के गिरोह जैसे हैं जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम।
तीन साल बाद अमेरिकी-आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य-अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें ‘बनाना रिपब्लिक’ के नाम से जाना गया।
डेविड स्पर, ‘द रेटरिक ऑफ़ एम्पायर’ (1993) में उद्धृत।
खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है।
1.2 पटरी पर स्लीपर

चित्र 3 - सिंहभूम के जंगलों में साल के तनों से ‘स्लीपरों’ का निर्माण, छोटा नागपुर, मई 1897.
रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन-विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति न थी।
नए शब्द
स्लीपरः रेल की पटरी के आर-पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं।
उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत (ओक) के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मज़बूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेज़ी जहाज़ भला कैसे बन सकते थे? और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी? 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन-संपदा का अन्वेषण करने के भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा।
1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के एक नई तरह की माँग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के रेल लाइनें अनिवार्य थीं। इंजनों को चलाने के ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के ‘स्लीपरों’ के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। एक मील लंबी रेल की पटरी के 1760-2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी।

चित्र 4 - बाँस के बेड़े कासालाँग नदी में बह कर जाते हुए, चिट्टागोंग पर्वतीय पद्टी.
भारत में रेल-लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेज़ी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 कि.मी. लंबी लाइनें बिछायी जा चुकी थीं। 1946 में इन लाइनों की लंबाई

चित्र 5 - रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के शहतीर सहेजता हुआ हाथी. औपनिवेशिक दौर में अकसर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदामों में भारो-भरकम लकड़ी को उठाने के किया जाता था।
स्रोत ख
‘मुल्तान और सुक्कूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनायी जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से, इसके 10 फुुट
इंच इंच (या 3.5 घन फ़ुट प्रति इकाई) के 600,000 स्लीपर की ज़रूरत होगी या कि क्यूबिक फ़ीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ़ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन-मील के हिसाब से सालाना मन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के भी भारी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन, सिंध और पंजाब के झाऊ (Tamarisk) और झांड (Jhand) के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नयी लाइन नॉर्दन स्टेट रेलवे, लाहैर से मुल्तान तक थी। आँकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के स्लीपर की ज़रूरत होगी।’ ई.पी.स्टेबिंग, द फ़ॉरैस्ट्स ऑफ़ इंडिया, भाग II (1923)।
क्रियाकलाप
एक मील लंबी रेल की पटरी के 1,760 से 2,000 तक स्लीपर की ज़रूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के एक औसत कद के पेड़ से 3-5 स्लीपर बन सकते हैं तो हिसाब लगा कर देखें कि एक मील लंबी पटरी बिछाने के कितने पेड़ काटने होंगे?

चित्र 6 - ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर को लौटती औरतें.

चित्र 7 - लट्ठे ले जाता हुआ ट्रक. लट्ठे काटने के किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन-उत्पाद इकड्ठा करने के जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों को जाते थे।
1.3 बागान
यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती माँग को पूरा करने के इन वस्तुओं के बागान बने और इनके भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ़ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे़ में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ़ कर दिया गया और चाय-कॉफ़ी की खेती की जाने लगी।

चित्र 8 - प्लेज़र ब्राँड चाय
2 व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत
पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज़ और रेल की पटरियाँ बिछाने के अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएँगे। इस उन्होंने डायट्रिच ब्रैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशविरे के बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया।
ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके कानूनी मंज़ूरी की ज़रूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगा कर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के आरक्षित किया जा सकेगा।
क्रियाकलाप
यदि 1862 में भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती और आप पर इतने व्यापक पैमाने पर रेलों के लिए स्लीपर और ईंधन आपूर्ति की ज़िम्मेवारी होती तो आप इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाते?

चित्र 9 - इटली स्थित टस्कनी में पोपलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा. पोपलर के जंगल मुख्यत: लकड़ी के लिए महत्त्व रखते हैं। पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए ये उपयोगी नहीं हैं। एक समान लंबाई वाले और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें। यही वह मॉडल है जिसे ‘वैज्ञानिक’ वानिकी ने प्रोत्साहित किया।

चित्र 10 - काँगड़ा का एक देवदार बागान, 1933. इंडियन फ़ारेस्ट रिकॉर्डस्, भाग XV से ।
इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सज़ा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इम्पीरियल फ़ॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे ‘वैज्ञानिक वानिकी’ (साइंटफ़िक फ़ॉरेस्ट्री) कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है।
वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप-जोख की और वन-प्रबंधन के योजनाएँ बनायीं। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली ज़मीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के तैयार हो जाए।

चित्र 11 - दि इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, भारत. ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल। स्रोत: इंडियन फ़ररेस्टर, खण्ड XXXI.
1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें दो बार संशोधन किए गए - पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया : आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को ‘आरक्षित वन’ कहा गया। गाँव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे।
नया शब्द
वैज्ञानिक वानिकी : वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं।
2.1 लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ?
एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे।

चित्र 12 - जंगलों से महुआ (Madhuca Indica) बीनना. गाँव वाले उजाला होने के पहले ही उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के जंगल चले जाते। महुआ के पेड़ बेशकीमती हैं। महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के भी किया जा सकता है। इसके बीजों से तेल भी बनाया जाता है।
जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग-अलग ज़रूरतों, जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन-विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के इमारती लकड़ी मुहैया करा सकें, ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबो और सीधी हों। इस सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गईं।
वन्य इलाकों में लोग कंद-मूल-फल, पत्ते आदि वन-उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मॉनसून के दौरान जब फ़सल कट कर घर न आयी हो। दवाओं के जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल होता है, लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औज़ार बनाने में किया जाता है, बाँस से बेहतरीन बाड़ें बनायी जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है - पत्तों को जोड़-जोड़ कर ‘खाओ-फेंको’ किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं, सियादी (Bauhiria vahili)की लताओं से रस्सी बनायी जा सकती है, सेमूर (सूती रेशम) की काँटेदार छाल पर सब्ज़याँ छीली जा सकती हैं, महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है।

चित्र 13 - सूखते हुए तेंदू-पत्ते. जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएँ और वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठे करते हैं।

चित्र 14 - खलिहानों से अनाज लाते हुए. खलिहानों से पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधों के आर-पार एक छड़ी में बंधी टोकरियों को लाते हैं जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रख कर लाती हैं।
क्रियाकलाप
वन-प्रदेशों में रहने वाले बच्चे पेड़-पौधों की सैकड़ों प्रजातियों के नाम बता सकते हैं। आप पेड़-पौधों की कितनी प्रजातियों के नाम जानते हैं?
वन अधिनियम के चलते देश भर में गाँव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद-मूल-फल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की गतिविधियाँ गैरकानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में के वन-रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगीं। मुफ़्त खाने-पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के सामान्य बात थी।
2.2 वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई?
यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखायी पड़ता है। एशिया, अफ़ीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं जैसे दक्षिण-पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिलपा, अफ़ीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के धया, पुंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं।
घुमंतू कृषि के जंगल के कुछ भागों को बारी-बारी से काटा और जलाया जाता है। मॉनसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्तूबर-नवंबर में फ़सल काटी जाती है। इन खेतों पर दो-एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के परती छोड़ दिया जाता है जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फ़सलें उगायी जाती हैं जैसे मध्य भारत और अफ़ीका में ज्वार-बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियाँ।

चित्र 15 - टौंग्या खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ किसानों को कुछ समय के बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीज़न से गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बाँसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे। औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थीं।
यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछेक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो ऐसी ज़मीन पर रेलवे के इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते।

चित्र 16 - जंगल के पेंदा या पोदू हिस्सों को जलाना. घुमंतू खेती में जंगलों को साफ़ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है।
साथ ही, जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इस सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणामस्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे-बड़े विद्रोहों के ज़रिए प्रतिरोध किया।
2.3 शिकार की आज़ादी किसे थी?
जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे-मोटे शिकार करके जीवनयापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर-कानूनी हो गयी। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा।
जहाँ एक तरफ़ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहज़ादों और सम्राटों को शिकार का मज़ा लेते हुए दिखाया गया है।

चित्र 17 - मछली मारने वाला लड़का. बच्चे अपने माँ-बाप के साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, वन-उत्पदों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते हैं। बाँस के ट्रैप को, जिसे यह लड़का अपने बाएँ हाथ में पकड़े है, बहाव के मुहाने पर रखने पर मछली इसमें चली आती है।

चित्र 18 - नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग. फ़ोटो में मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफ़सर और राजा जब शिकार के जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फ़ौज होती थी। गाँव के कुशल शिकारी हाँका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था।
किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियाँ लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। अग्रेज़ों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक-चिन्न थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार कर वे हिन्दुस्तान को सभ्य बनाएँगे। बाघ, भेड़िये और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कह कर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ,
स्रोत ग
बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गयी तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी:
‘हर रोज़ हम फ़ाका करते हैं, क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ़ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुज़ारते हैं। हम अब खाने के मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती? कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता है, लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती।
वेरियर एल्विन (1939); माधव गाडगिल व रामचन्द्र गुहा, ‘दिस फ़िशर्ड लैंड: एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया’ में उद्धृत।
2.4 नए व्यापार, नए रोज़गार और नई सेवाएँ
जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़ कर वन-उत्पदों का व्यापार करने लगे। महज़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के , उन्नीसवीं सदी के मध्य में ऊँची जगहों पर रह कर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली ऐमेज़ॉन के मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के जंगली रबड़ के वृक्षों से ‘लेटेक्स’ एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए।
हिंदुस्तान में वन-उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोये, हाथी-दाँत, बाँस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं।
स्रोत घ
पुतुमायो में रबड़ की निकासी
दुनिया भर में, बागानों में काम की स्थितियाँ भयावह थीं। ऐमेज़ॉन के पुटुमायो क्षेत्र में ‘पेरूवियन रबड़ कंपनी’ (ब्रिटिश व पेरूवियन साझे में) द्वारा रबड़ की निकासी हुईतोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। 1900-1912 के बीच पुटुमायो में 4,000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आयी। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया है कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया:
उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से ज़मीन ढक गयी। खून से नहाए हुए, दया की भीख माँगते जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया और मैनेजर चिल्लाया, " “मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूँ जो रबड़ लाने के दिए गए मेरें आदेश को नहीं मानते हैं।”
निकोलस डर्स्स (सं.) कॉलोनियलिज्म ऐन्ड कल्चर (1992) में माइकेल ताउसिग, ‘कल्चर ऑफ़ टेरर-स्पेस ऑफ़ डैथ’।
लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन-उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गईं। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसीडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को ‘अपराधी कबीले’ कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फ़ैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए।
काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के झारखंड के संथाल और उराँव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों, दोनों की भर्ती की गयी। उनकी मज़दूरी बहुत कम थी और कार्यपरिस्थितियाँ उतनी ही खराब। उन्हें उनके गाँवों से उठा कर भर्ती तो कर लिया गया था लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी।
नया शब्द
इजारेदारी: एकाधिकार।
3 वन-विद्रोह
हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ़ बगावत की। संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे।
3.1 बस्तर के लोग
बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इन्द्रावती नदी बस्तर के आर-पार पूरब से पश्चिम की तरफ़ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग-अलग ज़बानें बोलने के बावजूद इनके रीति-रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हरेक गाँव को उसकी ज़मीन ‘धरती माँ’ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गाँव को अपनी चौहद्दी पता होती है इस ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं।

चित्र 19 - बस्तर में सेना का कैंप 1910. बस्तर में सेना के एक कैंप का यह चित्र 1910 में लिया गया। संना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। चहाँ एक सिपाही विद्रोहियों से सुर्क्षा के कैंप की पहरेदारी कर रहा है।

चित्र 20 - सन् 2000 में बस्तर. 1947 में बस्तर रियासत को काँकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस ज़िले को एक बार फिर काँकेर, बस्तर और दांतेवा़ा़ जिलों में बाँट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह काँकेर वन क्षेत्र (घेरे में) से हो शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया।
यदि एक गाँव के लोग दूसरे गाँव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी, दांड़ या मान कहा जाता है। कुछ गाँव अपने जंगलों की हिफ़ाज़त के चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा-थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहाँ एक परगने (गाँवों का समूह) के गाँवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
3.2 लोगों के भय
औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के दो-तिहाई हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य-उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गाँवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन-विभाग के पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गाँवों को ‘वन ग्राम’ कहा जाने लगा। बाकी गाँवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवज़े के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गाँव वाले ज़मीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफ़सरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर माँग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया : पहले 1899-1900 में और फिर 1907-1908 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया।
स्रोत च
‘भेड़िया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ़ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के चल पड़ा। 10 फ़रवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस-चौकी तथा मारेंगा स्कूल जला दिया, केसलुर में लाईनें व पशु-अवरोधशाला और टोकापाल (राजुर) में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के भेजे गए स्टेट रिज़्र्र पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के दिलमिल्ली चले गए। बुद्ध माझी और हरचंद नाईक ने मुख्य दल की कमान सँभाली।’
डेब्रेट, पोलिटिकल एजेन्ट, छत्तीसगढ़ फ़्यूडेटरी स्टेट्स, का 23 जून, 1910 को कमिश्नर, छत्तीसगढ़ डिवीज़न, के नाम लिखा पत्र।
लोगों ने बाज़ारों में, त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गाँवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। काँगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालाँकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गाँव के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गाँव-गाँव चक्कर काटने लगे। यह गाँवों में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बगावत का संदेश था। हरेक गाँव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाज़ार लूटे गए, अफ़सरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह, मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा : ‘पुलिसवालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ़ से जगदलपुर में चला आ रहा था।’
अंग्रेज़ों ने बगावत को कुचल देने के सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाही लेकिन अंग्रेज़ फ़ौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियाँ चला दीं। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सज़ा देते सैनिक गाँव-गाँव घूमने लगे। ज़्यादातर गाँव खाली हो गए क्योंकि लोग भाग कर जंगलों में चले गए थे।
स्रोत छ
बस्तर में रहने वाले बुज़ुर्गा इस लड़ाई के बारे में, जिसे उन्होंने अपने माता-पिता से सुना था, बताते हैं :
कनकापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकेली ने बताया कि:
‘अंग्रेज़ों ने आकर ज़मीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न थी, इस ज़मीन ली जा रही है, यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई। उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेंरे पिता, पोदियामी तोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया। लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के था। अंग्रेज़ उनको घोड़ों से बाँध कर घसीटा करते थे। हरेक गाँव से दो-चार लोग जगदलपुर गए - चिदपाल के गार्गी देवा और मिखोला, माकी-मिरास के दोल और अबराबुंदी, बालेरास का वादापांदु, पालेम का उंगा और दूसरे ढेर सारे लोग।’
इसी तरह से नंदरासा के एक बुज़ुर्ग चेंद्रू ने कहा कि :
‘लोगों की तरफ़ पुरनिया थे — पालेम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोयेकाल धुर्वा और पंडवा माझी। हर परगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा धूर उड़ सकते थे इस उड़ निकले। लेकिन तीर-कमान वाले अब क्या करें? रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिप कर पेट के बल भागे। फ़ौज की पलटन भी भागी। जो लोग ज़िंदा बचे किसी तरह अपने गाँव-घर पहुँचे।’
अंग्रेज़ों को फिर से नियंत्रण पाने में तीन महीने (फ़रवरी-मई) लग गए। फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया।
बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में, विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज़ उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के 4,600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएँ। लेकिन, स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया।
आइए, अब एशिया के एक और हिस्से - इंडोनेशिया - की तरफ चलें। ज़रा देखें कि इसी वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था।
4 जावा के जंगलों में हुए बदलाव
जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल-उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएँ थीं। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहाँ डचों ने वन-प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की तरह वे भी जहाज़ बनाने के जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन् 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालाँकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गाँव थे लेकिन पहाड़ों में भी घुमतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे।
4.1 जावा के लकड़हारे
जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्त्व इस बात से आँका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बँटी तो यहाँ के 6,000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर-बराबर बाँट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब अठारहवीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्ररांभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया।
4.2 डच वैज्ञानिक वानिकी
उन्नीसवीं सदी में जब लोगों के साथ-साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना ज़रूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन-कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुँच पर बंदिशें थोप दीं। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के , सिर्फ़ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुज़रने वाली सड़क पर घोड़ा-गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़ कर आने-जाने के दंडित किया जाने लगा।

चित्र 21 - जंगल से सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी, औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर.
भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज़ और रेल-लाइनों के निर्माण ने वन-प्रबंधन और वन-सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। ज़्राहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गाँवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैन्डाँगडिएन्स्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन-ग्रामवासियों को लगान-माफ़ी के बजाय थोड़ा-बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा लेकिन वन-भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए।
4.3 सामिन की चुनौती
सन् 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रान्दुब्लातुंग गाँव के निवासी सुरोन्तिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूँकि हवा, पानी, ज़मीन और लकड़ी राज्य की बनायी हुई नहीं हैं इस उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब ज़मीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी ज़मीन पर लेट कर इसका विरोध किया जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया।
स्रोत ज
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफ़सर डर्क वॉन होज़ेनड्राप ने उपनिवेश कालीन जावा में कहा था: ‘बटाविया के लोगो! चौंक पड़ो। आश्चर्य से सुनो, मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है- उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धँसी है, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के पर्याप्त लकड़ी है, साथ ही जितनी ज़रूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के भी - इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देख-रेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे।
डर्क वॉन होज़ेनडॉर्प; पेलूसो, रिच फ़ॉरैस्ट्स, पुअर पीपुल, 1992 में उद्धृत।

चित्र 22 - इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, कालिमांतान व पशिचम इरियान में स्थित हैं। जावा ही वह जगह है जहाँ उचों ने अपनी ‘वैज्ञानिक वानिकी’ की शुुआत की थी। यह द्वीप जो अब चावल उत्पादन के मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था।
4.4 युद्ध और वन-विनाश
पहले और दूसरे विश्वयुद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्ययोजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्ज़े से ठीक पहले डचों ने ‘भस्म-कर-भागो नीति’ (Scorched Earth Policy) अपनायी जिसके तहत आरा-मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाएँ। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गाँव वालों ने इस अवसर का लाभ उठा कर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के इन ज़मीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियन्त्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की ज़िद के बीच टकराव पैदा हुआ।

चित्र 23 - इंडियन म्यूनिशन्स बोर्ड, सूले पैगोड़ा पर एकत्रित जहाज़ों में लादने को तैयार वॉर टिम्बर स्लीपर, 1917. पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते। दोनों विश्वयुद्धों का हिंदुस्तान, इडोनेशिया व दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्ययोजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के जमकर वृक्ष काटे।
4.5 वानिकी में नए बदलाव
अस्सी के दशक से एशिया और अफ़्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार-बार टकराव पैदा होते हैं। परिणामस्वरूप, वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिज़ोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इस बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडु, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझ कर इनकी रक्षा की। कुछ गाँव तो वन-रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं - इसमें हर परिवार बारी-बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन-समुदाय और पर्यावरणविद् अब वन-प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं।

चित्र 24 - डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रेमबैंग में लट्ठों का गोदाम.
क्रियाकलाप
1. जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ के जंगली इलाकों में कोई बदलाव आए हैं? ये बदलाव क्या हैं और क्यों हुए हैं?
2. एक औपनिवेशिक वनपाल और एक अदिवासी के बीच जंगल में शिकार करने के मसले पर होने वाली बातचीत के संवाद लिखें।
प्रश्न
1. औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया :
-
झूम खेती करने वालों को
-
घुमंतू और चरवाहा समुदायों को
-
लकड़ी और वन-उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को
-
बागान मालिकों को
-
शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज़ अफ़सरों को
2. बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएँ हैं?
3. सन् 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आयी। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताएँ :
-
रेलवे
-
जहाज़ निर्माण
-
कृषि-विस्तार
-
व्यावसायिक खेती
-
चाय-कॉफ़ी के बागान
-
आदिवासी और किसान
4. युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं?