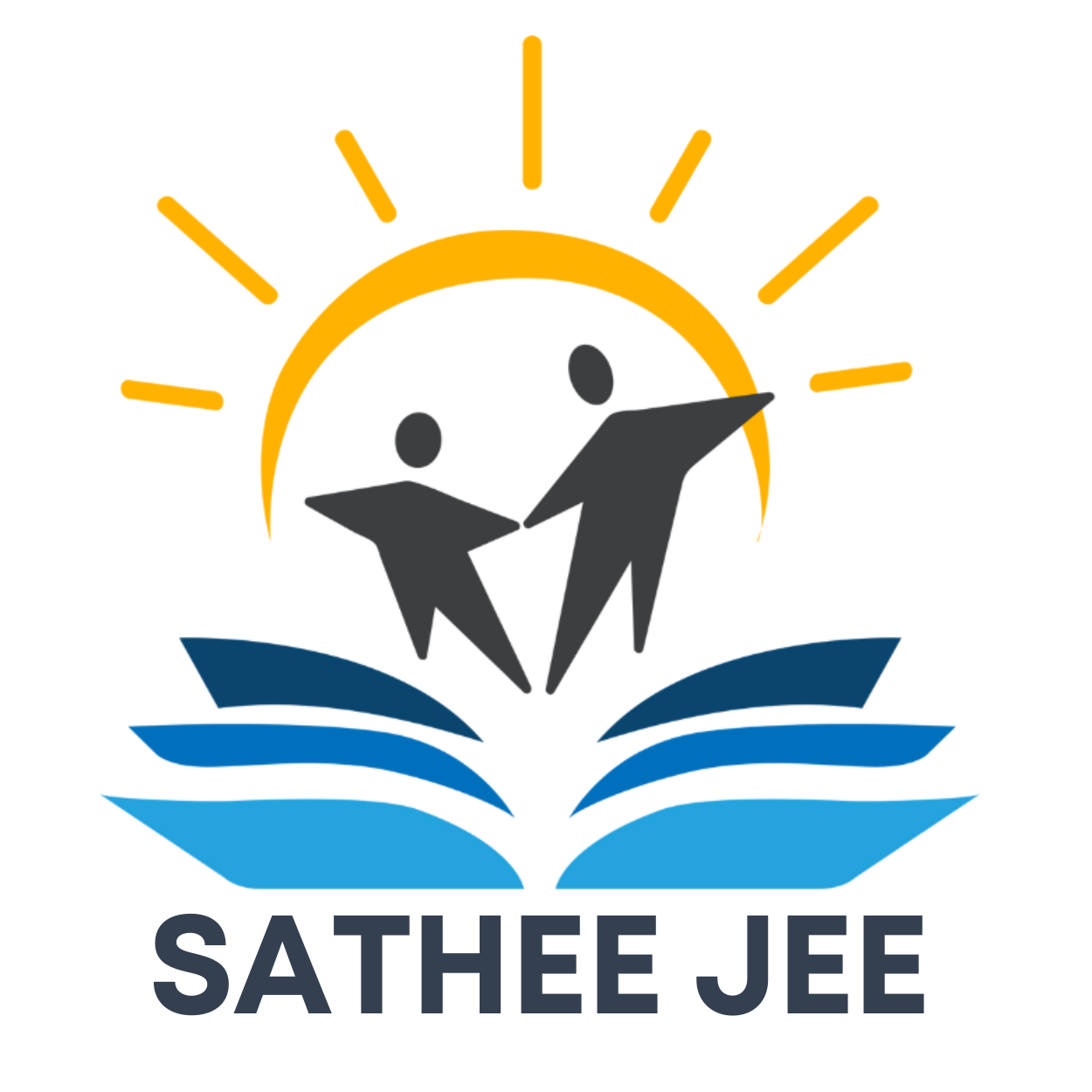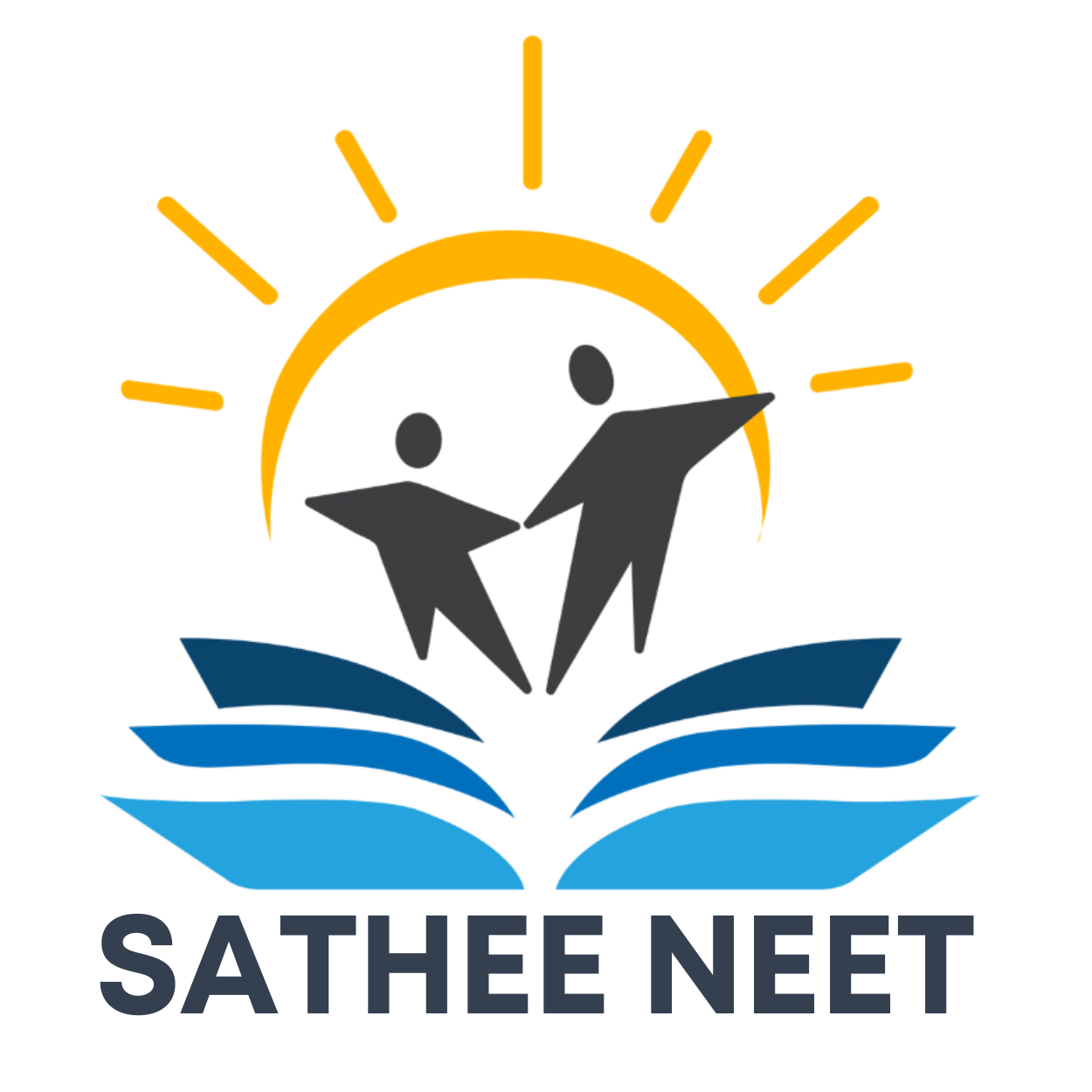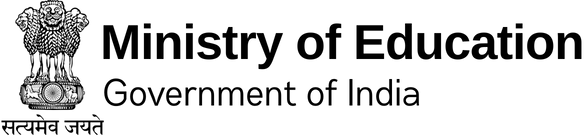अध्याय 06 अंतिम दौर - एक
भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है
भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नयी घटना थी जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बँधा था जिसका संचालन-केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था।
नया पूँजीवाद सारे विश्व में जो बाज़ार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढाँचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहों था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढाँचे का औपनिवेशिक और खेतिहर पुछल्ला बन कर रह गया।
अंग्रेज़ों ने अपने अंग्रेज़ी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक-से-अधिक रुपया, जल्दी-से-जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना ज़रूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेज़ों के स्वार्थ से अभिन्न हों।
ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में ज़मींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गाँव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे-मालगुज़ारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर ज़िले में कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी था।
इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए, अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया, इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को ‘कैपिटेशन चार्ज’ कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे।
उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी, इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमज़ोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है।
भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध
राममोहन राय - बंगाल में अंग्रेज़ी शिक्षा और समाचार पत्र
व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज़ों ने जिनमें शिक्षाविद्, प्राच्य-विद्या विशारद्, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेज़ी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेज़ों को ही है, जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापंसद करने के बावजूद, खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे-धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी, फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियाँ और दरवाज़े खोल दिए। धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ।
यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर हुआ। नयी तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके - यह सब ऐसी बातें थीं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतिहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान वैयक्तिक संपत्ति और ज़मींदारी ने ले लिया। मुद्रा-केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और ज़मीन बिकाऊ वस्तु हो गई।
देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन पचास वर्ष पहले स्थापित हो चुका था।
अट्ठारहवीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राममोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फ़ारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू-मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेज़ी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएँ सीखीं। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राममोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक साँचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक-विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव-विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए लिखा था।
इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उसके साथ संबद्ध हो
गयी थीं। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी।
राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन् 1780 के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था 1818 में अंग्रेज़ी में निकला था। उसी वर्ष श्रीरामपुर के बैपटिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक के बाद एक अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता (कोलकाता), मद्रास (चेन्नई) और बंबई (मुंबई) से अखबार और पत्रिकाएँ बड़ी तेज़ी से निकलने लगीं।
राममोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राममोहन राय दिल्ली-सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई।
सन् 1857 की महान क्रांति - जातीयतावाद
ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत, बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान, नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेज़ी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में मद्रास और मुंबई में थी। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश-विरोधी भावना खूब फैली थी।
मई सन् 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफ़िया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेज़ी से प्रसार हुआ और इसने जनांदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जनांदोलन के रूप में यह दिल्ली, संयुक्त प्रांत (जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है) मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलत: यह सामंतीय विस्फोट था, जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी-विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इनके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया।
इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था।
इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तांत्या टोपे जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेज़ों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सबके अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का है,
जो बीस वर्ष की आयु में लड़ते-लड़ते मारी गई। जिस अंग्रेज़ जनरल ने उसका मुकाबला किया उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में ‘सर्वोत्तम और सबसे बहादुर’ थी।
विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छप कर पहुँच पाई। सावरकर ने लगभग तीस वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ़ द वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल ज़ब्त कर ली गई और अब भी ज़ब्त है।
इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह नए सिरे से संगठित हुई।
हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन
तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट उन्नीसवीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज़ के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति-रिवाजों से खिन्न होकर, बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म-परिवर्तन कर लिया। राजा राममोहन राय ने हिंदू ‘ब्रह्म-समाज’ की स्थापना समाज-सुधारवादी आधार पर की। उनके बाद केशवचंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा।
भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढाँचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत
महत्त्वपूर्ण सुधार-आंदोलन की शुरुआत की लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था ‘वेदों की ओर लौटो।’ इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य-धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के-लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊँचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया।
लगभग स्वामी दयांनद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व समाने आया और नए पढ़े-लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे श्रीरामकृष्ण परमहंस थे। वे सीधे-सादे, विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्मसाक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्रीरामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे-धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए, उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था। फिर भी वे भारत के बहुरंगी साँचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन-कथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग में रोम्यां रोला थे, जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी।
विवेकानंद ने अपने गुरु-भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का
आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। वे बंगला और अंग्रेज़ी के ओजस्वी वक्ता थे और बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे-रोबीले, शालीन और गरिमावान। उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। 1893 ई. में उन्होंने शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म-सम्मेलन में भाग लिया। अमरीका में एक वर्ष से अधिक बिताया, यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुंतुनिया तक की और मिस्न, चीन और जापान भी गए। जो एक बार इस हिंदू संन्यासी को देख लेता था, उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, वे अंग्रेज़ों की लगन और अमरीकी लोगों की जीवंतता और समभाव के प्रशंसक थे। लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती हो गई।
उन्होंने वेदांत के अद्वैत-दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण-व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म-कांड के निरर्थक तात्विक-विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की-विशेषकर ऊँची जाति की छुआछूत की।
विवेकानंद ने बहुत-सी बातें कहीं लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा, वह थी ‘अभय’-निडर रहो। उनके अनुसार “अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है-हर तरह की दुर्बलता से बचो, दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी।” और सत्य की कसौटी है - “कोई भी चीज़ जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है, उसे ज़हर की तरह छोड़ दो, उसमें कोई जीवन नहीं है वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य
मज़बूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है।” “अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूँगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है …”
इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आपको खपा दिया। सन् 1902 में उनतालीस वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई।
विवेकानंद के ही समकालीन थे रवींद्रनाथ टैगोर। किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया था। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊँचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रवींद्रनाथ का स्थान इन सबसे ऊँचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे किंतु वे इतने संवदेनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। बीसवीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने ‘सर’ का खिताब लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था, उसने ‘शांति निकेतन’ को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव, विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नयी पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीयतावादी थे। अंतरराष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण, वे भारत के संदेश को दूसरे देशों में ले जाते रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओत-प्रोत था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे, विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना के। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी
ने की थी। अर्थात् उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे।
बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानताओं और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिज़ाज में एक-दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे, जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। गांधी, जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार

गांधी और टैगोर
रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों की, अपने-अपने ढंग की विश्वदृष्टि थी और इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग-अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक-दूसरे के पूरक थे।
अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती ऐनी बेसेंट का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। उदीयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था। कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उस नैराश्य
और अपमान के बोध को कम करता, जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश, अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है-हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों की भी और उन्हीं के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। बाद में दूसरे मतों में धर्म-परिवर्तन कर लेने के कारण, वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते।
प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। राममोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। एक ओर उन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसपान किया वहीं दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और शूरवीरों के विचारों और कार्यों से और उन पुरागाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था।
इसमें से बहुत-सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थीं। वे लोग परंपराओं से भलीभाँति परिचित थे। लेकिन धीरे-धीरे, विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्द्ध-धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई।
गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़ें। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग या बुर्जुआ वर्ग पैदा होता है। सन् 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। फिर भी, इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खाँ की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। वे इस बात के लिए बहुत
उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेज़ी शिक्षा को स्वीकार कर लें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था, उसका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से ज़ाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा-सा गया था।
सर सैयद उत्साही सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता ज़रूरी मालूम होती थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की और उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की, उसका एक घोषित उद्देश्य था, ‘भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना।’ वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे, उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रज़ों की सहायता और सहयोग चाहते थे। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफ़ादार रहे। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। उन्होंने कहा - याद रखो ‘हिंदू’ और ‘मुसलमान’ ये शब्द सिर्फ़ धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं - वरना सब लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, यहाँ तक कि ईसाई भी, जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं।
सर सैयद अहमद खाँ का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था, उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेज़ी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस शुरू की गई और उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया।
यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शमिल हैं, सभी ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी, हाँ उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेज़ी का ज्ञान हासिल कर लिया। नयी पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया।
वर्ष 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उस साल दो नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए - उर्दू में अल-हिलाल और अंग्रेज़ी में द कॉमरेड। अल-हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद (कांग्रेस के वर्तमान सभापति) ने किया। ये चौबीस वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो पंद्रह से बीस वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फ़ारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहाँ चल रहे थे। उन्होंने धर्म-ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए।
उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे।
आज़ाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी, गोकि कभी-कभी वह फ़ारसी पृष्ठभूमि के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती थी। नए विचारों के लिए उन्होंने नयी शब्दावली का प्रयोग किया और उर्दू भाषा जैसी आज है, उसे यह रूप देने में उनका निश्चित योगदान था। उनमें मध्ययुगीन पंडिताऊपन, अट्ठारहवीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था।
अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खाँ से उनका संबंध रहा था। लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थी। अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्ष्य रखते थे, वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। इसके लिए सरकार-समर्थक रवैया अनिवार्य था और राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों
का नेतृत्व कर रहा था और कभी-कभी प्रकट रूप से, पर अधिकतर परदे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई।
अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातनपंथी और राष्ट्रविरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा की, यद्यपि बुज़ुर्गों ने उन पर भौहें चढ़ाईं पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा कर दी।
तिलक और गोखले
नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन् 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्यवर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल-विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभरकर आए। लेकिन इसके सच्चे प्रतीक, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूँज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुज़ुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्त्व काफ़ी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियाँ सामने आ रही थीं।