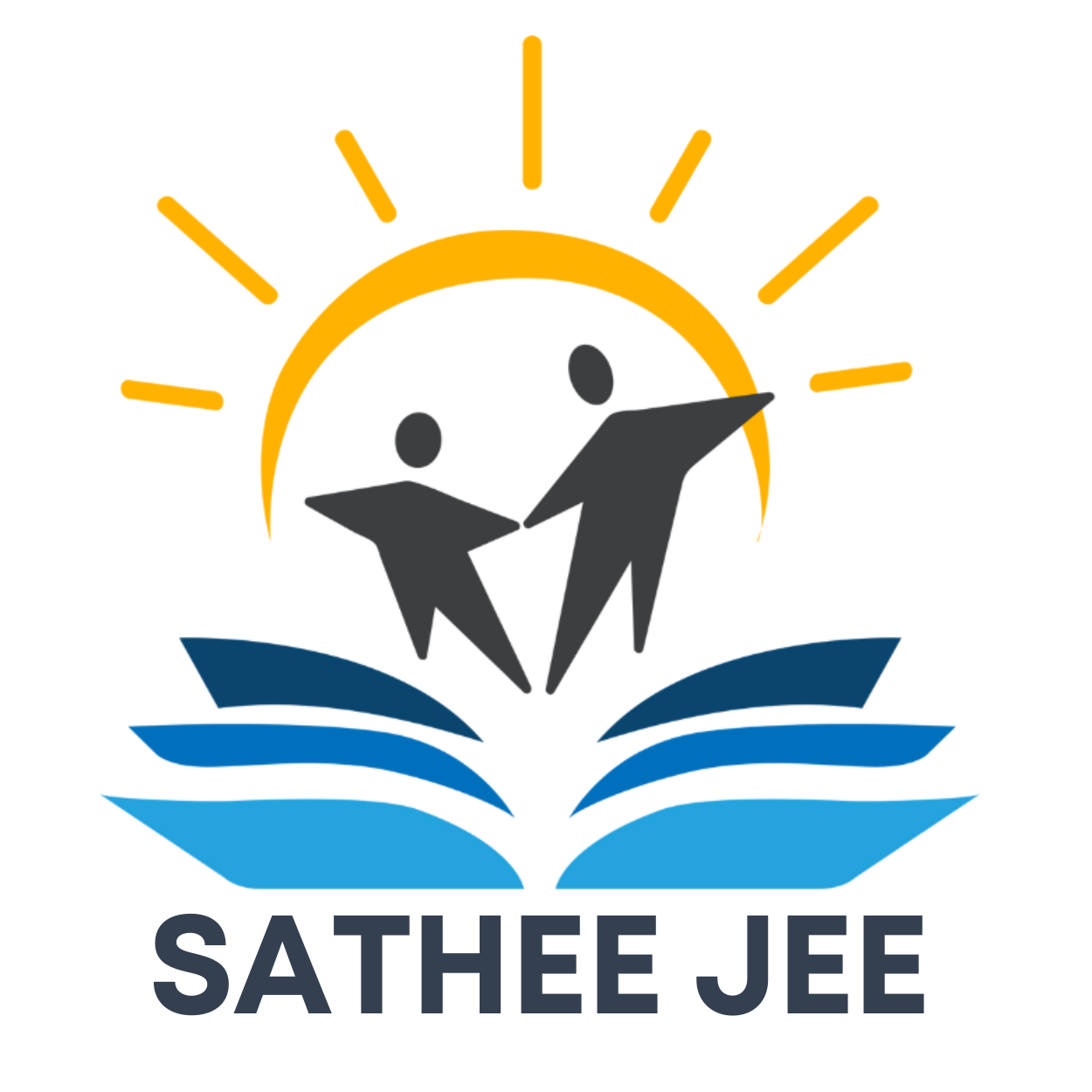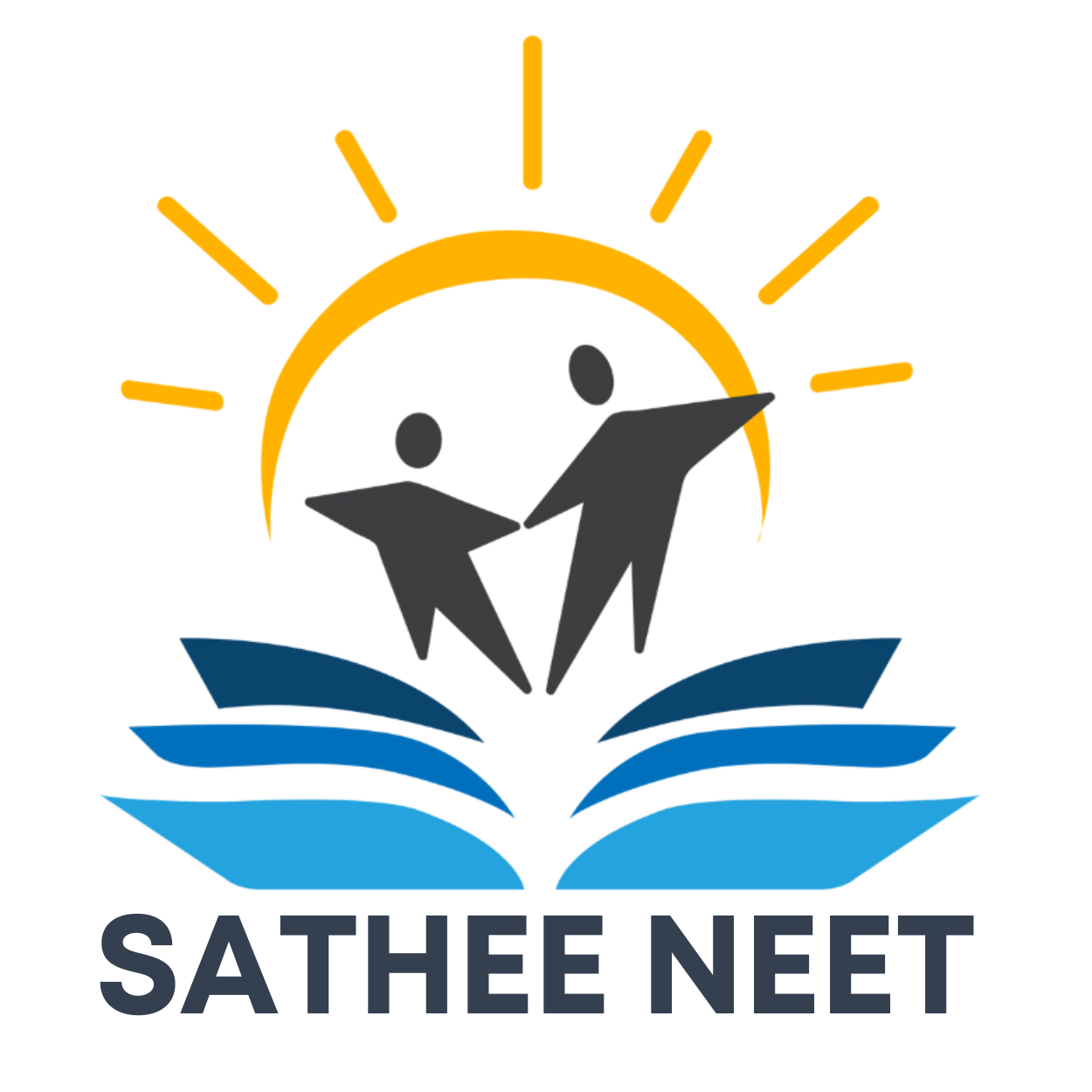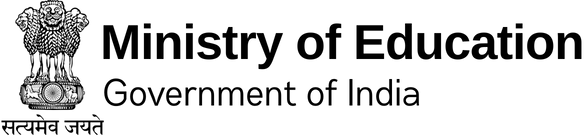अध्याय 04 युगों का दौर
गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद
मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाख्त्री या भारतीय-यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलीपुत्र तक पर हमला किया किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक-प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफ़गानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी-बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में

हिंद-यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का
ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ई.पू. पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज़्ब कर रहे थे।
मध्य-एशिया में शक (सीदियन) लोग ऑक्सस (अक्षु) नदी की घाटी में बस गए थे। यूइ-ची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर-भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। यूइ-चियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर-भारत
तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्खिन की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर-भारत पर और मध्य-एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मज़बूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का ज़िक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य-धर्म का स्वरूप कुछ मिला-जुला था जिसमें ज़रभुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा, जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, यूइ-चियों, ईरानियों, बाख्ती-यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती थीं। इनके आपसी प्रभावों के परिणामस्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से, इसी ज़माने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ई. में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफ़े मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे-किनारे तूर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ।
कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बँट गया-महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी-बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में
महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा (वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार) हीनयान को मानते रहे।
कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे, फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ़ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नयी जातियों का आगमन हुआ, तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया।
इस तरह ई. 320 में गुप्त-साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए, जो युद्ध और शांति, दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण-क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुलमिल गए थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी।
आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त्त या भारतवर्ष कहा था तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नयी जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली-जुली भारतीय-आर्य संस्कृति की मज़बूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज़्व होते गए। लेकिन समय-समय पर अजीब रस्मो-रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढाँचे को ही
नहीं तोड़ा बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढाँचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति-रिवाज और सामाजिक ढाँचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ प्रभावित हुईं जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतरराष्ट्रीय था, विश्वधर्म था। जैसे-जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ वैसे-वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार-बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने।

समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए-एक सिक्का
यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आपको उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ विकसित हो गईं। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था।
चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर डेढ़ सौ वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद
लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये ‘गोरे हूण’ कहलाते थे जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया।
उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा-लगभग आधी-शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे-छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी-कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज़्ब होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार सातवीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता-जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग (या युआन च्वान) भारत आया था ( 629 ई. में)। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जयिनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ई. में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था।
दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के एक हज़ार साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े-बड़े राज्य फूले-फले।
दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और[^5]
इनके जहाज़ दूर देशों तक माल पहुँचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए।
उत्तरी भारत पर बार-बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह ज़रूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक-परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नयी धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ, जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे।
शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके
बार-बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं।
मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो दो-दो, तीन-तीन सौ वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आपको इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया।
जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था, तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था।
इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेज़ी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेज़ी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था।
राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका।
प्रगति बनाम सुरक्षा
भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण-व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढाँचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे-बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है वहाँ भारत का सामाजिक ढाँचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति-रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था।
इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था, जिसे रीति-रिवाज से बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग-अलग रीति-रिवाजों, विश्वासों और जीवन-व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहें। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की।
समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढाँचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते-जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढाँचे में सिर्फ़ सतही
हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरकुश लगती हो, रीति-रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी।
ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज़्व कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग-थलग रहा, वहाँ वह अंतत: नष्ट हो गया और कभी-कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया।
भारत का प्राचीन रंगमंच
भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋवेद की उन ॠचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण-लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ई. पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य-रूपों का उल्लेख किया है।
रंगमंच की कला पर रचित नाट्यशास्त्र को ईसा की तीसरी शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी, जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो।
अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ई.पू. तीसरी शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके तेरह नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला
है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। वह ईसवी सन् के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़-पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुऱ्ान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्धचरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ।
यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ई. में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोंस कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। सर विलियम जोंस के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की।
कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वह चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य के शासन-काल में उज्जयिनी में था। माना जाता है कि वह दरबार के नौ रत्नों में से एक था। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है।
कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक प्रेमी, जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में, एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुँचाने के लिए कहता है।
कालिदास से संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी-शूद्रक का मृच्छकटिकम् यानी मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है। लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झाँकी प्रस्तुत करता है।
400 ई. के लगभग, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह विशाखदत्त का नाटक मुद्राराक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था, जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया है। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है।
राजा हर्ष, जिसने सातवीं सदी ई. में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए तीन नाटक मिलते हैं। सातवीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है।
संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही लेकिन उन्नीसवों शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा।
प्राचीन नाटकों की (कालिदास तथा अन्य लोगों के) भाषा मिली-जुली है-संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत, यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्रायः स्त्रियाँ प्राकृत, हालाँकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज-दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं।
इस ऊँचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएँ और महाकाव्यों से ली गई कथाएँ होती थीं। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग-अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत-नाटकों का चलन पूरे भारत में था क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी।
संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व
संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है-अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद वह नियत और व्याकरण के उस ढाँचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी-पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी।
सर विलियम जोंस ने 1784 में कहा था-“संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है, यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती-जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ़ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है।”
संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्त्वपूर्ण शब्द, जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित हैं।
दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति
रवींद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, “मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया।”
हमें केवल बीते हुए समय में जाने की ही ज़रूरत नहीं है, बर्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की ज़रूरत है जहाँ भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था।
पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी-कभी वृहत्तर भारत कहा गया है। लेकिन अब भी बहुत-सी कड़ियाँ नहीं मिलतीं। बहुत से अंतर्विरोध भी हैं। किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं और इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्र-पत्र हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएँ मिली हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर हैं-विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में।
ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईसवी तक उपनिवेशीकरण की चार प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच-बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर-दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों पर और महत्त्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया । इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया।
जावा स्पष्ट रूप से ‘यवद्वीप’ या जौ का टापू है। यह आज भी एक अन्न विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्राय: खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद-ब-खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है।
यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे-धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था।
संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता लगता है कि भारत और सुदूर पूरब के देशों के बीच कम-से-कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था।
यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज़ बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय (आंध्र) सिक्कों पर दोहरे-पाल वाले जहाज़ों का चिह्न अंकित है। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका-विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र हैं।
महाद्वीप के देशों बर्मा, स्याम और हिंद-चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था, टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन-पद्धति और सामान्य जीवन-दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने।
इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन तेरह सौ साल या इससे भी कुछ अधिक का है-ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर पंद्रहवों शताब्दी के अंत तक।
विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव
भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाईं। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है, चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े-बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियाँ थीं और इनमें से कुछ पदवियाँ और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की[^6]
मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलिपीन द्वीपों में लेखन-कला भारत से ही गई है।
कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर-फेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फ़ौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है।
लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। जावा में बोरोबुदुर में बुद्ध की जीवन-कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएँ अंकित की गई हैं।
अंगकोरवट के विशाल मंदिर के चारों तरफ़ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरें और नहरें हैं जिनके ऊपर पुल बने हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृद्धाकार सिर पत्थर में खुदा है। यह एक आकर्षक मुस्कराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है।
अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली पर उसका विकास ख्मेर प्रतिभा ने किया, या कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन (सप्तम) था, जो ठेठ भारतीय नाम है।
भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी न हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक पारदृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं; वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज़ है, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे।
भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है।
भारतीय संगीत, जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया था।
एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर, गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति-पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियाँ और चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। इसका निर्माण ईसवी सन् के आरंभ के आस-पास कुषाण युग में हुआ था।
भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है।
चौथी से छठी शताब्दी ईसवी में गुप्तकाल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफ़ाएँ खोदी गईं और उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। बाग और बादामी की गुफ़ाएँ भी इसी काल की हैं।
अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था-स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ़ देखो भी नहीं, क्योंकि वे खतरनाक हैं। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है-सुंदर स्त्रियाँ, राजकुमारियाँ, गायिकाएँ, नर्तकियाँ, बैठी और खड़ी, शृंगार करती हुईं या शोभा यात्रा में जाती हुईं। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत, लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है।
सातवीं-आठवीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफ़ाएँ तैयार हुईं, जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। एलीफ़ेंटा की गुफ़ाएँ भी इसी समय की हैं जहाँ प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम् की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था।
अंजता का एक चित्र

हाबलीपुरम् की एक इमारत
एलिफ़ेंटा की गुफ़ाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में हैं। हैवेल का कहना है कि इस क्षत-विक्षत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है।
ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। एप्सटीन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आह्बान करती है।
जावा में बोरीबुदुर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिपटोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। वह एक ऐसा चेहरा है, जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुँच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है।
भारत का विदेशी व्यापार
ईसवी सन् के पहले एक हज़ार वर्षों के दौरान, भारत का व्यापार दूर-दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाज़ारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था।
भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर-दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है। लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ई.पू. चौथी शताब्दी से ही किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने

महरौली (दिल्ली) में कुतुबमीनार के परिसर में खड़ा लौह-स्तंभ, जिसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ बाद
में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रँगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेज़ी में ‘इंडिगो’ कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेज़ी में यूनान के माध्यम से आया है।
ईसवी सन् की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायनशास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। भारतीय, प्राचीन काल से ही फ़ौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय फ़ौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी, विशेष रूप से युद्ध के
कामों में। भारतीयों को और बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध-विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य-युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था, गरचे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर-रचना और शरीर-विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्त-संचार की बात सुझाई जा चुकी थी।
खगोलशास्त्र, जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था जो अब भी प्रचलित है। जो लोग समुद्री-यात्रा पर निकलते थे, उनके लिए खगोलशास्त्र का ज्ञान व्यावहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था।
यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी, लेकिन जहाज़ बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा, विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह-तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औज़ारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायनशास्त्र एवं धातुशास्त्र संबंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने वश में रख सका।
प्राचीन भारत में गणितशास्त्र
यह माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर दस भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। ये अंक चिह्न बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिह्नों से एकदम भिन्न थे।
भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियाँ बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियाँ अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे बना रहा। जिसे ‘शून्य’ या ‘कुछ नहीं’ कहा जाता है वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था। बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था।
शून्यांक और स्थान-मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित में तेज़ी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ई. में हुआ था। भारतीय गणितशास्त्र में अगला महत्त्वपूर्ण नाम भास्कर ( 522 ई.) का और उसके बाद ब्रह्मपुत्र ( 628 ई.) का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोलशास्त्री भी था जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म 1114 ई. में हुआ था। उसने खगोलशास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर क्रमशः तीन ग्रंथों की रचना की। अंकगणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है, जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी गोकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है।
आठवों शताब्दी में खलीफ़ा अल्मंसूर के राज्यकाल में (753-774 ई.) कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोलशास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। इन्होंने अरबी जगत में गणितशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्याध्ययन का बड़ा केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था।
अरबी जगत से यह नया गणित, संभवतः स्पेन के मूर विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुँचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए। इनका सबसे पहला प्रयोग, जिसकी जानकारी मिलती है, 1134 ई. में सिसली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ई. में हुआ।
विकास और ह्रास
ईसवी सन् के पहले हज़ार वर्षों में, भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार-चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणामस्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर-दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन हज़ार वर्षों के बीच के समय में यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। यह भारत
का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है।
स्वर्ण-युग के समाप्त होने से पहले ही कमज़ोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर-पश्चिम से गोरे हूणों के दल के दल आते हैं और बार-बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं। किंतु धीरो-धीरे वे उत्तर-भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राज-सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद, अंतिम गुप्त सम्राट मध्य-भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर, बहुत प्रयत्न करके हूणों को निकाल बाहर करता है।
इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे-धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न हैं।
सातवों शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जयिनी (आधुनिक उज्जैन), जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमज़ोर पड़कर धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। नौवीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। ग्यारहवों शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर, एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है और उज्जयिनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह वैयाकरण और कोशकार था। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोलशास्त्र में थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य
का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएँ मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वत्ता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक-कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है।
इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमज़ोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण, आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला।
गरचे उत्तरी भारत छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शानिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत-ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शानिक विषयों (बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार) के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे, वैद्यक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया है।
इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय
में उज्जयिनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था।
ज्यों-ज्यों सहस्राब्दी समाप्ति पर आती है यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही। पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हों। आठवीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग-पद्धति के भ्रष्ट रूप।
साहित्य में भवभूति (आठवीं शताब्दी) आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय (बारहवीं शताब्दी) का है। कला में ई. वी. हैवेल के अनुसार सातवीं या आठवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से सोलहवीं शताब्दी में होने लगा। मेरा खयाल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही।
उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से नवीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोलवंशी ग्यारहवीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्रीविजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली।
समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन-शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुँच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी।
यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती
है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्धकौशल में उससे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन हज़ार वर्षों के अंत में बिलकुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार-बार आते हैं पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्तल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा-कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है।
सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ।
भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ़ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज-व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैरमिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था जिसे यहाँ की जाति-व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति-रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले चार-पाँच सौ वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले-फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैरमिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बँट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राहमण और क्षत्रिय वाणिज्य-व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने से ऊँची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया।
भारत के सामाजिक ढाँचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग-अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए, उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया।
इसी कारण हर तरफ़ ह्रास हुआ - विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे, भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएँ बढ़ने लगों और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसीलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका, लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही।