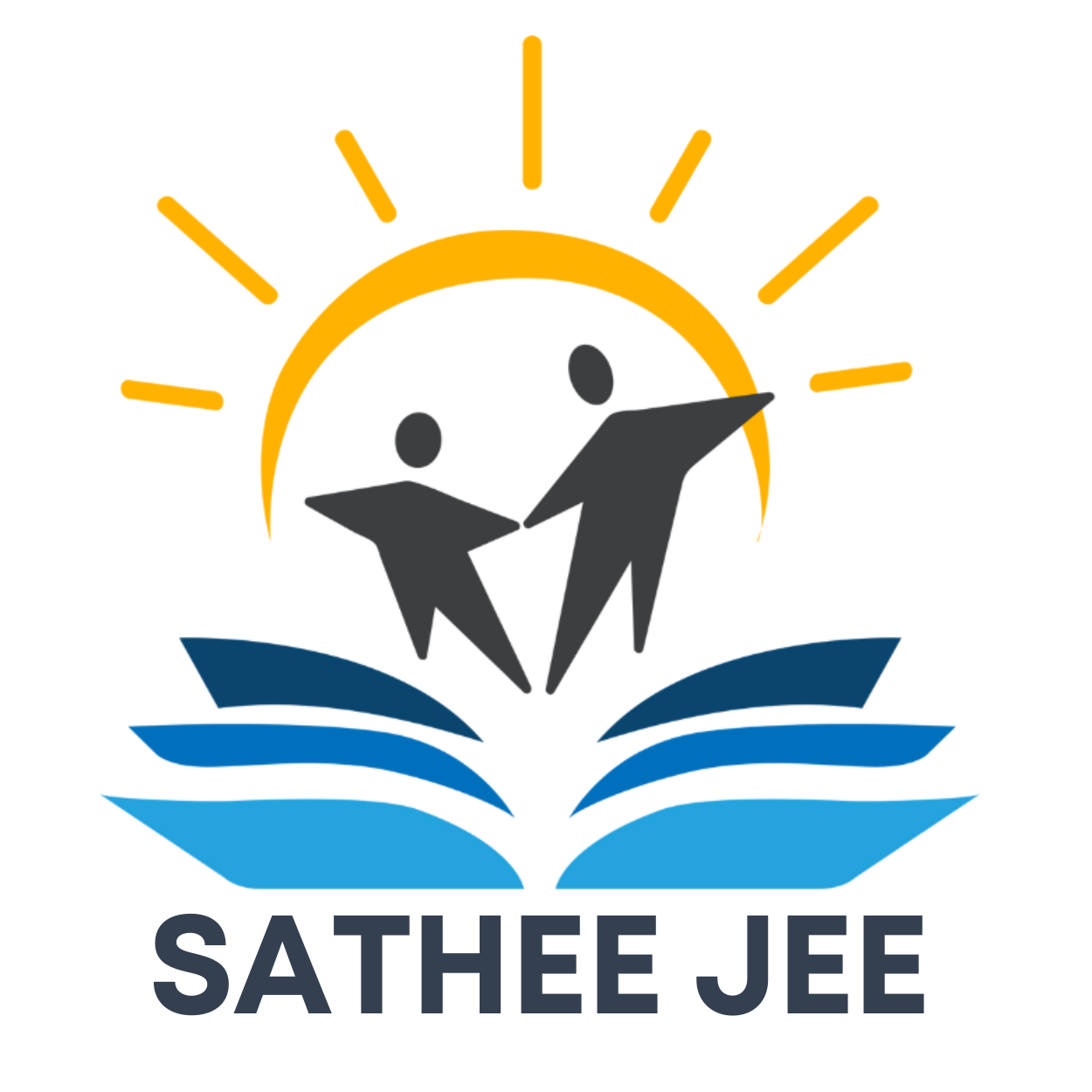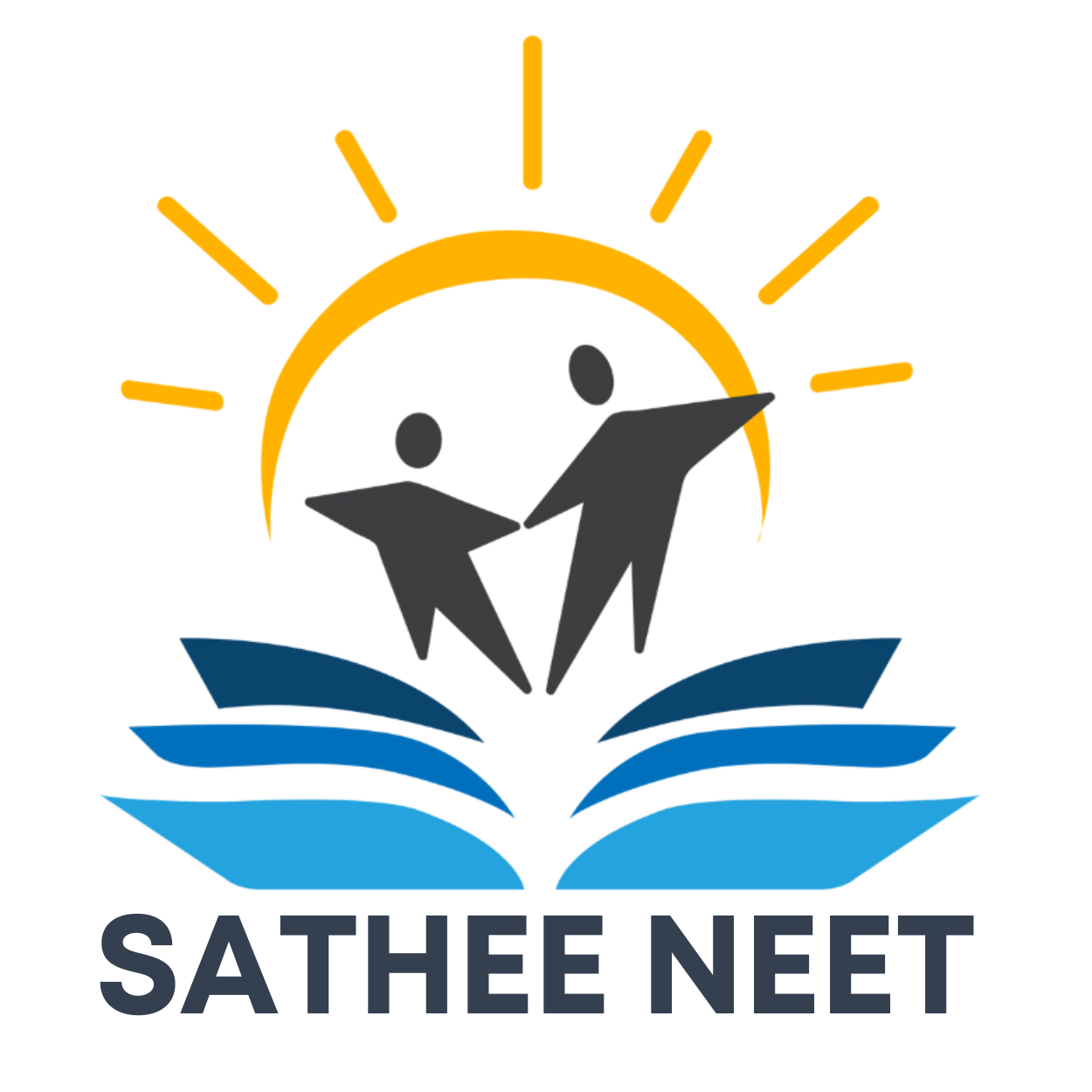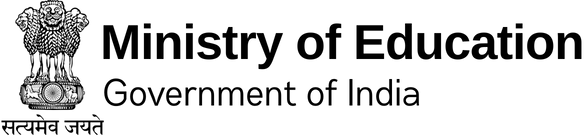अध्याय 03 सिंधु घाटी सभ्यता

एक हड़प्पाई मुहर
भारत के अतीत की सबसे पहली तसवीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर-दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्त्वपूर्ण नयी खोजें की जाएँ। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर-दूर जगहों पर मिले हैं-जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला ज़िले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं उससे बहुत अधिक है।
अब तक हम जो जान सके हैं, उसका बहुत महत्त्व है। सिंधु घाटी सभ्यता, आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुँचने में उसे हज़ारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं
थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी।
सिंधु घाटी सभ्यता ने फ़ारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं।
सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुज़रे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं। लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी शृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को छः-सात हज़ार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें
मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार
चली आती परंपरा और रहन-सहन की, लोक-प्रचलित रीति-रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फ़ैशन की याद दिलाता है।
यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर-बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर-तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख-सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिह्नों-अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है।
आर्यों का आना
सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएँ दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हज़ार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया, जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गाँवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे-धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण हैं कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊँची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नीवों पर ऊँचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान दो या तीन मंज़िले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊँचे उठने के कारण समय-समय पर उनकी
दीवारें भी ऊँची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्ययुग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया।
इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन-सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर-दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी पर इस बात का फ़ैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आँकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छा कर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे-धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड-खंड हो गए।
सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल-खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू-शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी गोकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर ज़ोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा, जो आर्य थे और उत्तर-पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए।
ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग एक हज़ार वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियाँ समय-समय पर आती रही हों और भारत में जज़्व होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल-जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल-जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ जिनमें दोनों सभ्यताओं के
तत्व साफ़ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत-सी जातियाँ आईं। सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल-मिलकर रह गए।
प्राचीनतम अभिलेख, धर्म-ग्रंथ और पुराण
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद हैं। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले।
आजकल अधिकांश विद्वान ॠवेद की ॠचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्समूलर ने इसे ‘आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द’ कहा है।
भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं।
वेद
बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म-ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्त्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव-मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति ‘विद्’ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा-सादा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति-पूजा है न देव-मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे।
पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव-जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव-मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य-प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोंमाद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकार्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई।
सभ्यता के उषाकाल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग, जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। पर इस सबमें साहस और आनंद का भाव था।
बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस खयाल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक-परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं-जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है।
हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएँ दिखाई पड़ती हैं-एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग-अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है।
जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने-नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन-दृष्टि, जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती
थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हज़ारों वर्ष बनी नहीं रह सकती।
भारतीय संस्कृति की निरंतरता
हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व-दृष्ट्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते-बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति-व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज-व्यवस्था को मज़बूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव-मन के लिए कारागृह बन गई।
फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढाँचे के भीतर बँधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ।
इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग-थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। तीन-चार हज़ार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है।
उपनिषद्
उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय-आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है।
उपनिषदों में जाँच-पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका ज़ोर अनिवार्य रूप से आत्म-बोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तुजगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है-आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में।
उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद-विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू-टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म-कांड और पूजा-पाठ को व्यर्थ बताया गया है।
उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है-‘असत् से मुझे सत् की ओर ले चल। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल।’ बार-बार हमें एक बेचैन मन झाँकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है-‘चरैवेति, चंरैवेति,’ - हे यात्री, इसलिए चलते रहो, चलते रहो।
व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ
उपनिषदों में बराबर इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन-मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग ज़रूरी है। इस प्रकार की तपस्या
का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलनों ने भारत को हिला दिया उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना ज़रूरी है।
भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन-शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड-खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढाँचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियाँ बहुत अनोखी थीं।
लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बँटा और बँधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व-बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैरमुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊँच-नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति-व्यवस्था में सख्ती के बढ़ने के साथ-साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुँधलाती चली गई।
भौतिकवाद
हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रथों को आरंभ में ताड़-पत्रों पर या भोज-पत्रों पर लिखा गया था। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत-सी
प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिलीं, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं।
जो पुस्तकें खो गई हैं, उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ़ इसकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ई.पू. चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है।
भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्मविज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा-प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू-टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आपको अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे-उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और नरक है और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं।
महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक
प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों-रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियाँ लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय-आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। उनकी विजयों और उस समय के गृहयुद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मज़बूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद, भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं।
इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है-अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ-कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात-पाँत की ऊँच-नीच में बँटे समाज को एकजुट रखते थे। उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेद-भाव पर छा गया और बराबर बना रहा।
भारतीय पुराकथाएँ महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप-आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएँ और प्रचलित कहानियाँ वीरगाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अडे रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवनपर्यंत और मरणोपरांत भी वफ़ादारी, साहस और लोक-हित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुँथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और
यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएँ वास्तविक हों या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एकरसता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं।
यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियाँ निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएँ आपस में गड्ड-मड्ड हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूलभुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हण की राजतरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की बारहवीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से।
ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी विरासत में मिली थीं। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंतकथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मज़बूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुँधलापन पैदा हुआ। ज़िदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई।
महाभारत
महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं; परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंतकथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग दस वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जाँच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है।
शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति-रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ पाँच भाइयों की पत्नी है। धीरे-धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुलमिल कर एक हो रहे थे और इस नयी स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला।
यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग-अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया।
महाभारत में हिंदुस्तान की (या जिसे दंतकथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है) बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त्त, यानी आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य-भारत में विंध्य
पर्वत तक फैले उत्तर-भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वह विराट गृहयुद्ध, जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज़ लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व चौदहवीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत (या संभवतः उत्तरी भारत) पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार (जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है) कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे।
महाभारत में कृष्ण से संबद्ध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवद्गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा, इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर ज़ोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोकमंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य-निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म, जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है, वह दिलचस्प है क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। ज़ाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद[^2]
से था यानी हिंसा की मानसकिता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था।
महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूँढ़ी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती ज़िदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है-“दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो।” इसमें लोक-मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है-“जो बात लोक-हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए।” फिर कहा गया है-“सच्चाई, आत्म-संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन-सफलता के साधन हैं जाति और कुल नहीं।” “धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है।” “सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है।” धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया है-“रेशम का कीडा अपने धन के बोझ से ही मरता है।” और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है-“असंतोष प्रगति का प्रेरक है।”
भगवद्गीता
भगवद्गीता महाभारत का अंश है परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्धकाल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय, जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है क्योंकि यह संकट-काल के लिए लिखी गई कविता है-राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के
संकट के लिए। गीता की असंख्य व्याख्याएँ की गईं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है, औरों ने धर्म-कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है।
इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध-क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है। उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किसलिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग-युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाज़ों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक-एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्ट्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के तीन मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी दो की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालाँकि उसे पूर्णरूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव-अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यावहारिक समस्याएँ इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है, अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए क्योंकि ये आदर्श समय-समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात् विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है-“सभी रास्ते मुझ तक आते हैं।” इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद ढाई हज़ार वर्षों में भारतवासी बार-बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुज़रे हैं, उन्हें एक के बाद एक, तरह-तरह के अनुभव हुए हैं। एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही।
प्राचीन भारत में जीवन और कर्म
बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक-कथाओं में मिलता है। इन जातक-कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक-कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों-द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक-परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ग्राम-सभाएँ एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य ज़रिया लगान था। माना जाता था कि ज़मीन पर लगाया जाने वाला कर, उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान, हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गाँव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढाँचा इन्हीं ग्राम-समुदायों से बनाया जाता था जिन्हें दस-दस और सौ-सौ के समूह में बाँट दिया जाता था।
जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभरकर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गाँवों की स्थापना थी। इस तरह एक गाँव बढ़इयों का था, एक गाँव लोहारों का था। इसी तरह और पेशों के लोगों के गाँव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गाँव
आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें ज़िदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गाँव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा।
जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवाँ जाया करते थे। भड़ौच से जहाज़ बेबिलोन (बावेरू) के लिए फ़ारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा (भागलपुर) और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक।
भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं, उत्तर-पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में हैं।
ईसा पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है, हालाँकि बाद के वैयाकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के[^3]
आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी-न-किसी तरह का संपर्क हो चुका था।
औषध-विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें भी थीं और अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध-विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे। किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्यपुस्तकें ईसवी सन् की शुरू की सदियों में लिखी गईं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य-चिकित्सा पर सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्यपुस्तकों में बहुत-सी बीमारियों का ज़िक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य-चिकित्सा, प्रसूति-विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफ़ाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य-प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर-फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य-क्रिया के औज़ारों का ज़िक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी; जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल हैं। घावों के जीवाणुओं को धुआँ देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व तीसरी चौथी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था।
महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा-प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह-तरह के विषय शामिल थे जिनमें सैनिक-प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएँ। इन वन-शिक्षालयों में प्रायः छोटे-छोटे गुट रहते थे, गोकि इस बात
के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे।
बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था। किंतु उत्तर-पश्चिम में, आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर-दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व छठी-सातवीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने भी यहों शिक्षा पाई थी।
इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा-पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध-काल में यह बौद्ध-ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा-पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खिंचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था।
उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुँधली-सी तसवीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ-पाँव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्त्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे।
मथुरा से प्राप्त महावीर की लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी की एक मूर्ति
महावीर और बुद्ध - वर्ण व्यवस्था
जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएँ थे। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इंकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं। उनके नज़ारिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन-धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है।
जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ई.पू. 544 में अस्सी वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत् शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ई.पू. 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत् 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख (मई-जून) के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था।
बुद्ध में लोक-प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्म-कांड एवं पुरोहितप्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नज़ारिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था, उनकी पद्धति

तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी।
बुद्ध ने वर्ण-व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ-व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया।
यह विचित्र और महत्त्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित-प्रपंच और वर्ण-व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने
बार-बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे-धीरे वर्ण-व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म, जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह ज़िदा है और जारी है तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति-व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, गोकि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा।
बुद्ध की शिक्षा
बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्मज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, “सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो।" इस धर्म में सब जातियाँ आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया क्योंकि “इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है।” अतः “मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए।” यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। “युद्ध में भले ही कोई हज़ार आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की
सारनाथ स्तूप - बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यहीं दिया था
जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है।” उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इंकार। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आपको उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं।
बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी।
जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन ‘चार आर्य सत्यों’ का निरूपण किया है उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है।
दुख की इस स्थिति के अंत से ‘निर्वाण’ की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, “जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता।” यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था-सही विश्वास, सही आकांक्षाएँ, सही वचन, सही आचरण, जीवनयापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद।
बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताईं जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियाँ लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियाँ हैं, उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं? आनंद ने उत्तर दिया-“पतझड़ की पत्तियाँ सब तरफ़ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती।” तब बुद्ध ने
कहा-" इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्री भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हज़ार और सत्य ऐसे हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती।"
बुद्ध-कथा
‘बुद्ध’ की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और काँसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की, या कम-से-कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए-शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफ़ानों और संघर्षों से दूर वे इतनी दूर, पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन-शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि शांत-दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए।
बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती-जागती, थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुज़रते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है।
चंद्रगुप्त और चाणक्य - मौर्य साम्राज्य की स्थापना
भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे-धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था।
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी
पाटलीपुत्र (आधुनिक पटना) थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहाँ नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी।
चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुँच गया। सिकंदर की मृत्यु के दो ही वर्ष में उसने पाटलीपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलीपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी।
यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है-भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सिल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज़ ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण ‘राजनीतिशास्त्र’ है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था - बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है - मुद्राराक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तसवीर उभरती है। साहसी और षड़यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से सँभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है, ऊँचे पदों की शान-शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन-मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता।
चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है।
पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर-व्यवस्था, सामाजिक रीति-रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग-धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज़ और जहाज़रानी, निगमें, जन-गणना, मत्स्य-उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल-सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी।
अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा-उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है, वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा, तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्ज़ी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे।
अशोक
273 ई.पू. में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी, विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल
अशोक का एक अभिलेख
दक्षिण-पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूरबी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली।
कर्लिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया।
अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फ़रमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फ़रमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं।
कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको (धर्म को) अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फ़रमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के सौवें -हज़ारवें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है।
फ़रमान में आगे कहा गया है-“इसके अलावा, यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव-मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म-संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो।”[^4]
इस अदुभुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आपको बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय, सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें, चाहे जिस समय और जहाँ भी हो

अशोक के समय में निर्मित साँची का स्तूप वह लोक-हित के लिए अवश्य काम करेगा।
खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्त्व दिया।
अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिज़ाइन से निकाला गया है जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला-परंपरा की विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं।
इकतालीस साल तक अनवरत शासन करने के बाद ई.पू. 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। एच.जी. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ़ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हज़ार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े-बड़े राजे-महाराजे, शहंशाह और नामीगिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है।